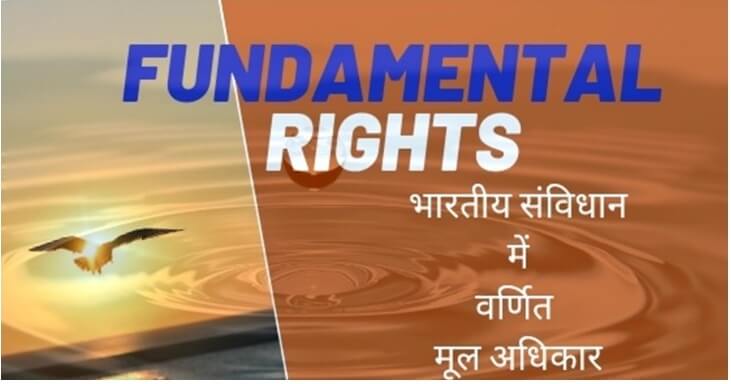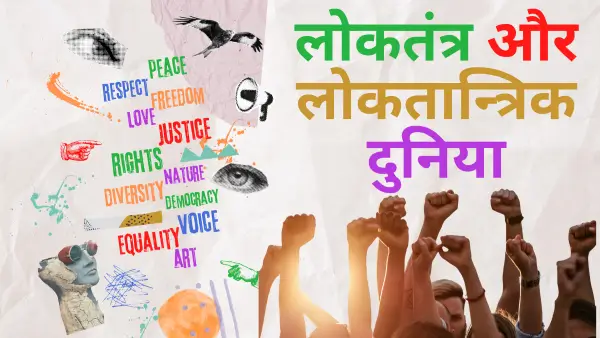आज हम भारतीय और वैश्विक परिपेक्ष्य में मतदान और मताधिकार को जानने वाले है. मतदान के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है. इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन केवल उन्हीं नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है. इस अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं. इसलिए, मताधिकार को समझने से पहले, निर्वाचन की प्रक्रिया को जानना महत्वपूर्ण है.
निर्वाचन क्या है? (What is Election)
भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें सरकार का गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है. निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिक शासन में सीधे तौर पर भाग लेते हैं. यह प्रक्रिया नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देती है. सीधे शब्दों में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को निर्वाचन कहा जाता है.
निर्वाचन के माध्यम से एक निश्चित समय के लिए प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है. इस प्रक्रिया में भाग लेकर भारत के नागरिक अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग करते हैं. भारत जैसा विशाल और विविध देश होने के बावजूद, यहां सभी नागरिकों को चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि चुनने का समान अधिकार प्राप्त है. यह व्यवस्था सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के नाम से जानी जाती है, जो लोकतंत्र की नींव है.
मताधिकार क्या हैं? (What are Voting Rights?)
मताधिकार एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है. इसका सीधा संबंध देश की संप्रभुता (सर्वोच्च सत्ता) से है. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार यह जनता में निहित है. जनता अपनी संप्रभुता का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर करती है. सरकार की सभी शक्तियों का अंतिम स्रोत यही जनता होती है.
सरल शब्दों में, मताधिकार वह अधिकार है जो नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और सरकार बनाने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेने की शक्ति देता है. भारत में यह एक राजनीतिक अधिकार है. इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची (निर्वाचन नामावली) में दर्ज है, वोट डालने के योग्य होते हैं.
भारतीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है. इसका अर्थ है कि देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक, चाहे वह महिला हो या पुरुष, को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार प्राप्त है. एक निर्धारित उम्र (भारत में 18 वर्ष) पार करने के बाद, देश के सभी योग्य नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिल जाता है. यह हमारे लोकतंत्र की समानता और समावेशिता को दर्शाता है.
आगे मतदान और मताधिकार पर भारतीय और पाश्चात्य विचारकों की 10 परिभाषाओं का संग्रह दिया गया है:
भारतीय विचारक (Indian Thinkers)
- बी.आर. अम्बेडकर: “प्रत्येक वयस्क को जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार होना चाहिए.”
- जवाहरलाल नेहरू: “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के कामकाज और सरकार की वैधता के लिए मौलिक हैं.”
- महात्मा गांधी: “स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को अपने शासन में हिस्सेदारी देना, और यह सबसे अच्छी तरह से वोट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है.”
- सरदार वल्लभभाई पटेल: “मतदान का अधिकार केवल एक विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य भी है जिसका उपयोग देश के हित में किया जाना चाहिए.”
- विनोबा भावे: “सच्चे लोकतंत्र का एहसास तब होता है जब समुदाय सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाने वाले निर्णय लेने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलकर काम करते हैं.”
पाश्चात्य विचारक (Western Thinkers)
- जॉन लॉक: “समय-समय पर चुनाव यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह रहे और उनकी इच्छा को प्रतिबिंबित करे.”
- जीन-जैक्स रूसो: “लोकप्रिय संप्रभुता के महत्व पर जोर दिया, जहाँ अंतिम शक्ति लोगों के पास होती है. चुनाव लोगों के लिए अपनी संप्रभुता का प्रयोग करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है.”
- जेम्स मैडिसन: “चुनाव मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों की शक्ति की जाँच करने में सक्षम बनाकर इस प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नियमित चुनाव किसी एक समूह को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी अधिकारी लोगों के प्रति जवाबदेह बने रहें.”
- जॉन स्टुअर्ट मिल: “सबसे अच्छी सरकार वह है जो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी को बढ़ावा देती है. इसे प्राप्त करने के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं, क्योंकि वे नागरिकों को ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देते हैं जो जनता के हित में कानून बनाएंगे.”
- अरस्तू: “नेताओं का चयन संयोग के बजाय योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए. आदर्श चुनावी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सबसे गुणी और जानकार व्यक्तियों को शासन करने के लिए चुना जाए.”
मताधिकार की विशेषताएं (Features of Voting Rights)
मताधिकार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है जो किसी भी लोकतंत्र की नींव है. यह सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है. इसके कई महत्वपूर्ण पहलू और विशेषताएं हैं जो एक मजबूत और समावेशी शासन प्रणाली के लिए आवश्यक हैं.
- समानता का सिद्धांत: मताधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक के मत का समान महत्व हो. यह व्यवस्था “एक व्यक्ति, एक वोट” के सिद्धांत पर आधारित है, जो लोकतंत्र में समानता के विचार को पुष्ट करती है.
- नागरिकों की भागीदारी: यह अधिकार नागरिकों को शासन प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेने का मौका देता है. जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाती है. इसके माध्यम से नागरिक सरकार के प्रदर्शन पर अपना मत व्यक्त करते हैं. वे यह तय करते हैं कि कौन उनका नेतृत्व करेगा. यह नागरिकों को सशक्त महसूस कराता है. साथ ही, जिससे लोकतंत्र की वैधता मजबूत होती है.
- शांतिपूर्ण परिवर्तन का साधन: मताधिकार के माध्यम से जनता बिना किसी हिंसा या क्रांति के शांतिपूर्वक तरीके से शासन में बदलाव ला सकती है. यदि लोग मौजूदा सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अगले चुनाव में अपनी पसंद के नए प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं. इस प्रकार मताधिकार क्रांति या हिंसा के बजाय, वोट के माध्यम से परिवर्तन लाने की शक्ति देता है. अतः मतदान लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान करता है.
- राजनीतिक शिक्षा: मतदान की प्रक्रिया नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक और शिक्षित बनाती है. लोग विभिन्न उम्मीदवारों, पार्टियों और उनके कार्यक्रमों को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक समझ बढ़ती है. यह लोकतंत्र की सफलता का आधार है.
- आत्म-सम्मान की भावना: मतदान का अधिकार नागरिकों में यह भावना पैदा करता है कि वे देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह अधिकार उन्हें सशक्त महसूस कराता है और उनमें आत्म-सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है.
- जवाबदेही का साधन: मताधिकार प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है. चुने हुए प्रतिनिधि यह जानते हैं कि उन्हें फिर से चुने जाने के लिए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा. नियमित चुनाव राजनेताओं याद दिलाता है कि उन्हें दोबारा चुना जाना है. इससे नेता सार्वजनिक हित में काम करने और अपने मतदाताओं की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं.
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा: यह अधिकार सभी नागरिकों को, उनकी सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, एक समान मंच पर लाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा मिलता है.
- नीतिगत प्रभाव: मतदान के जरिए नागरिक उन नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक नीतियां. अपने विचारों से सहमत प्रतिनिधियों को चुनकर, मतदाता सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.
- लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती: मतदान स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है. यह नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है.
मताधिकार के प्रमुख सिद्धांत (Key Theories of Voting Rights)
मताधिकार, विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है जो समय के साथ विकसित हुए हैं. ये सिद्धांत इस बात को तय करते हैं कि किसे और किस आधार पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए.
- जातीय सिद्धांत (Tribal Theory): इस सिद्धांत के अनुसार, मतदान एक स्वाभाविक अधिकार है. यह मानता है कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होना चाहिए क्योंकि यह उसके जीवन का एक सक्रिय हिस्सा है. यह प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं में प्रचलित था जहाँ लोग हाथ उठाकर वोट करते थे.
- सामंती सिद्धांत (Feudal Theory): यह सिद्धांत मानता है कि केवल उन्हीं लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए जिनके पास संपत्ति है. मध्य युग में, मताधिकार को सम्मान का प्रतीक माना जाता था. यह विचार प्रचलित था कि संपत्ति वाले लोग ही राष्ट्र के प्रति सबसे अधिक जवाबदेह होते हैं.
- प्राकृतिक सिद्धांत (Natural Theory): 17वीं और 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ यह सिद्धांत मानता है कि सरकार लोगों की सहमति से बनती है. इसलिए, शासक को चुनने का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है जो हर नागरिक को जन्म से ही प्राप्त होता है.
- वैधानिक सिद्धांत (Legal Theory): इसके अनुसार, मताधिकार कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक अधिकार है जिसे कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है. राज्य अपनी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर तय करता है कि किसे वोट देने का अधिकार मिलेगा.
- नैतिक सिद्धांत (Moral Theory): यह सिद्धांत मताधिकार को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानता है. यह कहता है कि वोट देने का अधिकार लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाता है. साथ ही, उन्हें यह तय करने में मदद करता है कि उन पर शासन कौन करेगा.
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise): यह आधुनिक लोकतंत्र में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है. इसके तहत, एक निश्चित उम्र (जैसे भारत में 18 वर्ष) के प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव (जाति, लिंग, धर्म, या आर्थिक स्थिति) के वोट देने का अधिकार होता है. यह सिद्धांत “एक व्यक्ति, एक वोट” की अवधारणा पर आधारित है.
- बहुमत मताधिकार का सिद्धांत (Plural Voting Theory): यह सिद्धांत “एक व्यक्ति, एक वोट” के विपरीत है. इसके अनुसार, किसी व्यक्ति को शिक्षा, संपत्ति या अन्य योग्यताओं के आधार पर एक से अधिक वोट देने का अधिकार होना चाहिए. हालांकि, यह सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्रों में स्वीकार्य नहीं है.
- भारित मताधिकार का सिद्धांत (Weighted Voting Theory): यह सिद्धांत मानता है कि वोट को गिनने के बजाय उसका “भार” तय किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि अधिक शिक्षित या अमीर व्यक्ति के वोट का महत्व एक साधारण व्यक्ति के वोट से अधिक हो सकता है. यह सिद्धांत भी आधुनिक लोकतंत्रों में कम प्रचलित है क्योंकि यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है.
मतदान में सुधार के उपाय (Measures to improve Voting)
मतदान प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए कई सुधार किए जा सकते हैं. ये सुधार न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाएंगे, बल्कि चुनावी प्रणाली में लोगों का विश्वास भी मजबूत करेंगे.
मतदाता जागरूकता अभियान
नागरिकों को मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके वोट की शक्ति के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है. सरकार और चुनाव आयोग को मिलकर ऐसे अभियान चलाने चाहिए जो यह स्पष्ट करें कि एक वोट कैसे सरकार की नीतियों और उनके अपने भविष्य को प्रभावित कर सकता है.
प्रक्रियात्मक सुधार
मतदान को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए. इसके साथ ही, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाना, मतदान के घंटों में लचीलापन लाना और वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था करना आवश्यक है. सुरक्षा उपायों को मजबूत करने से मतदाताओं में विश्वास बढ़ेगा.
प्रौद्योगिकी का उपयोग
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) जैसी तकनीकों का प्रभावी उपयोग पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है. मतदाता पहचान पत्र को डिजिटल करने और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा देने से प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी. भारतीय परिपेक्ष्य में आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़कर डुप्लिकेसी को रोक जा सकता है.
प्रवासी भारतीयों के लिए प्रावधान
ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी या अन्य कारणों से विदेशों या देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, उन्हें भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए.इसके लिए डाक मतपत्र (Postal Ballot) या अन्य सुरक्षित ऑनलाइन मतदान प्रणाली विकसित की जा सकती है. इस प्रकार वे भी अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित कर सकें.
सकारात्मक प्रोत्साहन
कुछ देशों में मतदान करने वाले नागरिकों को छोटे-मोटे प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जैसे कि सार्वजनिक सेवाओं में प्राथमिकता या कर छूट. इस तरह के उपाय लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं.
भारत में मतदान और मताधिकार (Voting and Suffrage in India)
मतदान का अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार होते हुए भी, एक “मूल अधिकार” (Fundamental Right) नहीं है. यह एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है, जिसे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से नियंत्रित और विनियमित किया जाता है. भारतीय संविधान और नियमों में मतदान और मताधिकार के प्रावधान निम्नलिखित हैं:-
1. संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों (Elections) से संबंधित है. इसमें अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक का वर्णन है. यह भाग भारत में चुनावों के प्रबंधन और संचालन के लिए एक मजबूत और निष्पक्ष तंत्र स्थापित करता है.
अनुच्छेद 324: चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
यह अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है. यह भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदान करता है. इसका मतलब है कि चुनाव आयोग इन चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है. इसमें मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना, और चुनाव आचार संहिता लागू करना जैसे कार्य शामिल हैं.
अनुच्छेद 325: धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अपात्र न होना
यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से रोका नहीं जाएगा. यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) के सिद्धांत को बढ़ावा देता है. साथ ही सुनिश्चित करता है कि सभी योग्य नागरिकों को समान रूप से मतदान का अधिकार मिले.
अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव
यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार मताधिकार के आधार पर होंगे. इसके अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक, जो अन्यथा कानून द्वारा अयोग्य नहीं है, मतदान करने का हकदार है.
अयोग्यता के कुछ सामान्य कारण हैं – गैर-नागरिकता, मानसिक अस्थिरता या किसी आपराधिक सजा के कारण. 61वां संविधान संशोधन, 1989: इस संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिससे अधिक युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिला.
अनुच्छेद 327: विधानमंडलों के लिए चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति
यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित सभी मामलों, जैसे कि मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अन्य आवश्यक प्रावधानों के लिए कानून बना सकती है.
अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की राज्य विधानमंडल की शक्ति
यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को अपने राज्य के भीतर चुनावों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, बशर्ते कि उन मामलों पर संसद ने कोई कानून न बनाया हो.
अनुच्छेद 329: चुनाव संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक
यह अनुच्छेद चुनावों से संबंधित मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप को सीमित करता है. इसका मतलब है कि किसी भी चुनाव को केवल एक चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जिसे संबंधित कानून के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए दायर किया जाता है. इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और समयबद्ध बनाए रखना है.
2. वैधानिक प्रावधान (कानून)
मतदान का अधिकार, हालांकि संविधान में निहित है, मुख्य रूप से कुछ कानूनों के माध्यम से शासित होता है. इन कानूनों में प्रमुख हैं:
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act, 1950):
- धारा 16: यह निर्धारित करती है कि गैर-नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है.
- धारा 19: इसके अनुसार, मतदाता की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वह उस निर्वाचन क्षेत्र में ‘सामान्य रूप से निवासी’ होना चाहिए.
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act, 1951):
- धारा 62: यह सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति को मतदान का अधिकार है. इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जेल में बंद व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होता.
3. अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
- डाक मतपत्र (Postal Ballot): निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 18 के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य कुछ विशेष श्रेणियों के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध है.
- अप्रवासी भारतीय (Non-Resident Indians – NRIs): जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20A के तहत अप्रवासी भारतीय मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से मतदान करना होता है.
- “इनकार का अधिकार” (Right to Reject): मतदान के अधिकार में “इनकार का अधिकार” भी शामिल है, जिसे “नोटा” (None of the Above) विकल्प के माध्यम से मान्यता दी गई है. यह मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का विकल्प देता है.