ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेम्जे मेकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को ‘साम्प्रदायिक निर्णय’ की घोषणा की. यह विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर जारी किया गया था. इसे ही कम्यूनल पंचाट भी कहा जाता हैं. इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिये विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक् निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था. मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया. इसे राष्ट्रवादियों ने साम्प्रदायिक निर्णय, उपनिवेशवादी शासन की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति का एक और प्रमाण माना.
साम्प्रदायिक निर्णय के प्रावधान
- मुसलमानों, सिखों एवं यूरोपियों को पृथक साम्प्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया.
- आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाईयों तथा स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया.
- प्रांतीय विधानमंडल में साम्प्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया गया.
- सभी प्रांतों को विभिन्न सम्प्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया.
- अन्य शेष मतदाता, जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया.
- बम्बई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से सात स्थान मराठों के लिये आरक्षित कर दिये गये.
- विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिये दोहरी व्यवस्था की गयी. उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया गया.
- सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों के निर्वाचन का अधिकार बना रहा.
- दलित जातियों के लिये विशेष निर्वाचन की यह व्यवस्था बीस वर्षों के लिये की गयी.
- दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गयी.
साम्प्रदायिक निर्णय पर कांग्रेस का पक्ष
यद्यपि कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी किंतु अल्पसंख्यकों से विचार-विमर्श किये बिना वह इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी. इस प्रकार साम्प्रदायिक निर्णय से गहरी असहमति रखते हुये कांग्रेस ने निर्णय किया कि वह न तो साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगी न ही इसे अस्वीकार करेगी.
साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा, दलितों को सामान्य हिन्दुओं से पृथक कर एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप मे मान्यता देने तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सभी राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया.
महात्मा गांधीजी की प्रतिक्रिया
गांधीजी ने साम्प्रदायिक निर्णय की राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा. उनका मत था कि यह हिन्दुओं एवं दलित वर्ग दोनों के लिये खतरनाक है. उनका कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गयी है. एक बार यदि पिछड़े एवं दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अश्पृश्यता को दूर करने का मुद्दा पिछड़ा जायेगा और हिन्दू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जायेगी.
बापू ने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचक मंडल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है. दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर न ही विधानमंडलों या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है और न ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की. अपितु सबसे मुख्य जरूरत समाज से अश्पृश्यता की कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की है.
गांधीजी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्म-निर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए. तथापि उन्होंने दलित वर्ग के लिये बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया. अपनी मांगों को स्वीकार किये जाने के लिये 20 सितंबर 1932 से गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गये.
कई राजनीतिज्ञों ने गांधीजी के अनशन को राजनीतिक आंदोलन की सही दिशा से भटकना कहा. इस बीच विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेता, जिनमें एम.सी. रजा, मदनमोहन मालवीय तथा बी.आर. अम्बेडकर सम्मिलित थे, सक्रिय हो गये. अंततः एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है.
पूना समझौता
सितंबर 1932 में डा. अम्बेडकर तथा अन्य हिन्दू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिन्दुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया. इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है. इस समझौते के अनुसार-
- दलित वर्ग के लिये पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिन्दुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गये.
- लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या 47 से बढ़कर 147 कर दी गयी.
- मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18, बम्बई एवं सिंध में 15-15, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिये सुरक्षित किये गये.
- केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिये संयुक्त व्यवस्था को मान्यता दी गयी.
- दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गयी.
सरकार ने पूना समझौते को साम्प्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया.
पूना समझौता: गांधी और अंबेडकर के दृष्टिकोणों का विश्लेषण
गांधी और अंबेडकर, भारतीय इतिहास के दो प्रमुख व्यक्तित्व, दोनों ही जाति व्यवस्था की बुराइयों के प्रबल आलोचक थे और दलित वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे. हालाँकि, इन दोनों नेताओं के दृष्टिकोणों में एक मूलभूत अंतर था. यह न केवल उनके दर्शन को दर्शाता था, बल्कि भारत के सामाजिक-राजनीतिक भविष्य के लिए उनके प्रस्तावित मार्ग को भी स्पष्ट करता था.
अंबेडकर, एक दूरदर्शी सामाजिक-राजनीतिक सुधारक के रूप में, जाति व्यवस्था को एक ऐसी संस्था मानते थे जो सुधार से परे थी और जिसका पूर्ण उन्मूलन ही एकमात्र समाधान था. उनका मानना था कि जाति एक ऐसा संरचनात्मक अवरोध है जो दलितों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को रोकता है.
वहीं, गांधी, एक आध्यात्मिक और नैतिक नेता के रूप में, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्षधर नहीं थे, बल्कि इसके भीतर व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने पर केंद्रित थे. वे ‘वर्णाश्रम’ धर्म को एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था मानते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करता है, और उनका मानना था कि जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को लोगों के हृदय परिवर्तन और नैतिक शुद्धि के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है.
राजनीतिक बनाम सामाजिक दृष्टिकोण
दोनों नेताओं के दृष्टिकोण में एक और महत्वपूर्ण अंतर यह था कि अंबेडकर जाति के प्रश्न को मूल रूप से एक राजनीतिक मुद्दा मानते थे. उनके लिए, दलितों का उद्धार केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में भागीदारी के माध्यम से ही संभव था. उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि दलित वर्ग राजनीतिक निर्णयों में समान रूप से भागीदार नहीं हैं, तो तथाकथित राजनीतिक लोकतंत्र केवल एक दिखावा है. यह वास्तव में उच्च जातियों के प्रभुत्व को बनाए रखेगा.
इसलिए, अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, ताकि वे अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुन सकें और अपनी आवाज़ को सशक्त रूप से उठा सकें.
इसके विपरीत, गांधीजी जाति को एक सामाजिक और नैतिक मुद्दा मानते थे. वे मानते थे कि हृदय परिवर्तन और उच्च जातियों में नैतिक चेतना जगाकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है.
गांधीजी का मानना था कि यदि समाज के उच्च वर्ग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें और दलितों के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, तो जाति व्यवस्था से जुड़ी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी. यह उनके ‘हरिजन’ आंदोलन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जहाँ वे उच्च जातियों को दलितों के प्रति सहानुभूति रखने और उन्हें भगवान के बच्चे (हरिजन) मानने का आह्वान करते थे.
अधिकार-आधारित बनाम आध्यात्मिकता-आधारित दृष्टिकोण
अंबेडकर का दृष्टिकोण एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण था. वे दलितों के लिए राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की मांग करते थे ताकि वे आत्म-सम्मान और गरिमा के साथ जी सकें. उन्होंने दलित शब्द का प्रयोग भी इसीलिए किया, ताकि इस समुदाय को एक स्पष्ट राजनीतिक पहचान दी जा सके और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष को संगठित किया जा सके. वे मानते थे कि केवल अधिकारों की गारंटी ही उन्हें समानता और न्याय दिला सकती है.
इसके विपरीत, गांधी का दृष्टिकोण आस्था और आध्यात्मिकता पर आधारित था. वे मानते थे कि सामाजिक बुराइयों का समाधान कानूनी या राजनीतिक हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि नैतिक शुद्धि और आध्यात्मिक जागरण से होगा. इसी कारण उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया, जो ‘भगवान के लोग’ को दर्शाता है, ताकि उच्च जातियों में उनके प्रति करुणा और दया का भाव जागृत हो सके. यह उनके दृष्टिकोण का सार था – कि सामाजिक परिवर्तन दिल और दिमाग में बदलाव से आता है, न कि कानून या राजनीति से.
पूना समझौता और भविष्य की प्रासंगिकता
पूना समझौता (1932) इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ था. इस समझौते ने, जिसने पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की, भारतीय राजनीतिक इतिहास और लाखों दलितों की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया. यह समझौता न केवल दो महान नेताओं के बीच का एक समझौता था, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सुधार के बीच एक संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास था.
हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पूना समझौते के बावजूद, जाति व्यवस्था से जुड़ा सामाजिक कलंक आज भी भारतीय समाज में एक गहरी समस्या बना हुआ है. इसलिए, सच्चे अर्थों में एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए, गांधीवादी दर्शन (जो समाज में हृदय परिवर्तन पर जोर देता है) और अंबेडकर की सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा (जो संरचनात्मक समानता और अधिकारों पर केंद्रित है) दोनों की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है.
इन दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय ही एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकता है जहाँ सभी नागरिकों को समानता, न्याय और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो.
पूना पैक्ट का वर्तमान प्रभाव
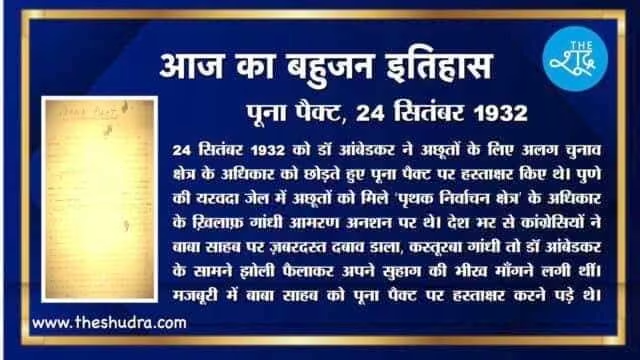
पूना पैक्ट की सबसे प्रमुख विरासत आज भी संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए सीटों का आरक्षण है. यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है. उदाहरण के लिए, लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं. यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश के सबसे बड़े विधायी निकायों में दलित समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, जैसा कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था.
कई अंबेडकरवादी विद्वान तर्क देते हैं कि पूना पैक्ट ने दलितों के प्रतिनिधित्व के स्वरूप को विकृत किया है. उनका मानना है कि पूना पैक्ट के बजाय, डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दलितों के लिए अधिक प्रभावी होती, क्योंकि यह उन्हें अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देती.
पूना पैक्ट के बावजूद, जाति व्यवस्था जैसी कुरीतियां भारतीय समाज में अभी भी बनी हुई हैं. इसका मतलब है कि पूना पैक्ट ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो दिया, लेकिन सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया.
गांधीजी का हरिजन अभियान
सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पुन पैक्ट के द्वारा हिन्दुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधीजी को बुरी तरह आहत कर दिया था. फिर भी गांधीजी ने पूना समझौते के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किये जाने का वचन दिया.
अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधीजी ने अपने अन्य कार्यों को छोड़ दिया तथा पूर्णरूपेण ‘अश्पृश्यता निवारण अभियान’ में जुट गये. उन्होंने अपना अभियान यरवदा जेल से ही प्रारंभ कर दिया था तत्पश्चात अगस्त 1933 में जेल से रिहा होने के उपरांत उनके आदोलन में और तेजी आ गयी.
अपनी कारावास की अवधि में ही उन्होंने सितम्बर 1932 में ‘अखिल भारतीय अश्पृश्यता विरोधी लीग’ का गठन किया तथा जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया. जेल से रिहाई के उपरांत वे सत्याग्रह आश्रम वर्धा आ गये. साबरमती आश्रम, गांधीजी ने 1930 में ही छोड़ दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि स्वराज्य मिलने के पश्चात ही वे साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) में वापस लौटेंगे.
7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधीजी ने अपनी ‘हरिजन यात्रा‘ प्रारंभ की. नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक गांधीजी ने पूरे देश की यात्रा की तथा लगभग 20 हजार किलोमीटर का सफर तय किया. अपनी यात्रा के द्वारा गांधीजी ने स्वयं द्वारा स्थापित संगठन ‘हरिजन सेवक संघ’ जगह-जगह पर कोष एकत्रित करने का कार्य भी किया.
गांधीजी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था-हर रूप में अश्पृश्यता को समाप्त करना. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह किया की गांवों का भ्रमण हरिजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का कार्य करें. दलितों को ‘हरिजन’ नाम सर्वप्रथम गांधीजी ने ही दिया था.
हरिजन उत्थान के इस अभियान में गांधीजी 8 मई व 16 अगस्त 1933 को दो बार लंबे अनशन पर बैठे. उनके अनशन का उद्देश्य, अपने प्रयासों की गंभीरता एवं अहमियत से अपने समर्थकों को अवगत कराना था. अनशन की रणनीति ने राष्ट्रवादी खेमे को बहुत प्रभावित किया. बहुत से लोग भावुक हो गये.
अपने हरिजन आंदोलन के दौरान गांधीजी को हर कदम पर सामाजिक प्रतिक्रियावादियों तथा कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा. उनके खिलाफ प्रदर्शन किये तथा उन पर हिंदूवाद पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया गया. सविनय अवज्ञा आदोलन तथा कांग्रेस का विरोध करने के निमित्त, सरकार ने इन प्रतिक्रियावादी तत्वों का भरपूर साथ दिया.
अगस्त 1934 में लेजिस्लेटिव एसेंबली में ‘मंदिर प्रवेश विधेयक’ को गिराकर, सरकार ने इन्हें अनुग्रहित करने का प्रयत्न किया. बंगाल में कट्टरपंथी हिन्दू विचारकों ने पूना समझौते द्वारा हरिजनों को हिन्दू अल्पसंख्यक का दर्जा दिये जाने की अवधारणा को पूर्णतयाः खारिज कर दिया.
गांधी जी के जाति संबंधी विचार
गांधीजी ने अपने पूरे हरिजन आंदोलन, सामाजिक कार्य एवं अनशनों में कुछ मूलभूत तथ्यों पर सर्वाधिक जोर दिया-
- हिन्दू समाज में हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचार तथा भेदभाव की उन्होंने तीव्र भर्त्सना की.
- दूसरा प्रमुख मुद्दा था- छुआछूत को जड़ से समाप्त करना. उन्होंने अश्पृश्यता की कुरीति को समूल नष्ट करने तथा हरिजनों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिये जाने की मांग की.
- उन्होंने इस बात की मांग उठायी कि हिन्दुओं द्वारा सदियों से हरिजनों पर जो अत्याचार किया जाता रहा है, उसे अतिशीघ्र बंद किया जाना चाहिए तथा इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए. शायद यही वजह थी कि गांधीजी ने अम्बेडकर या अन्य हरिजन नेताओं की आलोचनाओं का कभी बुरा नहीं माना. उन्होंने हिन्दू समाज को चेतावनी दी कि “यदि अश्पृश्यता का रोग समाप्त नहीं हुआ तो हिन्दू समाज समाप्त हो जायेगा. यदि हिंदूवाद को जीवित रखना है तो अश्पृश्यता को समाप्त करना ही होगा”.
- गांधीजी का सम्पूर्ण हरिजन अभियान मानवता एवं तर्क के सिद्धांत पर अवलंबित था. उन्होंने कहा कि शास्त्र छुआछूत की इजाजत नहीं देते हैं. लेकिन यदि वे ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं तो हमें उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना मानवीय प्रतिष्ठा के विरुद्ध है.
गांधीजी अस्पृश्यता निवारण के मुद्दे को अंतर्जातीय विवाह एवं अंतर्जातीय भोज जैसे मुद्दों के साथ जोड़ने के पक्षधर नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि ये चीजें स्वयं हिन्दू सवर्ण समाज एवं हरिजनों के बीच में भी हैं. उनका कहना था कि उनके हरिजन अभियान का मुख्य उद्देश्य, उन कठिनाइयों एवं कुरीतियों को दूर करना है, जिससे हरिजन समाज शोषित और पिछड़ा है.
इसी तरह उन्होंने जाति निवारण तथा छुआछूत निवारण में भी भेद किया. इस मुद्दे पर वे डा. अम्बेडकर के इन विचारों से असहमत थे कि छुआछूत की बुराई जाति प्रथा की देन है तथा जब तक जाति प्रथा बनी रहेगी यह बुराई भी जीवित रहेगी. अतः जाति प्रथा को समाप्त किये बिना अछूतों का उद्धार संभव नहीं है.
गांधीजी का कहना था कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई पाप नहीं है. हां, छुआछूत अवश्य पाप है. उनका तर्क था कि छुआछूत, जाति प्रथा के कारण नहीं अपितु ऊच-नीच के कृत्रिम विभाजन के कारण है. यदि जातियां एक दूसरे की सहयोगी एवं पूरक बन कर रहें तो जाति प्रथा में कोई दोष नहीं है. कोई भी जाति न उच्च है न निम्न. उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक एवं विरोधियों दोनों से आह्वान किया कि वे आपस में मिलकर काम करें क्योंकि दोनों ही छुआछूत के विरुद्ध हैं.
गांधीजी का विचार था कि छुआछूत की बुराई का उन्मूलन करने से उसका साम्प्रदायिकता एवं ऐसे ही अन्य मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसकी उपस्थिति का तात्पर्य होगा जाति प्रथा में उच्च एवं निम्न की अवधारणा को स्वीकार करना. गांधीजी ने छुआछूत के समर्थक दकियानूसी प्रतिक्रियावादी हिन्दुओं को ‘सेनापति‘ कहा.
किंतु वे इन पर किसी प्रकार का दबाव डाले जाने के विरोधी थे. उनका कहना था कि इन्हें समझा-बुझाकर तथा इनके दिलों को जीतकर इन्हें सही रास्ते पर लाना होगा न कि इन पर दबाव डालकर. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अनशन का उद्देश्य, उनके द्वारा चलाये जा रहे छुआछूत विरोधी आंदोलन के संबंध में उनके मित्रों एवं अनुयायियों के उत्साह को दुगना करना है.
अभियान का प्रभाव
गांधीजी ने बार-बार यह बात दुहराई कि उनके हरिजन अभियान का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है अपितु यह हिन्दू समाज एवं हिन्दुत्व का शुद्धीकरण आंदोलन है. वास्तव में गांधीजी ने अपने हरिजन अभियान के दौरान केवल हरिजनों के लिये ही कार्य नहीं किया.
उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया कि जनआंदोलन के निष्क्रिय या समाप्त हो जाने पर वे स्वयं को किस प्रकार के रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं. उनके आंदोलन ने राष्ट्रवाद के संदेश को हरिजनों तक पहुंचाया. यह वह वर्ग था, जिसके अधिकांश सदस्य खेतिहर मजदूर थे तथा धीरे-धीरे किसान आंदोलन तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे.



