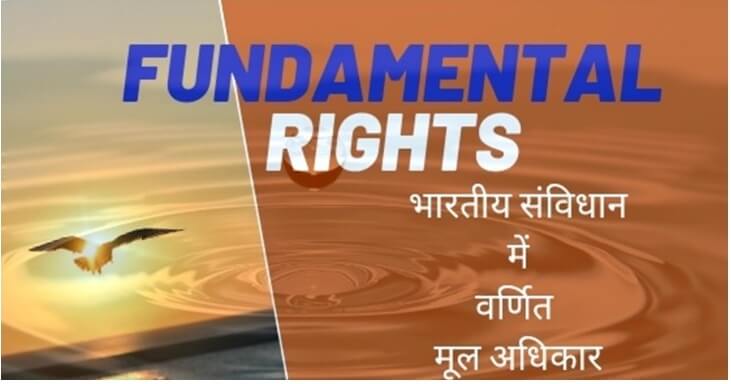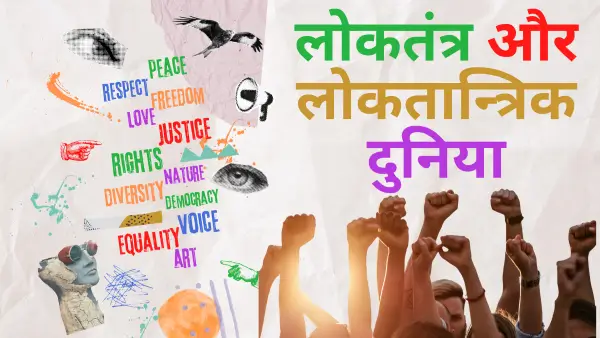भारत में सरकार का ढांचा संघीय स्वरूप का हैं. अर्थात यहाँ दो स्तर की सरकारें हैं- संघ सरकार और राज्य सरकार. भारतीय संविधान में दोनों तरह की सरकारों के कामकाज को निर्दिष्ट किया गया है. वास्तव में केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण देश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक विस्तृत होता है. लेकिन राज्य सरकार देश के एक हिस्से का शासन संचालित करती हैं.
जैसा कि हम जानते हैं, भारत राज्यों का एक संघ है. प्रत्येक राज्य की अपनी शासन प्रणाली है जो संघीय संसद की तर्ज पर है. लोकतंत्र में जनता केंद्र और राज्य स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करती हैं. लेकिन इसका मतलब सिर्फ़ लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने से जुड़ा है.
इसलिए आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उन्हें कौन लेता है, कौन उन्हें लागू करता है और यदि कोई विवाद होता है, तो कौन उन्हें सुलझाता है.
राज्य विधानमंडल
केंद्र में लोकसभा की तरह, राज्यों की अपनी विधान सभाएँ होती हैं. यह राज्य का निचला सदन सदन हैं. लेकिन, राज्यसभा की तरह कुछ राज्यों की अपनी विधान परिषदें हैं. यह राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन हैं. यह ध्यान देने योग्य है कि सभी राज्यों के पास अपने ऊपरी सदन यानी विधान परिषद नहीं हैं.
राज्य विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में हैं. ये हैं- आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश. इन द्विसदनात्मक सदन वाले राज्यों में निचला सदन विधानसभा हैं.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल परिभाषित की गई है. जनवरी 2020 तक, 28 राज्यों में से 6 में राज्य विधान परिषद है. परिषद रखने वाला नवीनतम राज्य तेलंगाना है. अन्य सभी राज्यों में मात्र विधान सभा हैं.
विधानसभा
विधान सभा राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है. इसे जनता का सदन या निचला सदन भी कहा जाता है. इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं. विधान सभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है. सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग-अलग होती है.
विधानसभा सदस्यों का चुनाव
विधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुना जाता है. प्रत्येक राज्य को अलग-अलग क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं. चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार विधान सभा का सदस्य (एमएलए) बन जाता है. उम्मीदवार अलग-अलग पार्टियों के नाम से चुनाव लड़ते हैं. इसलिए ये विधायक अलग-अलग राजनीतिक दलों के होते हैं.
विधानसभा उम्मीदवारों के लिए योग्यताएँ (अनु० 173):
(i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए.
(ii) उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
(iii) वह संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए.
(iv) वह पागल या दिवालिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए.
(v) उसे किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए.
(vi) उसे संसद के अधिनियम द्वारा निर्धारित अन्य सभी योग्यताएँ पूरी करनी चाहिए.
सदस्यों को अपना पद ग्रहण से ठीक पूर्व अनुच्छेद 188 के तहत तीसरी अनुसूची में दी गई प्रारूप के अनुसार शपथ लेना होता हैं.
कार्यकाल
विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल इसे कभी भी भंग कर सकते हैं. राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के दौरान इसका कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.
सत्र
राज्यपाल किसी भी समय सत्र बुला सकते हैं. लेकिन दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए.
संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अनुसार राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधानमंडल के दोनों या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा.
नाबाम-राबिया मामला (2016) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह व परामर्श से विधानसभा सत्र बुलायेगा. अनुच्छेद 174 व अनुच्छेद 163 को साथ-साथ पढ़ने का निर्देश भी दिया गया.
अनुच्छेद 174(2)क के अन्तर्गत राज्यपाल विधानमण्डल के किसी भी सदन का सत्रावसान और; अनुच्छेद 174(2)ख के अन्तर्गत राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकता है.
पंगु सत्र: एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्य काल की शुरुआत के बीच के काल में सम्पन्न होने वाले सत्र को ‘पंगुसत्र’ कहा जाता है.
आरक्षण का प्रावधान
संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है. यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग हैं. करीब-करीब इन वर्ग के राज्य में आबादी के अनुपात में ही सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाता हैं. (अनु० 332)
एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों का नामांकन: राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, यदि उनका मानना है कि विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है. 2020 में संविधान संसोधन द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया हैं.
विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
विधानसभा के सदस्य अपनी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं. अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों के दौरान अनुशासन बनाए रखता है, सदस्यों को पहचानता है और उन्हें बोलने की अनुमति देता है, मतदान के लिए प्रस्ताव रखता है और परिणाम घोषित करता है.
अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को आर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को सौंप सकते हैं. दोनों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता हैं. इसका निर्धारण संबंधित राज्य के सदन द्वारा किया जाता हैं.
विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य
1. कानून बनाने की शक्ति: विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची में समूहीकृत विषयों पर कानून बना सकती है. लेकिन विधान सभा द्वारा पारित कानून समवर्ती विषय से संबंधित संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ संघर्ष में आता है, तो संघ का कानून लागू होगा. द्वि-सदनीय विधायिका वाले राज्यों में विधान परिषद किसी विधेयक को 4 महीने तक विलंबित कर सकती है, लेकिन उस पर वीटो नहीं लगा सकती.
2. वित्तीय शक्तियाँ: विधानसभा राज्य के वित्त को नियंत्रित करती है. यह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को मंजूरी देती है जिसके माध्यम से यह सरकार को कर लगाने, कम करने या समाप्त करने का अधिकार देती है. राज्य सरकार इसकी मंजूरी के बिना धन खर्च नहीं कर सकती. विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्थगित नहीं कर सकती.
3. कार्यकारी शक्तियाँ: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है. विधान सभा के सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि लाकर मंत्रिपरिषद को इसके प्रति उत्तरदायी बनाते हैं. विधान सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती है.
4. संवैधानिक शक्तियाँ: संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है. इस प्रकार विधान सभा विधान परिषद के साथ संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेती है.
5. निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ:
(i) विधान सभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं.
(ii) यह विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करता है.
(iii) यह राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करता है.
(iv) सदस्य एक अध्यक्ष और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं.
विधान परिषद्
राज्य विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि वे विधायकों, स्थानीय निकायों, शिक्षकों, स्नातकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. विधान परिषद के प्रावधानों का उल्लेख दूसरे लेख में किया जाएगा. इसलिए उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा हैं.
राज्य कार्यकारिणी
भारत में राज्य कार्यकारिणी में भी संघ कार्यकारिणी की तरह दो भाग होते हैं –
1. नाममात्र कार्यकारिणी
2. वास्तविक कार्यकारिणी
राज्यपाल नाममात्र कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी होती है.
मंत्रिपरिषद
राज्य में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है, जो मंत्रिपरिषद के साथ-साथ इसका संवैधानिक प्रमुख होता है.
मंत्रिपरिषद का गठन
मंत्रिपरिषद के गठन में पहला कदम राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है. मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता हैं. मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना है. केवल राज्य विधानमंडल का सदस्य ही मंत्री या मुख्यमंत्री हो सकता है. लेकिन अगर कोई गैर-सदस्य नियुक्त किया जाता है तो उसे नामांकन/नियुक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर विधायक/एमएलसी बनना होगा.
राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की चार श्रेणियां होती हैं:-
1) कैबिनेट मंत्री: वे मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण और वरिष्ठतम सदस्य होते हैं. वे स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार संभालते हैं और उनकी संख्या आम तौर पर कम होती है.
2) राज्य मंत्री: दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री सूचीबद्ध हैं. वे कभी-कभी विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं और कभी-कभी उन्हें विभागों के प्रशासन में कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने की आवश्यकता हो सकती है. वे आम तौर पर मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं.
3) उप मंत्री: उप मंत्री मंत्रिपरिषद की तीसरी श्रेणी बनाते हैं. वे किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं रखते हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के साथ जुड़े होते हैं. उनके काम की प्रकृति वैसी ही होती है, जैसा उन्हें विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा सौंपा जाता है.
4) संसदीय सचिव: वे न तो उचित रूप से मंत्री कहलाते हैं और न ही वे किसी विभाग का प्रभार संभालते हैं. उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं. उनका मुख्य कार्य मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत कार्य करना होता है.
कार्यकाल
संवैधानिक शब्दावली में मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद पर बने रहते हैं. लेकिन संसदीय प्रणाली के तहत मंत्रालय सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और पांच वर्ष से पहले किसी भी समय विधानसभा का विश्वास खोने पर उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है. यह विधानसभा और मंत्रालय दोनों का सामान्य या सामान्य कार्यकाल है.
मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री से संबंध
मुख्यमंत्री की विशिष्ट स्थिति : मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री से संबंध समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के पास अपार शक्तियां होती हैं. उसकी स्थिति अद्वितीय होती है. वह अपने मंत्रियों की टीम का कप्तान होता है. वह पूरी राज्य सरकार और उसके प्रशासन की धुरी होता है. मुख्यमंत्री एक प्रमुख व्यक्ति होता है, वह अपने मंत्रि-ग्रहों में सूर्य के समान होता है. उसके पास विधायी, कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं. उसके किसी भी मंत्री की उससे तुलना नहीं की जा सकती.
मुख्यमंत्री के कार्यों और शक्तियों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है:
1. मंत्रिपरिषद का गठन: अपनी नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की सूची तैयार करता है और इस सूची को राज्यपाल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है. वह अपने मंत्रिपरिषद में किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है और राज्यपाल की स्वीकृति केवल एक औपचारिकता होती है.
2. विभागों का वितरण: मुख्यमंत्री मंत्रियों की कार्यकुशलता और महत्व के आधार पर मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है और उनके विभागों में फेरबदल कर सकता है.
3. मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन: मुख्यमंत्री समय-समय पर मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करता है, वह योग्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है और अक्षम मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटा सकता है.
4. राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी: मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है. वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराता है और राज्यपाल की सलाह को मंत्रिपरिषद तक पहुँचाता है.
5. जनता का नेता: मुख्यमंत्री राज्य की जनता का नेता होता है. राज्य की जनता राज्य के विकास और मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर देखती है. राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, इसलिए राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ही जनता का नेता होता है.
6. नियुक्तियों पर नियंत्रण: हालांकि राज्य में सभी उच्च नियुक्तियाँ जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालयों के कुलपति सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल द्वारा की जाती हैं, लेकिन वास्तव में इन उच्च नियुक्तियों को दिए जाने वाले व्यक्तियों की सूची मुख्यमंत्री द्वारा बनाई जाती है. यहाँ तक कि राज्यपाल की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं.
7. वित्त पर नियंत्रण: वित्त मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा और पसंद के अनुसार वित्त विधेयक तैयार करता है और उसे विधानमंडल में पेश करता है.
सीएम का पद
मुख्यमंत्री राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है. केंद्र में प्रधानमंत्री के समान ही राज्य में मुख्यमंत्री का पद पर होता है. लेकिन दोनों के अधिकारक्षेत्र अलग होते हैं. राज्य में कोई भी कार्य मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता. वह मंत्रालय के गठन, मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण, विभागों में फेरबदल और वास्तव में मंत्रिमंडल के जीवन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वह किसी भी मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है. उसका इस्तीफा पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है. वास्तव में वह वह धुरी है जिसके इर्द-गिर्द पूरा मंत्रिपरिषद और राज्य का पूरा प्रशासन घूमता है.
विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन
अनुच्छेद 170 खण्ड-2(1): प्रत्येक राज्य के भीतर सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए.
अनुच्छेद 170 खण्ड 3: प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे.
संविधान में राज्य सरकार
भारतीय संविधान का भाग VI, अध्याय III राज्यों के विधानमंडल से संबंधित है. इसमें अनुच्छेद 168 से 212 तक शामिल हैं. ये अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के गठन, संरचना, कार्यकाल, पदाधिकारियों, प्रक्रियाओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों का विस्तृत विवरण देते हैं.
यहाँ अनुच्छेद 168 से 212 तक का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
साधारण
- अनुच्छेद 168 – राज्यों के विधानमंडलों का गठन
- अनुच्छेद 169 – राज्यों में विधानपरिषदों का उत्सादन या सृजन
- अनुच्छेद 170 – विधानसभाओं की संरचना
- अनुच्छेद 171 – विधानपरिषदों की संरचना
- अनुच्छेद 172 – राज्य के विधानमंडलों की अवधि
- अनुच्छेद 173 – राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
- अनुच्छेद 174 – राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
- अनुच्छेद 175 – सदन या सदनों में अभिभाषण और उनकों संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
- अनुच्छेद 176 – राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
- अनुच्छेद 177 – सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
राज्य के विधान मंडल के अधिकारी
- अनुच्छेद 178 – विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 179 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 180 – अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 181 – जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
- अनुच्छेद 182 – विधानपरिषद का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 183 – सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 184 – सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 185 – जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
- अनुच्छेद 186 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 187 – राज्य के विधानमंडल का सचिवालय
कार्य संचालन
- अनुच्छेद 188 – सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 189 – सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
सदस्यों की निरर्हताएं
- अनुच्छेद 190 – स्थानों का रिक्त होना
- अनुच्छेद 191 – सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
- अनुच्छेद 192 – सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
- अनुच्छेद 193 – अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति
राज्य के विधानमंडलों की और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
- अनुच्छेद 194 – विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि
- अनुच्छेद 195 – सदस्यों के वेतन और भत्ते
विधायी प्रक्रिया
- अनुच्छेद 196 – विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के सम्बन्ध में उपबंध
- अनुच्छेद 197 – धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बन्धन
- अनुच्छेद 198 – धन विधेयकों के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 199 – “धन विधेयक” की परिभाषा
- अनुच्छेद 200 – विधेयकों पर अनुमति के लिए आरक्षित विधेयक
- अनुच्छेद 201 – वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया
वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया
- अनुच्छेद 202 – वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 203 – विधानमंडल में प्राक्कलनों के सम्बन्ध में प्रक्रिया
- अनुच्छेद 204 – विनियोग विधेयक
- अनुच्छेद 205 – अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
- अनुच्छेद 206 – लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
- अनुच्छेद 207 – वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
साधारणतया प्रक्रिया
- अनुच्छेद 208 – प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 209 – राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
- अनुच्छेद 210 – विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- अनुच्छेद 211 – विधानमंडल में चर्चा पर निर्बन्धन
- अनुच्छेद 212 – न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना
विभिन राज्यों के विधानमंडलों की स्थिति
भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, वर्तमान राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों/प्रशासकों की जानकारी नीचे दी गई है. यह जानकारी नवीनतम उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण इसमें परिवर्तन संभव है. भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं. इनमें से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) है, जबकि शेष 22 राज्यों में एकसदनीय विधानमंडल (केवल विधानसभा) है.
| क्र.सं. | राज्य | विधानसभा सीटें | विधान परिषद सीटें | वर्तमान राज्यपाल | वर्तमान मुख्यमंत्री |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 175 | 58 | श्री सैयद अब्दुल नज़ीर | श्री एन. चंद्रबाबू नायडू |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 60 | – | लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक | श्री पेमा खांडू |
| 3. | असम | 126 | – | श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य | श्री हिमंत बिस्वा सरमा |
| 4. | बिहार | 243 | 75 | आरिफ़ मोहम्मद ख़ान | श्री नीतीश कुमार |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 90 | – | श्री रमेन डेका | श्री विष्णुदेव साय |
| 6. | गोवा | 40 | – | श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई | श्री प्रमोद सावंत |
| 7. | गुजरात | 182 | – | श्री आचार्य देवव्रत | श्री भूपेंद्र पटेल |
| 8. | हरियाणा | 90 | – | श्री बंडारू दत्तात्रेय | श्री नायब सैनी |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 68 | – | श्री शिव प्रताप शुक्ल | श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू |
| 10. | झारखंड | 81 | – | श्री संतोष कुमार गंगवार | श्री चंपई सोरेन |
| 11. | कर्नाटक | 224 | 75 | श्री थावरचंद गहलोत | श्री सिद्दारमैया |
| 12. | केरल | 140 | – | श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर | श्री पिनरई विजयन |
| 13. | मध्य प्रदेश | 230 | – | श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल | श्री मोहन यादव |
| 14. | महाराष्ट्र | 288 | 78 | श्री सी.पी. राधाकृष्णन | श्री देवेन्द्र फडणवीस |
| 15. | मणिपुर | 60 | – | श्री अजय कुमार भल्ला | 13 फ़रवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन |
| 16. | मेघालय | 60 | – | श्री सी एच विजयशंकर | श्री कोनराड संगमा |
| 17. | मिजोरम | 40 | – | जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह | श्री लालदुहोमा |
| 18. | नागालैंड | 60 | – | श्री ला गणेशन | श्री नेफ्यू रियो |
| 19. | ओडिशा | 147 | – | डॉ. हरि बाबू कंभमपति | श्री मोहन चरण माझी |
| 20. | पंजाब | 117 | – | श्री गुलाब चंद कटारिया | श्री भगवंत मान |
| 21. | राजस्थान | 200 | – | श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े | श्री भजनलाल शर्मा |
| 22. | सिक्किम | 32 | – | श्री ओम प्रकाश माथुर | श्री पी.एस. गोले |
| 23. | तमिलनाडु | 234 | – | श्री आर.एन. रवि | श्री एम.के. स्टालिन |
| 24. | तेलंगाना | 119 | 40 | श्री जिष्णु देव वर्मा | श्री रेवंत रेड्डी |
| 25. | त्रिपुरा | 60 | – | श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू | डॉ. माणिक साहा |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 403 | 100 | श्रीमती आनंदीबेन पटेल | श्री योगी आदित्यनाथ |
| 27. | उत्तराखंड | 70 | – | लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवनिवृत) | श्री पुष्कर सिंह धामी |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 294 | – | डॉ. सी. वी. आनंद बोस | सुश्री ममता बनर्जी |
केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सीटें, मुख्यमंत्री और प्रशासक/उप-राज्यपाल/राज्यपाल
भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. इनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर) में अपनी विधानसभा और निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं.
| क्र.सं. | केंद्र शासित प्रदेश | विधानसभा सीटें | वर्तमान उपराज्यपाल/ प्रशासक | वर्तमान मुख्यमंत्री (यदि लागू हो) |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | एडमिरल डी.के. जोशी | – |
| 2. | चंडीगढ़ | – | श्री गुलाब चंद कटारिया (प्रशासक) | – |
| 3. | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | – | श्री प्रफुल्ल पटेल (प्रशासक) | – |
| 4. | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | 70 | श्री विनय कुमार सक्सेना | श्रीमति रेखा गुप्ता |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | 90 | श्री मनोज सिन्हा (लेफ्टिनेंट गवर्नर) | श्री उमर अब्दुल्ला |
| 6. | लद्दाख | – | ब्रिगेडियर (डॉ.) बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) | – |
| 7. | लक्षद्वीप | – | श्री प्रफुल्ल पटेल (प्रशासक) | – |
| 8. | पुडुचेरी | 30 + 3 मनोनीत | श्री के. कैलाशनाथन (लेफ्टिनेंट गवर्नर) | श्री एन. रंगासामी |
नोट:
- विधान परिषद वाले राज्यों में, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती है. उनकी वास्तविक संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है.
- यह जानकारी समय-समय पर बदल सकती है, विशेषकर मुख्यमंत्री और राज्यपालों के पदों पर.
राज्य के राज्यपाल पर लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें.