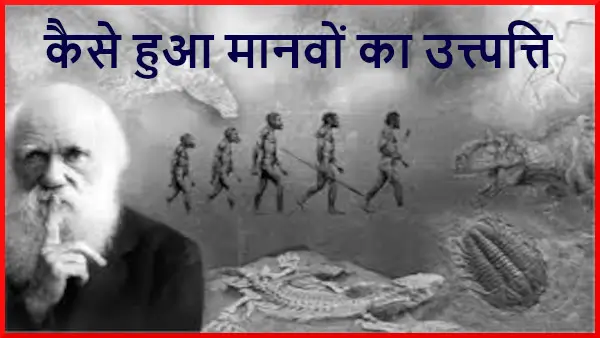“जैव प्रौद्योगिकी” (Biotechnology) शब्द का प्रयोग जीवित जीवों या उनके उत्पादों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य और मानव पर्यावरण में सुधार लाने के लिए किया जाता है. इसे 1919 में हंगरी के एक इंजीनियर कार्ल एरेकी ने गढ़ा था.
जैव प्रौद्योगिकी को उस तकनीक के रूप में वर्णित किया जाता है जो डीएनए में हेरफेर करके जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है. इसमें नई तकनीकें भी शामिल हैं जिनके परिणामों का अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है और जिनके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे स्टेम सेल, जीन थेरेपी और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग.
जैव प्रौद्योगिकी का विकास के कालक्रम (Timeline of Biotechnology Development)
मानव जीवन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है. यह विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ ही बिल्कुल नए स्वरूप में आ गया है. इसके विकास का इतिहास व कालक्रम इस प्रकार हैं:
6000 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक के प्रारंभिक अनुप्रयोग और अनुमान
1700 से 1900 तक
डीएनए तकनीक का आगमन: 1900 से 1953
डीएनए अनुसंधान की सीमाओं का विस्तार: 1953-1976
बायोटेक का उदय (Rise of Biotechnology): 1977 से 2001
पशु जैव प्रौद्योगिकी (Animal Biotechnology)
• पशु जैव प्रौद्योगिकी, वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए पशुओं या जलीय प्रजातियों द्वारा सामग्रियों के प्रसंस्करण या उत्पादन में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सिद्धांतों का अनुप्रयोग है.
• उदाहरणों में जीन नॉकआउट तकनीक का उपयोग करके ट्रांसजेनिक पशुओं का उत्पादन, दैहिक कोशिका नाभिकीय स्थानांतरण द्वारा क्लोन का उत्पादन, या बांझ जलीय प्रजातियों का उत्पादन शामिल है.
ट्रांसजेनिक
• 1980 के दशक के प्रारंभ से, ट्रांसजेनिक पशुओं या जलीय प्रजातियों के उत्पादन के तरीकों में सुधार किया गया है.
• ट्रांसजेनिक पशुधन और जलीय प्रजातियों का उत्पादन बढ़ी हुई वृद्धि दर, बढ़ी हुई दुबली मांसपेशियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, या पशु खाद के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए आहारीय फास्फोरस के बेहतर उपयोग के साथ किया गया है.
• मानव औषधियों के रूप में उपयोग के लिए अंडे, दूध, रक्त या मूत्र में मानव प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए भी ट्रांसजेनिक पशुओं का उत्पादन किया गया है.
• ट्रांसजेनिक पशुओं के उत्पादन की सफलता दर 10 प्रतिशत से भी कम है, जो उनके व्यापक उपयोग को सीमित करने वाला एक प्रमुख कारक है.
जीन नॉकआउट तकनीक
• इस तकनीक का उपयोग एक विशिष्ट जीन को निष्क्रिय करने के लिए किया गया है.
• यह “ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन” नामक प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्यों के लिए प्रतिस्थापन अंगों का एक संभावित स्रोत बनाता है. इस उद्देश्य के लिए सूअर एक प्रमुख पशु है जिस पर विचार किया जा रहा है.
• आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग सूअर के उस जीन को निष्क्रिय करने के लिए किया जा सकता है जो सूअर की कोशिकाओं पर एक कार्बोहाइड्रेट एपिटोप जोड़ता है जो सामान्यतः मानव कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ज़ेनोग्राफ्ट की तीव्र अस्वीकृति हो सकती है.
• नॉकआउट तकनीक प्रियन से जुड़े रोगों के प्रति प्रतिरोधी पशु भी उत्पन्न कर सकती है.
दैहिक कोशिका नाभिकीय स्थानांतरण
• यह पशु जैव प्रौद्योगिकी का एक और अनुप्रयोग है जिसका उपयोग लगभग समान पशुओं की कई प्रतियाँ बनाने के लिए किया जाता है, जिसे क्लोनिंग भी कहा जाता है.
• इस तकनीक में दैहिक कोशिकाओं का संवर्धन, उनके नाभिक को एक नाभिकरहित अंडकोशिका में सूक्ष्म रूप से इंजेक्ट करना और फिर भ्रूण को प्राप्तकर्ता मादा में स्थानांतरित करना शामिल है.
• दैहिक कोशिका नाभिकीय स्थानांतरण का उपयोग मवेशियों, भेड़ों, सूअरों, बकरियों, घोड़ों, खच्चरों, बिल्लियों, चूहों और चूहों के क्लोन बनाने के लिए किया गया है.
बांझ जलीय प्रजातियों का उत्पादन
• यह जलीय कृषि उत्पादन प्रणालियों से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में पलायन करने वाली गैर-देशी प्रजातियों द्वारा उत्पन्न पारिस्थितिक जोखिम का एक संभावित समाधान है.
• तकनीकों में गुणसूत्र पूरक को बदलकर व्यक्तियों को बांझ बनाना शामिल है, उदाहरण के लिए, दो के बजाय तीन गुणसूत्रों वाले त्रिगुणित व्यक्तियों का उत्पादन करके.
समस्याएँ और संभावनाएँ
• पशु जैव प्रौद्योगिकी अनिश्चितताओं, सुरक्षा संबंधी मुद्दों और संभावित जोखिमों का सामना करती है, जैसे अनावश्यक जीनों का उपयोग, अन्य जीवों में वाहकों का स्थानांतरण, पर्यावरण और पशु कल्याण पर संभावित प्रभाव, और मानव स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ.
• यूएसडीए जैव प्रौद्योगिकी जोखिम मूल्यांकन अनुदान कार्यक्रम और एनआरआई पशु संरक्षण कार्यक्रम इन जोखिमों से निपटने के लिए अनुसंधान का समर्थन करते हैं.
डीएनए क्या है?
• डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) एक अणु है जिसमें जैविक निर्देश होते हैं जो प्रत्येक प्रजाति को विशिष्ट बनाते हैं.
• यह कोशिका के एक विशेष क्षेत्र, जिसे नाभिक कहते हैं, के अंदर पाया जाता है.
• डीएनए गुणसूत्र नामक एक संरचना में कसकर पैक होता है.
• किसी जीव के नाभिकीय डीएनए के पूरे समूह को उसका जीनोम कहते हैं.
• मनुष्यों में माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए की थोड़ी मात्रा होती है, जो यौन प्रजनन के दौरान केवल मादा जनक से ही विरासत में मिलती है.
• डीएनए न्यूक्लियोटाइड नामक रासायनिक निर्माण खंडों से बना होता है, जिनमें एक फॉस्फेट समूह, एक शर्करा समूह और चार नाइट्रोजन क्षारों में से एक: एडेनिन (A), थाइमिन (T), ग्वानिन (G), और साइटोसिन (C) शामिल होते हैं.
• इन क्षारों का क्रम या अनुक्रम, डीएनए के एक रज्जुक में जैविक निर्देशों को निर्धारित करता है.
• एक डीएनए अनुक्रम जिसमें प्रोटीन बनाने के निर्देश होते हैं, जीन कहलाता है.
• मानव के लिए संपूर्ण डीएनए निर्देश पुस्तिका में लगभग 3 अरब क्षार और 23 जोड़ी गुणसूत्रों पर लगभग 20,000 जीन होते हैं.
• डीएनए के निर्देशों का उपयोग दो-चरणीय प्रक्रिया में प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है: मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (एमआरएनए) में प्रतिलेखन और फिर अमीनो एसिड में अनुवाद, जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं.
डीएनए की खोज किसने की?
• जर्मन जैव रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार 1800 के दशक के अंत में डीएनए का अवलोकन किया था.
• डीएनए और इसकी द्वि-कुंडलित संरचना के महत्व को 1953 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, मौरिस विल्किंस और रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने उजागर किया था.
डीएनए द्वि-कुंडलित (DNA Double Helix) क्या है?
• वैज्ञानिक डीएनए की घुमावदार, दो-रज्जुकीय रासायनिक संरचना का वर्णन करने के लिए “द्वि-कुंडलित” शब्द का उपयोग करते हैं, जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखती है.
• सीढ़ी के किनारे बारी-बारी से शर्करा और फॉस्फेट समूहों के तंतु हैं, जबकि प्रत्येक “पंक्ति” हाइड्रोजन बंधों द्वारा युग्मित दो नाइट्रोजन क्षारों से बनी है.
• इस युग्मन की विशिष्ट प्रकृति के कारण, एडेनिन (A) हमेशा थाइमिन (T) के साथ युग्मित होता है, और साइटोसिन (C) हमेशा ग्वानिन (G) के साथ युग्मित होता है.
• यह अनूठी संरचना अणु को कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देती है.
जीनोम मानचित्रण (Genome Mapping)
• वैज्ञानिक जीनोम के भीतर किसी विशिष्ट जीन का पता लगाने के लिए आनुवंशिक और भौतिक मानचित्रों का उपयोग करते हैं.
• आनुवंशिक मानचित्र: ये मानचित्र, अंतरराज्यीय राजमार्ग मानचित्र की तरह, दो वस्तुओं के बीच की दूरी का अप्रत्यक्ष अनुमान प्रदान करते हैं और कुछ वस्तुओं को क्रमबद्ध करने तक सीमित होते हैं. ये आनुवंशिक चिह्नक नामक स्थलों का उपयोग करते हैं.
• भौतिक मानचित्र: ये मानचित्र, सड़क मानचित्र के समान, माप में रुचिकर वस्तुओं के बीच की वास्तविक दूरी का अनुमान लगाते हैं, जिन्हें आधार युग्म कहा जाता है. ये वैज्ञानिकों को किसी जीन के स्थान का अधिक आसानी से पता लगाने में मदद करते हैं.
• भौतिक मानचित्रों के तीन सामान्य प्रकार हैं: गुणसूत्रीय या कोशिकाजनन संबंधी मानचित्र, विकिरण संकर (RH) मानचित्र, और अनुक्रम मानचित्र.
• सहलग्नता विश्लेषण: इस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग संभावित क्रॉसओवर पैटर्न और शामिल चिह्नकों के क्रम का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है. यह शोधकर्ताओं को चिह्नकों के प्रत्येक युग्म के बीच पुनर्संयोजन की संभावना का अनुमान लगाने की भी अनुमति देता है.