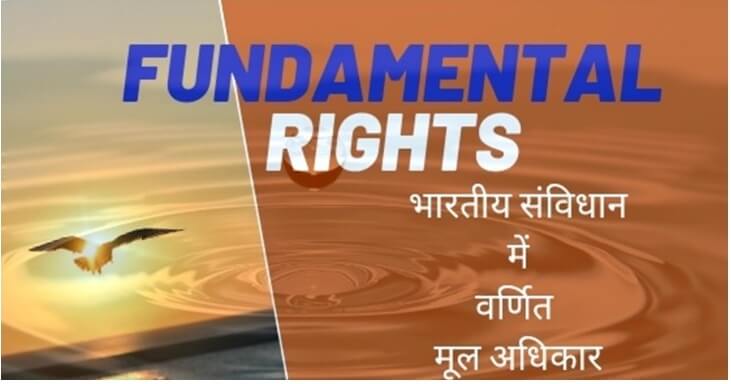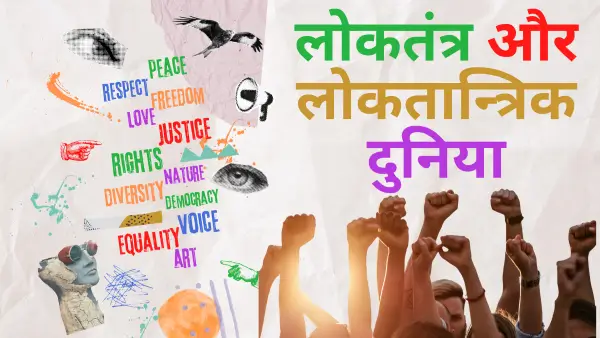राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन की गई हैं. इस अधिनियम को 12 अक्टूबर 1993 को 28 सितंबर 1993 के मानव अधिकार अध्यादेश के संरक्षण में एकीकृत किया गया था. पुनः, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 (PHRA) द्वारा संवैधानिक आधार दिया गया था.
NHRC भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है. यह मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है. इसे अधिनियम द्वारा “संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय रूप में सन्निहित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा और सम्मान से संबंधित अधिकार और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है.” के रूप में परिभाषित किया गया है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना
NHRC के संरचना का प्रावधान अधिनियम के धारा 3 में वर्णित हैं. इसके अनुसार, आयोग में कुल आठ सदस्य होते हैं. इसमें एक अध्यक्ष, एक वर्तमान अथवा पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक वर्तमान अथवा भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार के क्षेत्र में जानकारी रखने वाले कोई दो सदस्य तथा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचितजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं.
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है. इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है.
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति की संस्तुति पर किया जाता हैं. इस समिति के अन्य सदस्य- लोक सभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, सदन में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उप-सभापति होते हैं. इस प्रक्रिया का वर्णन अधिनियम के धारा 4 में हैं.
अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल (Term of office of Chairperson and Members)
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 6 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल (Term of office of Chairperson and Members) का प्रावधान किया गया है. यह धारा उनके पद पर बने रहने की अवधि और पुनः नियुक्ति से संबंधित नियमों को निर्धारित करती है.
- अध्यक्ष का कार्यकाल: अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है. एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद, अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते.
- सदस्यों का कार्यकाल: सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है. सदस्य भी पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, बशर्ते कि उनकी आयु सत्तर वर्ष से अधिक न हो.
नोट: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पहले 5 वर्ष का था. हालाँकि, 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके बाद कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया. कार्यकाल की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष ही है, और यह पहले की तरह ही लागू है. इसलिए, वर्तमान में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है, और वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र भी हैं.
कार्यवाहक अध्यक्ष
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 7 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष या सदस्य को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है. यह प्रावधान तब लागू होता है जब अध्यक्ष का पद किसी कारणवश खाली हो या वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो. इस तरह, धारा 7 यह सुनिश्चित करती है कि आयोग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और अध्यक्ष का पद खाली होने या उनके अनुपस्थित रहने पर भी कोई रुकावट न आए.
धारा 7 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- अध्यक्ष का पद खाली होने पर: यदि किसी भी कारण से अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं. यह नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक एक नया अध्यक्ष नियुक्त होकर पदभार ग्रहण नहीं कर लेता.
- अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाने पर: यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं. यह नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं कर देते.
अध्यक्ष और सदस्यों का निष्कासन
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 5 के अनुसार, अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है. यह निष्कासन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है.
- त्यागपत्र (Resignation): अध्यक्ष या कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे सकता है.
- निष्कासन (Removal): राष्ट्रपति किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं. हालांकि, ऐसा करने से पहले, राष्ट्रपति को यह मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजना होता है. सर्वोच्च न्यायालय मामले की पूरी जाँच करता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति अपना अंतिम निर्णय लेते हैं.
राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को हटाने के पाँच प्रमुख आधार इस प्रकार हैं:
- यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो.
- यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों के अलावा, किसी अन्य वेतनभोगी रोजगार में संलग्न हो.
- यदि वह मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो गया हो.
- यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो.
- यदि उसे किसी आपराधिक अपराध का दोषी ठहराया गया हो और उसे जेल की सजा मिली हो, और राष्ट्रपति की राय में उस अपराध में नैतिक अधमता (moral turpitude) शामिल हो.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन हैं, जिन्होंने दिसंबर 2024 में पदभार ग्रहण किया था. वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के शक्तियां व कार्य
लोक संहिता प्रक्रिया, 1908 (code of civil procedure, 1908) के अधीन आयोग को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं. आयोग अपने समक्ष प्रस्तुत किसी पीड़ित अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किसी याचिका पर स्वयं सुनवाई एवं कार्यवाही कर सकता है. इसके अतिरिक्त आयोग न्यायालय की स्वीकृति से न्यायालय के समक्ष लम्बित मानवाधिकारों के प्रति हिंसा सम्बन्धी किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है.
आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्वसूचित करके किसी भी कारागार का निरीक्षण कर सके अथवा परिस्थितियों के अनुसार अन्य नौकरशाहों को कारागारों के निरीक्षण सम्बन्धी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन (delegate) कर दे. आयोग द्वारा मानवाधिकारों से सम्बन्धित संधियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने सम्बन्धी आवश्यक संस्तुतियां भी की जाती हैं.
कार्य
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कार्यों की सूची में कुछ और महत्वपूर्ण कार्य जोड़े जा सकते हैं:
- NHRC को मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, बशर्ते उसे संबंधित न्यायालय की अनुमति मिल जाए.
- NHRC जेलों, अस्पतालों या किसी भी अन्य संस्था का दौरा कर सकता है, जहां लोग उपचार, सुधार या संरक्षण के उद्देश्य से रखे गए हों. इसका मकसद वहां की जीवन स्थितियों का अध्ययन करना और सुधार के लिए सिफारिशें करना है.
- आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है और उसे प्रोत्साहित करता है.
- आयोग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करता है और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है.
- आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है.
- आयोग केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच ही नहीं करता, बल्कि यह ऐसे मामलों को रोकने के लिए भी कार्य करता है.
- आयोग मानवाधिकारों के प्रचार और सुरक्षा के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य कर सकता है, जो उसे उचित लगें.
शिकायत करने की प्रक्रिया
आयोग में शिकायत दर्ज कराना अत्यंत सरल कार्य है. शिकायत निःशुल्क दर्ज की जाती है. आयोग द्वारा फैक्स और तार (telegraphic) द्वारा प्राप्त शिकायतें भी स्वीकार की जाती हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रतिवर्ष देश में मानवाधिकारों की स्थिति से सम्बन्धित एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है. इसके द्वारा इस रिपोर्ट को विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है. जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा ऐसा प्रतिवेदन सम्बद्ध राज्य की विधान सभा के सम्मुख रखा जाता है.
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के अंतर्गत, मानव अधिकारों के उल्लंघन अपराध सम्बन्धी विवादो के त्वरित निपटान हेतु मानव अधिकार न्यायालय का गठन किया जा सकता है. न्यायालय में विवादों को सुलझाने हेतु सरकार अधिसूचना के माध्यम से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी जिसने 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में वकालत की हो.
सशस्त्र बालों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतों के मामलों में आयोग स्वयं अपने संज्ञान पर अथवा किसी प्राप्त याचिका के आधार पर सरकार से मामले के सम्बन्ध में रिपोर्ट मांग सकता है. रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् सरकार की सिफारिशौं के अनुरूप आयोग शिकायत पर कार्यवाही को रोक सकता है. संघीय सरकार द्वारा उक्त मामले के संदर्भ में की गई कार्यवाही से आयोग को तीन माह अथवा आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अवगत कराना अनिवार्य है.
शिकायतों की प्रकृति
साधारणतः, आयोग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली मानवाधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी याचिकाओं की प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए-
- घटना शिकायत करने से एक वर्ष से अधिक समय पूर्व घटित होनी चाहिए;
- शिकायत अर्द्ध-न्यायिक प्रकार की होनी चाहिए;
- शिकायत अनिश्चित, अज्ञात अथवा छंद्म नाम से होनी चाहिए;
- शिकायत तुच्छ प्रकृति की नहीं होनी चाहिए;
- आयोग के विस्तार से बाहर की शिकायतें नहीं होनी चाहिए, तथा;
- उपभोक्ता सेवाओं एवं प्रशासनिक नियुक्तियों से सम्बन्धित मामले.
इसे भी पढ़ें – मानव अधिकार का अर्थ, इतिहास, वर्गीकरण, महत्व, चुनौती और भारत
आयोग की समीक्षा (पक्ष व विपक्ष में तर्क)
आयोग ने निःसंदेह अपने खाते में कुछ उपलब्धियां दर्ज की हैं. यह केंद्र सरकार को यातना एवं क्रूर, अमानवीय एवं निम्न दण्ड या व्यवहार के अन्य स्वरूपों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर के लिए मनाने में सफल हुआ. इस संरक्षा ने मृत्यु की समस्या को बेहतरीन तरीके से उजागर किया. इसने शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में मानवाधिकारों पर विशिष्टिकृत प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने में भी मदद की है.
हालांकि यह माना जाता रहा है कि आयोग अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया है. वर्ष 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने अधिकार संस्थानों के लिए एक व्यापक जनादेश निर्धारित किया, जिसमें यह अपेक्षित किया गया कि उनमें बहुलता, प्रतिनिधित्वकारी संगठन, व्यापक पहुँच और प्रभाविकता, स्वतंत्रता, पर्याप्त संसाधन तथा जाँच की पर्याप्त शक्ति शामिल होनी चाहिए.
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2(d) मानव अधिकारों को संविधान द्वारा प्रत्याभूत, जीवन समानता एवं वैयक्तिक गरिमा से सम्बद्ध अधिकार के तौर पर परिभाषित करता है या वे अंतरराष्ट्रीय अभिसमय या संविदा में उल्लिखित होते हैं. इसे भारत में न्यायालय द्वारा लागू कराए जाते हैं.
इस प्रकार यह कानून एनएचआरसी से सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर ध्यान लगाने की बजाय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर फोकस करने की अपेक्षा करता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है की मानव अधिकार आयोग सरकार पर नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराने के लिए दबाव डालने की प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाता.
आयोग की संरचना के संबंध में तीन आपतियां हैं. पहली, कानून ने चयन को संकीर्ण कर दिया है कि व्यक्ति को, केवल न्यायपालिका से सम्बद्ध होना चाहिए, मानवाधिकारों में किसी प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है. यह आयोग की परिप्रेक्ष्यों की बहुलता, विशेष रुझान एवं सभ्य समाज से विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करने से रोकता है.
दूसरा, अनुशंसा देने वाली समिति में राजनेता होते हैं. तीसरे, चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. आयोग की संरचना आमतौर पर गोपनीय फाइलों में टिप्पणी करने या राजनेताओं और उनके पसंदीदा नौकरशाहों के बीच बंद दरवाजों के पीछे चल रही बैठकों के दौरान निर्णित होती है.
अधिनियम की धारा-11 के अनुसार, केंद्र सरकार आयोग को अनुसंधान, जांच, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य के लिए अधिकारी एवं अन्य स्टाफ मुहैया कराएगी. कानून के इस प्रावधान से आयोग अपने कार्य की जरूरत के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है.
आयोग में कार्य करने वाले अधिकतर अधिकारी एवं स्टाफ भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों से आते हैं. सरकारी कार्यालयों में काफी समय तक कार्य करने के बाद वे आयोग में आते हैं, जिससे उनकी एक निश्चित सोच, बदलावों के प्रति बेहद प्रतिरोध, कार्य की नौकरशाही पद्धति और अन्य समान/सदृश आदतों का एक भारी-भरकम बैकलॉग होता है. अक्सर, उन्हें मानव अधिकार दर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और न ही वे इसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं.
आयोग को एक निश्चित मात्रा में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं. हालांकि, अध्ययन प्रकट करता है कि अधिकतर शिकायतें तीन या चार राज्यों से ही प्राप्त होती हैं. अधिकारों के प्रति जागरूकता, मात्र कुछ राज्यों तक सीमित होने से सभी मामले सूचित नहीं होती. लगभग आधे मामलों को प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया जाता है. ये मामले वे होते हैं जो आयोग के चार्टर में नहीं आते या समयबद्ध होते हैं या अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति के होते हैं. इस तरह लोगों में आयोग के चार्टर के बारे में बेहद अज्ञानता होती है.
आयोग में प्रत्येक वर्ष लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है. आयोग को इसके कार्यों में पूरी तरह स्वतंत्र समझ जाता है, यद्यपि अधिनियम ऐसा उल्लेख नहीं करता. वास्तव में, अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो आयोग की सरकार पर निर्भरता को कम करते हैं. लेकिन आयोग अपने मानव संसाधन सम्बन्धी जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर है. तब बेहद महत्वपूर्ण बात वित्त की है.
अधिनियम की धारा-32 के तहत् केंद्र सरकार, आयोग की अनुदान के तौर पर इतना धन देगी, जितना वह उपयुक्त समझे. इस प्रकार, मानव शक्ति एवं धन संबंधी जरूरतों, जो अत्यधिक महत्व के हैं, के परिप्रेक्ष्य में आयोग स्वतंत्र नहीं है.
सशस्त्र बालों के कर्मियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की शिकायत की जांच करने का अधिकार अधिनियम द्वारा आयोग की नहीं दिया गया है. क्योंकि मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की बड़ी तादाद सशस्त्र बलों के कर्मियों के खिलाफ होती हैं, स्वाभाविक रूप से इन मामलों में लोगों की शिकायतों के एनएचआरसी द्वारा निपटान में अधिनियम इसे कमजोर बना देता है.
आयोग को अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं है. अधिनियम की धारा-18 के अनुसार, आयोग द्वारा हुई जांच में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले स्पष्ट होने पर, आयोग केवल दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने और पीड़ित को रहत देने की सरकार को सलाह दे सकता है. यदि कोई सरकार सलाह मानने से इंकार कर देती है तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आयोग को इसकी सलाह को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य करने को सशक्त करता हो.
राज्य मानवाधिकार आयोग
राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission – SHRC) की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई हैं. इसका उद्देश्य राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच संभव करना हैं. यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की तरह ही कार्य करता है. लेकिन इसका क्षेत्राधिकार केवल संबंधित राज्य तक सीमित होता है.
गठन
अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारें एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती हैं. आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं.
अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है. वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं. अध्यक्ष या सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है.
राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना
मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो इसे अधिक प्रभावी बनाते हैं. आयोग में अब एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं.
अध्यक्ष (Chairperson): आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है.यह प्रावधान 2019 के संशोधन से आया है, जिसने अध्यक्ष पद के लिए योग्यता का विस्तार किया है. पहले, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बन सकते थे.
सदस्य (Members): आयोग में दो सदस्य होते हैं, जिनकी योग्यता इस प्रकार है:
- एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए, जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो.
- दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो.
नियुक्ति समिति (Appointment Committee)
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है. इस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है. समिति की संरचना इस प्रकार है:
- अध्यक्ष: मुख्यमंत्री
- इसके 3 सदस्य इस प्रकार होते हैं:
- राज्य के गृह मंत्री
- राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता
- राज्य विधानसभा के अध्यक्ष
यदि किसी राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) है, तो निम्नलिखित दो व्यक्ति भी समिति के सदस्य होते हैं:
- विधान परिषद के अध्यक्ष
- विधान परिषद में विपक्ष के नेता
कार्य और शक्तियाँ
राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समान ही हैं. ये निम्नलिखित हैं:
- आयोग स्वयं या किसी याचिका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है.
- यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े किसी भी न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है.
- आयोग राज्य की जेलों और अन्य निरोध स्थलों में कैदियों की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए दौरा कर सकता है.
- यह मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है, जागरूकता फैलाता है और मानवाधिकार साक्षरता को प्रोत्साहित करता है.
- यह मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों का अध्ययन करता है और उनके कार्यान्वयन पर सिफारिशें देता है.
- मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच के बाद, आयोग संबंधित सरकार को मुआवजा, कानूनी कार्यवाही शुरू करने या अन्य सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिशें कर सकता है.
- आयोग की सिफारिशें अनिवार्य रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं. लेकिन सरकार को आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एक महीने के भीतर देनी होती है.
राज्य मानवाधिकार आयोगों की सूची
कृपया ध्यान दें: मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों का पद बदलता रहता है. नीचे दी गई ‘वर्तमान अध्यक्ष‘ की जानकारी समय-समय पर बदल सकती है. सबसे सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखना उचित होगा.
| क्र. सं. | राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) | गठन की तिथि | मुख्यालय शहर | प्रथम अध्यक्ष | वर्तमान/कार्यवाहक अध्यक्ष |
| 1. | आंध्र प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग | 2000 (अविभाजित) | अमरावती (वर्तमान) | न्यायमूर्ति बी सुब्बू रेड्डी | न्यायमूर्ति मन्नव भास्कर राव |
| 2. | असम राज्य मानवाधिकार आयोग | 1996 | गुवाहाटी | न्यायमूर्ति एस.एन. फूकन | न्यायमूर्ति सुब्रता रॉय |
| 3. | बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग | 3 जनवरी 2000 | पटना | न्यायमूर्ति एस.एन. झा | न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा (पूर्व) (पद रिक्त) |
| 4. | छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग | 2001 | रायपुर | न्यायमूर्ति सी.बी. बासु | न्यायमूर्ति गिरिजा शंकर बाजपेयी |
| 5. | गोवा राज्य मानवाधिकार आयोग | 2011 | पणजी | न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा | न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां (कार्यवाहक) |
| 6. | गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग | 2006 | गांधीनगर | न्यायमूर्ति एस.एन. झा | न्यायमूर्ति पी.बी. देसाई |
| 7. | हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग | 2012 | चंडीगढ़ | न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन | न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल |
| 8. | हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग | 2005 | शिमला | न्यायमूर्ति ए.के. श्रीवास्तव | न्यायमूर्ति पी.एस. राणा |
| 9. | जम्मू और कश्मीर मानवाधिकार आयोग | 1997 | श्रीनगर/जम्मू | न्यायमूर्ति आर.पी. सेठी | आयोग निष्क्रिय (केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद) |
| 10. | झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग | 2001 | रांची | न्यायमूर्ति आर.के. देब | न्यायमूर्ति संतोष कुमार सतपथी |
| 11. | कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग | 2005 | बेंगलुरु | न्यायमूर्ति एस.आर. नायक | न्यायमूर्ति विश्वनाथ शेट्टी |
| 12. | केरल राज्य मानवाधिकार आयोग | 1998 | तिरुवनंतपुरम | न्यायमूर्ति एम.एम. परीड पिल्लै | न्यायमूर्ति एंटनी डोमिनिक |
| 13. | मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग | 1995 | भोपाल | न्यायमूर्ति आर.एन. दत्त | न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन |
| 14. | महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग | 2001 | मुंबई | न्यायमूर्ति अरविंद सावंत | न्यायमूर्ति के.एस. झावेरी |
| 15. | मणिपुर राज्य मानवाधिकार आयोग | 1999 | इम्फाल | न्यायमूर्ति आर.के. पटनायक | न्यायमूर्ति पी.पी. गुप्ता |
| 16. | ओडिशा राज्य मानवाधिकार आयोग | 2000 | भुवनेश्वर | न्यायमूर्ति डी.पी. मोहपात्रा | न्यायमूर्ति बिजॉय कृष्ण पाटी |
| 17. | पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग | 1997 | चंडीगढ़ | न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद | न्यायमूर्ति आनंद मोहन बसु |
| 18. | राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग | 18 जनवरी 1999 | जयपुर | न्यायमूर्ति कांता भटनागर | न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास |
| 19. | तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग | 1997 | चेन्नई | न्यायमूर्ति आर.के. पटनायक | न्यायमूर्ति जयचंद्रन |
| 20. | तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग | 2019 | हैदराबाद | न्यायमूर्ति चंद्रैया | न्यायमूर्ति जी. चंद्रैया |
| 21. | उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग | 7 अक्टूबर 2002 | लखनऊ | न्यायमूर्ति ए.एस. गोयल | न्यायमूर्ति बी.के. नारायण |
| 22. | उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग | 2005 | देहरादून | न्यायमूर्ति एस.सी. ढींगरा | न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट |
| 23. | पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग | 1995 | कोलकाता | न्यायमूर्ति एस.के. मुखर्जी | न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य |
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:
- वर्तमान में भारत के लगभग 26 राज्यों में मानवाधिकार आयोग सक्रिय हैं.
- दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार से संबंधित मामलों की देखरेख राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा ही की जाती है.
- कुछ राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में अभी तक अपने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है. इन राज्यों के मामले भी NHRC द्वारा ही देखे जाते हैं.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) पर 5 FAQs
1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) की संरचना में क्या अंतर है?
NHRC की संरचना में एक अध्यक्ष और चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं. अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे व्यक्ति होते हैं, जबकि सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं.
वहीं, SHRC में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं. SHRC के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं. दोनों आयोगों में मानवाधिकारों के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले एक सदस्य का होना अनिवार्य है. ये अंतर आयोगों के पदानुक्रम और अधिकार क्षेत्र को दर्शाते हैं.
2. आयोगों की शक्तियों और सीमाओं का संक्षेप में वर्णन करें.
दोनों मानवाधिकार आयोगों के पास दीवानी न्यायालयों की शक्तियाँ होती हैं, जो उन्हें गवाहों को बुलाने, शपथ पर साक्ष्य लेने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अधिकार देती हैं. हालाँकि, उनकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वे किसी दोषी को सीधे दंडित नहीं कर सकते.
आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सरकारों को मुआवजा या अन्य सुधारात्मक उपायों की सिफारिश कर सकते हैं. यह सीमा उनकी प्रभावशीलता को कम करती है, क्योंकि सरकारें अक्सर उनकी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती हैं.
3. NHRC और SHRC की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है?
आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है. NHRC के मामले में, समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि SHRC के मामले में मुख्यमंत्री होता है.
इसके अतिरिक्त, उन्हें केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर और सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है. उनके वेतन और सेवा की शर्तें सरकार के नियंत्रण में नहीं होतीं, बल्कि उन्हें अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है, जिससे उनकी स्वायत्तता बनी रहती है.
4. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आयोगों को कैसे प्रभावित किया है?
2019 के संशोधन ने आयोगों की संरचना और कार्यकाल में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. NHRC और SHRC दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है. इसके अलावा, NHRC के अध्यक्ष के लिए योग्यता का दायरा बढ़ाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है, जबकि पहले केवल मुख्य न्यायाधीश ही योग्य थे. SHRC के अध्यक्ष के लिए भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को योग्य बनाया गया है.
5. आयोगों द्वारा किन मामलों की जाँच नहीं की जा सकती है?
आयोगों की जाँच का दायरा कुछ सीमाओं के अधीन है. वे उन शिकायतों की जाँच नहीं कर सकते जो घटना की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुरानी हों. इसके अतिरिक्त, सशस्त्र बलों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में आयोग की शक्तियाँ सीमित होती हैं. ऐसे मामलों में, आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, लेकिन वह सीधे तौर पर इसकी जाँच नहीं कर सकता. यह प्रावधान आयोगों की जाँच के दायरे को एक निश्चित समय सीमा और क्षेत्राधिकार तक सीमित करता है.