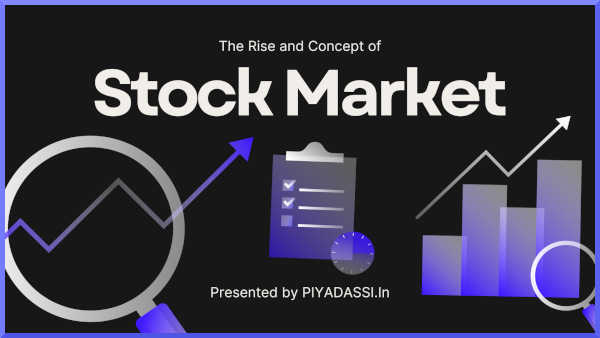भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई, जब 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ. इसका उद्देश्य किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाना था. यह आंदोलन यूरोपीय मॉडल, विशेष रूप से जर्मनी के रायफाइज़न मॉडल से प्रेरित था.
वैश्विक सहकारी आंदोलन की नींव 1844 में रोशडेल पायनियर्स ने लंकाशायर, इंग्लैंड में रखी. यह सस्ते और गुणवत्तापूर्ण सामान प्रदान करने के लिए शुरू हुआ था. इस मॉडल में अधिशेष समुदाय को लौटाया जाता था. इसी आधार पर भारत में सर फ्रेडरिक निकोल्सन की 1890 के दशक की रिपोर्ट ने सहकारी समितियों की स्थापना को गति दी. इसके बाद यह आंदोलन विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में फैल गया.
सहकारिता क्या हैं? (What is Co-Operation in Hindi)
सहकारिता का अर्थ है- साथ-साथ मिलकर कार्य करना. यानी अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना, सहकारिता है. इसे एक स्वैच्छिक संघ भी कहा जाता है जो लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित और संयुक्त स्वामित्व वाले उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है.
यह दो शब्दों से बना है – “सह” (साथ) और “कारिता” (कार्य). इसका अर्थ है एक साथ काम करना या सहयोग करना. सहकारिता में, सदस्य स्वेच्छा से एक साथ आते हैं और किसी साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं. इसके सदस्य संगठन के मालिक होते हैं और उसके कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं. इसका उद्देश्य सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है. सहकारी समितियाँ स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपने सदस्यों की मदद करती हैं.
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (International Cooperative Alliance- ICA), सहकारिता (Cooperative) को “संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के स्वायत्त संघ” के रूप में परिभाषित करता है.
भारत में सहकारिता आंदोलन (Co-Operative Movement in India)
भारत का सहकारिता आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पहल है. इस आंदोलन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है.
सहकारिता आंदोलन की जड़ें 19वीं शताब्दी के अंत में हैं, जब कृषि क्षेत्र में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ. औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उद्योगों को प्रभावित किया, जिससे लोग कृषि पर निर्भर हो गए. इस दौरान, भूमि का असमान वितरण, अनिश्चित वर्षा, और साहूकारों से उच्च ब्याज दर वाले ऋणों ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया.
इससे पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक सहकारी प्रथाएं मौजूद थीं, जैसे देवराय, वनराय, चिट फंड, कुरी, भीषी, और फड़, जो संसाधनों को साझा करने और आर्थिक समस्याओं का सामूहिक समाधान करने के लिए थीं. 1901 के अकाल आयोग की रिपोर्ट के बाद, 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसने औपचारिक सहकारी समितियों की नींव रखी.
विकास (Development)
सहकारिता आंदोलन का विकास दो चरणों में हुआ: औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद.
A. औपनिवेशिक काल (1904-1947):
1904 के अधिनियम के तहत शुरुआत में केवल ऋण संबंधी सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया. 1911 तक, 5,300 से अधिक समितियां और 3 लाख से अधिक सदस्य थे.
1912 में सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे गैर-ऋण सहकारी समितियों (जैसे विपणन और उपभोक्ता सहकारी) को बढ़ावा मिला. मैकलैगन समिति (1914) ने तीन-स्तरीय संरचना (प्राथमिक, केंद्रीय, प्रांतीय बैंक) की सिफारिश की.
1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया, जिससे राज्यों ने अपने अधिनियम बनाने शुरू किए. 1925 में बंबई सहकारी अधिनियम ने “एक सदस्य, एक वोट” की अवधारणा पेश की.
1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना और 1937 में मेहता समिति ने बहुउद्देशीय समितियों की सिफारिश की. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कृषि की बढ़ती कीमतों ने गैर-ऋण सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया.
B. स्वतंत्रता के बाद (1947 से अब तक):
स्वतंत्रता के बाद, सहकारिता को मिश्रित अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया गया, जिसमें सार्वजनिक, निजी, और सहकारी क्षेत्र शामिल थे. पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में सहकारी बैंकों और समितियों को ग्रामीण विकास का आधार माना गया.
1962 में कृषि पुनर्वित्त निगम, 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), और 1981 में NABARD की स्थापना हुई. 1967 में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई.
2002 में राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की गई, जो स्वायत्त और आत्मनिर्भर सहकारी समितियों को बढ़ावा देती है. हाल के वर्षों में, 2021 में केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने इस आंदोलन को और मजबूत किया.
आज, भारत में लगभग 6 लाख सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जिनमें 10 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं, और ये कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास, और विपणन जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं.
कानूनी प्रावधान (Legal Provisions)
सहकारिता आंदोलन की कानूनी रूपरेखा समय के साथ विकसित हुई है, जिसमें संवैधानिक और विधायी प्रावधान शामिल हैं:
A. संवैधानिक प्रावधान:
- 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने भाग IXB जोड़ा, जिसमें सहकारी समितियों के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं.
- अनुच्छेद 19(1)(c) में “सहकारी” को “असोसिएशन और यूनियन” के अंतर्गत शामिल किया गया, जिससे इसे मौलिक अधिकार का दर्जा मिला.
- अनुच्छेद 43B के तहत राज्य को सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया.
B. महत्वपूर्ण अधिनियम और नीतियां:
- 1904: सहकारी ऋण समिति अधिनियम (पहला कानूनी ढांचा, ऋण पर केंद्रित).
- 1912: सहकारी समिति अधिनियम (गैर-ऋण गतिविधियों और फेडरेशनों को शामिल).
- 1942: बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम (बहु-राज्य समितियों के लिए).
- 1984: बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (1984, 1942 अधिनियम को बदलते हुए).
- 2002: राष्ट्रीय सहकारी नीति, कंपनियां (संशोधन) अधिनियम, और NCDC संशोधन अधिनियम.
- 2021: केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, जो सहकारी समितियों के लिए “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देती है.
- राज्य-विशिष्ट कानून: कई राज्यों ने स्वायत्त सहकारी समितियों के लिए समानांतर कानून बनाए, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना (1995), मध्य प्रदेश (1999), और बिहार (1996).
स्तर (Levels)
सहकारिता आंदोलन को तीन-स्तरीय संरचना में संगठित किया गया है, जैसा कि मैकलैगन समिति (1914) ने सिफारिश की थी:
- प्राथमिक स्तर: गांवों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), डेयरी सहकारी, और उपभोक्ता सहकारी समितियां.
- जिला स्तर: जिला सहकारी बैंक, विपणन समितियां, और अन्य क्षेत्रीय संगठन.
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर: राज्य सहकारी बैंक, NAFED, IFFCO, KRIBHCO, और NCDC जैसे संगठन, जो राष्ट्रीय नीतियों को लागू करते हैं.
गुण और दोष (Merits and Demerits)
गुण (Merits)
- आर्थिक सशक्तिकरण: सहकारी समितियों ने किसानों, मजदूरों, और छोटे उद्यमियों को सस्ते ऋण और बाजार तक पहुंच प्रदान की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ.
- ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास, और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया.
- सामाजिक एकता: विभिन्न जातियों, समुदायों, और वर्गों को एक मंच पर लाकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया.
- लोकतांत्रिक प्रबंधन: सहकारी समितियां सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती हैं.
- सफल मॉडल: AMUL, IFFCO, और NAFED जैसे संगठनों ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया.
दोष (Demerits)
- राजनीतिक हस्तक्षेप: कई सहकारी समितियों में राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार की समस्या रही है, जो उनकी स्वायत्तता को सीमित करती है.
- प्रबंधकीय कमियां: प्रशिक्षित कर्मचारियों और पेशेवर प्रबंधन की कमी ने उनकी दक्षता को प्रभावित किया है.
- वित्तीय अस्थिरता: कुछ समितियां कुप्रबंधन और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) से जूझ रही हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता प्रभावित हुई है.
- सीमित दायरा: सहकारिता का लाभ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, और शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम है.
- जागरूकता की कमी: कई क्षेत्रों में लोगों को सहकारी समितियों के लाभों की जानकारी नहीं है, जिससे उनकी भागीदारी कम हुई है.
- अन्य चुनौतियां: अशिक्षा, जाति संघर्ष, गरीबी, और पारंपरिक खेती के तरीके भी बाधाएं रहे हैं.
महत्वपूर्ण संस्थाएं और योगदान
कुछ प्रमुख सहकारी संस्थाओं में शामिल हैं:
- NAFED: विपणन सहकारी का शीर्ष संगठन.
- IFFCO और KRIBHCO: किसान सेवाओं में उत्कृष्टता.
- AMUL और Sudha: डेयरी क्षेत्र में वैश्विक पहचान.
- NCDC: राष्ट्रीय स्तर पर विकास को बढ़ावा देना.
भारत में वर्तमान स्थिति
सहकारिता आंदोलन भारत में ग्रामीण और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. 2025 में, 8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, बैंकिंग, और आवास में सक्रिय हैं. सरकार ने PACS के लिए मॉडल विनियम अपनाए हैं, जिससे उन्हें 25 से अधिक गतिविधियाँ करने की अनुमति मिली है.
63,000 PACS को ₹2,516 करोड़ के बजट के साथ कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिसमें से 62,318 PACS 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल हैं, और 15,783 पहले से ही ऑनबोर्ड हैं. इसके अलावा, 9,000 से अधिक नए PACS/दुग्ध/मत्स्य पालन सहकारी समितियाँ अनावृत पंचायतों में स्थापित की गई हैं.
अंतरराष्ट्रीय पहल
भारत ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में ICA वैश्विक सम्मेलन के दौरान UN अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष (IYC) 2025 का आधिकारिक शुभारंभ किया. यह आयोजन भारत की सहकारी नवाचार की दीर्घकालिक विरासत और समान, टिकाऊ विकास में इसके योगदान को उजागर करता है.
IYC 2025 सहकारिता की परिवर्तनशील शक्ति को बढ़ावा देने, नीतियों को मजबूत करने, और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारियाँ बनाने का लक्ष्य रखता है.
अंत में,
भारत का सहकारिता आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का एक मजबूत स्तंभ रहा है. इसने लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास को बढ़ावा दिया है. हालांकि, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रबंधकीय कमियां, और आधुनिकीकरण की आवश्यकता इसके सामने चुनौतियां हैं. हाल ही में, 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना इस आंदोलन को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.