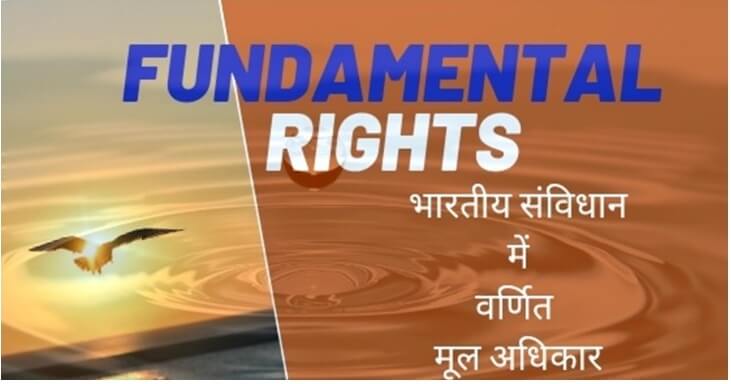यह लेख भारत में वामपंथी उग्रवाद के उद्भव, कारणों, विभिन्न चरणों, लक्ष्यों व उद्देश्यों, प्रभावित क्षेत्रों, सांगठनिक ढांचे, आंतरिक सुरक्षा से संबंध, सरकारी प्रयासों व योजनाओं, तथा वर्तमान स्थिति का तथ्यात्मक रूप से वर्णन करती है. लेख में केवल प्रामाणिक या सरकारी स्त्रोतों से प्राप्त अनंतिम तथ्यों व आंकड़ों को समाहित किया गया है.
वामपंथी उग्रवाद (Leftist Extremism in Hindi) क्या है?
वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism – LWE) उन समूहों और विचारधाराओं को संदर्भित करता है जो हिंसक क्रांति के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते हैं. ये समूह लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के विरोधी होते हैं और उन्हें नष्ट करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं. भारत में इसे मुख्य रूप से ‘नक्सलवाद’ या ‘माओवाद’ के नाम से जाना जाता है.
वामपंथी उग्रवाद की जड़ें माओत्से तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद में निहित हैं. इसे माओवाद कहते हैं. माओवाद सशस्त्र संघर्ष और किसानों व आदिवासियों की लामबंदी (mobilization) में विश्वास रखता है. इसका लक्ष्य “दीर्घकालिक जनयुद्ध” (Protracted People’s War) के माध्यम से एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है.
वामपंथी उग्रवाद (LWE) भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है. सशस्त्र विरोध का कारण सामाजिक-आर्थिक असमानता है. इससे देश के कुछ सबसे दूरस्थ, अविकसित और आदिवासी-बहुल क्षेत्रों को प्रभावित रहे है. यह आंदोलन सशस्त्र विद्रोह और समानांतर शासन संरचनाओं के माध्यम से भारतीय राज्य को कमजोर करने का लक्ष्य रखता है. यह विशेष रूप से सुरक्षा बलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाता है.
भारत सरकार ने इस समस्या की गंभीरता को पहचानते हुए, 19 अक्टूबर, 2006 को गृह मंत्रालय में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग का सृजन किया. यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को एक गंभीर और समग्र आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में वर्गीकृत किया है.
वामपंथी उग्रवाद का उद्भव और विकास
भारत में वामपंथी उग्रवाद का इतिहास 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव में हुए आदिवासी-किसान विद्रोह से जुड़ा है. यह आंदोलन जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में शुरू हुआ था. इस उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर ही ‘नक्सलवाद’ कहा गया. विद्रोह का नेतृत्व चारु मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी जैसे नेताओं ने किया था. इन्होंने स्थानीय असंतोष को एक व्यापक वैचारिक आंदोलन में बदलने का प्रयास किया.
प्रारंभिक चरण में, यह उग्रवादी आंदोलन पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गया और विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में अन्य समूहों द्वारा आगे बढ़ाया गया. 1969 में, माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (CPI-ML) की स्थापना हुई. सीपीआई (एमएल) ने संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खारिज कर दिया और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक क्रांति को बढ़ावा दिया.
यह स्वतंत्रता के बाद भारत में सशस्त्र किसान विद्रोह का पहला प्रमुख उदाहरण है. हालांकि, 1971 में, सत्यनारायण सिंह ने नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया. इस कारण से सीपीआई-एमएल दो भागों में विभाजित हो गई. चारु मजूमदार की मृत्यु (1972) के बाद पार्टी में विश्वसनीय नेतृत्व की कमी हो गई और यह कई गुटों में खंडित हो गई. इससे 1974 में सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के रूप में पुनर्गठित किया गया.
1980 के दशक में, नक्सलवाद का पुनरुत्थान अधिक हिंसक रूप में हुआ. इस चरण में, आंदोलन ने पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक अपना प्रभाव बढ़ाया, जिसमें एक दीर्घकालिक युद्ध की रणनीति का पालन किया गया 9. यह पुनरुत्थान बिखरे हुए गुटों के लिए एक नए सिरे से संगठित होने और अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने का अवसर बन गया.
वर्ष 2004 में दो प्रमुख नक्सली समूह – पीपल्स वार (पी.डब्ल्यू.) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एम.सी.सी.आई.) – ने विलय करके सीपीआई (माओवादी) पार्टी बनाई. पीपल्स वार आंध्र प्रदेश में सक्रिय था और एम.सी.सी.आई. बिहार और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय था. यह विलय एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था. इससे आंदोलन की बिखरी हुई शक्तियां एकजुट हुई. एकजुट संगठन समन्वित तथा प्रभावी प्रतिरोध में सक्षम हुआ.
वर्ष 2008 तक अधिकांश अन्य नक्सली समूहों का विलय भी सीपीआई (माओवादी) में हो गया. इस प्रकार यह भारत में सबसे प्रमुख और हिंसक वामपंथी उग्रवादी संगठन बन गया. इस तरह यह संगठन आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया. सीपीआई (माओवादी) और इसके सभी प्रमुख संगठनों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है.
वामपंथी उग्रवाद के मूल कारण
वामपंथी उग्रवाद के उद्भव के कई गहरे सामाजिक-आर्थिक और शासन संबंधी कारण हैं. व्यापक गरीबी और आय असमानता ने असंतोष और अशांति को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है. ऐसे लोग जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं होता, वे नक्सलवादी विचारों से जल्दी प्रभावित होते हैं. नक्सलवाद उच्च गरीबी दर वाले अविकसित क्षेत्रों में पनपता है.
ऐतिहासिक भूमि अलगाव ने हाशिए पर पड़े समुदायों में असंतोष को बढ़ाया है. आदिवासी और जनजातीय आबादी के लिए भूमि अधिकारों की कमी भी इसका एक कारण है. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जैसे कानूनों ने आदिवासियों को वनोपज के संग्रह से भी वंचित किया. वे अपने जीवन यापन के लिए इसी पर निर्भर थे. खनन और विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया गया है. इस कारण उनमें आक्रोश और अन्याय की भावना उत्पन्न हुई है. जनजातीय समुदाय विशेष रूप से जमींदारों, साहूकारों और खनन कंपनियों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं. नक्सली इन विवादों का फायदा स्वयं को हाशिए पर पड़े लोगों के संरक्षक के रूप में पेश करने के लिए करते हैं.
निम्न जीवन-स्तर, विकास का अभाव और बुनियादी सेवाओं की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है. स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी ने आदिवासियों, दलितों अन्य पिछड़े समूहों में आक्रोश बढ़ाया है.
लेकिन, वामपंथी उग्रवाद के मूल कारण केवल सामाजिक-आर्थिक अभाव नहीं हैं. यह उग्रवादी समूहों द्वारा जानबूझकर विकास को बाधित करने और शासन में रिक्तता पैदा करने की एक रणनीति भी है. नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं. वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं. माओवादी जानबूझकर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल मार्गों, पुलों, स्वास्थ्य अवसंरचना और संचार सुविधाओं को निशाना बनाते हैं, जिससे विकास की प्रक्रिया दशकों पीछे धकेल दी जाती है.
यह एक “स्व-पूर्ति भविष्यवाणी” है जहां शासन की अनुपस्थिति उनके नियंत्रण को मजबूत करती है. यह रणनीति दर्शाती है कि वामपंथी उग्रवाद का उद्देश्य केवल “अधिकारों के लिए लड़ना” नहीं है, बल्कि एक समानांतर व्यवस्था स्थापित करना है. वे लोगों को मुख्यधारा से कटे हुए रखना चाहते हैं ताकि वे अपनी पुरानी विचारधारा को बनाए रख सकें.
इसके अतिरिक्त, खराब शासन और भ्रष्टाचार ने भी इस समस्या को बढ़ावा दिया है. प्रशासनिक उदासीनता, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और न्याय या बुनियादी अधिकारों को प्रदान करने में विफलता लोगों को नक्सली समूहों की ओर धकेलती है. ये त्वरित और वैकल्पिक शासन प्रणालियों का वादा करते हैं. नक्सली लोगों से वसूली करते हैं और समानांतर अदालतें भी लगाते हैं.
वामपंथी उग्रवाद के लक्ष्य और उद्देश्य
वामपंथी उग्रवादी संगठनों का प्राथमिक लक्ष्य हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना है. वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं. वे वर्तमान व्यवस्था को पूंजीवादी और सर्वहारा विरोधी मानते है.
सीपीआई (माओवादी) का उद्देश्य विद्यमान लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़ फेंकना तथा कथित ‘न्यू डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन’ में अपने आपको स्थापित करना है. वे अपने प्रमुख साधन के रूप में हिंसा तथा सहायक साधनों के रूप में प्रमुख संगठनों और रणनीतिक संयुक्त मोर्चों का सहायता लेते है.
‘न्यू डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन’ की अवधारणा माओवादी विचारधारा का एक केंद्रीय लक्ष्य है. इसके द्वारा वे मौजूदा सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखते हैं. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, माओवादी विद्रोह का सिद्धांत हिंसा को मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचों को शिकस्त देने के मुख्य साधन के रूप में महिमामंडित करता है.
वे अपने उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित मानते हैं. हिंसा को केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि एक “प्राथमिक साधन” के रूप में महिमामंडित किया जाता है. यह दर्शाता है कि हिंसा कोई आकस्मिक परिणाम नहीं है, बल्कि उनके मूल सिद्धांत का एक अभिन्न अंग है.
नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ‘क्रांतिकारी पीपल्स कमेटियां’ (RPC) स्थापित करते हैं. यह नागरिक प्रशासनिक मशीनरी के रूप में कार्य करती हैं. ये कमेटियां अत्यंत प्रारंभिक प्रशासनिक कार्य करती हैं और सशस्त्र इकाइयों को रसद सहायता भी प्रदान करती हैं. ‘जनताना सरकार’ और ‘क्रांतिकारी पीपल्स कमेटियां’ का गठन से ज्ञात होता है कि उनका लक्ष्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक, समानांतर राज्य स्थापित करना है.
वामपंथी उग्रवाद का लक्ष्य भारतीय लोकतांत्रिक राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है. वामपंथी उग्रवाद की समस्या का समाधान केवल गरीबी उन्मूलन से नहीं हो सकता. इसके लिए उनके वैचारिक जड़ों और राज्य को कमजोर करने के उनके रणनीतिक प्रयासों को भी संबोधित करना होगा.
वामपंथी उग्रवाद का सांगठनिक ढांचा
सीपीआई (माओवादी) का सांगठनिक ढांचा एक जटिल, बहु-स्तरीय प्रणाली है. यह केवल सशस्त्र संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक, खुफिया और नागरिक-प्रशासनिक विंग भी शामिल हैं. यह खासियत इसे भारतीय राज्य के खिलाफ एक व्यापक और दीर्घकालिक युद्ध छेड़ने में सक्षम बनाता है. सीपीआई (माओवादी) की पार्टी संरचना केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय समिति (CC), पोलित ब्यूरो (PB) और केंद्रीय सैन्य आयोग (CMC) से बनी है.
पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) सीपीआई (माओवादी) का सशस्त्र विंग है. इसका गठन मौजूदा सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक ढांचों को शिकस्त देने के लिए हिंसा को प्राथमिक साधन के रूप में महिमामंडित करने के उद्देश्य से किया गया है. पीएलजीए तीन बलों से बना है:
- मुख्य बल (Main Force): इसमें कंपनियां, प्लाटून, विशेष एक्शन टीमें (हत्या दस्ते) और खुफिया इकाइयां शामिल हैं.
- द्वितीयक बल (Secondary Force): इसमें विशेष गुरिल्ला स्क्वॉड, स्थानीय गुरिल्ला स्क्वॉड, प्लाटून और जिला/मंडल स्तरीय एक्शन टीम शामिल हैं.
- आधार बल (Base Force): इसमें पीपल्स मिलिशिया, ग्राम रक्षक दल, आत्म रक्षक दल और आत्मरक्षा स्क्वॉड शामिल हैं.
विद्रोह के प्रथम स्तर पर, पीएलजीए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेता है. यह मौजूदा शासन व्यवस्था के ढांचों के बुनियादी स्तर पर रिक्तता पैदा के उद्देश्य पर काम करता है. वे निम्न स्तर के सरकारी अधिकारियों, स्थानीय पुलिस थानों के पुलिस कार्मिकों, मुख्यधारा में शामिल राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं तथा पंचायतीराज प्रणाली के जनप्रतिनिधियों की हत्या करके इसे हासिल करते हैं.
अर्धशहरी तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को एकजुट करने के लिए दिखावटी लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से अनेक प्रमुख संगठनों का गठन किया गया है. इनमें से अधिकांश संगठनों का नेतृत्व ऐसे सुप्रशिक्षित बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है जिनका माओवादियों के विद्रोह के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास है.
ये संगठन की विचारधारा के हिंसक स्वरूप को छुपाने के लिए एक मुखौटा के रूप में कार्य करते हैं. इनके महत्वपूर्ण कार्यों में ‘पेशेवर क्रांतिकारियों’ की भर्ती, विद्रोह के लिए निधियां जुटाना, भूमिगत कैडरों के लिए शहरी क्षेत्रों में शरण स्थल बनाना, गिरफ्तार किए गए कैडरों को कानूनी सहायता प्रदान करना और प्रासंगिकता/सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर आंदोलन करके जन-समर्थन जुटाना शामिल है. ये प्रमुख संगठन माओवादी एजेंडा को आगे बढ़ाने और प्रवर्तन प्रणाली को कमजोर करने के लिए चतुराई से शासकीय ढांचों तथा विधिक प्रक्रियाओं का भी प्रयोग करते हैं.
सीपीआई (माओवादी) का एक खुफिया तंत्र भी है जिसे पीपल्स सिक्योरिटी सर्विस (PSS) के नाम से जाना जाता है. इसके अतिरिक्त, माओवादी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ‘क्रांतिकारी पीपल्स कमेटियां‘ (RPC) स्थापित करते हैं. यह नागरिक प्रशासन की मशीनरी हैं और अत्यंत प्रारंभिक प्रशासनिक कार्य करती हैं. यह समूह सशस्त्र इकाइयों को रसद सहायता भी प्रदान करती हैं.
यह संरचना दर्शाती है कि माओवादी केवल गुरिल्ला युद्ध पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि एक “समग्र युद्ध” लड़ रहे हैं जिसमें राजनीतिक लामबंदी, प्रचार, खुफिया जानकारी और यहां तक कि समानांतर शासन (RPC) भी शामिल है. इस जटिल संरचना को समझना सरकार की बहु-आयामी रणनीति (SAMADHAN) की आवश्यकता को पुष्ट करता है.
प्रभावित क्षेत्र और भौगोलिक विस्तार
नक्सलवाद का प्रभाव क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से “रेड कॉरिडोर” के रूप में जाना जाता है. 2021 तक इसमें मध्य और पूर्वी भारत के लगभग 25 जिले शामिल थे. वर्तमान में, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य माना जाता है.
गृह मंत्रालय की नवीनतम समीक्षा के आधार पर, योजना, कार्यान्वयन और विभिन्न हस्तक्षेपों की निगरानी के लिए 7 राज्यों के 18 जिलों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. वामपंथी उग्रवाद के संभावना वाले 10 राज्यों के 48 जिलों को कौशल विकास योजनाओं के तहत शामिल हैं. इन 48 जिलों में शामिल हैं:
- आंध्र प्रदेश: विशाखापत्तनम (1)
- तेलंगाना: खम्मम (1)
- बिहार: जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, बांका, नवादा (9)
- छत्तीसगढ़: दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, राजनांदगांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव (9)
- झारखंड: चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह, खूंटी, रांची, दुमका, रामगढ़, सिमडेगा (16)
- मध्य प्रदेश: बालाघाट, मंडला (2)
- महाराष्ट्र: गढ़चिरौली और गोंदिया (2)
- ओडिशा: गजपति, मलकानगिरी, रायगड़ा, देवगढ़, संबलपुर, कोरापुट (6)
- उत्तर प्रदेश: सोनभद्र (1)
- पश्चिम बंगाल: पश्चिम मिदनापुर (लालगढ़ क्षेत्र) (1)
सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है. अप्रैल 2018 में यह संख्या 126 से घटकर 90 हो गई. फिर, जुलाई 2021 में 70 और अप्रैल 2024 तक यह और घटकर 38 रह गई है. वर्ष 2022 में, वामपंथी उग्रवाद रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या 90 से घटकर 45 रह गई थी .
सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है. इसमें छत्तीसगढ़ के चार (बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, और सुकमा), झारखंड का एक (पश्चिमी सिंहभूम) और महाराष्ट्र का एक (गढ़चिरौली) जिले शामिल है. ‘डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न’ (जिनमें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है) की संख्या भी 9 से घटकर 6 हो गई है. इनमें आंध्र प्रदेश (अल्लूरी सीताराम राजू), मध्य प्रदेश (बालाघाट), ओडिशा (कालाहांडी, कंधमाल, और मलकानगिरी), और तेलंगाना (भद्राद्री-कोठागुडेम) शामिल हैं.
वामपंथी उग्रवाद का आंतरिक सुरक्षा से संबंध
वामपंथी उग्रवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और प्रत्यक्ष खतरा है. वर्ष 2004 से 31 मार्च, 2025 तक, वामपंथी उग्रवादियों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में लगभग 8895 लोगों की हत्या की गई है. मारे गए अधिकांश नागरिक आदिवासी होते हैं जिनको मारे जाने से पूर्व अक्सर ‘पुलिस मुखबिर’ की संज्ञा दी जाती है.
सीपीआई (माओवादी) की भारत में अपने जैसी विचारधारा वाले विद्रोही/आतंकवादी संगठनों को मिलाकर ‘यूनाइटेड फ्रंट’ बनाने की भी एक रणनीतिक योजना है, और यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनमें से अनेक संगठनों को भारत-विरोधी विदेशी ताकतों द्वारा सहायता की जाती है.
सरकारी प्रयास और योजनाएं
भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद की समस्या का समग्र रूप से प्रभावी तरीके से निराकरण करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपना रही है, जिसमें सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार और हकदारियां सुनिश्चित करना, शासनप्रणाली में सुधार और जन अवबोधन प्रबंधन शामिल है. ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं. इसलिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई मुख्यत: राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है. केंद्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है तथा अनेक तरीकों से उनके प्रयासों में सहायता और समन्वय करती है.
वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार ने ‘समाधान’ (SAMADHAN) सिद्धांत को अपनाया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई, 2017 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया था. यह सिद्धांत एक व्यापक, खुफिया-संचालित और प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है. यह पारंपरिक कानून प्रवर्तन से आगे बढ़कर समस्या के सभी पहलुओं को संबोधित करता है. ‘समाधान’ के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:
- S – स्मार्ट लीडरशिप (Smart Leadership)
- A – आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy)
- M – प्रेरणा और प्रशिक्षण (Motivation and Training)
- A – एक्शनेबल इंटेलिजेंस (Actionable Intelligence)
- D – डैशबोर्ड आधारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs) और मुख्य परिणाम क्षेत्र (KRAs) (Dashboard-based Key Result Areas and Key Performance Indicators)
- H – हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी (Harnessing Technology)
- A – प्रत्येक थिएटर/नाटकशाला हेतु कार्ययोजना (Action Plan for Each Theatre)
- N – वित्तपोषण तक पहुंच नहीं (No access to Financing)
इस रणनीति के तहत कई प्रमुख योजनाएं और पहलें लागू की गई हैं:
- सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना: यह योजना वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की क्षमता में वृद्धि करती है. इसमें सुरक्षा संबंधी व्यय, वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा बल कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि, समर्पण करने वाले कैडरों को मुआवजा, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना तथा प्रचार सामग्रियों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है. 2017-18 से अब तक इस योजना के तहत 2655.65 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
- विशेष केंद्रीय सहायता (SCA): 2017 में अनुमोदित इस योजना का उद्देश्य अत्यधिक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में तात्कालिक प्रकृति की सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करना है. 2017-18 से अब तक राज्यों को 3724.95 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
- विशेष अवसंरचना योजना (SIS) और फोर्टीफाइड पुलिस थानों की योजना: यह योजना सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराती है. इसमें फोर्टिफाइड (किलेबंद) पुलिस स्टेशनों का निर्माण शामिल है. इस योजना के तहत 1741 करोड़ रुपये की परियोजनाओं/कार्यों को मंजूरी दी गई है. योजना के तहत 306 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से 226 का निर्माण किया जा चुका है. कुल मिलाकर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 626 फोर्टिफाइड पुलिस थानों का निर्माण किया गया है.
- केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (ACALWEM): यह योजना अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और हेलीकॉप्टरों (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/भारतीय वायु सेना आदि) को किराए पर लेने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान करती है. पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान हेलीकॉप्टरों और सुरक्षा शिविरों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए 560.22 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
- सिविक ऐक्शन प्रोग्राम: यह योजना सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच दूरी को कम करने तथा सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा प्रदर्शित करने के लिए है. 2017-18 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 142.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
- मीडिया प्लान: यह योजना माओवादी दुष्प्रचार का मुकाबला करने और सरकार की विकास पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है. 2017-18 से इस योजना के तहत 52.52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
- सड़क संपर्क परियोजनाएं (RRP-I और RCPLWE): वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार के लिए कई पहलें की गई हैं. सड़क आवश्यकता योजना-I (RRP-I) के तहत 5361 किमी सड़कों में से 5204 किमी का निर्माण किया जा चुका है. सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE) में 12,228 किलोमीटर सड़क और 705 पुल संबंधी कार्य स्वीकृत हैं. अब तक 9506 किलोमीटर सड़क और 479 पुल संबंधी कार्य पूर्ण हो चुके हैं.
- दूरसंचार कनेक्टिविटी: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए तीन परियोजनाएं लागू की जा रही हैं. इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 10,511 मोबाइल टावरों की स्थापना की योजना है. अब तक 7,777 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं. पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र को 1 दिसंबर, 2025 तक मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस करने का लक्ष्य है.
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme): गृह मंत्रालय को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी का काम सौंपा गया है. इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) चल रहे हैं.
सरकार द्वारा एक मजबूत निगरानी तंत्र भी स्थापित किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री, गृह सचिव और अपर सचिव नियमित आधार पर वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा करते हैं. विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ बैठक और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित मॉनीटरिंग की जाती है.
वर्तमान स्थिति
भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है. यह सरकार की बहु-आयामी रणनीति के सकारात्मक परिणामों को दर्शाता है. वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 के उच्च स्तर (1936 घटनाएं) में काफी कमी आई है. वर्ष 2024 तक यह 81% घटकर 374 रह गई है.
परिणामी मौतों की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2010 में जहां मृत्यु की संख्या सर्वाधिक 1005 दर्ज की गई थी. =वहीं वर्ष 2024 में कुल मौतों (नागरिकों + सुरक्षा बलों) की संख्या 150 रह गई है, जो 2010 की तुलना में 85% की कमी है. 2022 में पहली बार चार दशकों में वामपंथी हिंसा के कारण मृत्यु की संख्या 100 से कम हुई और यह मात्र 98 रह गई थी.
वामपंथी उग्रवाद का भौगोलिक दायरा भी सिकुड़ गया है. अप्रैल 2018 में 126 जिलों से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अप्रैल 2024 में 38 रह गई है. सुरक्षा वैक्यूम को भरने के लिए 2019 से लेकर अभी तक 195 नए कैंप स्थापित किए गए हैं.
सुरक्षा बलों द्वारा आक्रामक रणनीति अपनाई गई है, जिसमें डिफेंसिव नीति को बदलकर ओफेंसिव रणनीति पर जोर दिया गया है. फरवरी 2022 में झारखंड के लोहरदगा जिले में नव स्थापित सुरक्षा कैंपों का उपयोग करके 13 दिवसीय संयुक्त अभियान को कई सफलताएं मिलीं.
वित्तीय प्रतिबंध (चोकिंग) की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. राज्यों द्वारा 21 करोड़ रुपये, ED द्वारा 10.64 करोड़ रुपये और NIA द्वारा 37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. एनआईए में वामपंथी उग्रवाद के मामलों के लिए एक अलग वर्टिकल स्थापित किया गया है. एनआईए को अब तक 61 मामलों की जांच सौंपी गई है.
झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं में स्थित बूढ़ा पहाड़ 32 वर्षों से नक्सलियों का गढ़ रहा था. इसे नक्सलियों के कब्जे से पूर्ण रूप से मुक्त कराना “नक्सल फ्री भारत” की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता है. बिहार, झारखंड और ओडिशा को वामपंथी उग्रवाद से लगभग मुक्त करा लिया गया है.
यह महत्वपूर्ण गिरावट वामपंथी उग्रवाद गतिविधि में बहु-आयामी रणनीति का परिणाम है, जिसमें आक्रामक सुरक्षा अभियानों को विकास पहलों के साथ जोड़ा गया है. इससे वामपंथी उग्रवादियों का प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ा है और उनके शीर्ष नेतृत्व को निष्क्रिय करने में सफलता मिली है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2026 से पहले देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है.
अंत में (Conclusion)
भारत में वामपंथी उग्रवाद की जड़ें आर्थिक असमानता, भूमि अधिकार विवाद और शोषण हैं. उग्रवादी समूह इन समस्याओं का लाभ उठाते हुए विकास कार्यों में बाधा डालते हैं. वे हिंसक क्रांति के जरिये लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराकर समानांतर माओवादी शासन स्थापित करना चाहते हैं.
इसके जवाब में भारत सरकार ने ‘समाधान’ सिद्धांत के तहत सुरक्षा, विकास, शासन सुधार और जनजागरूकता का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया. सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति और विकास परियोजनाओं के संयुक्त प्रयासों से हिंसा और प्रभावित इलाकों में उल्लेखनीय कमी आई है.
हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है और उग्रवाद अंतिम चरण में है. फिर भी इसके मूल कारणों के समाधान और उग्रवादी विचारधारा के मुकाबले के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं. यदि मूल कारणों को समाप्त न किया गया तो इसके फिर से पनपने का भी खतरा है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिकायतों के वैध मंच उपलब्ध हैं. हिंसा आधारित विचारधारा भारत की सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती.