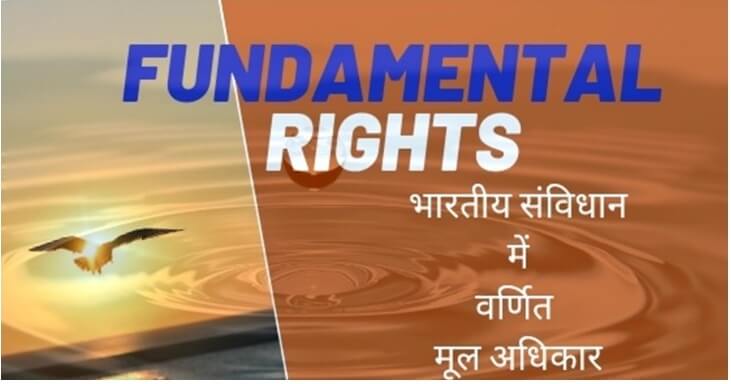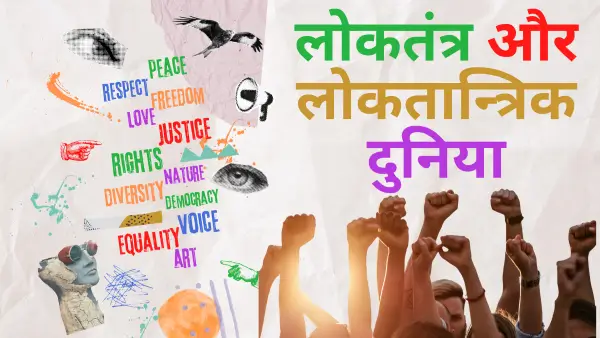आज भारत में 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के प्रावधान हैं. लेकिन यह आजादी के करीब पाँच दशकों बाद देशभर में लागू हो सका. यह समानता और सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ के रूप में देश को मजबूती प्रदान करता है. तो आइए आज हम इससे जुड़े संवैधानिक व कानूनी प्रावधान, इसके विशेषताएं, उपलब्धियां व अन्य तथ्यों को जानते हैं.
कैसे लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009?
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आजाद भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं. प्रारंभ में भारत के संविधान के नीति-निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 (Article 45) में शिक्षा की घोषणा की गई थी. इसके अनुसार, सभी राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधी के भीतर सभी बालक और बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी. यहीं से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा (Free Education) व्यवस्था के प्रयास आरंभ हुआ.
आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक अधिकार खंड में एक नया अनुच्छेद 21क (Article 21A) को जोड़ा गया. इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (free and compulsory education) देने की एक ऐसी नीति बनाएगा जो राज्य विधि द्वारा आधारित और उपबंध हो.
इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4क में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 (ट) (Fundamental Duty 51(T) जोड़ा गया. इसके अनुसार, माता-पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें.
उपरोक्त प्रावधानों के अधीन 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act 2009) पास किया गया. इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं.
इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्ग के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा. सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को लागू कर दिया. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में बहुमत से पारित कर दिया गया था तथा यह 1 अप्रैल 2010 (1st April 2010) से पूरे भारत में लागू हो गया.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य (Goal of RTE Act 2009)
भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है. हमारे संविधान के द्वारा ही मनुष्य को मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं. संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए है. इनका उपयोग कर व्यक्ति अपना समुचित कर सकता है और देश के विकास में भी भागीदार बन सकता है. किंतु किसी भी नागरिक का पूर्ण विकास तब तक असंभव हो सकता है, जब तक वह शिक्षित ना हो. इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लाया गया.
इसका मुख्य उदेश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है. इसका एक अन्य उद्देश्य देश में अशिक्षा का उन्मूलन कर सभी नागरिकों में आधुनिक सोच व समझ विकसित करना भी हैं.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएँ (Key Features of Right to Education Act 2009)
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (right to Education Act 2009) है. इस अधिनियम में प्रयुक्त विशेष शब्दों को परिभाषित किया गया है. इस तरह इसके विशेषताएं इस प्रकार हैं:
1. निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा: किसी भी वर्ग के बालक और बालिकाओं को यह अधिकार होगा कि वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा आसपास के किसी भी विद्यालय से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं. बशर्ते वह बालक और बालिका 6 से 14 वर्ष के अंतराल में ही आते हो.
2. प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष उपबंध: यदि कोई बच्चा ऐसा है, जो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका है तो वह बालक बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है. यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है, तो उसके बाद भी वह पढ़ाई पूरी होने तक निशुल्क शिक्षा प्राप्त करता रहेगा.
3. स्थानांतरण का अधिकार: यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारणवश कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान होगा.
4. विद्यालय स्थापित करने के कर्तव्य: इस अधिनियम के लागू होने के 3 सालों के भीतर राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को पड़ोस के स्कूलों को स्थापित करना होगा जिस क्षेत्र में एक स्कूल नहीं है वहाँ स्कूलों को स्थापित करना होगा.
5. उत्तरदायित्व का विभाजन: केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों की एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और साधन उपलब्ध कराएगी जिससे विद्यालय स्थापित किए जा सकेंगे हैं.
6. राज्य सरकारों के कर्तव्य: राज्य सरकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति निश्चित करेगी. साथ ही यह भी वह सुनिश्चित करेगी, कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो सके. राज्य सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता निश्चित करेंगी और बच्चों को उन्नत किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध कराएगी ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके.
7. स्थानीय पदाधिकारियों के कर्तव्य: स्थानीय पदाधिकारी उपर्युक्त धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार समस्त कर्तव्यों के साथ-साथ अपने क्षेत्र में बालकों का अभिलेख करेगी विद्यालयों के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित होगी और शैक्षिक कैलेंडर तैयार होंगे.
8. माता-पिता और संरक्षक का कर्तव्य: प्रत्येक अभिभावक और माता-पिता का यह उत्तरदायित्व कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए जरूर भेजें.
9. विद्यालय पूर्व शिक्षा का व्याख्या: 3 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना और जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी जरूरी इंतजाम भी करेंगे.
10. विद्यालय की जवाबदेही: सरकारी विद्यालय तो निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही और साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे.
11. प्रवेश व अन्य शुल्क: सरकारी विद्यालय ना तो दान याचना लेगा और ना ही बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा.
12. आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा.
13. प्रवेश से इंकार ना करना: स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
14. रोकने और निष्कासन का प्रावधान: किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा.
15. शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न: बालक को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएँ विद्यालय में नहीं दी जाएगी.
16. मान्यता प्रमाण: बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा और उन स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक पूरे करते हो.
17. विद्यालय के मान और मानक: जो स्कूल अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके थे तथा निर्धारित मानक पूरे नहीं करते हैं उन्हें अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर समस्त मानक पूरे करने होंगे.
18. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति: केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मान और मानकों की अनुसूची में परिवर्तन या लोप करके उसका संशोधन भी कर सकती है.
19. विद्यालय प्रबंधन समिति: अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे यह समिति स्कूल के कामकाज का मॉनिटर जैसे कार्य करेगी.
20. विद्यालय विकास योजना: धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति स्कूल विकास की योजना बनाने और उसकी संतुति करने का कार्य करेगी.
21. शिक्षकों की योग्यतायें और सेवा निबंधन: शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निदान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा.
22. छात्र-शिक्षक अनुपात: इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा, कि विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात प्राध्यापक को जोड़कर एक अनुपात 40 से अधिक ना हो अर्थात 1 शिक्षक पर 40 छात्र.
23. रिक्तियां: राज्य सरकार और स्थानीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद स्वीकृत पद संख्या के 10 फीसद से अधिक ना हो.
24. गैर-शैक्षिक प्रयोजन: शिक्षकों से गैरशैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियाकलापों में स्वयं को नहीं लगाया जायेगा.
25. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया: सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार (परिषद) संविधान में निहित मूल्यों के अनुसार इसका निर्धारण करेगा और बच्चे के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ-साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त करने का भी काम करेगा. मूल्यांकन व्यापक और सतत प्रकार का होगा.
26. परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र: किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई परीक्षा नहीं देनी होगी. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा.
27. निगरानी: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेगी.
28. शिकायतों को दूर करना: बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेगी.
29. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन: प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी. इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावकारी ढंग से लागू करना तथा इसके बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा.
30. राज्य सलाहकार परिषद का गठन: प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकारें करेंगी. इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावकारी ढंग से लागू करना और राज्य सरकार को परामर्श देना होगा.
31. निर्देश जारी करने की शक्ति: धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन समितियों को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेंगे और निर्देश दे सकेंगे.
32. अभिनियोजन व नियोजन: अधिनियम का पालन न करने पर धारा 13, 18 और 19 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कोई भी अभियोजन समुचित सरकार दादा तो सरकारी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के करना संशिथित नहीं किया जाएगा.
33. संरक्षण: इस अधिनियम के द्वारा या बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में सरकार, आयोग, स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन समितिया अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा आया वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी.
34. राज्य सरकारों के नियम बनाने की शक्ति: राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी.
35. इस अधिनियम में शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन का भी निषेध किया गया है.
शिक्षा के अधिकार से जुड़े न्यायिक मामले
जागरूक नागरिक शिक्षा के अधिकार को लागू करवाने के लिए अदालत भी गए. इस प्रकार अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय व टिप्पणियों का सार इस प्रकार हैं:
- मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के एक अभिन्न अंग के रूप में घोषित किया. न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध है और सरकार इसे वंचित नहीं कर सकती.
- उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को दोहराते हुए कहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21, 41 और 45 के संयोजन के रूप में देखा और इस बात पर जोर दिया कि राज्य का यह दायित्व है कि वह सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे. इस फैसले ने भविष्य के 86वें संवैधानिक संशोधन (2002) की नींव रखी.
- अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी. न्यायालय ने RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को बरकरार रखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वंचित बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले.
- सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ और अन्य (2012): इस महत्वपूर्ण मामले में, उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) की धारा 12 की वैधता को सही ठहराया. यह धारा सभी विद्यालयों, चाहे वे सरकारी हों या निजी, के लिए आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चों को 25% आरक्षण देना अनिवार्य बनाती है. न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सभी बच्चों, विशेषकर जो प्राथमिक शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है. इस फैसले ने निजी स्कूलों में वंचित बच्चों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया.
- मास्टर जय कुमार अपने पिता मनीष कुमार बनाम आधारशिला विद्या पीठ और अन्य (2024): इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला दिया. न्यायालय ने यह माना कि गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा प्रदान करना एक सार्वजनिक कर्तव्य है. इस निर्णय के माध्यम से, न्यायालय ने यह स्थापित किया कि यदि किसी बच्चे को आरक्षण के तहत सीट आवंटित की गई है, तो उस बच्चे को प्रवेश देने से मना करना RTE अधिनियम का सीधा उल्लंघन माना जाएगा. यह फैसला निजी स्कूलों की जवाबदेही को और मजबूत करता है और वंचित बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है.
सरकार द्वारा स्थापित समितियाँ और आयोग
केंद्र सरकार ने समय-समय पर शिक्षा के लिए आयोग व समितियों का गठन किया. इनके संस्तुतियों ने शिक्षा का अधिकार कानून के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया.
- राममूर्ति समिति (1990): आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित इस समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 1986 की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था. समिति ने बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की और इसे संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया.
- प्रोफेसर यशपाल समिति (1992): इस समिति का मुख्य उद्देश्य “शिक्षा बिना बोझ के” की अवधारणा को बढ़ावा देना था. समिति ने समझ और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा में रटकर सीखने की पद्धति को कम करने की सिफारिश की. इसने पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को अधिक बाल-केंद्रित और प्रासंगिक बनाने का सुझाव दिया.
- तपस मजूमदार समिति (1999): तपस मजूमदार की अध्यक्षता में गठित इस समिति को सर्वोच्च न्यायालय के उन्नीकृष्णन फैसले के बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाने का कार्य सौंपा गया था. समिति की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि इस अधिकार को लागू करने के लिए लगभग ₹1.37 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी. इस रिपोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया.
अन्य महत्वपूर्ण प्राधिकरण
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020: यह नीति एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है और RTE की कुछ सीमाओं को संबोधित करती है. NEP 2020 का उद्देश्य आयु सीमा को 3 से 18 वर्ष तक बढ़ाना है, जिसमें प्रारंभिक बचपन की शिक्षा (ECCE) को भी शामिल किया गया है. इसने सीखने के परिणामों पर जोर दिया और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (FLN) को प्राथमिकता दी.
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA): वर्ष 2001 में शुरू किया गया यह अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम था. इसने बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की भर्ती और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बाद में, इसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) के साथ मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान के रूप में एकीकृत किया गया, जिससे शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक एक व्यापक दृष्टिकोण मिल सके.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की उपलब्धियाँ (Achievements of RTE 2009)
RTE अधिनियम ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया, जिससे देश में शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ. इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:
- शिक्षकों की गुणवत्ता और जवाबदेही में वृद्धि: अधिनियम ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की और विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) सुनिश्चित किया, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ.
- समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन: RTE ने दिव्यांग बच्चों (CWSN) के लिए समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाया, जिससे मुख्यधारा के विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उचित वातावरण और संसाधन उपलब्ध हो सके.
- वित्तीय भागीदारी: अधिनियम के तहत शिक्षा के वित्तपोषण की जिम्मेदारी केंद्र (60%) और राज्य (40%) सरकारों के बीच साझा की गई, जिससे कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता सुनिश्चित हुई. पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है.
RTE की सीमाएँ और चुनौतियाँ
उपलब्धियों के बावजूद, RTE अधिनियम कई सीमाओं और चुनौतियों से ग्रस्त है:
- बुनियादी ढाँचे का असमान कार्यान्वयन: कई विद्यालयों, विशेषकर निजी और दूरदराज के क्षेत्रों में, अधिनियम द्वारा निर्धारित सख्त बुनियादी ढाँचे के मानदंडों को पूरा करने में चुनौतियाँ आती हैं.
- 25% कोटा का कार्यान्वयन: निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है. शुल्क प्रतिपूर्ति में देरी जैसी समस्याओं के कारण कई स्कूल इसका पालन नहीं करते.
- गुणवत्ता बनाम पहुँच: अधिनियम ने शिक्षा तक पहुँच तो बढ़ाई है, लेकिन सीखने के परिणामों में सुधार एक चुनौती बनी हुई है. ASER (Annual Status of Education Report) जैसी रिपोर्टें बताती हैं कि बच्चे बुनियादी पढ़ने और गणितीय कौशल में पीछे रह जाते हैं.
- आयु वर्ग की सीमा: अधिनियम केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कवर करता है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसे 0 से 18 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए, जैसा कि NEP 2020 में प्रस्तावित है.
- इनपुट-उन्मुख दृष्टिकोण: RTE का फोकस मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे (कमरे, शौचालय) और PTR जैसे इनपुट पर रहा है, जबकि सीखने के परिणाम (आउटपुट) संतोषजनक नहीं हैं.
- ‘नो डिटेंशन पॉलिसी‘ का प्रभाव और संशोधन: इस नीति का उद्देश्य बच्चों को तनाव-मुक्त वातावरण देना था, लेकिन इससे सीखने के परिणामों में गिरावट की आलोचना हुई. 2019 में, इसे संशोधित करके कक्षा 5 और 8 में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई, ताकि शैक्षणिक जवाबदेही बहाल हो सके.
- शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता: शिक्षकों की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी चुनौती है.
RTE को प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम
अधिनियम की सीमाओं को दूर करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाने चाहिए:
- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को RTE के अंतर्गत लाना: संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को कुछ प्रावधानों से छूट मिली है, लेकिन इन्हें RTE के तहत लाने से शिक्षा में एकरूपता आएगी.
- शिक्षक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान: केवल योग्यता मानदंड निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है; नियमित और उच्च गुणवत्ता वाले इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं.
- शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर: इनपुट-उन्मुख दृष्टिकोण से हटकर अब आउटपुट-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जहाँ सीखने के परिणामों का नियमित मूल्यांकन हो.
- शिक्षण पेशे को आकर्षक बनाना: प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए वेतन, भत्ते और कैरियर के अवसरों में सुधार करना महत्वपूर्ण है.
- समाज का समर्थन: शिक्षा को केवल सरकारी या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं मानना चाहिए; अभिभावकों और पूरे समाज को बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए.
समग्र शिक्षा अभियान का एकीकरण
2018-19 में लॉन्च किए गए समग्र शिक्षा अभियान ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों को एकीकृत करके RTE की सीमाओं को दूर करने का प्रयास किया है. इसने तीन योजनाओं (सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और शिक्षक शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजना) को एक ही छत के नीचे लाकर स्कूली शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है.
आगे की राह (Conclusion)
शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने शिक्षा तक पहुँच में सुधार करके एक मजबूत नींव रखी है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने RTE की सीमाओं को संबोधित करने का प्रयास किया है, जैसे कि आयु वर्ग को 3-18 वर्ष तक विस्तारित करना और सीखने के परिणामों पर जोर देना. RTE और NEP के बीच सामंजस्य स्थापित करके, भारत सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. वस्तुतः, RTE केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है.