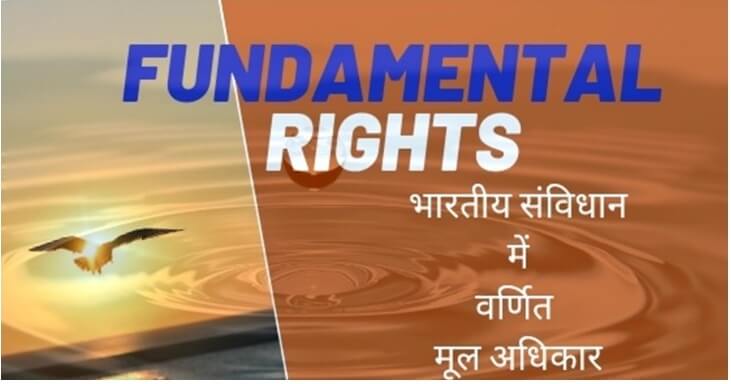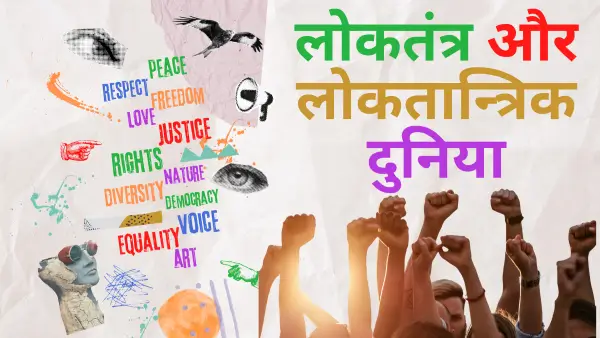भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हैं. इसका वर्णन संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के उपबंध में है. इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय आबादी के हितों की रक्षा करना, उनकी संस्कृति को संरक्षित करना और उन्हें आत्म-शासन का अधिकार प्रदान करना है. ये दोनों प्रावधान और लागू होने वाले क्षेत्र अलग-अलग हैं.
पांचवीं और छठी अनुसूची क्या हैं?
अधिकांश अनुसूचित जनजातियाँ देश के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहाँ वे पीढ़ियों से एकांतवास में रहकर अपनी विशिष्ट संस्कृति विकसित करती आई हैं. उन्हें बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं रहा है. स्वतंत्रता के बाद, इन क्षेत्रों को संविधान के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया और प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गईं.
संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक विशेष प्रणाली की व्यवस्था की गई है. अनुच्छेद 244(1) के अनुसार, पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं. वहीं, अनुच्छेद 244(2) के तहत, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय बहुल क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार किया जाता है.
अनुच्छेद 244 और छठी अनुसूची के तहत इन क्षेत्रों को “जनजातीय क्षेत्र” के रूप में नामित किया गया है, जो तकनीकी रूप से पांचवीं अनुसूची के “अनुसूचित क्षेत्रों” से अलग हैं. इस प्रकार, पांचवीं और छठी अनुसूचियाँ क्रमशः अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान करती हैं.
विशेष प्रावधान की जरूरत
आज़ादी और संविधान लागू होने से पहले, ब्रिटिश सरकार की आदिवासी आबादी के प्रति अलगाव और गैर-हस्तक्षेप की नीति ने उन्हें धीरे-धीरे जंगलों और पहाड़ों की ओर सीमित कर दिया. इस अलगाव के कारण ये जनजातियाँ अशिक्षित, गरीब और अविकसित रह गईं. वे अपने पारंपरिक कानूनों और रीति-रिवाजों द्वारा शासित थीं. कुछ जनजातियाँ खेती पर निर्भर थीं, जबकि अन्य की आजीविका शिकार और भोजन संग्रहण पर आधारित थी. इस प्रकार, ‘भूमि’, ‘जल’ और ‘जंगल’ उनकी आजीविका के दो मूलभूत संसाधन हैं, जिनसे उनका गहरा भावनात्मक लगाव है. ये संसाधन उन्हें समान दर्जा, सम्मान और आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण प्रदान करते हैं.
परिणामस्वरूप, उनका जीवन और दृष्टिकोण देश के अन्य हिस्सों, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों के लोगों से भिन्न है. इन विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों को समझते हुए, संविधान निर्माताओं ने उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, शोषण से बचाव और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्थाएँ लागू कीं.
संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है. संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक उदाहरण यह स्थापित करते हैं कि केवल ‘औपचारिक’ समानता का दृष्टिकोण अस्वीकार्य है. इसके बजाय, समानता को सार्थक बनाने के लिए ‘मौलिक’ दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें ऐतिहासिक भेदभाव को समाप्त करने और इसके वर्तमान प्रभावों को उलटने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं.
अनुच्छेद 15: राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है. यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है.
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता के किसी भी रूप को प्रतिबंधित करता है और राज्य से सकारात्मक व सक्रिय दृष्टिकोण की अपेक्षा करता है.
अनुच्छेद 38: राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व सौंपता है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे, आय की असमानताओं को कम करे और व्यक्तियों व समूहों के बीच स्थिति की असमानताओं को समाप्त करे.
अनुच्छेद 39: वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों के तहत आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, और आर्थिक प्रणाली में धन के संकेन्द्रण को कम करने की नीति पर जोर देता है.
अनुच्छेद 46: राज्य को कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का दायित्व सौंपता है.
ढेबर आयोग की अनुशंसाएँ
प्रथम अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को ढेबर आयोग के नाम से भी जाना जाता है. इस समिति ने पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों की अनुशंसा की है:
1. जनजातीय आबादी की अधिकता
2. क्षेत्र की सघनता और उचित आकार
3. क्षेत्र की अविकसित प्रकृति
4. लोगों के आर्थिक स्तर में स्पष्ट असमानता
5. एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई, जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका
ये मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों का चयन उनकी जनजातीय विशेषताओं, विकास की स्थिति और प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाए. साथ ही, आयोग ने “आदिम जनजातीय समूहों (Primitive Tribal Groups – PTGs)” की एक अलग श्रेणी बनाने की सिफारिश की, जिसे बाद में 2006 में “विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups – PVTGs)” नाम दिया गया.
बारदलोई समिति की छठी अनुसूची पर सिफ़ारिशें
गोपीनाथ बारदलोई की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत के संविधान की छठी अनुसूची के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समिति को पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और अधिकारों की रक्षा के लिए सिफारिशें देने का काम सौंपा गया था, विशेषकर अविभाजित असम के पहाड़ी जिलों के लिए।
बारदलोई समिति की प्रमुख सिफारिशें, जो बाद में संविधान की छठी अनुसूची का आधार बनीं, इस प्रकार हैं:
- स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils – ADCs) का गठन की सिफारिश
- स्वायत्त जिला परिषदों के तहत क्षेत्रीय परिषदों (Regional Councils) के गठन की सिफारिश
- विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता
- जनजातीय भूमि और संसाधनों का संरक्षण
- जनजातीय पहचान और संस्कृति का संरक्षण
- विकास और प्रशासन में जनजातीय भागीदारी
- राज्यपाल को इन स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों को गठित या पुनर्गठित करने की शक्ति
पांचवीं अनुसूची के विशेषताएँ व प्रशासन
पांचवीं अनुसूची के तहत “अनुसूचित क्षेत्र” उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है, जिन्हें संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है. इसमें कहा गया है: “इस संविधान में, ‘अनुसूचित क्षेत्र’ से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है, जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं.”
भारत का राष्ट्रपति असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते है.
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर होता है. संघ की कार्यपालिका इन क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी निर्देश राज्य को दे सकता है. यदि संघ चाहे तो वह अपने निर्णय के लिए राज्य को इन क्षेत्रों में लागु करने को बाध्य कर सकता है. इन क्षेत्रों के राज्यपालों को प्रतिवर्ष और जब राष्ट्रपति चाहे, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट सौंपना होता है.
जनजातीय सलाहकार परिषद्
अनुसूचित जनजातियाँ निवास वाले घोषित या अघोषित अनुसूचित क्षेत्र में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद् का गठन अनिवार्य है. जनजातीय सलाहकार परिषद् में अधिकतम 20 सदस्य होते है. इनमें से 3/4 सदस्य सम्बन्धित राज्य के विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से लिये जाते है.
राज्यपाल को परिषद् के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व नियुक्ति की पद्धति एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है. यह परिषद् राज्य की अनुसूचित जनजातियों के ‘कल्याण और उन्नति’
से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देती है जो राज्यपाल द्वारा निर्देशित किये गए हों.
अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि
राज्यपाल को अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू करे या न करे. राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व सुशासन हेतु नियम बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है जो इस प्रकार है-
- संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम में संशोधन या निरसन कर सकेगा, जो उस क्षेत्र पर लागू होने वाले हों.
- ऐसे क्षेत्रों के भूमि के हस्तांतरण को सीमित या निषिद्ध अथवा भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेगा. साहूकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित कर सकेगा.
- राज्यपाल कोई विनियम तब तक नहीं बना पाएगा, जब तक उसने ‘जनजाति सलाहकार परिषद्’ से परामर्श नहीं कर लिया हो. ऐसे विनियम को राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत करना होगा और उसकी अनुमति के बिना कोई विनियम प्रभावी नहीं होगा. अतः राज्यपाल की शक्ति वस्तुतः राष्ट्रपति के अधीन है.
- संसद को शक्ति प्राप्त है कि पांचवीं अनुसूची के किसी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन व निरसन कर सकती है. (यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है.)
अधिसूचित पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा
भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य और उनके क्षेत्र/जिले है:
| क्र.सं. | राज्य | पूर्ण रूप से शामिल जिले | आंशिक रूप से शामिल जिले |
| 1. | आंध्र प्रदेश | – | पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम |
| 2. | छत्तीसगढ़ | सरगुजा, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरबा, जशपुर, कांकेर, बलरामपुर, सूरजपुर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव | बालोद, धमतरी, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, बिलासपुर |
| 3. | गुजरात | डांग, दाहोद, नर्मदा, तापी | सूरत, भरूच, वलसाड, वडोदरा, पंचमहल, साबरकांठा, नवसारी |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | लाहौल और स्पीति, किन्नौर | चंबा |
| 5. | झारखंड | रांची, खूंटी, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ | पलामू, गढ़वा, गोड्डा |
| 6. | मध्य प्रदेश | झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, अलीराजपुर | धार, खरगोन (पश्चिम निमाड़), खंडवा (पूर्वी निमाड़), रतलाम, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद, शहडोल, उमरिया, श्योपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, अनूपपुर, बुरहानपुर |
| 7. | महाराष्ट्र | – | ठाणे, पुणे, नासिक, धुले, नादुरबार, जलगांव, अहमदनगर, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, गढ़चिरौली, चंद्रपुर |
| 8. | ओडिशा | मलकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़, मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट | संबलपुर, क्योंझर, खंधमाल, कालाहांडी, बालासोर, गजपति, गंजम |
| 9. | राजस्थान | बांसवाड़ा, डूंगरपुर | उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ |
| 10. | तेलंगाना | – | आदिलाबाद, खम्मम, महबूबनगर, वारंगल |
यह जानकारी दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार है. (स्रोत दस्तावेज)
छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र
संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत छठी अनुसूची का प्रावधान हैं. बारदलोई कमिटी की सिफारिशों पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दी गई. छठी अनुसूची के तहत, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है. राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्ता मिलती है.
इसके अंतर्गत उत्तर पूर्व के चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है. इन जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िले के रूप में प्रशासित किया जाता है. अगर किसी ज़िले में विभिन्न अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हों, तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में विभाजित करने का अधिकार प्राप्त है.
राज्यपाल को लोक अधिसूचना द्वारा स्वायत्त ज़िले में स्वायत्त क्षेत्र बनाने, पहले से शामिल स्वायत्त क्षेत्र को हटाने, नए स्वायत्त जिले बनाने, स्वायत्त ज़िले के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, दो या अधिक स्वायत्त ज़िले को मिलाकर एक बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार है.
ज़िला परिषद् तथा प्रादेशिक/क्षेत्रीय परिषद्
इसमें कुल 30 सदस्य होते है, जिसमें 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित व 26 सदस्य वयस्क मताधिकार से निर्वाचित किए जाते है. इस संबंध में केवल असम की बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अपवाद है जिसके 40 से ज्यादा सदस्य हैं और 39 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है.
निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है (बशर्ते परिषद् को पहले विघटित न कर दिया जाए). मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं. अगर किसी स्वायत्त ज़िले के भीतर स्वायत्त क्षेत्र का गठन किया गया है तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक् क्षेत्रीय परिषद् का प्रावधान है.
ज़िला परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषद् की शक्तियां
ये परिषदें भूमि, वन, नहर, खेती, गाँव प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह एवं सामाजिक रीति-रिवाज के संबंध में विधि बना सकती हैं. इसे राज्यपाल की अनुमति से परिषदों को भू-राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण की तथा कुछ निश्चित कर लगाने की शक्ति प्राप्त है. राज्यपाल को विशेष परिषदों के आपसी विवादों के निपटारे हेतु न्यायालयों के गठन की शक्ति प्राप्त है.
ज़िला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को अधिकार है कि वह राज्य के न्यायालय का अपवर्जन करके ग्राम परिषदों या न्यायालय का गठन कर सके. परिषदों द्वारा बनाई गई विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक राज्यपाल अनुमति प्रदान न कर दे. जिन मामलों में कम-से-कम 5 साल कारावास, उम्रकेद या मृत्युदंड का प्रावधान है, उन पर विचारण करने का अधिकार इन न्यायालयों को राज्यपाल की सहमति के बाद ही मिलेगा.
इस प्रकार इन परिषद व जिलों को विधायी, कार्यकारी, न्यायिक व वित्तीय शक्तियां प्राप्त है.
स्वायत्त ज़िलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन की जाँच
राज्यपाल को अधिकार है कि वह ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में किसी भी समय जाँच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये एक आयोग नियुक्त कर सकता है. यह आयोग शिक्षा, चिकित्सा, संचार, नवीन कानून की आवश्यकता (विधि, नियमों, विनियमों) के संबंध में जाँच करता है. आयोग की रिपोर्ट प्रत्येक संबंधित मंत्री द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई के स्पष्टीकरण सहित खंडों में राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.
परिषद् का निष्प्रभावी होना तथा विघटन
ज़िला परिषदों या क्षेत्रीय परिषदों की किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा व लोकव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अंदेशा दिखे, तो राज्यपाल ज़िला परिषदों या क्षेत्रीय परिषदों को निलंबित कर सकता है. छठी अनुसूची में संसद द्वारा किया गया संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है.
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र
| राज्य | ऑटोनॉमस काउंसिल |
| भाग I (असम) | उत्तर-कछार हिल्स जिला (दिमा हाओलांग)कार्बी-आंगलोंग जिलाबोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला |
| भाग II (मेघालय) | खासी हिल्स जिलाजयंतिया हिल्स जिलागारो हिल्स जिला |
| भाग II-A (त्रिपुरा) | त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला |
| भाग III (मिजोरम) | चकमा जिलामारा जिलालाई जिला |