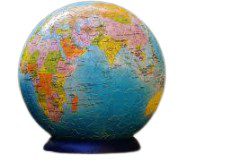विभिन्न तत्वों का जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, और वायुमंडल के बीच निरंतर प्रवाह और परिवर्तन होता रहता है, जिसे जैव भू-रसायन चक्र (Biogeochemical Cycles) कहा जाता है. ये चक्र पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता और पारिस्थितिकी तंत्रों की कार्यशीलता के लिए रासायनिक तत्वों का चक्रीय संचलन अत्यंत महत्वपूर्ण है.
जैव भू-रसायन चक्र क्या हैं? (What is Biogeochemical Cycle in Hindi)
जैव भू-रासायनिक चक्र वह मौलिक प्रक्रिया है जिसमें अजैविक तत्वों, जैसे कि खनिज और गैसें, का उपयोग जीवित जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं. फिर अकार्बनिक या अजैविक रूप में पर्यावरण में वापस आ जाते हैं. यह जीव (bio) और भू-भाग (geo) या वातावरण के मध्य का एक जटिल रासायनिक चक्र है. इसलिए इसे जैव-भू रसायन चक्र कहा जाता हैं.
जैव भू-रसायन चक्र का महत्व (Importance of Biogeochemical Cycle)
इन चक्रों का महत्व कई स्तरों पर समझा जा सकता है:
- तत्वों की निरंतर उपलब्धता: जैव भू-रसायन चक्र द्वारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर और जल जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति कायम रहता है. ये तत्व जीवों की शारीरिक वृद्धि, ऊतकों के निर्माण और संवर्धन के लिए अपरिहार्य हैं. इन चक्रों मे बाधा जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की कमी का कारण हो सकती है.
- पारिस्थितिक तंत्र का कार्य: पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन जीवों को बनाने वाले पदार्थ लगातार संरक्षित और पुनर्चक्रित होते रहते हैं. पदार्थ के संरक्षण का नियम बताता है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूप या स्थान बदलता है. इस सिद्धांत का अर्थ है कि मानवीय गतिविधियों द्वारा पर्यावरण में जारी कोई भी पदार्थ, जैसे प्रदूषक, प्रणाली के भीतर ही रहेगा. यह केवल अपना रूप (जैसे गैसीय से ठोस) या स्थान (जैसे वायुमंडल से जल निकाय) बदल सकता है. यह दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणामों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है. मतलब आज परित्यक्त पदार्थ भविष्य में भी प्रभाव डाल सकते हैं, भले ही वे अब दिखाई न दें.
- पर्यावरणीय संतुलन और जलवायु विनियमन: जैविक प्रक्रियाएं अजैविक भंडारों को प्रभावित करती हैं. साथ ही, अजैविक स्थितियां जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं. इस प्रकार, पर्यावरण में किसी भी एक घटक में व्यवधान अनिवार्य रूप से पूरे चक्र में और अंततः अन्य संबंधित चक्रों में भी व्यापक प्रभाव डालेगा. इसलिए, पर्यावरणीय समस्याओं को एकीकृत दृष्टिकोण से समझना और संबोधित करना आवश्यक है.
जैव भू-रसायन चक्रों के प्रकार (Types of Biogeochemical Cycles)
जैव भू-रासायनिक चक्रों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
- गैसीय चक्र: इन चक्रों में तत्व मुख्य रूप से वायुमंडल में गैसीय रूप में मौजूद होते हैं. इनमें जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र शामिल हैं.
- अवसादी चक्र: इन चक्रों में तत्व मुख्य रूप से पृथ्वी की पपड़ी में ठोस या अवसादी रूप में पाए जाते हैं. फॉस्फोरस चक्र और सल्फर चक्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं.
प्रमुख जैव भू-रसायन चक्रों का उदाहरण व संक्षिप्त विवरण
| चक्र का नाम | मुख्य भंडार | प्रमुख प्रक्रियाएँ | प्रमुख मानवीय प्रभाव | चक्र का प्रकार |
| जल चक्र | महासागर, बर्फ की चादरें, ग्लेशियर, भूजल, झीलें, वायुमंडल, मिट्टी की नमी | वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, संग्रहण/अपवाह, अंतःस्यंदन, ऊर्ध्वपातन | जलवायु परिवर्तन से वर्षा पैटर्न में बदलाव, प्रदूषण | गैसीय |
| कार्बन चक्र | वायुमंडल (CO2), महासागर, जीवाश्म ईंधन, तलछटी चट्टानें, जीवमंडल | प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपघटन, दहन, महासागरीय अवशोषण, अवसादन | जीवाश्म ईंधन दहन, वनों की कटाई, भूमि उपयोग परिवर्तन, महासागरीय अम्लीकरण | गैसीय |
| ऑक्सीजन चक्र | वायुमंडल (21%), पृथ्वी की पपड़ी (ऑक्साइड), जल भंडार | प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, दहन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण | जीवाश्म ईंधन दहन, वनों की कटाई (अप्रत्यक्ष) | गैसीय |
| नाइट्रोजन चक्र | वायुमंडल (78%), जीवमंडल, मृदा, जल भंडार | नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अवशोषण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण | नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, जीवाश्म ईंधन दहन, पशुपालन | गैसीय |
| फॉस्फोरस चक्र | चट्टानें (स्थलमंडल), समुद्री तलछट, जीवमंडल | अपक्षय, अवशोषण, खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरण, अवसादन | फॉस्फेट-आधारित उर्वरकों का उपयोग, सीवेज डिस्चार्ज (यूट्रोफिकेशन) | अवसादी |
| सल्फर चक्र | वायुमंडल, सागर, भूमिगत पारिस्थितिकी, चट्टानें, जीवाश्म ईंधन | दूषण, सल्फर ऑक्सीकरण, सल्फेट कमीकरण, जैविक समेकरण, ज्वालामुखी स्रोत | जीवाश्म ईंधन दहन, औद्योगिक गतिविधियाँ (अम्ल वर्षा) | अवसादी |
जैव भू-रसायन चक्रों के अंतर्संबंध
तत्वों का जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच निरंतर संचलन और परिवर्तन एक चक्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों को दूसरे चक्रों में भी व्यापक प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है. यह पृथ्वी की प्रक्रियाओं की प्रणालीगत प्रकृति को दर्शाता है.
इन अंतर्संबंधों के कुछ विशिष्ट उदाहरण निम्नलिखित हैं:
- जल एक परिवहन माध्यम के रूप में: जल चक्र अन्य पोषक तत्वों के चक्रण के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करता है. पानी की गति सल्फर और फॉस्फोरस जैसे तत्वों के नदियों, झीलों और महासागरों में लीचिंग के लिए महत्वपूर्ण है. इसलिए, जल चक्र में किसी भी व्यवधान का अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की उपलब्धता और चक्रण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.
- कार्बन-नाइट्रोजन युग्मन: कार्बनिक पदार्थों में कार्बन और नाइट्रोजन का युग्मन अपघटन दरों और पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है.
- फॉस्फोरस की सीमा: प्राथमिक उत्पादकता पर फॉस्फोरस की सीमा कार्बन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन की मांग को प्रभावित करती है. यदि फॉस्फोरस सीमित है, तो पौधे पर्याप्त मात्र में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अवशोषित नहीं कर पाएंगे. इसी प्रकार, नाइट्रोजन की भी कम आवश्यकता होगी.
- सूक्ष्मजैविक मध्यस्थता: सूक्ष्मजीव तत्वों के परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे विभिन्न चक्रों के बीच संबंध स्थापित होते हैं. उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन चक्र में बैक्टीरिया की भूमिका इसे अन्य चक्रों से जोड़ती है.
- ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन: ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चक्र श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, जो वायुमंडलीय संरचना के संतुलन को बनाए रखते हैं.
इस प्रकार, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों में जैव भू-रसायन चक्र अलग-थलग नहीं होते हैं, बल्कि एक जटिल, एकीकृत प्रणाली के रूप में परस्पर जुड़े होते हैं.
मानवीय गतिविधियों का जैव भू-रसायन चक्रों पर प्रभाव
मानवीय गतिविधियों द्वारा कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का पृथ्वी की पपड़ी और वायुमंडल से पर्यावरण में संचलन कई गुना बढ़ गया है. यह दर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक दरों से बहुत भिन्न है. इससे प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक सिंक (जैसे महासागर, वन) इन तत्वों को इस त्वरित गति से अवशोषित नहीं कर पाते हैं. ये अतिरेक पदार्थ कई वर्षों तक विभिन्न घटकों में संचयित रहते है. इससे जलवायु परिवर्तन तथा यूट्रोफिकेशन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं.
प्रमुख मानवीय गतिविधियाँ और उनके विशिष्ट प्रभाव निम्नलिखित हैं:
- जीवाश्म ईंधन दहन (Fossil Fuel Combustion): जीवाश्म ईंधन को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की बड़ी मात्रा निकलती है. इससे ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है. जीवाश्म ईंधन के जलने से निकल सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण है.
- वनों की कटाई (Deforestation): जंगलों को साफ करने से कार्बन चक्र में बाधा आती है. पेड़ कटने से प्रकृति द्वारा CO2 अवशोषित करने की क्षमता में गिरावट होती है. यदि इन लकड़ियों को जलाया जाता है या वे सड़ते हैं, तो इनमें संग्रहीत कार्बन पुनः CO2 के रूप में वायुमंडल में चला जाता हैं. इससे जहाँ बायोमाह में कार्बन कम होता है, वहीं वायुमंडलीय CO2 का स्तर काफी अधिक बढ़ जाता है.
- कृषि (Agriculture): कृषि पद्धतियाँ जैव भू-रासायनिक चक्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं.
- उर्वरकों का उपयोग: नाइट्रोजन और फॉस्फोरस-आधारित उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी और जल निकायों में इनकी मात्रा बढ़ा सकती है. ये दोनों जल निकायों में बहकर यूट्रोफिकेशन उत्पन्न कर सकते है. यह हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन का कारण बनता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन की कमी होती है.
- नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) उत्सर्जन: नाइट्रोजन-आधारित उर्वरकों के उत्पादन के से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है. यह एक शक्तिशाली ग्रीन्हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है.
- पशुपालन: पशुधन उत्पादन से आंतों के किण्वन और खाद प्रबंधन के माध्यम से मीथेन निकलती है. यह भी एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है.
- नगरीकरण और औद्योगिक गतिविधियाँ (Urbanization and Industrial Activities): औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान प्रदूषकों और कचरे का उत्सर्जन वायु, जल और मिट्टी को प्रदूषित करता है. यह विभिन्न तत्वों के चक्रण में बाधक है. कई औद्योगिक इकाइयों से सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन के आक्साइड बड़ी मात्रा में निकलते है. प्रकृति इसके उत्पादन के गति से इनका अवशोषण नहीं कर पाता है. इस तरह निकले अतिरेक पदार्थ प्रदूषण के मुख्य कारण है.
पर्यावरणीय परिणाम
मानवीय गतिविधियों के कारण जैव भू-रासायनिक चक्रों में होने वाले परिवर्तनों के दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम होते हैं:
- ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन: वायुमंडलीय CO2 और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है.
- महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification): महासागरों द्वारा CO2 के बढ़ते अवशोषण से अम्लता का स्तर बढ़ जाता है. यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है. अपने खोल और कंकाल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट पर जीवों के लिए यह घातक है.
- यूट्रोफिकेशन और जल गुणवत्ता का क्षरण: अतिरिक्त नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है.
- अम्ल वर्षा: सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है. यह मिट्टी की उर्वरता को कम करती है. यह वनों को भी नुकसान पहुंचाती है और मानव निर्मित संरचनाओं को खराब करती है.
- जैव विविधता हानि: पारिस्थितिकी तंत्रों में व्यवधान और प्रदूषण से जैव विविधता को खतरा होता है, जिससे आवासों का नुकसान और प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम बढ़ जाता है.
ये प्रभाव स्थानीयकृत नहीं हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर फैलते हैं और कई चक्रों में व्यापक रूप से फैलते हैं. यह पर्यावरणीय चुनौतियों की प्रणालीगत प्रकृति को रेखांकित करता है.
निष्कर्ष
इन समस्याओं का हल निकालने के लिए हमें समग्र (holistic) सोच अपनानी होगी. हमें इन चक्रों को अच्छे से समझना होगा और ऐसी टिकाऊ (sustainable) आदतें अपनानी होंगी जो संतुलन बहाल करें. उदाहरण के लिए – उपभोग को सीमित व संतुलित रखना, अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल, पेड़ लगाना और बचाना, मिट्टी का सही प्रबंधन, खेती में खाद का समझदारी से उपयोग और कारखानों का प्रदूषण कम करना.
इन चक्रों का संतुलन बनाए रखना सिर्फ प्रकृति के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य और जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है.