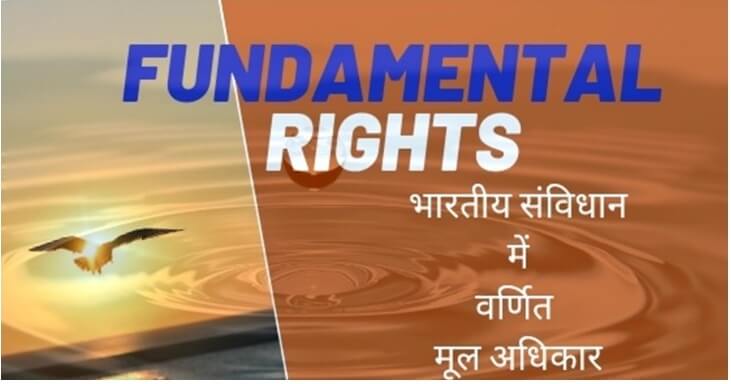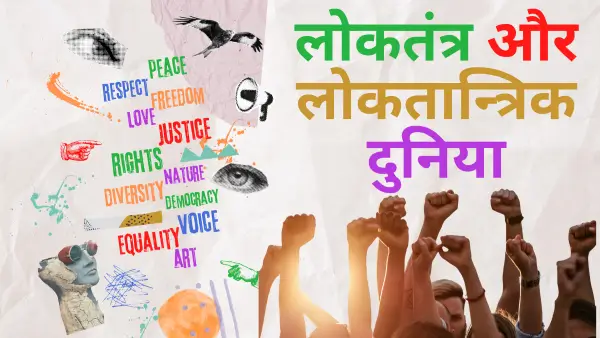नागरिकता (Citizenship) किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी और सामाजिक संबंध है. यह संबंध नागरिक (Citizen) को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि उस पर कुछ कर्तव्य भी लागू करता है. नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति को समाज का हिस्सा बनाती है और उसे स्थानीय समुदाय के साथ जोड़ती है.
नागरिकता की प्रसिद्ध परिभाषाएँ (Famous Definitions of Citizenship)
नागरिकता की कई परिभाषाएँ हैं, जो विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती हैं. यहाँ कुछ सबसे प्रसिद्ध परिभाषाएँ दी गई हैं:
- अरस्तू ने नागरिकता को राज्य के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया. उनके अनुसार, एक नागरिक वह है जो न्यायपालिका और विधायी कार्यों में भाग लेता है.
- टी.एच. मार्शलने अपनी पुस्तक “सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास” में नागरिकता को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया:
- नागरिक नागरिकता (Civil Citizenship): इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं, जैसे भाषण, विचार और धर्म की स्वतंत्रता.
- राजनीतिक नागरिकता (Political Citizenship): इसमें राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार शामिल है, जैसे मतदान करना और सार्वजनिक पद धारण करना.
- सामाजिक नागरिकता (Social Citizenship): इसमें आर्थिक और सामाजिक कल्याण का अधिकार शामिल है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा.
- आधुनिक परिभाषाएँ: वर्तमान में नागरिकता को अक्सर एक “कानूनी स्थिति” के रूप में देखा जाता है जो किसी व्यक्ति को एक विशेष देश के नागरिक के रूप में पहचानती है. इसमें पासपोर्ट रखने, मतदान करने और सामाजिक सुरक्षा लाभों का उपयोग करने जैसे अधिकार शामिल होते हैं. यह स्थिति व्यक्ति पर देश के कानूनों का पालन करने और राष्ट्र के प्रति वफादारी रखने का कर्तव्य भी लागू करती है.
नागरिकता का सिद्धांत (Theories of Citizenship)
नागरिकता के मुख्य रूप से दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं: जूस सोली और जूस सैंग्विनिस. इन सिद्धांतों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति जन्म के समय किस देश का नागरिक होगा.
1. जूस सोली (Jus Soli) – ‘मिट्टी का अधिकार‘
जूस सोली एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “मिट्टी का अधिकार”. इस सिद्धांत के अनुसार, किसी व्यक्ति को उस देश की नागरिकता मिलती है जहाँ उसका जन्म हुआ है, चाहे उसके माता-पिता की नागरिकता कुछ भी हो. यह सिद्धांत अक्सर उन देशों में अपनाया जाता है जो आप्रवासियों को अपने समाज में एकीकृत करना चाहते हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में नागरिकता इसी आधार पर दिया जाता है. अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति अमेरिका की भूमि पर पैदा होता है, वह स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिक बन जाता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता-पिता किस देश के नागरिक हैं या उनका कानूनी दर्जा क्या है. कनाडा भी इसी सिद्धांत का पालन करता है. कनाडा में जन्मे बच्चे को स्वचालित रूप से कनाडाई नागरिकता मिल जाती है.
2. जूस सैंग्विनिस (Jus Sanguinis) – ‘रक्त का अधिकार‘
जूस सैंग्विनिस का अर्थ है “रक्त का अधिकार”. इस सिद्धांत के तहत, किसी व्यक्ति की नागरिकता उसके माता-पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है, न कि उसके जन्म स्थान पर. यह सिद्धांत अक्सर उन देशों में अपनाया जाता है जो अपनी राष्ट्रीय पहचान और जातीयता को बनाए रखना चाहते हैं.
जर्मनी और जापान की नागरिकता इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं. 2000 के दशक में कानून में बदलाव से पहले, जर्मनी मुख्य रूप से जूस सैंग्विनिस सिद्धांत का पालन करता था. एक बच्चे को जर्मन नागरिकता तभी मिलती थी जब उसके माता-पिता जर्मन नागरिक हों, भले ही वह बच्चा जर्मनी में ही पैदा हुआ हो.
जापान में नागरिकता का निर्धारण मुख्य रूप से माता-पिता की नागरिकता के आधार पर किया जाता है. यदि एक जापानी नागरिक का बच्चा विदेश में पैदा होता है, तो उसे जापानी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन एक विदेशी माता-पिता के बच्चे को जापान में जन्म लेने पर स्वचालित रूप से जापानी नागरिकता नहीं मिलती.
अधिकांश देश इन दोनों सिद्धांतों का मिला-जुला रूप अपनाते हैं. उदाहरण के लिए, भारत में नागरिकता जन्म और वंश (दोनों) के आधार पर दी जाती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें और अपवाद भी लागू होते हैं.
नागरिक कौन है? (Who is a Citizen?)
नागरिक किसी समुदाय अथवा राज्य मेँ निवास करने वाला वह व्यक्ति होता है, जिसे उस समुदाय अथवा राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है. नागरिक विदेशियोँ से भिन्न है, क्योंकि विदेशियोँ को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीँ होते, जो किसी राज्य की पूर्ण सदस्यता के लिए अनिवार्य हैं.
प्रत्येक संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र मेँ रहा है, तथा
- जो भारत के राज्य क्षेत्र मेँ जन्मा था या,
- उसके माता-पिता मेँ से कोई भारत के राज्य मेँ जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र मेँ मामूली तौर पर निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा.
भारत में नागरिकता का सिद्धांत (Theory of Citizenship in India)
भारत ने नागरिकता के लिए किसी एक सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, बल्कि यह जूस सोली (जन्म स्थान के आधार पर) और जूस सैंग्विनिस (वंश के आधार पर) दोनों का एक मिश्रित रूप है.
भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, भारत में नागरिकता मुख्य रूप से पाँच तरीकों से प्राप्त की जा सकती है:
1. जन्म से नागरिकता (जूस सोली का संशोधित रूप)
यह सिद्धांत भारत में समय-समय पर संशोधित हुआ है.
- 26 जनवरी, 1950 से 1 जुलाई, 1987 के बीच जन्मे व्यक्ति: इस अवधि में भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, भारत का नागरिक माना जाता था.
- 1 जुलाई, 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति: इस अवधि के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाता है, जब उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो.
- 3 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति: इस समय के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता तब मिलती है जब उसके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, या माता-पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो.
2. वंश के आधार पर नागरिकता (जूस सैंग्विनिस)
यह सिद्धांत उन लोगों पर लागू होता है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है.
- 26 जनवरी, 1950 से 10 दिसंबर, 1992 के बीच जन्मे व्यक्ति: यदि कोई व्यक्ति इस अवधि में भारत के बाहर पैदा हुआ है, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक थे.
- 10 दिसंबर, 1992 के बाद जन्मे व्यक्ति: इस अवधि के बाद, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो. यह संशोधन लिंग-समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था.
- 3 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति: भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता तब मिलेगी, जब उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर उसका पंजीकरण भारतीय वाणिज्य दूतावास में करवा लिया जाए.
3. पंजीकरण द्वारा नागरिकता (Citizenship by Registration)
कुछ श्रेणियों के लोग, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति और नाबालिग बच्चे, भारत सरकार के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.
4. देशीयकरण द्वारा नागरिकता
एक विदेशी व्यक्ति जिसने भारत में एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 11 साल) तक निवास किया हो, वह कुछ शर्तों को पूरा करने पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.
5. क्षेत्र के समावेशन द्वारा नागरिकता
यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो भारत सरकार अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता प्रदान कर सकती है. उदाहरण के लिए, गोवा, पुडुचेरी, और सिक्किम के भारत में विलय के समय वहां के निवासियों को इसी तरीके से नागरिकता दी गई थी.
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 (Indian Citizenship Act 1955)
- भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 मेँ उपबंध है, कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत मेँ जन्मा कोई भी व्यक्ति, कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए पूरे भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था.
- पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, जिसमे पुरुष तथा भारतीय महिला की संतान भारतीय होगी. 1991 के संशोधन द्वारा भारतीय विवाहित पुरुष की संतान भी भारतीय होगी.
- भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A, असम के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है. यह धारा 25 मार्च, 1971 से पहले राज्य में प्रवेश करने वाले पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) के लोगों को नागरिकता प्रदान करती है. इसे 1985 के असम समझौते को लागू करने के लिए लागू किया गया था. यह प्रावधान प्रवासियों को उनकी प्रवेश तिथि (1 जनवरी, 1966 से पहले, या 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 के बीच) के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है और उनके नागरिक बनने की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है.
भारतीय संविधान में नागरिकता (Citizenship in Indian Constitution)
| भाग 2 (नागरिकता) | |
| अनुच्छेद 5 | संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता |
| अनुच्छेद 6 | पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियोँ के नागरिकता के अधिकार |
| अनुच्छेद 7 | पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियोँ के नागरिकता के अधिकार |
| अनुच्छेद 8 | भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियोँ के नागरिकता के अधिकार |
| अनुच्छेद 9 | विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियोँ का नागरिक न रह जाना. |
| अनुछेद 10 | नागरिकता के अधिकारोँ का बना रहना |
| अनुच्छेद 11 | संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना |
- अनुच्छेद 6 मेँ संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियो की नागरिकता के अधिकारोँ का उपबंध किया गया है.
- अनुच्छेद 8 मेँ कोई व्यक्ति या उसके माता पिता मेँ से कोई पितामह या पितामही, मातामह या मातामही मेँ से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 मेँ यथा परिभाषित भारत मेँ जन्मा था, और जो भारत के बाहर किसी देश मेँ निवास कर रहा है. उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा.
- यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो तो भारत की उसकी नागरिकता का उसका अधिकार खत्म हो जाएगा.
- राष्ट्रहित मेँ भारत सरकार किसी व्यक्ति को दो नागरिकताएं स्वीकार करने की अनुमति दे सकती है, जैसे सांस्कृतिक राजदूत के आधार पर अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को दोहरी नागरिकता का अधिकार दिया गया है.
दोहरी नागरिकता के अपवाद (Exceptions to Dual Citizenship)
- राजनीतिक शरण, जैसे दलाई लामा को भारत ने शरण दे रखी है.
- विदेश का राजाध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता किसी उपद्रव के बाद किसी अन्य देश मेँ शरण लेता है, तो उनका प्रत्यर्पण नहीँ किया जा सकता और साथ ही साथ उसे देश की नागरिकता प्रदान की जाती है.
- विदेशो के राजाध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जब भी भारत आते है तो उन्हें सम्मान के लिए भारत की नागरिकता से विभूषित किया जाता है.
- किसी भी प्रकार की नागरिकता का विधान संसदीय विधि के अलावा और तरीकोँ से नहीँ छीना जा सकता है (अनुच्छेद 10)
- संसद को भारत की नागरिकता अर्जन या निरसन की निर्बाध शक्तियाँ हैं.
नागरिक और गैर–नागरिक मेँ अंतर
- नागरिक समाज समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होते और गैर-नागरिक को समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे गैर-नागरिक के पास अनुच्छेद 15.16,19,29,30 तथा 326 के अनुसार मताधिकार नहीँ है.
- नागरिकोँ को राष्ट्र की और से विशेष दायित्व सोंपे जा सकते हैं, पर गैर-नागरिकोँ को नहीँ.
नागरिकता कानून मेँ संशोधन, 1992
1992 ई. मेँ संसद ने सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया. जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई की भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उनकी मां भारत की नागरिकता है, भारत को नागरिकता प्राप्त होगी. इससे पूर्व उसी दशा मेँ किसी बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो. इस प्रकार अब नागरिकता के प्रसंग मेँ बच्चे का माता को पिता के समकक्ष स्थिति प्रदान कर दी गई.
नागरिकता की समाप्ति (End of Citizenship)
- दूसरी नागरिकता स्वीकार करने या अज्ञातवास के द्वारा यदि कोई भारतीय लगातार 70 वर्ष तक अज्ञात रहा है तो उसे मृत मान लिया जाता है, और बाद मेँ यह प्रकट हो जाए तो उसे सिद्ध करना पडता है.
- इसी काम मेँ जो भी पेंशनधारी होती हैं उन्हें जीवित होने का लिखित स्व-प्रमाण देना पडता है.
- जो अपराधी विदेश मेँ भाग जाते है, तो भारत सरकार उसे नोटिस देती है, जो प्रत्यर्पण संधि के अनुरुप होगा.
दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship)
अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद को नागरिकता से संबंध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है. तदनुसार, संसद मेँ 1955 मेँ नागरिकता अधिनियम लागू किया.
अनुच्छेद 9 के कथानुसार, नागरिकता का अर्थ पूर्ण नागरिकता है. संविधान में बँटी हुई निष्ठा को स्वीकृति नहीँ देता. भारतीय न्यायालयों ने नियमित रुप से दोहरी नागरिकता को अस्वीकार किया है. नागरिकता अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के साथ साथ अन्य देश के संविधान के प्रति निष्ठावान नहीँ हो सकता.
| प्रवासी भारतीयोँ को मत देने का हक़ देने का विचार विदेश मेँ रह रहे भारतीय (एन.आर.आई) को दोहरी नागरिकता के उपहार के बाद सरकार द्वारा उन्हें मतदान का अधिकार देने का भी निर्णय लिया गया है. इसके लिए पढ़ें- मताधिकार व इसके सिद्धांत, विशेषताएं और भारत में मतदान » Piyadassi |
यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह भारतीय नागरिक स्वतः खो देता है. उदाहरणार्थ, कोई शिशु जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक है, किसी दूसरे देश मेँ जन्म लेता है और व्यस्क होने पर उस देश की नागरिकता का परित्याग नहीँ करता, तो वह भारत की नागरिकता को देता है. दोहरी नागरिकता के निषेध का कारण यह है कि नागरिकता से कुछ कर्तव्य अपेक्षित है, यथा- आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना मे सेवा प्रदान करना.
विदेशियोँ को अप्राप्त अधिकार
भारत में रह रहे विदेशियों को संविधान में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते है. इसका मूल कारण उनका भारत का नागरिक न होना हैं.
- धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान या इनमे से किसी आधर पर विभ्र्द न किये जाने का अधिकार (अनुच्छेद 15).
- लोक नियोजन के विषय मेँ अवसर की समता का अधिकार (अनुच्छेद 16).
- अनुच्छेद 19 के तहत, 6 आधारभूत स्वतंत्रताओं का अधिकार.
- मतदान का अधिकार.
- अनुच्छेद 29 व 30 मेँ प्रदत्त सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार.
- कतिपय पदों (यथा-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यो के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इत्यादि) पर आसीन होने का अधिकार.
- केंद्र मेँ किसी भी सदन अथवा राज्य स्तर पर चुनाव लड़ने तथा चुने जाने का अधिकार द्वारा विनियमन किया जाना.
भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005
- भारतीय मूल के लोगोँ को दोहरी नागरिकता देने संबंधी भारतीय नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005, नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित करता है जिसके अंतर्गत नागरिकता अधिनियम, 1955 की चौथी अनुसूची को निकाल दिया गया है.
- इसके अंतर्गत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशो मेँ 26 जनवरी, 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं.
- किसी अपराध मेँ लिप्त या संदिग्ध आचारण वाले प्रवासी भारतीयोँ को दोहरी नागरिकता नहीँ मिल सकेगी.
- दोहरी नागरिकता के आधार पर प्रवासी मतदान मेँ भाग नहीँ ले सकते है, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद के चुनाव मेँ भाग नहीँ ले सकते है और न ही किसी संवैधानिक पद, जैसे – राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकते हैं.
नागरिकता और मतदाता सूची पुनरीक्षण
नागरिकता पुनरीक्षण और मतदाता सूची पुनरीक्षण दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, हालांकि ये संबंधित हैं. हाल ही में बिहार में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के तहत इस पर काफी चर्चा हुई है.
नागरिकता पुनरीक्षण (Citizenship Review)
नागरिकता पुनरीक्षण का अर्थ है किसी व्यक्ति के नागरिकता के दर्जे की वैधता की जांच करना. यह प्रक्रिया आमतौर पर केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) के अधिकार क्षेत्र में आती है. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, नागरिकता खोने या प्राप्त करने के प्रावधानों का पुनरीक्षण किया जाता है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र व्यक्ति ही देश के नागरिक हों.
मतदाता सूची पुनरीक्षण (Electoral Roll Revision)
मतदाता सूची पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत की जाती है. इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, ताकि इसमें केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हों, और डुप्लिकेट या अपात्र नामों को हटाया जा सके. यह नागरिकों के मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है.
बिहार में SIR और इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान
बिहार में हाल ही में हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) ने नागरिकता पुनरीक्षण और मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच के अंतर को स्पष्ट किया.
निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को “अत्यधिक त्रुटिपूर्ण” पाया, जिसमें बड़ी संख्या में नाम डुप्लिकेट थे या नागरिकता संदिग्ध थी. इसके बाद, आयोग ने SIR अभियान शुरू किया. इस अभियान के तहत, बिहार में 2003 के बाद से मतदाता बने लोगों से उनकी नागरिकता का प्रमाण मांगा गया.
- SIR की प्रक्रिया:
- मतदाता सूची से संदिग्ध नामों की पहचान की गई.
- संदिग्ध लोगों को नोटिस भेजकर नागरिकता के दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया.
- जो लोग दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए.
विवाद (Dispute)
इस प्रक्रिया पर राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया. कई याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग को सीधे तौर पर नागरिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार गृह मंत्रालय के पास है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत मतदाता सूची को संशोधित करने और त्रुटियों को दूर करने का अधिकार है. हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह केवल पहचान के लिए एक दस्तावेज है. साथ ही, 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के अधिकार पर मुहर लगाई कि वह मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर सकता है, लेकिन यह भी कहा कि नागरिकता का निर्धारण एक अलग और लंबी प्रक्रिया है जिसका पालन करना आवश्यक है.
संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान में नागरिकता और चुनाव से संबंधित प्रावधान अलग-अलग हैं.
- नागरिकता: संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं. अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है. इसी के तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया गया है.
- मतदान का अधिकार: अनुच्छेद 326 के अनुसार, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे. इसके तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो मतदाता सूची में पंजीकृत है, उसे मतदान का अधिकार है.
- निर्वाचन आयोग के अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने, मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार है. इसी शक्ति का उपयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य किया.