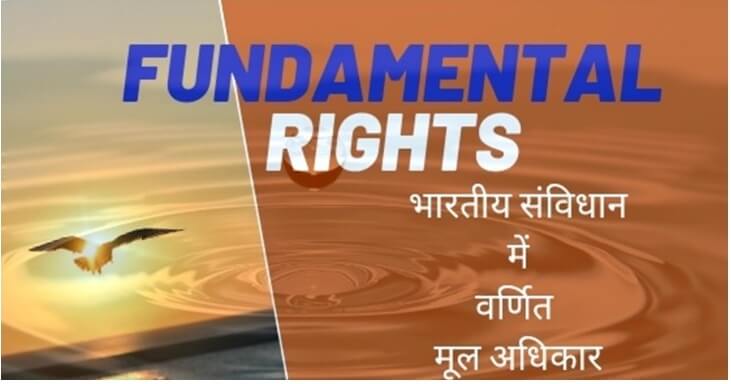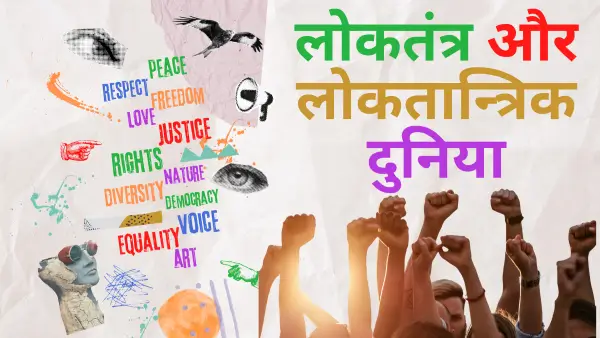भारतीय संस्कृति व समाज की विशिष्ट या अनन्य विशेषता विविधता में एकता है. उसकी एक विशेषता ने ही इसे अनन्त काल से अब तक जीवित रखा है. भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से अनेक भिन्नतायें पाई जाती है. इन मिन्नताओं के होते हुए भी सम्पूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं.
इस सन्दर्भ में सर हर्बर्ट रिजले ने उचित ही लिखा “भारत में धर्म, रीति-रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एकरूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है. वास्तव विचारों तथा में भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती.”
सी० ई० एम० जोड ने विविधता में एकता के सम्बन्ध में लिखा है, “जो भी कारण जातियों के अनेक तत्त्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है.”
विविधता में एकता के प्रकार (Types of Unity in Deversity in Hindi)
भारत के समाज व संस्कृति के जिन क्षेत्रों में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं वे क्षेत्र निम्नलिखित हैं:–
(1) ऐतिहासिक विविधता में एकता (Unity in Historical Diversity)
प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न धर्मों एवं प्रजातियों के लोग आते रहे हैं. उनके इतिहास में भिन्नता का होना स्वाभाविक ही है. किन्तु जब वे भारत में स्थायी रूप से बस गये तो उन्होंने एक समन्वित संस्कृति एवं सामान्य इतिहास का निर्माण किया. मुगल, तुर्क, अफ़गान, शक व पारसियों का भारत आना और यहाँ के समाज में घुलमिलकर रहना इसका बेहतरीन उदाहरण है.
(2) प्रजातीय विविधता में एकता (Unity in Racial Diversity)
प्रजातीय दृष्टि से भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायबघर अथवा द्रवण-पात्र कहा गया है. जहाँ विश्व की प्रमुख तीन प्रजातियों- श्वेत, पीत एवं काली तथा उनकी उप-शाखाओं के लोग निवास करते हैं. उत्तरी भारत में आर्य प्रजाति और दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति के लोगों का बाहुल्य है. प्रजातीय भिन्नता होने पर भी यहाँ अमेरिका व अफ्रीका की भाँति प्रजातीय संघर्ष एवं टकराव नहीं हुआ है, वरन् उनमें पारस्परिक सद्भाव और सहयोग ही रहा है. भारत में विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण भी हुआ है, अतः इसे प्रजाति मिश्रण का द्रवण- पात्र भी कहते हैं.
(3) भौगोलिक विविधता में एकता (Unity in Geographical Diversity)
भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विभिन्नतायें व्याप्त हैं. यह उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबन्धों की जलवायु का प्रदेश है. चेरापूँजी में वर्ष में लगभग 600 इंच वर्षा होती है तो दूसरी ओर राजस्थान के थार के मरुस्थल में 5 इंच से भी कम वर्षा होती है. अधिक उपजाऊ तथा कम उपजाऊ दोनों ही प्रकार के प्रदेश यहाँ पाये जाते हैं. उत्तर में हिमालय पर्वत हैं, उसके बाद मैदानी भाग हैं और दक्षिण भारत एक पठारी एवं प्रायद्वीपीय प्रदेश है. इन विविधताओं के बावजूद भी सम्पूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है.
यह भौगोलिक व मौसूम की विविधता ने जरूरत के हिसाब से क्षेत्रीय पहनावा, जीवनशैली, खानपान और आजीविका को आकार आकार दिया है. लेकिन, देश की प्राकृतिक सीमाओं ने इसे अन्य देशों से अलग किया है. इस विभाजन ने देशवासियों में एक क्षेत्र में निवास करने की भावना जागृत की है. इस तरह उनमें एकता एवं जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम पैदा किया है.
“माता भूमि पुत्रों अहं पृथिव्या” (पृथ्वी मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ) “जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ (जिस धरती पर जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी प्यारी आदि अवधारणाओं ने इस देश में एकता, राष्ट्र भक्ति, त्याग और बलिदान की भावना पैदा की है.
(4) धार्मिक विविधता में एकता (Unity in Religious Diversity)
भारत विभिन्न धर्मों की जन्म भूमि है. हिन्दू, जैन, बौद्ध एवं सिख धर्मों का उदय भारत में हुआ तथा इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशों से यहाँ आये. प्रत्येक धर्म में कई मत-मतान्तर एवं सम्प्रदाय पाये जाते हैं और उनके नियमों एवं मान्यताओं में अनेक विविधताएँ हैं. इतना होने पर भी विभिन्न धर्मावलम्बी सदियों से भारत में एक साथ रह रहे हैं. ऊपरी तौर पर इन धर्मों में हमें भिन्नता दिखाई देती है, किन्तु सभी के मूल सिद्धान्तों में समानता है.
सभी धर्म अध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, सत्य, अहिंसा, आदि में विश्वास करते हैं. देश के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों ने विभिन्न धर्म के लोगों में एकता का संचार किया तथा धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना ने भी एकीकरण में योग दिया.
प्राचीन काल से ही भारत में धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में आत्मसात एवं पर- संस्कृतिग्रहण की प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तन होता रहा है. आर्य एवं द्रविड़ संस्कृतियों का यहाँ पूर्व-काल में समन्वय हुआ, उसके बाद इस्लाम एवं ईसाई संस्कृतियों का.
मुगल शासकों के समय में हिन्दू एवं इस्लाम धर्मों का समन्वय हुआ. अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया जिसमें हिन्दू एवं इस्लाम का समन्वय था. नानक एवं कबीर पन्थ में भी ऐसा ही समन्वय है. हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं सिख धर्मों के लोगों के देश के विभिन्न भागों में साथ-साथ रहने से भारत में एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ.
(5) सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता में एकता (Unity in Socio-Cultural Diversity)
भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवार, विवाह, रीति-रिवाजों, वस्त्र-शैली आदि में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है, उसके बावजूद भी भारतीय समाज व्यवस्था एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं.
संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति-प्रथा, ग्राम पंचायत, गोत्र व वंश-व्यवस्था भारतीय समाज के आधार रहे हैं. अध्यात्मवाद, ईश्वर, धार्मिक कर्मकाण्ड, पुनर्जन्म, स्वर्ग-नरक आदि में सभी भारतीयों का विश्वास है. सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों एवं त्योहारों का प्रचलन सामान्य रूप से सारे देश में रहा है.
हिन्दुओं एवं मुसलमानों में परस्पर कला, धर्म, खान-पान, वस्त्र-शैली, भाषा एवं साहित्य आदि के क्षेत्र में आदान-प्रदान होने के कारण समन्वय स्थापित हुआ है. भारत के विभिन्न लोगों में हिन्दुओं के तीर्थ स्थल हैं. हिन्दुओं के अतिरिक्त जैन, बौद्ध और सिख धर्मों के पवित्र स्थल भी यहाँ विद्यमान हैं. सम्पूर्ण देश में शास्त्रीय संस्कृति के कुछ विशिष्ट तत्त्व पाये गये हैं.
भारत की सांस्कृतिक विरासत कई संस्कृतियों के समन्वय का एक जीवित उदाहरण है. वर्तमान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है. भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा विभिन्न समुदायों के शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करता है. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा बिना भेदभाव के सभी लोगों के जीवन स्तर के उन्नत बनाने का यहाँ प्रयत्न किया गया है.
(6) भाषायी विविधता में एकता (Unity in Language Diversity)
भारत में कई प्रकार की भाषाओं एवं बोलियों का प्रचलन आदिकाल से ही रहा है. हिन्दी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, उड़िया, असमी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं मलयालम आदि भाषायें भारत में विभिन्न भागों में बोली जाती है. भाषा की इस विविधता के बावजूद भी सभी भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव होने के कारण उनमें एकरूपता पायी जाती है. एक भाषा बोलने वाले लोग देश के विभिन्न भागों में बसे पैदा हैं.
भारतीय संविधान में देश के विभिन्न इलाकों के 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है. देश में 1,600 से अधिक बोलियां भी प्रचालन में हैं. 1956 में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया. इस तरह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय पहचान और भाषाओं को संरक्षित रखना सुनिश्चित किया गया.
त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को हिन्दी, अंग्रेजी एवं एक अन्य प्रान्त की भाषा सिखायी जाती है. इससे विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच एकता के भाव भारतीय संविधान में भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है.
(7) राजनीतिक विविधता में एकता (Unity in Political Diversity )
राजनीतिक दृष्टि से भी भारत में विविधता और एकता रही है. अंग्रेजों के पूर्व सामन्तों के विभिन्न राज्य रहे हैं. प्रथम बार अंग्रेजों के समय में सारे देश पर एक ही सत्ता का शासन कायम हुआ. स्वतन्त्रता के बाद सारे देश में एक ही प्रजातन्त्रीय सरकार की स्थापना हुई विभिन्न प्रान्तों में प्रान्तीय सरकारें हैं. दूसरी ओर प्रान्तों ने मिलकर भारत संघ का निर्माण किया है. इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भी भारत एक इकाई है. इस एकता का प्रदर्शन चीन एवं पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान हुआ जब सभी भारतवासी एक राष्ट्र के रूप में उठ खड़े हुए.
सम्पूर्ण देश के लिए एक ही संविधान बनाया गया है. संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, विशेषाधिकारों का अन्त कर दिया है, समाज के पिछड़े एवं दुर्बल वर्गों तथा निम्न जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है. देश में समान कानून की व्यवस्था की गई है. इन सब प्रयत्नों से देश एकता के सूत्र में बँध गया है.
विविधता में एकता को मज़बूत करने के उपाय
भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता से है. यह एक ऐसी अवधारणा है जो देश के अलग-अलग धर्म, भाषा, जाति, और संस्कृति के लोगों को एक साथ जोड़ती है. इस एकता को और भी मज़बूत बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं:
1. संवैधानिक सुरक्षा उपाय
भारतीय संविधान देश के एकता की नींव रखता है. हमारे संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो हर नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा देते हैं:
- अनुच्छेद 14: यह सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है. इसका मतलब है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, चाहे उसकी जाति, धर्म, या लिंग कुछ भी हो.
- अनुच्छेद 15: यह धर्म, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध करता है. यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को इन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों या सुविधाओं से वंचित न किया जाए.
- अनुच्छेद 25-28: ये अनुच्छेद नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं. हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है. यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता (secularism) की एक मज़बूत मिसाल है.
- अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रावधान (अनुच्छेद 29 और 30): अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, जिससे उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार मिलता है. वहीं, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है. ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय भी मुख्यधारा में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें.
2. शिक्षा और जागरूकता
शिक्षा एक शक्तिशाली माध्यम है जो बच्चों को बचपन से ही विविधता का सम्मान करना सिखा सकती है.
- मूल्य-आधारित शिक्षा: स्कूलों में ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना ज़रूरी है जो सहिष्णुता, करुणा और सम्मान जैसे मूल्यों पर ज़ोर दे. पाठ्यक्रम में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और क्षेत्रों की कहानियों को शामिल करने से बच्चों में आपसी समझ बढ़ती है.
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम: ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ जैसी योजनाएं विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देती हैं. इस पहल के तहत, राज्य एक-दूसरे की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को सीखते हैं, जिससे उनके बीच आपसी जुड़ाव बढ़ता है. स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना ज़रूरी है जहाँ छात्र दूसरे राज्यों के छात्रों के साथ मिलकर काम करें.
3. सरकारी पहल
सरकार ने भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
- राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council – NIC): यह एक सलाहकार निकाय है जिसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है.
- राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (National Foundation for Communal Harmony – NFCH): यह संस्था सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और हिंसा से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने का काम करती है.
- कल्याणकारी योजनाएं: ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड‘ जैसी योजनाएं क्षेत्रीय असमानताओं को कम करती हैं. यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकता है, जिससे लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति जुड़ाव की भावना मज़बूत होती है.
4. सांस्कृतिक समारोह और उत्सव
त्योहार और समारोह लोगों को एक साथ लाते हैं और उनमें एकता की भावना जगाते हैं.
- राष्ट्रीय त्योहार: स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) जैसे राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में मनाए जाते हैं. इन दिनों होने वाली परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत की विविधता को दर्शाते हैं, जहाँ विभिन्न राज्यों की झाँकियाँ और लोकनृत्य एक ही मंच पर प्रदर्शित होते हैं.
- क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहार: दीवाली, ईद, क्रिसमस, और गुरुपर्व जैसे त्योहार सभी समुदाय मिलकर मनाते हैं. ये आपसी सौहार्द और जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं. इसके अलावा, लोहड़ी (पंजाब), ओणम (केरल), बिहू (असम) और पोंगल (तमिलनाडु) जैसे क्षेत्रीय त्योहारों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से हर क्षेत्र का सम्मान बढ़ता है.
5. मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका
मीडिया और नागरिक समाज इस प्रक्रिया में एक सेतु का काम करते हैं.
- मीडिया की भूमिका: मीडिया सकारात्मक कहानियों को सामने ला सकता है. यह उन प्रयासों को उजागर कर सकता है जहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलकर काम करते हैं या एक-दूसरे की मदद करते हैं. उदाहरण के लिए, अगर किसी आपदा के समय सभी समुदाय एकजुट होकर राहत कार्य में मदद करते हैं, तो ऐसी कहानियों को मीडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए.
- गैर-सरकारी संगठन (NGO) और नागरिक समाज: ये संगठन जमीनी स्तर पर काम करते हैं. NGOs और समाज के संगठन असमानता और भेदभाव के मुद्दों को सुलझाने में मदद करते हैं. ये विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित करके गलतफहमियों को दूर करने का काम करते हैं, जिससे समाज में शांति और भाईचारा बना रहता है.
इन सभी प्रयासों से भारत अपनी अतुलनीय विविधता को बनाए रखते हुए एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है.
विविधता में एकता ही भारत की शक्ति का आधार कैसे हैं?/ इसका महत्व
भारत की “विविधता में एकता” सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यह देश के अस्तित्व, सामाजिक संरचना और प्रगति का मूल सिद्धांत है. यह विचार भारत की अनूठी पहचान है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. यह विविधता हमें कमज़ोर नहीं करती, बल्कि हमें अधिक मज़बूत बनाती है. आइए इसके महत्व को विस्तार से समझते हैं.
1. सामाजिक सद्भाव और आपसी सम्मान
विविधता में एकता का सबसे बड़ा महत्व सामाजिक सद्भाव में है. जब अलग-अलग समुदायों के लोग एक-दूसरे के रीति-रिवाजों और जीवन शैली को समझते हैं, तो उनमें आपसी सम्मान और सहिष्णुता की भावना बढ़ती है. यह समझ समाज में संघर्ष की संभावनाओं को कम करती है और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है. भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व, सभी समुदाय एक साथ मनाते हैं, जो इस सद्भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है.
2. मजबूत लोकतंत्र और समावेशी शासन
एक विविध समाज में, विभिन्न समूहों और समुदायों के विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है. भारत की निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक दल इस विविधता को दर्शाते हैं. क्षेत्रीय दलों का उदय, विभिन्न राज्यों की मांगों को पूरा करने वाली नीतियाँ और भाषाई पहचान को सम्मान देना हमारे लोकतंत्र की गहराई को दर्शाता है. यह समावेशी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवाज़ों को सुना जाए, जिससे एक न्यायपूर्ण और सशक्त शासन प्रणाली बनती है.
3. समृद्ध सांस्कृतिक विरासत
भारत की सांस्कृतिक विरासत इसकी विविधता का ही परिणाम है. यहाँ विभिन्न परंपराओं, कला रूपों, नृत्यों, संगीत और व्यंजनों का अद्भुत मिश्रण है. यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हमारे धरोहर स्थल, जैसे अजंता-एलोरा की गुफाएँ और ताजमहल, विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाते हैं. इसके अलावा, योग और आयुर्वेद जैसी प्राचीन भारतीय प्रथाओं ने वैश्विक पहचान हासिल की है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है. यह समृद्ध धरोहर न केवल हमारी पहचान है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भारत का गौरव भी बढ़ाती है.
4. आर्थिक विकास में योगदान
विविधता आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है. भारत में प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट कलाएँ, शिल्प और संसाधन हैं. उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत के मसाले, राजस्थान के हस्तशिल्प और पूर्वोत्तर के चाय बागान. ये सभी मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. पर्यटन उद्योग, जो भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता पर निर्भर करता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है. यह विविधता विभिन्न विचारों और कौशलों को एक साथ लाती है, जिससे नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है.
5. वैश्विक प्रभाव और सॉफ्ट पावर
भारत की विविधता उसे वैश्विक मंच पर एक अनूठी स्थिति प्रदान करती है. हमारा समावेशी और बहुलवादी चरित्र दुनिया के लिए एक उदाहरण है. भारत की संस्कृति, सिनेमा (बॉलीवुड), और भोजन ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है. यह “सॉफ्ट पावर” का एक शक्तिशाली स्रोत है, जो बिना किसी बल प्रयोग के अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करता है. हमारी वसुधैव कुटुम्बकम् (पूरी दुनिया एक परिवार है) की अवधारणा इसी विविधता में एकता की भावना का विस्तार है.
संक्षेप में, भारत में विविधता में एकता का सिद्धांत न केवल हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है, बल्कि यह हमारी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का भी आधार है. यह एक ऐसी ताकत है जो हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है.
‘विविधता में एकता‘ की चुनौतियाँ
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ‘विविधता में एकता’ एक आदर्श है, जिसे बनाए रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ये चुनौतियाँ न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को भी कमजोर करती हैं. आइए, इन चुनौतियों को विस्तार से समझते हैं.
1. सांप्रदायिकता और धार्मिक संघर्ष
भारत की एकता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सांप्रदायिकता है. विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समय-समय पर होने वाले तनाव, धार्मिक ध्रुवीकरण और घृणास्पद भाषण सामाजिक शांति को बाधित करते हैं. कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूह अपने स्वार्थ के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं, जिससे भीड़ हिंसा और आपसी अविश्वास बढ़ता है. यह स्थिति भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमजोर करती है और ‘सबका साथ, सबका विकास’ जैसे सिद्धांतों के लिए खतरा पैदा करती है.
2. क्षेत्रवाद और भाषाई संघर्ष
क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जहाँ लोग अपनी क्षेत्रीय या भाषाई पहचान को राष्ट्रीय पहचान से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं. भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने के बावजूद, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान की मांगें अक्सर राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बनती हैं. उदाहरण के लिए, गोरखालैंड और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांगें यह दर्शाती हैं कि कुछ समूह अपनी अनूठी पहचान और विकास के लिए अलग राज्य चाहते हैं. ऐसे आंदोलनों से कभी-कभी हिंसक संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकता है.
3. आर्थिक असमानताएँ
भारत में आर्थिक विकास असमान रहा है, जिसके कारण कुछ राज्यों और क्षेत्रों ने दूसरों की तुलना में अधिक प्रगति की है. यह असमानता न केवल क्षेत्रीय असंतोष को बढ़ावा देती है, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं को भी जन्म देती है. जब लोग अपने क्षेत्र में अवसर नहीं पाते, तो वे बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे सामाजिक-आर्थिक तनाव बढ़ता है. यह आर्थिक असमानता विविधता में एकता की भावना को कमजोर करती है, क्योंकि लोग अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरे क्षेत्रों या समुदायों को दोषी ठहराते हैं.
4. जातिगत और सामाजिक असमानताएँ
यद्यपि भारतीय संविधान ने जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और भेदभाव को दंडनीय अपराध घोषित किया है, फिर भी जातिगत असमानताएँ समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं. जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव और बहिष्कार आज भी कई रूपों में मौजूद है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में. यह सामाजिक असमानता विभिन्न समुदायों के बीच दरार पैदा करती है और हाशिए पर रहने वाले समूहों को विकास की मुख्यधारा से अलग कर देती है. आरक्षण जैसी नीतियों के बावजूद, जातिगत पहचान आज भी कई सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती है.
5. राजनीतिक शोषण और पहचान की राजनीति
राजनीति में ‘पहचान की राजनीति’ एक बड़ी चुनौती है. जब राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर लोगों को विभाजित करते हैं, तो यह समाज में विभाजन को गहरा करता है. राजनीतिक नेता अक्सर ऐसे मुद्दों को उभारते हैं जो लोगों को एकजुट करने के बजाय उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं. इस तरह की राजनीति से ‘विविधता में एकता’ का मूल विचार कमजोर होता है और राष्ट्रीय हित की बजाय व्यक्तिगत या समूह हित को बढ़ावा मिलता है.
इन चुनौतियों का समाधान केवल कानूनों और नीतियों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और सभी समुदायों के बीच आपसी संवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है. इन चुनौतियों पर काबू पाकर ही भारत अपनी विविधता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकता है.