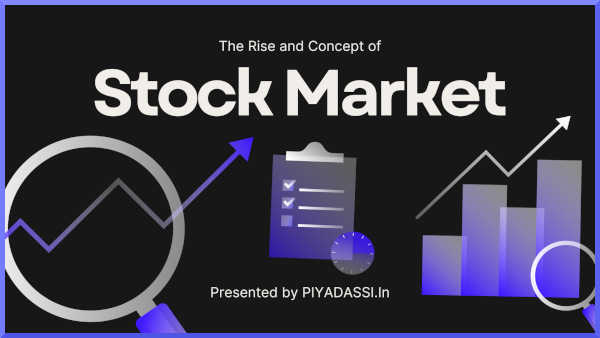आईपीओ यानि इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) एक निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक बाज़ार में प्रवेश करने का पहला कदम है. इसे प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के नाम से भी जाना जाता है. यह प्रक्रिया कंपनी को आम जनता से पूंजी जुटाने, ब्रांड की दृश्यता और विश्वसनीयता बढ़ाने तथा शुरुआती निवेशकों को निकास का अवसर प्रदान करती है. भारतीय शेयर बाज़ार आईपीओ का परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है. इस लेख में आईपीओ की गहन समीक्षा की गई है.
2024 में भारतीय आईपीओ बाज़ार ने विश्व में रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन किया. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसे नियामक निकायों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने आईपीओ बाज़ार को निवेशकों के लिए अधिक कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया है. लेकिन, हर आईपीओ एक लाभकारी सौदा नहीं होता है. इसमें अंतर्निहित जोखिम शामिल होते हैं, जैसे कि अस्थिरता और ओवरवैल्यूएशन की संभावना.
आईपीओ क्या है? (What is an IPO)
इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक निजी कंपनी पहली बार इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए आम जनता को अपने शेयर बेचती है. इससे संबंधित निजी कंपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली इकाई में बदल जाती है. आईपीओ के बाद आम निवेशक उस कंपनी के स्वामित्व का एक हिस्सा शेयर के रूप में खरीद सकते हैं. निवेशकों को कंपनी के विकास का लाभ प्राप्त होता है. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के विस्तार, नवाचार या ऋण चुकाने के लिए आवश्यक धन जुटाना होता है.
आईपीओ का उद्देश्य और महत्व
इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूंजी जुटाना है. यह रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने, कर्ज़ों को चुकाने, नई मशीनरी खरीदने या व्यावसायिक विस्तार करने जैसे कार्यों के लिए जुटाई जाती है. शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी के दृश्यता, विश्वसनीयता और ब्रांड इक्विटी में उल्लेखनीय वृद्धि होती है. सार्वजनिक पेशकश को पूरा करने के लिए कंपनियों को सेबी (SEBI) जैसी नियामक संस्थाओं की गहन जाँच प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है. यह नियामक स्वीकृति एक तरह का बाज़ार प्रमाणन है जो कंपनी की वित्तीय अखंडता और पारदर्शिता को प्रमाणित करता है.
बढ़ी हुई विश्वसनीयता अक्सर कंपनियों को निजी समकक्षों की तुलना में अधिक अनुकूल क्रेडिट उधार की स्थितियाँ प्रदान करती है. साथ ही, भविष्य में अधिग्रहणों के लिए स्टॉक को भुगतान के साधन के रूप में उपयोग करने में मदद करती है. इस प्रकार, आईपीओ एक सकारात्मक चक्र शुरू करता है जहाँ पूंजी जुटाना और ब्रांड निर्माण एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं.
उद्यम पूंजीपति (Venture Capitalists) और एंजेल निवेशक अक्सर स्टार्टअप में शुरुआती चरण में भारी निवेश करते हैं. उनका निवेश तभी फलदायक होता है जब उन्हें अपनी हिस्सेदारी बेचकर लाभ कमाने का मौका मिले. एक सफल आईपीओ इस निकास को संभव बनाता है, जिससे उनके निवेश चक्र पूरे होते हैं और उन्हें अन्य नई कंपनियों में फिर से निवेश करने के लिए आवश्यक पूंजी मिलती है. इस तरह, एक जीवंत आईपीओ बाज़ार न केवल बड़ी कंपनियों के लिए, बल्कि पूरे स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक जीवनरेखा का काम करता है.
आईपीओ में निवेश के अवसर
निवेशक आईपीओ में भाग लेने के कई कारण होते हैं. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह उन्हें एक ऐसे व्यवसाय में हिस्सेदारी खरीदने का अवसर प्रदान करता है. सफल आईपीओ में निवेश से अक्सर लिस्टिंग के दिन ही उच्च रिटर्न और पूंजीगत लाभ की संभावना रहती है. इसे “लिस्टिंग गेन” कहा जाता है. इसके अलावा, आईपीओ में निवेश करना किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक प्रभावी तरीका भी है. यह उन्हें विभिन्न उद्योगों की नई कंपनियों में छोटे शेयरों के माध्यम से निवेश करने की अनुमति देता है.
ऐतिहासिक विकास और वर्तमान
भारतीय पूँजी बाज़ार का इतिहास काफी पुराना है. भारत में ही एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), की स्थापना 1875 में हुई थी. लेकिन, भारतीय बाज़ार में आईपीओ के आधुनिक युग की शुरुआत 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऐतिहासिक आईपीओ से मानी जाती है. रिलायंस ने इस सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 2.8 मिलियन शेयर जारी किए. इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी को भारत में “इक्विटी कल्चर” की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, भारतीय आईपीओ बाज़ार में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया. 2021 में भारतीय कंपनियों ने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से अब तक की सबसे अधिक राशि जुटाई.
वर्ष 2024 भारतीय आईपीओ बाज़ार के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है. एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस वर्ष इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के मामले में वैश्विक लीडर के रूप में उभरा, जहाँ दुनिया के कुल पब्लिक इश्यू में देश की हिस्सेदारी 23% रही. कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से $19.5 बिलियन (लगभग ₹1.69 लाख करोड़) से अधिक की रिकॉर्ड पूंजी जुटाई. इस दौरान, हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, जिसका आकार ₹27,870 करोड़ था.
आईपीओ बाज़ार में इस तेजी का कारण व्यापक आर्थिक कारक हैं. बाज़ार विश्लेषण से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के भारी निवेश, कॉर्पोरेट कंपनियों की अच्छी कमाई और केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी ने 2020 की दूसरी छमाही से बाज़ार में मजबूती लाई है. साथ ही, कोविड-19 महामारी के दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी. उसके बाद आर्थिक गतिविधियों में नए उछाल ने आईपीओ बाजार को आकर्षक बना दिया. यह दर्शाता है कि आईपीओ की सफलता केवल किसी एक कंपनी की वित्तीय स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह देश की समग्र अर्थव्यवस्था और बाज़ार के बुलिश रुझान से भी गहराई से जुड़ी हुई है.
इस अवधि में एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति एसएमई (SME) आईपीओ में मजबूत वृद्धि है. 2024 में कुल 268 आईपीओ में से 178 एसएमई कंपनियों द्वारा लाए गए थे. यह एसएमई क्षेत्र के बढ़ते महत्त्व और निवेशकों के बीच छोटे उद्यमों में निवेश की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत देता है.
हालांकि, यहाँ एक विरोधाभास भी देखने को मिलता है. एक तरफ तो कुल जुटाई गई पूंजी रिकॉर्ड स्तर पर थी, दूसरी तरफ सार्वजनिक होने वाली कंपनियों के औसत बाज़ार पूंजीकरण में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है. यह 2021 में ₹3,800 करोड़ से घटकर 2023 में ₹2,770 करोड़ हो गया. यह आँकड़ा दर्शाता है कि बाज़ार अब अधिक संख्या में छोटी कंपनियों को समायोजित कर रहा है. इससे निवेशकों के लिए जोखिम भी बढ़ गया है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में अस्थिरता और प्रदर्शन की अनिश्चितता अधिक होती है.
आईपीओ के प्रकार
आईपीओ के शेयरों की कीमत तय करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियों का उपयोग किया जाता है: निश्चित मूल्य निर्गम और बुक बिल्डिंग.
निश्चित मूल्य निर्गम (Fixed Price Issue)
निश्चित मूल्य निर्गम एक सीधी और पारंपरिक विधि है जहाँ कंपनी सार्वजनिक पेशकश खोलने से पहले ही प्रति शेयर एक निश्चित कीमत तय कर देती है. इस कीमत को प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है. यह पूरी आईपीओ प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहती है. इस प्रकार के आईपीओ निवेशकों के लिए पारदर्शिता और पूर्वानुमान में आसानी प्रदान करती है. हालांकि, इसमें एक बड़ा नुकसान भी है. चूँकि कीमत पहले से तय होती है, यह बाज़ार में शेयरों की वास्तविक मांग को प्रतिबिंबित नहीं कर पाती. इससे कंपनी द्वारा अपने निर्गम को अंडरप्राइस या ओवरप्राइस करने का जोखिम रहता है.
बुक बिल्डिंग (Book Building Issue)
बुक बिल्डिंग एक अधिक लचीली और बाज़ार-संचालित मूल्य निर्धारण प्रक्रिया है. इस विधि में, कंपनी एक निश्चित कीमत तय करने के बजाय शेयरों के लिए एक प्राइस बैंड (जैसे ₹90 से ₹100 प्रति शेयर) निर्धारित करती है. इस बैंड में निचला मूल्य को फ्लोर प्राइस और ऊपरी मूल्य को कैप प्राइस कहा जाता है. निवेशक इस निर्धारित सीमा के भीतर अपनी बोलियाँ लगाते हैं. अंत में, बोली अवधि के दौरान प्राप्त मांग के आधार पर अंतिम “कट-ऑफ” कीमत निर्धारित की जाती है. इसी कीमत पर शेयरों का आवंटन होता है.
बुक बिल्डिंग से उचित व बेहतर मूल्य की खोज हो पाती है. यह तरीका शेयर का सही और निष्पक्ष मूल्य निर्धारित करने में मदद करता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर निवेशकों की मांग पर आधारित होता है.
तुलनात्मक विश्लेषण
| पहलू | निश्चित मूल्य निर्गम | बुक बिल्डिंग |
| कीमत निर्धारण | जारीकर्ता कंपनी द्वारा पहले से निर्धारित और स्थिर. | निवेशक की मांग के आधार पर एक प्राइस बैंड के भीतर तय. |
| मूल्य खोज | बाज़ार की वास्तविक मांग को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता. | बाज़ार-संचालित, जो उचित मूल्य खोज को संभव बनाता है. |
| पारदर्शिता | निवेशकों के लिए स्पष्ट और पूर्वानुमान योग्य. | उच्च पारदर्शिता, क्योंकि बिडिंग रुझान वास्तविक समय में देखे जा सकते हैं. |
| जोखिम | ओवरप्राइसिंग या अंडरप्राइसिंग का जोखिम अधिक. | ओवरप्राइसिंग का जोखिम कम, क्योंकि अंतिम कीमत मांग पर आधारित होती है. |
| आवेदन प्रक्रिया | आवेदन के समय पूरा भुगतान आवश्यक. | आवेदन के समय केवल आवेदन राशि का भुगतान या खाता अवरुद्ध करना आवश्यक. |
भारत में आईपीओ लाने की प्रक्रिया
भारत में आईपीओ लाने की प्रक्रिया एक जटिल और बहु-स्तरीय प्रक्रिया है जो सेबी (SEBI) और अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित सख्त दिशानिर्देशों का पालन करती है. इस प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं:
- चरण 1: तैयारी और इन्वेस्टमेंट बैंक की नियुक्ति: सबसे पहले, कंपनी आईपीओ की प्रक्रिया को शुरू करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स या अंडरराइटर जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकों की एक टीम को नियुक्त करती है. यह टीम कंपनी की वित्तीय स्थिति का गहन अध्ययन करती है और एक रणनीतिक योजना तैयार करती है.
- चरण 2: डीआरएचपी (DRHP) तैयार करना और नियामक फाइलिंग: कंपनी और उसके बैंकर्स मिलकर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) नामक एक विस्तृत दस्तावेज़ तैयार करते हैं. इस दस्तावेज़ में कंपनी के वित्तीय इतिहास, व्यापार मॉडल, जोखिमों, प्रबंधन टीम और आईपीओ के उद्देश्यों का संपूर्ण विवरण होता है. यह दस्तावेज़ सेबी (SEBI) और कंपनियों के रजिस्ट्रार (RoC) के पास अनुमोदन के लिए दायर किया जाता है.
- चरण 3: स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन और रोड शो: सेबी की मंजूरी मिलने के बाद, कंपनी अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) या दोनों में आवेदन करती है. इस चरण में, कंपनी के अधिकारी संभावित निवेशकों को आकर्षित करने और आईपीओ का प्रचार करने के लिए “रोडशो” आयोजित करते हैं.
- चरण 4: बोली, आवंटन और लिस्टिंग: आईपीओ जनता के लिए निर्धारित अवधि के लिए खुलता है. निवेशक अपने डीमैट अकाउंट द्वारा शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं. भारत में, यह आवेदन प्रक्रिया अक्सर ASBA (Application Supported by Blocked Amount) के माध्यम से होती है. ASBA द्वारा आईपीओ आवंटन होने तक राशि निवेशक के खाते में अवरुद्ध रहती है.
- कई बार किसी आईपीओ की मांग अत्यधिक होती है, जिससे यह ओवरसब्सक्राइब्ड हो जाती है. इस स्थिति में शेयरों का आवंटन आवेदकों को आनुपातिक रूप से या एक लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है. आवंटन प्रक्रिया पूरी होने पर, सफल आवेदकों के डीमैट खाते में शेयर जमा किए जाते हैं. असफल आवेदकों को उनकी अवरुद्ध राशि वापस कर दी जाती है.
- चरण 5: लिस्टिंग और कारोबार: आवंटन के बाद, कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं. इसके तुरंत बाद ये शेयर सार्वजनिक रूप से ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं.
सम्बद्ध संस्थान
आईपीओ की सफल निष्पादन एक जटिल तंत्र से गुजरता है. इसमें कई प्रमुख संस्थान अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभाते हैं.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में प्रतिभूति बाज़ार का प्रमुख नियामक निकाय है. इसकी स्थापना 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी. इसका प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बाज़ार के विकास को बढ़ावा देना और धोखाधड़ी व अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को रोकना है. सेबी आईपीओ लाने की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियाँ सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करें.
मर्चेंट बैंकर और अंडरराइटर
मर्चेंट बैंकर (जिसे इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहते हैं) वह संस्था है जो पूरी आईपीओ प्रक्रिया में जारीकर्ता कंपनी को वित्तीय और कानूनी सलाह प्रदान करती है. यह बैंक डीआरएचपी तैयार करने से लेकर आईपीओ की कीमत निर्धारित करने और निवेशकों से संपर्क करने तक सभी प्रमुख कार्यों का प्रबंधन करता है.
अंडरराइटर अक्सर मर्चेंट बैंकरों का हिस्सा होते हैं. ये आईपीओ के वित्तीय जोखिम का मूल्यांकन करते हैं. वे शेयरों की मांग का विश्लेषण करते हैं. ये आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब न होने पर बचे शेयरों को खरीदने का जोखिम भी ले सकते हैं. इस प्रकार जारीकर्ता कंपनी के लिए पूंजी निवेश की गारंटी मिलती है.
रजिस्ट्रार (Registrar)
आईपीओ रजिस्ट्रार वह संस्था है जो आईपीओ आवंटन प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए ज़िम्मेदार होती है. यह बोली डेटा को मान्य करता है, विभिन्न निवेशक श्रेणियों (जैसे खुदरा, क्यूआईबी, एनआईआई) में आवंटन का निर्धारण करता है. सफल बोलीदाताओं के डीमैट खाते में शेयर जमा करता है.
ये संस्थान एक सहजीवी तंत्र का निर्माण करते हैं. सेबी बाज़ार में विश्वास और सुरक्षा के लिए नियामक ढाँचा स्थापित करता है. अंडरराइटर इस विश्वास का लाभ उठाकर कंपनी को सफलतापूर्वक पूंजी जुटाने में मदद करते हैं. रजिस्ट्रार एक निष्पक्ष और पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया सुनिश्चित करके निवेशकों के हितों की रक्षा करते हैं. यह सहजीवी संबंध भारतीय पूँजी बाज़ार की दक्षता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.
भारत में आईपीओ से जुड़े कानून
भारतीय आईपीओ बाज़ार को कई कानूनी और नियामक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका उद्देश्य बाज़ार की अखंडता बनाए रखना और निवेशकों की सुरक्षा करना है.
निर्धारित पात्रता
आईपीओ जारी करने की इच्छुक कंपनी को सेबी द्वारा निर्धारित कुछ वित्तीय मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है. इनमें पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम ₹3 करोड़ की निवल मूर्त परिसंपत्तियाँ, कम से कम ₹1 करोड़ का निवल मूल्य और पिछले पाँच वर्षों में से किसी तीन वर्ष में कम से कम ₹15 करोड़ का औसत परिचालन लाभ शामिल है.
सेबी ने बाज़ार को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. सबसे प्रमुख है आईपीओ लिस्टिंग की समय-सीमा को T+6 दिनों से घटाकर T+3 दिन करना. यह परिवर्तन आवेदकों के पूंजी अवरुद्ध रहने की अवधि को काफी कम कर देता है. इससे वित्तीय तरलता बढ़ती है और लिस्टिंग व आवेदन के बीच की अवधि में बाज़ार की अस्थिरता का जोखिम कम होता है. यह कदम सीधे तौर पर बाज़ार की दक्षता और निवेशकों के हित को बढ़ावा देता है.
सेबी ने एंकर निवेशकों (Anchor Investors) के लिए लॉक-इन अवधि भी बढ़ा दी है. अब वे 90 दिनों की लॉक-इन अवधि के बाद ही अपने आधे शेयर बेच सकते हैं. इस कदम का उद्देश्य लिस्टिंग के बाद एंकर निवेशकों द्वारा शेयरों की त्वरित बिक्री से होने वाली उच्च अस्थिरता को रोकना है. यह नए और खुदरा निवेशकों को खतरे से बचाता है.
‘बिक्री के लिए ऑफर’ (Offer for Sale) पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं. अब 20% से अधिक हिस्सेदारी वाले हितधारक अपने हिस्सा का 50% (आधा) शेयर ही बेच सकते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि आईपीओ का प्राथमिक उद्देश्य कंपनी के लिए नई पूंजी जुटाना रहे, न कि केवल प्रमोटरों को निकास का अवसर प्रदान करना.
प्रमुख कानूनी अधिनियम
आईपीओ की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम 1956/2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, और प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम 1956 जैसे कई कानूनी अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत आती है 32.
आईपीओ के फायदे और नुकसान
कंपनियों के लिए
- लाभ
- पूंजी जुटाना: आईपीओ कंपनियों को बैंकों से उच्च ब्याज वाले ऋण लिए बिना बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने की अनुमति देता है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, वे इस तरीके से अपने फाइनेंस का 20% तक जुटा सकते हैं.
- ब्रांड और विश्वसनीयता: सार्वजनिक होने से कंपनी को कई तरह के जानकारी जनता के सामने रखना होता है. यह कंपनी के प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में वृद्धि करता है. यह उपभोक्ताओं और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाता है.
- अधिग्रहण की क्षमता: सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड स्टॉक का उपयोग अन्य कंपनियों के अधिग्रहण या कर्मचारियों को स्टॉक-आधारित मुआवजे के रूप में किया जा सकता है.
- हानि
- लागत और जटिलता: आईपीओ प्रक्रिया महंगी और जटिल होती है. इसमें कानूनी, वित्तीय और नियामक शुल्क शामिल होते हैं.
- नियामक बोझ: एक सार्वजनिक कंपनी को तिमाही वित्तीय रिपोर्टिंग और सख्त नियामक अनुपालन के बोझ का सामना करना पड़ता है.
- गोपनीयता का नुकसान: कंपनी को अपने वित्तीय और परिचालन विवरणों को सार्वजनिक करना पड़ता है, जिससे उसकी गोपनीयता कम हो जाती है.
निवेशकों के लिए
- लाभ
- शुरुआती निवेश का अवसर: निवेशकों को एक संभावित रूप से आशाजनक कंपनी में उसके विकास के शुरुआती चरण में निवेश करने का मौका मिलता है.
- उच्च रिटर्न की संभावना: सफल आईपीओ से शेयर की कीमत में अच्छी वृद्धि हो सकती है, जिससे निवेशकों को पर्याप्त पूंजीगत लाभ मिल सकता है.
- पोर्टफोलियो विविधीकरण: आईपीओ में निवेश से निवेशक के पोर्टफोलियो में विविधता आती है, जिससे समग्र जोखिम कम हो सकता है.
- जोखिम/ हानि
- उच्च अस्थिरता: आईपीओ में अक्सर अत्यधिक अस्थिरता होती है. लिस्टिंग के बाद शेयरों की कीमत में उतार-चढ़ाव काफी अधिक हो सकता है.
- ओवरवैल्यूएशन की संभावना: कुछ आईपीओ की कीमत बाज़ार की वास्तविक मांग से अधिक हो सकती है. इससे लिस्टिंग के बाद कीमत में गिरावट आ सकती है.
- डेटा की कमी: एक नई सार्वजनिक कंपनी के पास एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड या ऐतिहासिक प्रदर्शन डेटा की कमी होती है, जिससे निवेश के फैसले में अनिश्चितता बढ़ सकती है.
निष्कर्षतः, आईपीओ में निवेश करना एक जोखिम भरा फैसला होता है. इसके लिए गहन शोध, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और उद्योग के रुझानों की सावधानीपूर्वक समझ की आवश्यकता होती है. इसलिए, आईपीओ को केवल लिस्टिंग गेन की लॉटरी के रूप में नहीं देखना चाहिए.