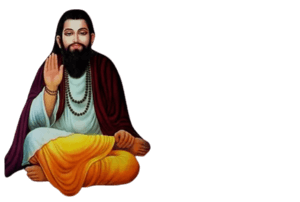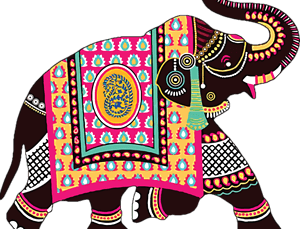यूरोपीय संघ वर्तमान में विश्व में सफलतम क्षेत्रीय संगठन है। यह 27 यूरोपीय देशों का समूह है. यह पेरिस संधि (1951) तथा रोम संधि (1957) के अधीन स्यापित यूरोपीय समुदाय (ईसी) के आधार पर गठित किया गया है. एकल यूरोपीय अधिनियम (1986), यूरोपीय संघ के लिये मैस्ट्रिच (Mastricht) संधि (1991) तथा अम्स्टर्डम प्रारूप संधि (1997), आदि संधियों ने इसके गठन को संपूरकता प्रदान की.
औपचारिक नाम: यूनियन यूरोपीने (फ्रेंच) [Union Europeenre (French)|
यूरोपैसके यूनियन [Europaische Union (German)] ;
यूनिओने यूरोपिआ (इतालवी) [Unione Europea (Italian)]
मुख्यालयः ब्रूसेल्स (बेल्जियम).
सदस्यता: आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, फ़िनलैंड, फ़्रांस, यूनान, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, और स्वीडन.
ईयू के नए सदस्य: हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, साइप्रस, स्लोवाकिया, माल्टा, बुल्गारिया, रोमानिया, लाटविया, लिथुआनिया ने 1 मई 2004 तक औपचारिक तौर पर संघ की सदस्यता ग्रहण की. 1 जनवरी, 2007 को बुल्गारिया और रोमानिया ने संघ की सदस्यता ली. क्रोएशिया 1 जुलाई, 2013 को यूरोपीय संघ में शामिल हुआ जिससे ईयू की कुल सदस्य संख्या 28 हो गई. लेकिन, 2020 में ब्रिटेन के अलग होने से यह 27 रह गई.
आधिकारिक भाषाएं: डेनिश, डच, अंग्रेजी, फिनिश, फ्रेंच, गेलिक, जर्मन, यूनानी, इटालियन, पुर्तगाली, स्पेनिश तथा स्वीडिश.
उद्भव एवं विकास
यूरोपीय संघ (European Union-EU) का प्रादुर्भाव यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय (ईसीएससी) से हुआ, जिसकी स्थापना बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड द्वारा 1951 में पेरिस में एक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी. ईसीएससी का औपचारिक नाम- कम्युनौटी यूरोपीने डु कार्बोन एट डी आई एशैर या सीईसीए (Communaute Europeenne du Charbon et de I’Acier or CECA) था. इस संगठन का प्रस्ताव फ़्रांस के तत्कालीन-विदेश मंत्री श्री रॉबर्ट स्कूमैन ने रखा था.
ईसीएससी के प्रमुख प्रावधान थे- सदस्य देशों में कोयला और इस्पात उत्पादन का एकीकरण, तथा; कोयला, लौह-अयस्क और रद्दी धातु के अंतरा-समुदाय व्यापार पर सभी प्रकार के आयात करों और प्रतिबंधों की समाप्ति. पेरिस संधि का जुलाई 1952 से 50 वर्षों के लिये प्रभाव में आना तय हुआ. कोयला, इस्पात, लौह-अयस्क और रद्दी धातु के लिये 1 फरवरी, 1953 को, इस्पात के लिये 1 मई, 1953 को तथा विशिष्ट इस्पात के लिये 1 अगस्त, 1954, को सामूहिक बाजार का गठन किया गया.
ईसीएससी की सफलता ने सामूहिक बाजार को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत करने के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया. सदस्यों ने इसे घनिष्ठ आपसी राजनीतिक तालमेल के लिये लाभप्रद समझा. फलतः ईसीएससी के छह सदस्यों ने मार्च 1957 में रोम में दो पृथक् संधियों पर हस्ताक्षर किए, जो कि रोम संधियों के नाम से जानी जाती हैं.
इन संधियों के अंतर्गत दो और यूरोपीय समुदाय गठित हुये-यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी अथवा साझा बाजार), तथा; यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय [ईएईसी अथवा यूरेटॉम; औपचारिक नाम-कम्युनौटी यूरोपीने डी आई एनर्जी एटोमिके अथवा सीईईए (EAEC or the Euratom; formal name—Communaute Europeenne der Energie Atomique or the CEEA).
ईईसी की स्थापना मुह्य रूप से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये की गई थी- यूरोपीय सीमा शुल्क संघ की स्थापना; एक साझा बाह्य शुल्क की व्यवस्था, जिसमें सदस्यों के बीच व्यापार में सभी अवरोधों को समाप्त करने का प्रावधान हो. यूरेटॉम की स्थापना आर्थिक विस्तार के लिये बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने तथा नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की व्यवस्था करने के उद्देश्यों से की गई.
आरंभ में इन तीन समुदायों, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोपीय समुदाय (European Communities–EC) तथा अनौपचारिक रूप से एकल यूरोपीय समुदाय (singular European Community–EC) के नाम से जाना जाता था, की सहायता के लिए कई सामूहिक और पृथक् संस्थाओं या अंगों की व्यवस्था की गई. जहां एक ओर एक सामूहिक न्यायालय और साझा एसेम्बली (या यूरोपीय संसद, जिसकी स्थापना यूरोपीय समुदाय की कुछ विशिष्ट संस्थाओं पर अभिसमय के द्वारा हुई) थे.
वहीं दूसरी ओर प्रत्येक समुदाय के अपने पृथक् अधिशासी अंग (ईईसी और यूरेटॉम दोनों में आयोग तथा ईसीएससी में शीर्ष सत्ता के नामों से ज्ञात) तथा नीति-निर्धारक संस्था (ईईसी तथा यूरेटॉम में परिषद के नाम से तथा ईसीएससी में विशेष मंत्रिपरिषद के नाम से ज्ञात) थे. बाद में अप्रैल 1965 में यूरोपीय समुदायों के लिये एक साझा परिषद और एक साझा आयोग के गठन के लिये एक संधि (विलय संधि के नाम से लोकप्रिय) पर हस्ताक्षर हुए.
यह संधि जुलाई 1967 में प्रभाव में आई. विलय संधि में यूरोपीय समुदायों के लिये साझा संस्थाओं के प्रावधान थे. ऐसी संस्थाओं में मंत्रिपरिषद, आयोग, संसद (एसेम्बली) और न्यायालय सम्मिलित थे. अतः व्यक्तिगत आयोगों और परिषदों के अधिकारों को साझा आयोग (अधिशासी) तथा सामूहिक परिषद (नीति-निर्धारण) में स्थानांतरित कर दिया गया.
इन सभी तीन समितियों के मूल छह सदस्यों में छह अन्य नए सदस्य सम्मिलित किये गये- डेनमार्क, आयरलैंड, और युनाइटेड किंगडम 1973 में, यूनान 1981 में और पुर्तगाल एवं स्पेन 1986 में.
1986 के एकल यूरोपीय अधिनियम (एसईए) ने रोम संधि में कुछ और संशोधन कर दिए, जैसे-नीति- निर्धारण प्रक्रिया में यूरोपीय संसद की अधिक भागीदारी; यूरोपीय परिषद को अधिकृत मान्यता, तथा; 20वीं सदी के अंत तक पूर्ण आर्थिक और मौद्रिक विलय की प्राप्ति. एसईए जुलाई 1987 में प्रभाव में आया.
1991 की मैस्ट्रिच संधि (यूरोपीय संघ संधि के नाम से लोकप्रिय) ने पुरानी संधियों में कुछ और संशोधन कर दिए तथा आर्थिक और मौद्रिक संघ तथा राजनीतिक संघ के विलय पर विचार किया. एकल मुद्रा की स्थापना (कुछ निश्चित शर्तों के साथ, जैसे-युनाइटेड किंगडम को इससे बाहर रहने की छूट) तथा एक क्षेत्रीय केंद्रीय बैंक का प्रावधान इस संधि के कुछ विशिष्ट तत्व थे. राजनीतिक संघ के संबंध में संधि में कहा गया कि, कोई भी यूरोपीय देश संघ का सदस्य बन सकता है, अगर वह कुछ पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है.
1 नवंबर, 1998 को मैस्ट्रिच संधि के प्रभाव में आने के साथ ही यूरोपीय समुदाय का नाम (ईसी) यूरोपीय संघ (ईयू) हो गया.
फिर भी, ईयू मात्र ईसी का एक अन्य नाम नहीं है. इसने ईसी के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों के अतिरिक्त सहयोग के दो नये विषयों-साझा विदेश और सुरक्षा नीति तथा न्याय एवं आंतरिक मामले, को अपने कार्यक्षेत्र में जोड़ा.
(ईसी/ईयू शब्द ने कुछ भ्रांतियां पैदा की हैं. ईयू के विस्तृत ढांचे के अधीन तीन यूरोपीय समुदाय आज भी अस्तित्व में हैं. इन तीनों समुदायों को आज भी कभी-कभी ईसी के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है, यहां तक कि ईयू के अधिकारियों के द्वारा भी. लेकिन वास्तविक रूप में सामूहिकता दर्शाने के लिये ईयू शब्द आज अधिक उपयुक्त है, विशेषकर तब जब टीईयू ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय समुदाय करने के लिए ईईसी संधि को संशोधित कर दिया है.)
लिस्बन संधि ने एम्सटर्डम संधि (1997) द्वारा जारी प्रक्रिया को संपन्न करने और नीस संधि (2001) द्वारा संघ की क्षमता और लोकतांत्रिक सत्ता में अभिवृद्धि करने के कार्य को जारी रखने का उद्देश्य लिया.
जैसाकि लिस्बन संधि द्वारा संशोधित संधि ने मूलभूत अधिकारों के ईयू चार्टर का संदर्भ प्रदान किया और इस दस्तावेज को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया. इस प्रकार यूरोपीय संघ की संधि, यूरोपीय संघ के कामकाज की संधि और मूल अधिकारों के चार्टर को एक समान कानूनी वैधता दी गई और संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ के कानूनी आधार का गठन किया गया. हालांकि, चार्टर की पाठ्यसामग्री कहीं दिखाई नहीं देती, यहां तक कि परिशिष्ट में भी नहीं.
यूनाइटेड किंगडम ने इस बात की लिखित गारंटी सुनिश्चित की कि यूरोपीय न्यायालय चार्टर का इस्तेमाल ब्रिटेन के श्रम कानूनों या अन्य कानूनों को परिवर्तित करने के लिए नहीं किया जा सकता जो सामाजिक अधिकारों से संव्यवहार करते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों की इस पर राय में भिन्नता है कि यह किस प्रकार प्रभावी होंगे. पोलैंड ने चार्टर से विकल्प छांटने में विजय हासिल की क्योंकि इसने परिवार सम्बन्धी मामलों और नैतिकता, जैसे गर्भपात पर राष्ट्रीय नियंत्रण बनाए रखने पर बल दिया.
यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि यूरोपीय संघ विस्तारित सदस्यता के साथ दक्षतापूर्वक निरंतर कार्य कर सके, नाइस संधि (1 फरवरी, 2003 से प्रवृत्त) ने इसके आकार को निर्धारित करने और ईयू संस्थानों की प्रक्रियाओं संबंधी नियमों को तय किया.
2001 में ईयू के लेकन शिखर बैठक में एक घोषणा जारी की गई जिसे यूरोप के भविष्य के लिए ईयू की संधियों के पुनर्गठन एवं सरलीकरण पर अभिसमय कहा गया, और प्रश्न उठाया गया कि क्या इसका अंतिम परिणाम एक संविधान का निर्माण होगा. अभिसमय ने फरवरी 2002 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और इसके गठन का ड्राफ्ट अक्टूबर 2004 में हस्ताक्षर किया गया. इसने सभी सदस्य देशों को इसके लागू होने की नियत तारीख (1 नवम्बर, 2006) से पूर्व या तो संसदीय मत या राष्ट्रीय जनमत संग्रह के द्वारा इसकी पुष्टि हेतु 2 वर्ष का समय दिया.
फ्रांस एवं नीदरलैंड, हालांकि, ने कहा कि 2005 के जनमत संग्रह के अनुरूप बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के वे संवैधानिक संधि को स्वीकार करने में अक्षम होगे. यूनाइटेड किंगडम ने भी संयत संशोधित संधि पर जोर दिया, जिनकी ईयू की पूर्व की संधियों की तरह संसदीय मत के जरिए पुष्टि की जा सके.
यह पुष्टिकरण प्रक्रिया के लिए एक अत्यधिक कठोर अवनति थी. जून 2007 में, यूरोपीय परिषद् एक राजनितिक समझौता करने और इसे एक वैधानिक रूप देने के लिए एक अंतर्सरकारी कांफ्रेस के लिए संक्षिप्त एवं स्पष्ट जनादेश पर सहमत हुई. यह समझौता सुधार संधि के तौर पर जाना जाता है. बाद में इस संधि को लिस्बन संधि के नाम से जाना जाता है जिसे फिर से पुष्टिकरण के लिए लाया गया. ईयू नियमों के तहत् सभी 27 सदस्य राज्यों को इसके अस्तित्व में आने से पूर्व इसकी पुष्टि करनी होती है.
अक्टूबर 2009 में, हालांकि, आयरिश जनमत संग्रह ने संधि का अनुमोदन किया (पिछले निरस्त को पलटते हुए) और अंतिम अनिच्छुक पृष्ठांकन के लिए रास्ता साफ किया. चेक गणराज्य ने जल्दी ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए. संधि का क्रियान्वयन 1 दिसंबर, 2009 से प्रारंभ हुआ.
जबकि लिस्बन संधि में संविधान द्वारा लागू कई बदलाव मौजूद थे, मुख्य अंतर यह था कि जहाँ संविधान ईयू की सभी पूर्व संधियों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर एकदम नई शुरुआत करने की बात करता है, वहीं नई संधि ईयू संधि (मैस्ट्रिच) को संशोधित कर यूरोपियन कम्युनिटी (रोम) को स्थापित करती है.
इस प्रक्रिया में, टीईसी (Treaty Establishing the European Community) का नाम परिवर्तित कर ट्रीटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन (Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU) रखा गया.
यूरोपीय संघ सुधार संधि (लिस्बन संधि)
यूरोपीय संघ में निर्णय प्रक्रिया में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण संधि (लिस्बन संधि) पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर लिस्बन में किए थे. संधि के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-
- यूरोपीय संघ में 6-6 माह की चक्रीय क्रमानुसार अध्यक्षता के स्थान पर 2.5-2.5 वर्ष के कार्यकाल वाले अध्यक्ष का प्रावधान इसमें किया गया.
- यूरोपीय संसद में सर्वसम्मति से पारित होने की आवश्यकता वाले मुद्दों की संख्या घटाई गई है. इससे सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपेक्षाकृत कम मुद्दों पर वीटो किया जा सकेगा.
- यूरोपीय संसद के आकार को छोटा करते हुए सदस्य राष्ट्रों के मतों का आवंटन इन राष्ट्रों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा. छोटे राष्ट्रों को इससे कोई नुकसान न हो, इसके लिए इस प्रावधान की 2014 के बाद ही लागू किया जाएगा.
- सदस्य राष्ट्रों की कॉमन विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मामलों के प्रमुख का पद अधिक मजबूत किया जाएगा.
- यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी-यूरोपीय आयोग के सदस्यों की संख्या 27 से घटाकर 17 करने का प्रस्ताव नई संधि में किया गया है. आयोग के सदस्यों का चुनाव 5-5 वर्ष के कार्यकाल हेतु चक्र क्रमानुसार किया जाएगा.
- संधि में मौलिक मानवाधिकारों एवं विधिक अधिकारों के यूरोपीय चार्टर का प्रावधान भी किया गया है. ब्रिटेन एवं पोलैण्ड ने इस चार्टर को बाध्यकारी बनाने से इंकार किया है.
यूनियन (टीएफईयू) किया गया. लिस्बन संधि द्वारा निम्नांकित पांच विषय यूरोपीय संघ के एकमात्र क्षेत्राधिकार में रखे गए-
- कस्टम यूनियन का संचालन;
- आंतरिक बाजारों के लिए प्रतियोगिता संबंधी नियमों का निर्धारण;
- सदस्य राष्ट्रों की मौद्रिक नीति;
- सामान्य मत्स्यपालन नीति तथा समुद्री जैविक संसाधनों का संरक्षक;
- सामान्य व्यापारिक नीति.
इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसे विषय हैं जिन पर यूरोपीय संघ का क्षेत्राधिकार सदस्य राष्ट्रों के साथ-साथ संचालित होता है. 1 दिसंबर 2009 से लिस्बन संधि के प्रवृत्त होने से ईयू के कई पहलुओं में परिवर्तन हुआ. विशेष रूप से इसने यूरोपीय संघ के वैधानिक ढांचे में परिवर्तन किए. ईयू के तीन स्तंभों का विलय कर एक एकमात्र वैधानिक संगठन बनाया. साथ ही यूरोपीय परिषद् का एक स्थायी अध्यक्ष बनाया.
उद्देश्य यूरोपीय संघ के मुख्य उद्देश्य हैं-आर्थिक और सामाजिक संसक्ति को मजबूत करना; आर्थिक और मौद्रिक संघ (जिसमें एकल मुद्रा का प्रावधान हो) की स्थापना करना; साझा विदेश और सुरक्षा नीति का क्रियान्वयन करना; संघ के लिये सामूहिक नागरिकता की व्यवस्था करना, तथा; न्यायिक एवं आंतरिक विषयों में घनिष्ठ सहयोग विकसित करना. ईयू का परम लक्ष्य है-यूरोपवासियों के मध्य एक निरंतर घनिष्ठ संघ की स्थापना करना, जिसके सभी निर्णय यथा संभव नागरिकों के निकट हों.
ईईसी, ईसीएससी और यूरेटॉम के अपने-अपने स्वतंत्र उद्देश्य भी हैं, जिनकी चर्चा अपेक्षित इसीएससी के मुख्य उद्देश्य हैं- कोयले और इस्पात की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना; न्यूनतम व्यवहारिक मूल्य निर्धारित करना; सीमा शुल्क संघ के अधीन सभी उपभोक्ताओं के लिये कोयले और इस्पात के वितरण एवं विपणन में समानता स्थापित करना; संसाधनों का युक्तिमूलक उपयोग सुनिश्चित करने ले लिए उद्योगों का विनियमन करना: उत्पादन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना, और; उद्योगों के श्रमिकों के कार्य एवं जीवन स्तर में सुधार करना.
ईईसी के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं- सम्पूर्ण समुदाय की आर्थिक गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास को प्रोत्साहन; सतत और संतुलित विस्तार; अधिक स्थायित्व; जीवन स्तर के सुधार में तेजी और अपने सदस्य देशों के मध्य घनिष्ठ सम्पर्क. अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ईईसी ने एक साझा बाजार की स्थापना की है तथा यह निरन्तर सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों के निकट पहुंच रहा है.
यूरेटॉम निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील है-अनुसंधान विकास, सूचनाओं का प्रसार, एकीकृत सुरक्षा मानकों का प्रवर्तन; सरल निवेश व्यवस्था; आणविक पदार्थों की आपूर्ति में नियमित और समान वितरण व्यवस्था; यह सुनिश्चित करना की आणविक पदार्थों का उपयोग सिर्फ निर्दिष्ट कार्यों में ही हो रहा है अथवा नहीं; आणविक पदार्थों के संबंध में कुछ निश्चित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का प्रयोग; नाभिकीय उद्योगों के कार्मिकों और निवेश पूंजी के उन्मुक्त आवागमन के लिये एक साझा बाजार की स्थापना, और; परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों को प्रोत्साहन.
संरचना
ईयू के संगठनात्मक ढांचे में यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद (मंत्रिपरिषद), यूरोपीय आयोग (या यूरोपीय समुदायों का आयोग), यूरोपीय समुदाय न्यायालय, यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक तथा अनेक सलाहकारी और परामर्शदाता निकाय सम्मिलित हैं.
यूरोपीय परिषद
यूरोपीय परिषद सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा/या शासनाध्यक्षों को एक मंच पर लाती है. परिषद की बैठक को सामान्यतया यूरोपीय शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है. परिषद ईयू के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है, इसे राजनीतिक दिशा देती है तथा इसके विकास के लिये प्रेरणा प्रदान करती है. यह विदैशिक मामले, सुरक्षा, न्याय और आन्तरिक विषयों के संबंध में सामूहिक नीतियां तैयार करती है.
रोम और पेरिस की संधियों में यूरोपीय परिषद के गठन पर विचार नहीं किया गया. इस परिषद के गठन को एसईए में औपचारिक रूप दिया गया. यूरोपीय परिषद और मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से ईयू प्रणाली के अंतर्गत अन्तर-सरकारवाद का प्रतिनिधित्व करती हैं.
परिषद की वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक होती है तथा इसकी अध्यक्षता छह महीनों के लिए निर्धारित रहती है. यह वर्ष में एक बार संघ की प्रगति का ब्यौरा यूरोपीय संसद में प्रस्तुत करती है.
यूरोपीय संसद
यूरोपीय संसद ईयू की प्रतिनिधि सभा है. इसमें सदस्य देशों के कुल 626 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव पांच वर्षों के लिये होता है. सभी ईयू देशों के नागरिक अपने दत्तक निवास-देश में मत देने या चुनाव लड़ने के अधिकारी होते हैं.
1 मई, 1999 को लागू हुई एम्सटर्डम संधि, तथा मैस्ट्रिच संधि के पश्चात् संसद के अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है. आज इसे व्यापक विधायी अधिकार प्राप्त हैं, जैसे- ईयू के विशाल बजट का विश्लेषण करने का अधिकार तथा कुछ निश्चित आंतरिक विषयों पर विधान बनाने के संबंध में मंत्रिपरिषद के साथ सह-निर्णय (co-decision) का अधिकार. यूरोपीय परिषद से यह आशा भी की जाती है कि वह विदेश और सुरक्षा नीतियों की वर्तमान स्थिति के संबंध में संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे. यूरोपीय आयोग के गठन में संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं. वह पूरे आयोग को बखास्त कर सकती है.
प्रत्येक महीने में स्ट्रासबर्ग में संसद की पूर्ण बैठक होती है. संसदीय समितियों की बैठक ब्रुसेल्स में होती है.
यूरोपीय संघ परिषद (मंत्रिपरिषद)
परिषद यूरोपीय संघ का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है. यह 15 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से बनी होती है तथा ईयू के सामूहिक दृष्टिकोण के विपरीत प्रत्येक सदस्य देश के राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है. मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही सदस्य देश एक-दूसरे की राष्ट्रीय नीतियों में समन्वय स्थापित करते हैं तथा आपसी एवं अन्य संस्थाओं के साथ उत्पन्न मतभेदों को दूर करते हैं. परिषद संघ के बजट प्रस्तावों तथा विधानों को तैयार करने में संसद के साथ तथा नीतियों के क्रियान्वयन में आयोग के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाकर रखती है. कुछ विशेष नीतियों से जुड़े विषयों पर विचार करने के लिये विशिष्ट परिषदों (जैसे-कृषि परिषद) का गठन किया गया है.
सभी निर्णय निर्विरोध या उचित बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं. सदस्य देशों के मतों की संख्या का निर्धारण एक निश्चित भारित (weightage) प्रणाली के आधार पर किया जाता है. मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रत्येक छह महीने पर सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है.
मंत्रिपरिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स, (बेल्जियम) में है. अप्रैल, जून और अक्टूबर महीनों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की प्रत्येक मासिक बैठक बुसेल्स में होती है. इन तीन महीनों में मंत्रिपरिषद की बैठक लक्जमबर्ग में होती है.
यूरोपीय आयोग
यह ईयू के अधिशासी अंग के रूप में कार्य करता है तथा संगठन के दैनिक प्रशासन के लिये उत्तरदायी है. इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी कारवाई के लिये प्रस्ताव रखने और मंत्रिपरिषद के निर्णयों को क्रियान्वित करने के अधिकार प्राप्त हैं. यदि कोई संस्था या देश ईयू के एक अंग के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में असफल रहता है तो आयोग उसके विरुद्ध यूरोपीय न्यायालय में मामला दर्ज कर सकता है.
आयोग में 20 सदस्य (आयुक्त/कमिश्नर के नाम से ज्ञात) होते हैं, जिनकी नियुक्ति सदस्य देशों के द्वारा पांच वर्षों के लिये होती है. प्रत्येक कमिश्नर को किसी विशिष्ट क्षेत्र का कार्य सौंप दिया जाता है. मैस्ट्रिच संधि के तहत किसी ईयू सदस्य देश के दो से अधिक कमिश्नर नियुक्त नहीं हो सकते हैं और प्रत्येक सदस्य देश का कम-से-कम एक कमिश्नर अवश्य होना चाहिए. सदस्य देश सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन करते हैं और फिर अध्यक्ष से परामर्श करके अन्य कमिश्नरों का चुनाव करते हैं.
अध्यक्ष और कमिश्नरों की नियुक्तियों को यूरोपीय संसद का अनुमोदन प्राप्त होना अनिवार्य है तथा ये नियुक्तियां अंतिम रूप से सदस्य देशों के ‘सामूहिक समझौते’ (Common Accord) के द्वारा होती हैं. कमिश्नर अपने कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा इन्हें किसी राष्ट्रीय सरकार के निर्देशन में कार्य करने से स्पष्ट रूप से मना किया जाता है. आयोग में निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं तथा यह सामूहिक रूप से यूरोपीय संसद के प्रति जवाबदेह होता है. आयोग की सहायता के लिये 23 महानिदेशकों और एक बड़े अधिकारी तंत्र का प्रावधान किया गया है.
आयोग का मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है. इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं-डेनिश, डच, इंग्लिश, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, यूनानी, इटालवी, पुर्तगाली, स्पेनिश और स्वीडिश.
यूरोपीय समुदाय न्यायालय
15 न्यायाधीशों तथा 9 महाधिवक्ताओं (advocatesgeneral) से बना यूरोपीय न्यायालय लक्जमबर्ग में अवस्थित है. इसके प्रमुख कार्य हैं- ईयू संधियों और विधानों की व्याख्या करना तथा सदस्य देशों के घरेलू न्यायालयों द्वारा निर्दिष्ट प्रांसगिक कानूनी पहलुओं तथा संधियों के क्रियान्वयन से उठे विवादों में निर्णय प्रेषित करना. इसके निर्णय सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं.
1989 में गठित प्रथम दृष्टांत (Court of First Instance) ईसी के प्रतियोगिता नियमों (competition rules) के अंतर्गत दर्ज मामलों तथा समुदाय के अधिकारियों द्वारा उठाए गए मामलों की जांच करता है.
यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय
15 सदस्यों से बना यह न्यायालय ईयू की समस्त आय और व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करने के लिये उत्तरदायी होता है. 1975 में स्थापित तथा 1977 से प्रभावी इस न्यायालय का मुख्यालय लक्जमबर्ग में है.
सलाहकारी और परामर्शकारी निकाय
तीन मुख्य सलाहकारी समितियां इस प्रकार हैं- आर्थिक और समाजिक समिति, ईसीएससी परामर्श समिति और क्षेत्रीय समिति.
आर्थिक और सामाजिक समिति की स्थापना एक परामर्शकारी निकाय के रूप में 1958 में हुई. इसमें तीन प्रकार के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं- नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि, श्रमिक संघों के प्रतिनिधि और विशेष क्षेत्रों (जैसे-कृषक, उपभोक्ता, आदि) के प्रतिनिधि. यह समिति प्रभावों के संबंध में सलाह देती है.
इसीएससी परामर्शक समिति में कोयला और इस्पात उद्योगों के से जुड़े अनेक समूहों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, जैसे-उत्पादक, श्रमिक, उपभोक्ता और व्यापारी. यूरोपीय परिषद द्वारा नियुक्त यह समिति कोयला एवं इस्पात नीतियों के संबंध में यूरोपीय आयोग की सलाह देती है.
क्षेत्रीय समिति में ऐसे सदस्य होते हैं, जो क्षेत्रीय और स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते करते हैं यह समिति शिक्षा, संस्कृति, लोक स्वास्थ्य, पर-यूरोपीय नेटवर्कों तथा आर्थिक एवं सामाजिक सामंजस्य जैसे विषयों पर सलाह देती है.
ईयू के संगठनात्मक ढांचे में निम्नांकित संस्थाएं भी सम्मिलित होती हैं.
यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)
इस बैंक की स्थापना रोम संधि के अंतर्गत 1958 में हुई. इसके मुख्य उद्देश्य है-पूंजी परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के द्वारा क्षेत्रीय विकास में तेजी लाना, उपक्रमों में आध्रुनिकीकरण और परिवर्तन लाना तथा नई गतिविधियों को विकसित करना.
यूरोपीय केंद्रीय बैंक प्रणाली (ईएससीबी)
इस प्रणाली में यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) तथा 15 राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक (यूरो क्षेत्र के 11 देश और विशेष दर्जे वाले 4 देश) सम्मिलित होते हैं. ईएससीबी के मुख्य कार्य हैं- सदस्य देशों की मौद्रिक नीति की व्याख्या और क्रियान्वयन; विदेशी मुद्रा विनियमन का संचालन; सम्मिलित सदस्य देशों की अधिकारिक विदेशी मुद्रा निधि का धारण और उसका प्रबंधन; भुगतान-प्रणाली के सरल संचालन को प्रोत्साहन; क्रेडिट संस्थाओं के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से जुड़े योग्य प्राधिकरणों की नीतियों को सहयोग तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता.
यूरोपीय समुदाय सांख्यिकीय कार्यालय (यूरोस्टैट)
यह कार्यालय सदस्य देशों के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित, संवित और प्रकाशित करता है.
यूरोपोल
इसकी स्थापना 1994 में हुई. यह ईयू देशों के मध्य आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये एक चैनल का कार्य करता है.
गतिविधियों
एकल आंतरिक बाजार की स्थापना आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना की दिशा में प्रगति, यूरोपीय मौद्रिक संघ की स्थापना, सामूहिक कृषि नीति एवं सामूहिक मत्स्य नीति का विकास ईयू/ईसी की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां रही हैं.
एसईएस के अधीन गाठी एकल आतंरिक बाज़ार व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी और सेवओंब के निर्बाध आदान-प्रदान के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को समाप्त करके आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देता है. एसईए के अस्तित्व में आने से पहले भी ईईसी/ईयू ने एक साझा बाजार की पूंजी और श्रम के निर्बाध आवागमन के प्रावधान थे. सदस्य देशों ने समुदाय के आंतरिक व्यापार में आयात-शुल्क, कोटा और अन्य अवरोधों को हटाने तथा गैर-सदस्यीय देशों के लिये ईसी की सामूहिक आयात-शुल्क व्यवस्था को यथावत् रखने के लिये कई कदम उठाए.
ईसी ने गैर-सदस्यीय देशों के साथ कई अधिमान्य व्यापार समझौते किये, 40 से अधिक अल्प-विकसित अफ्रीकी, कैरेबियाई और प्रशांत (एसीपी) देशों के साथ 1975 और 1979 में लोम (Lome) में हुए समझेते इसी श्रेणी के थे. इन समझौतों के अंतर्गत एसीपी देशों के विविध प्रकार के प्राथमिक उत्पादों और निर्मित वस्तुओं के लिये ईसी बाजार में शुल्क रहित प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराई गयी. 1995 में प्रभाव में आये सेनगन समझौते (SchengenAccord) ने हस्ताक्षरकर्ता ईयू तथा गैर-ईयू देशों के लोगों और वस्तुओं पर लागू सीमा नियंत्रणों को समाप्त कर दिया.
एकल आंतरिक बाजार में आर्थिक और मौद्रिक संघ का प्रावधान था. सहभागी देशों की मुद्रा-विनिमय दरों को विचल-सीमा (fluctuation margin) के अंदर रखने, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने, अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं से यूरोपीय व्यापार की रक्षा करने तथा आर्थिक अभिसरण (convergence) की दिशा में कार्य करने के उद्देश्य से 1979 यूरोपीय मौद्रिक प्रणाली ईएमएस का गठन किया गया.
ईएमएस के गठन के बाद तत्कालीन ईईसी के खाते की इकाई के रूप में यूरोपीय मुद्रा इकाई (ईसीयू) को अपनाया गया. वर्ष 1981 तक ईसीयू ने ईईसी द्वारा सामूहिक कृषि नीति, यूरोपीय विकास कोष और बजट के लिये व्यवहार में लाये गये सभी मात्रकों का स्थान ले लिया. ईसीयू सदस्य देशों की आर्थिक शक्ति के आधार पर भारित (weighted) मुद्रा मुल्यों का औसत था. प्रत्येक दिन राष्ट्रीय मुद्राओं के ईसीयू मूल्य की गणना और प्रकाशन होता था.
ईएमएस के गठन के पश्चात् सदस्य देशों की मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से विनिमय दर प्रणाली (ईआरएम) शुरू की गई. ईआरएम का प्रशासन सदस्य देशों के वित मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के द्वारा दैनिक आधार पर होता था. ईआरएम के अंतर्गत प्रत्येक मुद्रा के लिये ईसीयू में केंद्रीय दर (विचल-सीमा के निर्धारण के साथ) निर्धारित होता था. अगर कोई मुद्रा विचल-सीमा के शीर्ष या आधार को छूती, तो केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दरों पर उस मुद्रा की खरीदने या बेचने के लिये बाध्य होते थे.
इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ अन्य मुद्रा स्थिरीकरण उपाय इस प्रकार थे- राष्ट्रीय ब्याज दरों में समायोजन; एक केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य केंद्रीय बैंकों से उधार लेने की व्यवस्था; यूरोपीय मुद्रा सहयोग कोष से धन निकासी की सुविधा, तथा; अवमूल्यन या पुनर्मूल्यन के प्रावधान. 1993 में यूरोपीय वित्त बाजार में गहन मुद्रा अटकलबाजी के कारण ईआरएम लगभग समाप्त हो गया.
इस अटकलबाजी के कारण यूरोपीय बाजार में कमजोर मुद्राओं के मूल्य में काफी उतार-चढ़ाव आया. इस पर नियंत्रण पाने के लिये विचल सीमा को और विस्तृत किया गया. लेकिन, अनेक यूरोपीय मुद्राएं या तो ईआरएम से बाहर रहीं या विस्तृत सीमा के अंदर विचलित होने के लिये छोड़ दी गई.
आर्थिक और मौद्रिक एकीकरण का दूसरा चरण 1994 में शुरू हुआ जब मैस्ट्रिच संधि के अंतर्गत यूरोपीय मुद्रा संस्थान (ईएमआई) का गठन हुआ. इस संस्था के गठन को ईएमयूके अंतिम लक्ष्य (एकल मौद्रिक नीति तथा एकल मुद्रा की स्थापना) की प्राप्ति के लिये आवश्यक समझा गया.
मैस्ट्रिच संधि के अंतर्गत सभी ईयू सदस्य देशों ने ईएमयू की सदस्यता ग्रहण करने के लिये अपने आपको प्रतिबद्ध किया. मैस्ट्रिच संधि तथा दो अन्य प्रोटोकॉलों ने ईएमयू के अंतिम चरण में प्रवेश के लिये अनेक अभिसरण मानदंडों का निर्धारण किया. ये मानदंड निम्नांकित हैं-
- वार्षिक मुद्रास्फीति औसत मूल्य स्थायित्व में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 3 देशों के स्तर से डेढ़ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- दीर्घकालीन ब्याज दर (वार्षिक औसत) मूल्य स्थायित्व में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तीन देशों के स्तर से दो प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- सरकारी घाटे (संपूर्ण लोक उपक्रम) को जीडीपी से 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा इस स्तर के आसपास होना चाहिए अथवा अस्थाई रूप से तथा इस स्तर से थोड़ा अधिक निकट होना चाहिए.
- सकल सरकारी ऋण को जीडीपी से 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए या संतोषप्रद ढंग से इस स्तर की ओर घटते हुए नजर आना चाहिए.
- किसी देश की विनिमय दर को उस देश की अपनी पहल के द्वारा बिना किसी गंभीर तनाव या अवमूल्यन के सामान्य ईआरएम पट्टी (band) के अधीन होना चाहिए.
दिसंबर 1995 में ईएमयू की नई मुद्रा को यूरो नाम दिया गया. मई 1998 में यूरो के संरक्षक के रूप में ईसीबी का गठन हुआ. यूरो के अस्तित्व में आने के बाद ईसीबी ने ईएमआई के उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर ले लिया. ईसीबी को संघ के अंदर बैंक नोट के निगमन को अधिकृत करने तथा राष्ट्रीय सरकारों की तरह सहभागी देशों की मौद्रिक नीतियों को प्रबंधित करने के अधिकार प्राप्त हैं.
मैस्ट्रिच संधि के मानदंडों को पूरा करने वाले सदस्य देशों (जिनकी संख्या 11 थी) ने ईएमयू के अधीन 1 जनवरी, 1999 को यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू किया. ये ग्यारह देश थे-ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन.
यूरो क्षेत्र विश्व के कुल आर्थिक उत्पादन का 20 प्रतिशत उत्पादित करता है तथा यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है.
1968 में गठित सीमा शुल्क संघ के अंतर्गत किसी सदस्य देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का ईयू के अंदर निर्बाध वितरण संभव है. साथ ही, विश्व के शेष देशों के साथ व्यापार के लिये अनेक सामूहिक व्यवस्थाएं की गई हैं. सदस्य देश व्यक्तिगत स्तर पर गैर-सदस्यीय देशों के साथ द्वि-पक्षीय समझौते नहीं कर सकती हैं. यह अधिकार ईयू में निहित है. ईसी और एफ्टा के मध्य हुई एक संधि के द्वारा 1991 में यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) का गठन किया गया.
सीएपी यूरोपीय परिषद द्वारा दिसंबर 1960 में निर्धारित मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है. कृषि उत्पादकता बढ़ाना और कृषि समुदाय के लिए एक स्वस्थ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना सीएपी
| यूरो मुद्रा |
| यूरो संकेत एक यूनानी episelon (वर्णमाला का पांचवां वर्ण) है, जो दो समानान्तर रेखाएं काटती हैं. ये समानांतर रेखाएं स्थायित्व की प्रतीक हैं. बैंक नोट सभी ईएमयू देशों में समान होते हैं तथा इनके सात मूल्य वर्ग (denominations) होते है-5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 यूरो. इनकी आकृतियां 20वीं सदी की यूरोपीय वास्तुकला के सात विभिन्न कालों का प्रतिनिधित्व करती है- शास्त्रीय (classical), रोमन (Romanesque), गॅाथिक (Gothic) पुनर्जागरण (Renaissance), बरोक (Baroque) रोकोको (Rococo) तथा लौह और कांच वास्तुशिल्प. मुद्रा मूल्य वर्ग रंग और आकार में भिन्न हैं. बड़े मूल्य वर्ग वाले नोट का आकार बड़ा होता है. दृष्टिहीन व्यक्ति नोट को पहचान सकें, इस उद्देश्य से नोट में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं. एक यूरो एक सौ सेंटों (Cents) में विभक्त होता है. जहां तक अग्र भाग का प्रश्न है, यूरो सिक्के एकसमान होते हैं, लेकिन इसके पृष्ठ भाग में देश-विशेष के संकेत उत्कीर्ण रहते हैं. यूरो सिक्कों को भी आठ मूल्य वर्गों में विभाजित किया गया है-1, 2, 5, 10, 20 तथा 50 सेंट, 1 यूरो तथा 2 यूरो.मास्ट्रिश्च संधि के दस्तावेजों में यूरोप में मौद्रिक एवं आर्थिक एकीकरण एवं साझी मुद्रा यूरो के प्रचलन के लिए चार प्रमुख शर्तों का उल्लेख किया गया- मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण; निम्न ब्याज दर; सरकारी ऋण का जीडीपी के 60 प्रतिशत से अधिक न होना; वार्षिक बजट घाटा जीडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक न होना. इस संधि में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के देशों से उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने का अनुरोध किया गया, ताकि वे यूरोप की साझी मुद्रा यूरो में अपनी भागीदारी दर्ज कर सके. यूरोप के अब तक (2014 तक) 18 राष्ट्रों ने यूरो में भागीदारी हेतु सभी आवश्यक पूर्व शर्तों को पूरा कर लिया है. यूरोपीय देश एस्टोनिया ने भी 1 जनवरी, 2011 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दिया है. इससे यूरो जोन में शामिल देशों की कुल संख्या 17 हो गई तथा 28 सदस्यीय यूरोपीय संघ में अभी भी 10 देश ऐसे हैं जहां यूरो आधिकारिक मुद्रा नहीं है. उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2014 को लाटविया ने यूरो मुद्रा को स्वीकार कर लिया. |
के मुख्य लक्ष्य हैं. सीएपी बाजार में स्थिरता और तर्कसंगत उपभोक्ता मूल्य सुनिश्चित करता है. साझा मूल्य और समान एवं स्थिर मुद्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1990 में एक साझा बाजार का गठन किया गया. वर्तमान में साझा बाजार संगठन में यूरोपीय समुदाय के 95 प्रतिशत कृषि उत्पाद सम्मिलित हैं.
सीएफपी 1983 में प्रभाव में आया, जिसके तहत ईयू के सभी मछुआरों को सदस्य देशों की जल सीमा में समान पहुंच प्राप्त है.
मैस्ट्रिच संधि के अंतर्गत यूरोपीय संघ परिवहन, दूरसंचार और ऊर्जा के मौलिक ढांचे के विकास के लिये पार-यूरोपीय नेटवर्को की स्थापना एवं विकास में अपना योगदान देता है.
पर्यावरण की रक्षा के लिए एसईए ने एक पर्यावरण नीति का प्रतिपादन किया, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना है. 1993 में यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी का गठन किया गया. यह एजेंसी कोपेनहेगेन (डेनमाक) में अवस्थित है. यह यूरोपीय सूचना एवं अवलोकन नेटवर्क (ईआईओनेट) के माध्यम से यूरोपीय पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिये प्रयत्नशील है.
बेरोजगारी और सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों से जुड़ी अन्य समस्याओं से लड़ने के लिये एक यूरोपीय सामाजिक कोष का गठन किया गया है.
समस्याजनक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने और मौलिक आर्थिक ढांचे में सुधार लाने के लिये एक यूरोपीय क्षेत्रीय विकास कोष की स्थापना की गई है.
यूरेटॉम अनुसंधान करता है तथा श्रमिकों एवं अन्य लोगों के लिये एकसमान नाभिकीय सुरक्षा स्तर सुनिश्चित करता है. यह नाभिकीय उद्योगों के लिए निवेश और कार्मिकों का निर्बाध आदान-प्रदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक साझा बाजार गठित करने का प्रयास करता है.
यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 का नोबल शांति पुरस्कार यूरोप में शांति एवं सौहार्द, लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के उन्नयन में योगदान के लिए प्रदान किया गया. 1 जुलाई, 2013 को क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बन गया. 8वीं यूरोपीय संसद के मई 2014 के चुनाव में यूरो के प्रति संशय रखने वाले दलों की बढ़ी संख्या देखि गयी.
यूरोपीय संघ की कोई एकबद्ध सेना नहीं है. स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (एसआईपीआरआई) के मुताबिक, वर्ष 2010 में फ्रांस ने रक्षा पर 44 बिलियन पौंड (59 बिलियन डॉलर) खर्च करके अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान हासिल किया जबकि यूनाइटेड किंगडम ने तकरीबन 38 बिलियन डॉलर (58 बिलियन डॉलर) खर्च करके चौथा बड़ा देश था.
यूरोपियन कमीशन ह्यूमेनिटेरियन ऐड ऑफिस या ईसीएचओ ईयू से लेकर विकासशील देशों तक मानवतावादी मदद प्रदान करता है. वर्ष 2006 में, इसका बजट तकरीबन 671 मिलियन पॉड था, जिसमें से 48 प्रतिशत अफ्रीकी, प्रशांत एवं कैरिबियाई देशों पर खर्च किया गया.
यूरोपीय विकास निधि (2008-2013 तक 22.7 बिलियन पौंड) का निर्माण सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से किया गया. ईडीएफ का लक्ष्य 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन अभिवृद्धि करना है. हालांकि चार देशों-स्वीडन, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और डेनमार्क ने 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है. वर्ष 2011 में ईयू की आर्थिक मदद 0.42 प्रतिशत थी जिसने इसे विश्व का सर्वाधिक समर्पित आर्थिक मदद प्रदान करने वाला बनाया.
वर्ष 2012 में ईयू का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 16.073 ट्रिलियन अंतरराष्ट्रीय डॉलर था, यह क्रय शक्ति समता के संदर्भ में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 20 प्रतिशत है.
वर्ष 2007 में ईयू के सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि ईयू 20 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेगा इससे 1990 के स्तर की तुलना में 2020 तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 20 प्रतिशत तक घट जाएगा.
क्रोएशिया को छोड़कर, जो 1 जुलाई, 2013 को ईयू में शामिल हुआ, 1 जनवरी, 2012 तक ईयू की सदस्य देशों की संयुक्त जनसंख्या 503,679,780 थी. ईयू के 16 शहरों की जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक है, जिसमें लंदन में सर्वाधिक है.
वर्ष 2010 में, ईयू में रहने वाले 47.3 मिलियन लोग ऐसे थे, जो अपने निवासी देश से बाहर जन्मे थे. यह ईयू की कुल जनसंख्या का 9.4 प्रतिशत है.
ब्रेक्सिट (Brexit)
ब्रेक्सिट (Brexit) दो शब्दों “ब्रिटिश” (British) और “एग्जिट” (Exit) को मिलाकर बना है. यह यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के यूरोपीय यूनियन (EU) से बाहर निकलने की प्रक्रिया को दर्शाता है. यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 31 जनवरी 2020 को पूरी हुई.
ब्रेक्सिट के मुख्य कारण:
- संप्रभुता (Sovereignty): ब्रेक्सिट के समर्थकों का एक मुख्य तर्क यह था कि यूरोपीय संघ की सदस्यता के कारण ब्रिटेन को अपने कानून और नीतियां बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी. वे चाहते थे कि देश अपनी संप्रभुता को वापस प्राप्त करे और अपने फैसले खुद ले सके, खासकर व्यापार, सीमा नियंत्रण और कानूनी मामलों में.
- आप्रवासन (Immigration): यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नागरिकों के लिए “मुक्त आवागमन” की नीति थी, जिसका अर्थ था कि वे बिना किसी रोक-टोक के ब्रिटेन में काम करने और रहने आ सकते थे. कई ब्रिटिश नागरिकों को लगता था कि इससे उनके देश में आप्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं और नौकरियों पर दबाव पड़ रहा है.
- अर्थव्यवस्था (Economy): कुछ लोगों का मानना था कि यूरोपीय संघ की सदस्यता से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है. उनका तर्क था कि ब्रिटेन को EU के बजट में भारी मात्रा में योगदान देना पड़ता था, जबकि उन्हें इसके बदले में उतना लाभ नहीं मिल रहा था. इसके अलावा, EU के कड़े नियमों को भी व्यापार के लिए बाधा माना गया.
- लोकतंत्र (Democracy): समर्थकों का मानना था कि यूरोपीय संघ की नौकरशाही लोकतांत्रिक रूप से जवाबदेह नहीं है. वे चाहते थे कि ब्रिटेन की संसद ही अपने नागरिकों के लिए अंतिम कानून बनाने वाली संस्था हो, न कि ब्रुसेल्स में स्थित EU मुख्यालय.
इन कारणों के चलते, 23 जून 2016 को ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह (referendum) हुआ, जिसमें 51.9% लोगों ने EU से बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया. इस जनमत संग्रह के नतीजे के बाद, ब्रेक्सिट की प्रक्रिया शुरू हुई. आखिरकार 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया.
भारत-EU संबंध
यूरोपीय संघ (EU) भारत के साथ शांति स्थापना, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निकटता से काम कर रहा है. जैसा कि भारत ने 2014 में OECD द्वारा निम्न से मध्यम आय वाले देश (lower-middle income) की श्रेणी से मध्यम-उच्च आय वाले देश की श्रेणी की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, भारत-EU सहयोग पारंपरिक वित्तीय सहायता से साझेदारी की दिशा में केंद्रित हो गया है. यह साझेदारी साझा प्राथमिकताओं जैसे कि सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास आदि पर बल दे रही है.
- संयुक्त घोषणा व शिखर सम्मेलन: वर्ष 2017 के भारत-EU शिखर सम्मेलन में नेताओं ने एजेंडा 2030 (Sustainable Development Goals) के क्रियान्वयन के लिए सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया था; तथा भारत-EU विकास संवाद के विस्तार पर सहमति हुई थी.
- वस्तु व् सेवाओं का व्यापार: वर्ष 2023 में भारत और EU के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार लगभग €124 अरब रहा, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 12.2% है. सेवाओं का व्यापार भारत-EU के बीच €59.7 अरब की सीमा पर है. वर्ष 2024 में EU द्वारा भारत से आयात लगभग US$ 77.06 अरब रहा. उसी वर्ष EU से भारत के लिए निर्यात लगभग US$ 52.34 अरब रहा.
- व्यापार एवं निवेश वार्ता (Negotiations):
- “Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA)” नामक भारत-EU मुक्त व्यापार एवं निवेश समझौता वार्ता का प्रारंभ 2007 में हुआ था, लेकिन कई कारणों से वार्ता वर्ष 2013 के बाद स्थगित हो गई थी.
- बाद में, वर्ष 2021 में नेताओं ने यह तय किया कि BTIA (या अन्य समान व्यापक FTA) वार्ताएं पुनः शुरू हों, और 2025 के दौरान एक संतुलित, महत्वाकांक्षी एवं पारस्परिक लाभकारी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कार्य किया जाए.
- 28 फरवरी 2025 को भारत के दौरे पर EU के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की टीम ने मिलकर यह सहमति जतायी कि दोनों पक्ष वर्ष 2025 के अंत तक वार्ताओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखें.
यूरोपीय संघ के सदस्य देश
वर्तमान में (2025 तक) EU के 27 सदस्य देश हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने 31 जनवरी 2020 को EU से बाहर (Brexit) हो गया. यहाँ यूरोपीय संघ (EU) के सभी 27 वर्तमान सदस्य देशों की पूरी सूची उनके सदस्यता वर्ष सहित प्रस्तुत है:
| क्र. सं. | देश | सदस्यता का वर्ष |
| 1. | बेल्जियम | 01-01-1958 |
| 2. | फ्रांस | 01-01-1958 |
| 3. | जर्मनी | 01-01-1958 |
| 4. | इटली | 01-01-1958 |
| 5. | लक्समबर्ग | 01-01-1958 |
| 6. | नीदरलैंड | 01-01-1958 |
| 7. | डेनमार्क | 01-01-1973 |
| 8. | आयरलैंड | 01-01-1973 |
| 9. | यूनाइटेड किंगडम* | 01-01-1973 (31-01-2020 को EU से बाहर – Brexit) |
| 10. | ग्रीस | 01-01-1981 |
| 11. | पुर्तगाल | 01-01-1986 |
| 12. | स्पेन | 01-01-1986 |
| 13. | ऑस्ट्रिया | 01-01-1995 |
| 14. | फिनलैंड | 01-01-1995 |
| 15. | स्वीडन | 01-01-1995 |
| 16. | साइप्रस | 01-05-2004 |
| 17. | चेक गणतंत्र | 01-05-2004 |
| 18. | एस्टोनिया | 01-05-2004 |
| 19. | हंगरी | 01-05-2004 |
| 20. | लातविया | 01-05-2004 |
| 21. | लिथुआनिया | 01-05-2004 |
| 22. | माल्टा | 01-05-2004 |
| 23. | पोलैंड | 01-05-2004 |
| 24. | स्लोवाकिया | 01-05-2004 |
| 25. | स्लोवेनिया | 01-05-2004 |
| 26. | बुल्गारिया | 01-01-2007 |
| 27. | रोमानिया | 01-01-2007 |
| 28. | क्रोएशिया | 01-07-2013 |