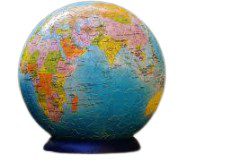कृषि (Agriculture) शब्द की व्युत्पत्ति विज्ञान के अनुसार कृषि का अभिप्राय कर्षण से या खींचने से होता है. कृषि का अंग्रेजी पर्याय Agriculture लेटिन भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है. Ager ( agerfiels or soil) तथा Culture (cultura- the care of tillingh) से मिलकर बना है. लैटिन शब्द Ager का अर्थ खेत होता है, वहीं cultura का अर्थ, सीखना या ज्ञान होता है. इस तरह हम खेती के ज्ञान को कृषि (Agriculture) कह सकते है.
एक रूप में कृषि मानव समूह द्वारा मिट्टीयों पर की जाने वाली कला है, या वह कार्य है, जिससे के परिणाम स्वरूप फसलें उत्पन्न होती है. इस प्रकार विभिन्न समाज में इसको करने की अलग – अलग तरीके है, क्योकीं मानव अपने अपनी सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप ही कार्य करता है.
कृषि की परिभाषा (Definition of Agriculture)
- लौंगमेन :- के आधुनिक शब्दकोश के अनुसार कृषि फसलें पैदा करने के लिये बड़े पैमाने में भूमि को जोतने की कला है.
- हम्फ्री :-ने अपने विश्व कोश में कृषि के अंतर्गत शस्य उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को ही सम्मिलित किया है.
- वाटसन :- ने कृषि को मृदा की खेती की संज्ञा दी है, जिसमें फसलें उगाना तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित है.
- ग्रिग :- कृषि की फसलों का उत्पादन करने के लिए मिट्टी पर खेती करने की क्रिया माना है.
- बुकानन :- वस्तुत: कृषि फसलों उत्पादन से कही अधिक व्यापक है. यह मानव द्वारा पर्यावरण का रूपांतरण है. जिससें फसलों एवं पशु के लिए अनुकुलतम दशायें सुनिश्चित की जा सके तथा विवेकपूर्ण चयन से इनकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सके.
कृषि के प्रकार (Types of Agriculture)
भारत में कृषि पद्धतियॉ अपनाई जाती है.
1. आर्द्र कृषि –
भारत के उन क्षेत्रों में जहॉ वर्षा 200 सेमी. से अधिक सालाना होती है और समतल धरातल पर कॉप मिट्टी की प्रधानता है वहॉ वर्षा के सहयोग से आर्द्र कृषि की जाती है, जिसमें धान, मक्का, कोदो, साग-सब्जी, गन्ना, जूट, चाय आदि की प्रधानता है. यहॉ धान की दा े फसलें उगाई जाती है. बंगाल, ब्रम्हापुत्र घाटी, हिमालयी क्षेत्र, केरल, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भारत के अन्य प्रदेशों में तट कृषि का अधिक प्रचलन है.
2. गहन निर्वाह कृषि (Intensive Subsistence Agriculture)
इस प्रकार के कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औज़ारों की सहायता से अधिक परिश्रम करके कृषि करता है. ऐसे कृषि का कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होना है. इस प्रकार की कृषि दक्षिणी, दक्षिणी-पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है.
3. आदिम निर्वाह कृषि (Primitive Subsistence Agriculture)
इसको भी पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है-
(i) स्थानांतरणशील कृषि (ii) चलवासी पशुचारण
(i) स्थानांतरणशील कृषि (Shifting Agriculture)
इसे ‘झूम कृषि’, ‘कर्तन एवं दहन कृषि’ (Slash and Burn Agriculture) आदि नामों से जाना जाता है. जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की अधिकता है जैसे नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाट वहॉ परिवर्तनशील कृषि की जाती है. इसे झूमिंग कृषि कहते है. यह कृषि भी पूर्णता: वर्षा आधारित है.
इसमें वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा राख को मृदा में मिलाकर उस भूखंड पर कृषि की जाती है. जब मृदा में कार्बनिक तत्त्वों की कमी, निक्षालन (Leaching) तथा वनस्पतियों के बार-बार जलाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, तो उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर कर्तन एवं दहन की क्रिया द्वारा कृषि करता है. मतलब, 2-3 फसलें लेने के बाद जंगल काट कर खेत बना लिये जाते है और पुराने खेत का त्याग कर दिया जाता है.
चूंकि इन आदिवासियों को मिट्टी की उर्वरता बनाये रखने का ज्ञान नहीं है और न भूमि की कमी है. अत: वहॉ सदियों पूर्व प्रचलित कृषि पद्धति आज भी प्रयोग में लाई जा रही है. इससे होने वाली हानियों से ये बेखबर है. सरकार इस पद्धति को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है.
वैश्विक स्तर पर अमेज़न बेसिन के सघन जंगली क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया व उत्तर-पूर्वी भारत में इस प्रकार की खेती किया जाता है. इसे ‘कर्तन और दहन’ या ‘स्थानांतरी’ कृषि भी कहा जाता है. इस पद्धति से मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसल मुख्य रूप से उगाए जाते है.
इस प्रकार के कृषि को विश्व और भारत के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है-
विश्व के स्थानांतरणशील कृषि के नाम (Names of shifting agriculture in the world)
| नाम | देश/स्थान |
| मिल्पा | मेक्सिको और मध्य अमेरिका |
| कोनूको | वेनेज़ुएला |
| रोका | ब्राज़ील |
| मसोलें | काँगो एवं मध्य अफ्रीका |
| लदांग | इंडोनेशिया एवं मलेशिया |
| रे | वियतनाम |
| तुंगिया | म्याँमार |
| चेना | श्रीलंका |
| कैंगिन | फिलीपींस |
भारत में स्थानांतरणशील कृषि संबंधी राज्य (Shifting Agriculture states in India)
| नाम | राज्य |
| झूम | उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड) |
| बेवर या दहिया | मध्य प्रदेश |
| पोडु/पेंडा | आंध्र प्रदेश |
| कुमारी | पश्चिमी घाट |
| कोमान/पामाडाबी | ओडिशा |
| वालेरे/वाल्टरे | दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान |
| खिल | हिमालयन क्षेत्र |
| कुरुवा | झारखंड |
| पामलू | मणिपुर |
| दीपा | छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, अंडमान – निकोबार द्वीप समूह |
(ii) चलवासी पशुचारण (Nomadic Herding)
चलवासी पशुचारण सहारा के अर्द्धशुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेशों, मध्य एशिया और भारत के राजस्थान तथा जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है. भारत के राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में पशुपालन का घुमन्तु तरीका अपनाया जाता है.
इन इलाकों में विषम जलवायु होता है. इसलिए अलग-अलग मौसम में अलग-अलग स्थानों पर चारागाह और जल उपलब्ध होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए ये पशुपालक निश्चित रास्तों से अपने पशु के साथ प्रवास करते है. इस तरह प्रकृति से इन्हें पशु चारा और जल मिल पाता है.
भेड़, ऊंट, याक, बकरियां और अन्य अनुकूल मवेशी पशुचारण के लिए चुना जाता है. इन मवेशियों से इन्हें दूध, मांस, खाल, ऊन और अन्य पशु उत्पाद प्राप्त करते है. ये उत्पाद आर्थिक महत्व के होते है और पशुपालकों का निर्वाहन में अहम् भूमिका निभाता है.
4. सिंचित कृषि (Irrigation Agriculture)-
जिन क्षेत्रों में 50 से 100 सेमी. वार्षिक वर्षा होती है वहॉ जमीन में नमी की कमी होती है. शुष्क काल में यह क्षेत्र बिल्कुल नमी विहीन हो जाता है. फलत: ऐस क्षेत्रों में सिंचाई की मदद से donoफसलें खरीफ और रबी उगाई जाती है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूर्वी तटीय डेल्टाई भाग और मध्यवर्ती प्रायद्वीप की कुछ नदी घाटियों एवं तालाबों के समीपवर्ती भागो में ऐसी कृषि की जाती है.
5. अर्द्ध सिंचित कृषि –
जिन भागों में 100 सेमी. से 200 सेमी. वर्षा होती है. जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ओर पूर्वी मध्य प्रदेश, वहॉ की खरीफ की फसल ें पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है जिसमें धान की कृषि प्रधान रूप से की जाती है. शुष्क काल में रबी की फसलें सामान्य: सिंचाई से की जाती है क्योंकि जमीन में कुछ नमी बनी रहती है. गेहॅु, चना, तिलहन और गन्ना इस समय विशेष रूप से उगाये जाते है.
6. शुष्क कृषि –
जिन क्षेत्रों में 50 सेमी के आस-पास वर्षा होती है वहॉ मिट्टी की नमी के आधार पर शुष्क कृषि की जाती है. ऐसी कृषि में उन फसलों की प्रधानता होती है जा कम नमी के बावजूद उपज दे सके जैसे – चना, ज्वार-बाजरा, तिलहन, जौ, केसरी आदि. दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कनार्टक, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, एवं तमिलनाडु के पठारी भागों में एसे ी कृषि की जाती है.
7. पहाड़ी कृषि –
पहाड़ी ढालों पर जहॉ वषार् और धूप की सुविधा उपलब्ध होती है वहॉ सीढ़ीदार खेतों से अनाज एवं फल की कृषि की जाती है. हिमालय में कश्मीर से लेकर पूर्वी भाग तक इस प्रकार की कृषि की जाती है. लेकिन कुछि क्षेत्रों में विकसित बागवानी का भी प्रचलन है. चाय की कृषि इसका प्रमुख उदाहरण है. कुछ क्षेत्रों में फल के बागों की प्रधानता है विशेषकर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के हिमालय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय के बागों की प्रधानता है.
8. रोपण कृषि-
इस प्रकार के कृषि में मुख्यतः बागवानी और वाणिज्यिक महत्व के फसल उपजाए जाते है. रबर, चाय, केला, काजू, कहवा और कपास इसके मुख्य फसल है. ये फसल ख़ास इलाकों में ही उगाए जा सकते है. इसलिए इन इलाकों में इससे जुड़े उद्योगों और यातायात सेवा का भी विकास हो जाता है. रोजगार के दृष्टि से भी इस प्रकार के कृषि काफी अच्छे साबित होते है.
भारत और श्रीलंका में चाय, ब्राजील में कॉफ़ी, मलेसिया में रबर इसके उदाहरण है. रोपण कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाए जाते है.
9. मिश्रित कृषि-
इस प्रकार के कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और पशु चारा उपजाने तथा पशुपालन के लिए किया जाता है. यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से, यूरोप, अर्जेंटीना, दक्षिण-पूर्व ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और नूज़ीलैण्ड में प्रचलित है.
10. वाणिज्यिक कृषि-
इस प्रकार के कृषि का उद्देश्य कृषि उत्पाद का व्यापार करना या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल का प्रबंध करना होता है. इसमें खेतों के बड़े इलाके उपयोग में लाए जाते है. सामान्यतः बड़े और आधुनिक मशीनों और कृषि वैज्ञानिकों के मदद से वृहद् उत्पादन किया जाता है.
उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का शीतोष्ण घास का मैदानों में इसका प्रसार है. गेंहू और मक्का इसकी मुख्य फसल है. इसमें मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि और रोपण कृषि शामिल है.
कृषि विधियाँ और तकनीकें (Agricultural methods and techniques)
विश्व में कृषि से बेहतर उपज व अन्य कारणों से अलग-अलग तकनीकों व विधियों का उपयोग किया जाता है. ये तकनीक व विधियाँ इस प्रकार हैं:
परती छोड़ना (Fallow Farming)
लगातार एक ही खेत में खेती करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है. इस समस्या से निपटने के लिए, किसान खेत को कुछ समय, आमतौर पर तीन से चार साल तक, बिना बुवाई के खाली छोड़ देते हैं. इस प्रक्रिया को परती छोड़ना कहा जाता है. इस अवधि में, मिट्टी को प्राकृतिक रूप से अपनी खोई हुई उर्वरता वापस पाने का मौका मिलता है, जिससे वह अगली फसल के लिए तैयार हो जाती है. यह एक सदियों पुरानी और टिकाऊ विधि है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखती है.
चक्रीय कृषि (Crop Rotation)
चक्रीय कृषि एक ऐसी आधुनिक और प्रभावी तकनीक है जिसमें परती छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसमें किसान एक ही खेत पर अलग-अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है. इस प्रणाली में, अक्सर फलीदार फसलें जैसे दालें, मटर या सोयाबीन को शामिल किया जाता है. ये फसलें जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया की मदद से हवा से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाती हैं, जिससे मिट्टी और भी उपजाऊ बनती है.
मिश्रित शस्यन (Mixed Cropping)
मिश्रित शस्यन में एक ही खेत पर एक साथ कई तरह की फसलें बोई जाती हैं. यह विधि इसलिए कारगर है क्योंकि इसमें एक फसल द्वारा उपयोग किए गए पोषक तत्वों की भरपाई दूसरी फसल कर देती है. इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है. इसके अतिरिक्त, इस तकनीक में अक्सर फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन को भी जोड़ा जाता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है और कृषि प्रणाली अधिक मजबूत बनती है.
द्विफसली कृषि (Double Cropping)
द्विफसली कृषि एक वर्ष में एक ही खेत पर दो अलग-अलग फसलें उगाने की तकनीक है. इस विधि का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हुए अधिकतम पैदावार प्राप्त करना है. इसमें आमतौर पर एक नाइट्रोजन-स्थिरीकरण वाली फसल (जैसे दालें) को शामिल किया जाता है. यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है या पर्याप्त वर्षा होती है. इसका सीधा मतलब है कि किसान एक साल में दो अलग-अलग मौसमों में फसल उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं.
रिले कृषि (Relay Cropping)
रिले कृषि, जिसे रिले फसल भी कहते हैं, एक बेहद अनूठी और गहन कृषि तकनीक है. इसमें पहली फसल की कटाई से पहले ही, उसके बीच खाली जगह में दूसरी फसल की बुवाई कर दी जाती है. इस तरह, किसान को पहली फसल के कटने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और समय की बचत होती है. यह विधि द्विफसली कृषि से अलग है क्योंकि इसमें दोनों फसलें कुछ समय के लिए एक साथ बढ़ती हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र से मिलने वाली पैदावार अधिकतम हो जाती है.
कृषि का महत्व (Importance of Agriculture)
कृषि, व्यवसाय और समाज दोनों के लिए आवश्यक है. यह कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलबध करवाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बरकरार रखता है. इस तरह यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में मदद करता है.
1. कच्चे माल की आपूर्ति
कृषि द्वारा हमे लकड़ी प्राप्त होता है, जो कई उत्पाद के निर्माण में काम आता है. यह खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने वाली जड़ी-बूटियों, मसाले और अति आर्थिक महत्व का रेशा तक हमे प्रदान करता है. उदाहरण के लिए, मक्का भोजन का एक स्रोत है. लेकिन इसका उपयोग इथेनॉल बनाने में भी होता है, जो एक जैव ईंधन है. इसी तरह, पौधों पर आधारित रेजिन और पेंट जैसे उत्पादों के लिए आवश्यक कई उत्पादों का आपूर्ति कृषि के माध्यम से होता है.
2. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना
विश्व के कई हिस्सों में कृषि उपज अधिक है तो कुछ हिस्सों में काफी कम. ऐसे में सुचारु कृषि के माध्यम से ही कमी या अधिकता को पाटा जा सकता है. किसी भी व्यवधान का व्यापक प्रभाव हो सकता है, जो दुनिया भर में खाद्य संकट उत्पन्न कर सकता है. उदाहरण के लिए, 2022 में रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने से गेंहू की वैश्विक उपलब्धता में कमी आई और खाद्य संकट की स्थिति से विश्व को गुजरना पड़ा.
3. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
कृषि कई प्रकार का रोजगार उपलब्ध करवाता है. भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि पर निर्भर होता है. कृषि अनुसंधान, खाद, कृषि उपज का परिवहन, कृषि उपकरण और बीजों के कारोबार शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन में सहायक है. प्रति किसान कृषि जोतो का सही आकार उत्पादकता और प्रति-व्यक्ति आय में काफी सुधार ला सकता है.
लकड़ी और बांस का उपयोग आवास और आधारभूत संरचना के विकास में भी किया जाता है. इनसे बने मकान कंक्रीट के तुलना में काफी सस्ते, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ होते है.
प्रमुख कृषि उत्पाद और इनके महत्व (Main Agriculture Produces and its Values)
कृषि उपभोक्ता और व्यावसायिक बाजारों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है. हम अपने दिनचर्या का शुरुआत भी किसी न किसी कृषि उत्पाद से ही करते है. हमारे टूथपेस्ट का पुदीना भी एक कृषि उत्पाद ही है. यह बाजार को कई प्रकार के आवश्यक उत्पाद प्रदान करती है:
- फल और सब्जियाँ: ये आहार संबंधी मुख्य खाद्य पदार्थ हैं. ये विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो पोषण मूल्य और स्वाद दोनों को बढ़ाते हैं.
- पशु चारा: कृषि घास और अनाज जैसे चारे का उत्पादन करती है, जिसपर मुर्गी पालन जैसे पशुधन उद्योगों का विकास निर्भर है.
- प्राकृतिक रबर: दुनिया में 1.4 बिलियन से अधिक वाहन है. इनके टायरों के लिए आवश्यक प्राकृतिक रबर का अधिकांश हिस्सा एशिया के छोटे पैमाने के किसानों द्वारा किया जाता है.
- कपड़ों के लिए रेशा: कपास का रेशा विशाल वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है. दुनिया भर में कपड़ा फाइबर का लगभग 31% कपास से ही बनता है.
- जैव ईंधन: मकई, गणना और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जाता है. ये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण संतुलन का काम करता है.
- औद्योगिक उत्पाद: कृषि उत्पादों से प्राप्त जैव-रसायनों का उपयोग डिटर्जेंट से लेकर उर्वरकों तथा पेट्रोलियम-आधारित उत्पादों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है.
- फार्मास्यूटिकल्स: पौधे प्राकृतिक उपचार और दवाओं के लिए सामग्री प्रदान करते हैं, जैसे कि फॉक्सग्लोव पौधे से प्राप्त हृदय की दवा डिगॉक्सिन.
कृषि को प्रभावित करने वाले तत्व (Factors affecting Agriculture)
कृषि को प्रभावित करने में भिन्न- भिन्न प्रकार के कारकों एवं तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है.
1. बाजार –
बाजार से कृषि पर प्रभाव पड़ता है. जिन क्षेत्रों में बाजार काफी दूर है. उन क्षेत्रों में कृषि के रूप में विभिन्नता पायी जाती है. दूरी बढ़ने पर किसानों का े अपने उत्पादित पदार्थों का उचित फायदा नहीं मिल पाता है. कभी-कभी तो बाजार के दूर होने पर उत्पादन का लागत भी नहीं निकल पाता है. किन्तु इसी के विपरीत अगर बाजार समीप होता है. तो किसान उत्पादन लागत के ं साथ मुनाफा भी कमा सकता है.
2. परिवहन –
परिवहन एक महत्वपूर्ण तथ्य है. इसकी समुचित व्यवस्था होने से समय की अत्यधिक बचत होती है. कृषि उत्पाद के आदान- प्रदान में तेजी आती है. तथा जल्दी समाप्त होने अथवा नष्ट होने वाले प्रदार्थो को जल्दी से परिवहन द्वारा बाजार तक पहुंचाया जा कर लाभ कमाया जा सकता है.
3. श्रम –
कृषि को प्रभावित करने वाले तत्वों में श्रम एक विशिष्ट कारक है. कृषि ज्यादा मानवीय श्रम के द्वारा ही संपन्न होती है. श्रमिकों की उचित व्यवस्था अच्छे परिणाम के लिये अत्यन्त आवश्यक है. इसके अभाव में परिणाम की आकांक्षा व्यर्थ है.
4. जोत आकार –
कृषि को कृषिजोत का आकार बहतु प्रभावित करता है. किसी भी फसल ें की कृषि उसके जोत के आकार पर निर्भर करता है. जितना बढ़ा जोत उतनी अच्छी सिंचार्इं एवंउतना ही अच्छा उत्पादन अत: जोत का आकार अच्छे उत्पादन को इंगित करता है.
5. मृदा –
कृषि की आधारशिला मिट्टी है. जो परोक्ष तौर पर उपयोगी है. मिट्टी के अलग- अलग प्रकार होते है इसकी उपजाऊ क्षमता इसे भिन्न भिन्न करती है. उत्तम कृषि हेतु मृदा की अहम 56 भूमिका है. इसके अभाव में तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है. मृदा का तापक्रम, मृदा की उर्वरता मृदा जिवांश आदि कृषि को प्रभावित करती है.
6. जलवायु –
भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में प्रमुख कारक जलवायु का स्थान है. इसके माध्यम से कृषि के विभिन्न प्रकार के स्वरूप निर्धारित एवं नियंत्रित होते है. विशेषकर आज के वैज्ञानिक युग में कृषि पर जलवायु का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है. अत: इसे जलवायु पर निर्भर एक उद्योग कह सकते है.
7. तापमान –
एक उचित तापमान बीजों के जमने या अंकुरण, वनस्पतियों के वर्धन होने के लिए बहुत आवश्यक है. काइेर् भी बीज या पौधा उपयुक्त तापमान की कमी में विकसीत नहीं हा े सकता.
8. सौर प्रकाश –
सौर प्रकाश का वनस्पतियों के विकास एवं वितरण को प्रभावित करने में विशिष्ट योगदान होता है. वनस्पतियों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. और सूर्य के इसी विकिरण उर्जा से पौधों की पर्णहरीतिमा के माध्यम से कुछ तरंग का अवशोषण करके भाजे न बनाते है. इसके अभाव में भोजन बना पाना असंभव है.
9. वर्षा –
मृदा के विभिन्न प्रकार के पोशक तत्व को पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है. जल की पूर्ति करने हेतु वृष्टि या कृत्रिम माध्यमों द्वारा सिंचाई की जाती है. इसलिए फसलों हेतु अनुकूल तापमान ही की तरह अनुकूलतम नमी की मात्रा भी आवश्यक है. पौधे नमी अपने जड़ो से धारण करते है. अत: मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है.
10. वायु –
वायु कृषि को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती है. नमी एवं तापमान दोनों का ही परिवहन हवा के जरिये होता है. जिससे वाश्पीकरण की प्रक्रिया संभव होता है. हवा के माध्यम से ही बीजो व परागों का प्रसरण होता है.
11. पाला –
कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान बिना समय के पड़ने वाले पाले से होता है.
12. उच्चावच –
किसी प्रदेश की उच्चतम एवं न्यूनतम भागो के ऊचाई के अन्तर को उच्चावच की संज्ञा प्रदान की है. यह खेती को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है. क्योंकि फसलों के वितरण एवं सम्बंधित कार्य धरातलीय स्वरूप पर ही आधारित है.