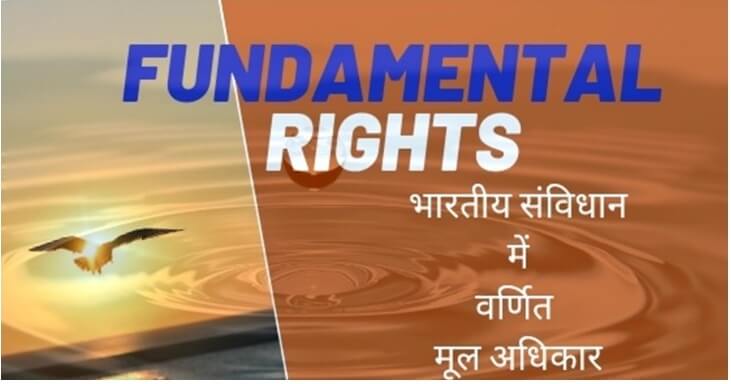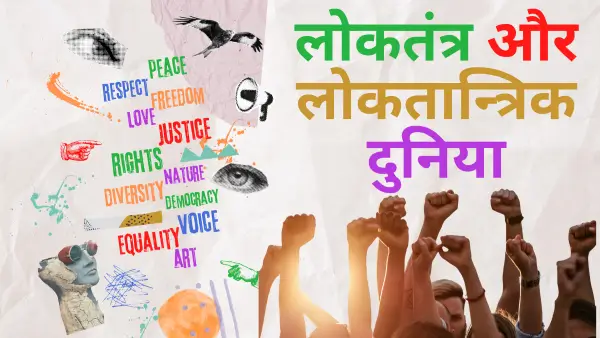भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का एक अंग है. महान्यायवादी (AG) देश कासर्वोच्च विधि अधिकारी होता है. संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद से संबंधित प्रावधान किए गए है. कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह एवं परामर्श देना इनका मुख्य काम है.
औपनिवेशिक काल में भारत का महान्यायवादी
भारत का महान्यायवादी का पद ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान अस्तित्व में आया है. इसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया था. शुरुआत में इस पद को एडवोकेट जनरल कहा जाता था.
भारत सरकार अधिनियम 1935 में नियुक्ति की शर्तें और कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देने के उनके कार्य निर्दिष्ट किए गए थे. स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 76 में शामिल किया गया और एडवोकेट जनरल के पद का नाम बदलकर महान्यायवादी (Attorney General) कर दिया गया.
नियुक्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के नियुक्ति का प्रावधान है. इन नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है.
कार्यकाल
अनुच्छेद 76 (4) के अनुसार, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ही अपने पद पर कार्यरत रहता है. इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष के लिए की जाती है. महान्यायवादी का कार्यकाल अनिश्चित होता है. (अर्थात राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत)
वेतन एवं भत्ते
महान्यायवादी के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं. वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे. उसे एक संसद सदस्य की तरह ही सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त हों.
कार्य एवं शक्तियां
- अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको निर्देशित करें या सौंपे. संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है.
- यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हो सकता, बोल सकता है किन्तु उसे मत (वोट) देने का अधिकार प्राप्त नहीं है.
- संविधान के अनुच्छेद 76(3) के अनुसार, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए किसी भी मामले में उन्हें केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है.
- वह किसी भी न्यायिक कार्यवाही में भाग भी ले सकता है. निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है. लेकिन सरकार के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकता है.
- महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं. सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं. जो अन्य विधि अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं.
- राज्य सरकारों को विधि सहायता या परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता (Advocate general) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है. महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है. महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह एवं परामर्श देता है. वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है.
स्वतंत्र भारत के पहले महान्यायवादी
भारत के प्रथम महान्यायवादी एम. सी. सीतलवाड़ थे. वे 28 जनवरी, 1950 से 1 मार्च, 1963 तक इस पद पर रहे. वर्तमान में (16वें) आर. वेंकटरमणी महान्यायवादी हैं और वर्तमान में तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं.
भारत का महान्यायवादी की सूची (List of AGs in India)
| क्र.सं. | नाम | कार्यकाल |
| 1. | एम. सी. सीतलवाड़ | 1950–1963 |
| 2. | सी. के. दफ्तरी | 1963–1968 |
| 3. | निरेन डे | 1968–1977 |
| 4. | एस. एन. गुप्ते | 1977–1979 |
| 5. | एल. एन. सिन्हा | 1979–1983 |
| 6. | के. पराशरन | 1983-1989 |
| 7. | सोली जे. सोराबजी (सबसे छोटा कार्यकाल) | 1989-1990 |
| 8. | जी. रामास्वामी | 1990-1992 |
| 9. | मिलन के. बनर्जी | 1992-1996 |
| 10. | अशोक देसाई | 1996-1998 |
| 11. | सोली सोराबजी | 1998-2004 |
| 12. | मिलन के. बनर्जी | 2004-2009 |
| 13. | गुलाम ई. वाहनवती | 2009-2014 |
| 14. | मुकुल रोहतगी | 2014-2017 |
| 15. | के.के. वेणुगोपाल | 30.06.2017-30.09.2022 |
| 16. | आर वेंकटरमणी | 1.10.2022 से लगातार |