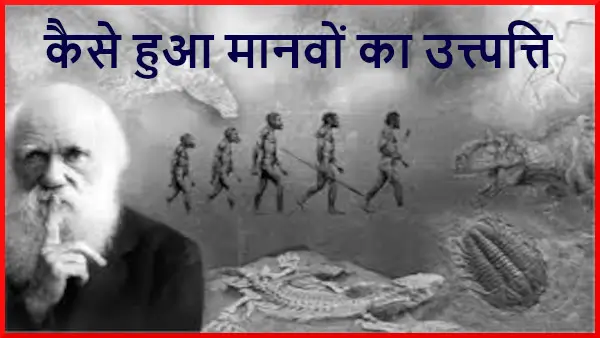क्लोनिंग को जैव प्रौद्योगिकी का ही एक शाखा माना जाता है. इस प्रक्रिया है में किसी डीएनए खंड, जीव या कोशिका की आनुवंशिक रूप से समान प्रतियां बनाई जाती हैं. इस प्रति को क्लोन और तकनीक को क्लोनिंग कहा जाता है. उत्पादित क्लोन में मूल जीव या कोशिका के समान ही आनुवंशिक संरचना होती है. सरल शब्दों में, यह अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करने का कार्य है. उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं.
क्लोनिंग कैसे सम्पन्न होता हैं?
एक बच्चा एकल कोशिका (अंडा कोशिका) से बनता है. इसमें पिता और मां दोनों का डीएनए होता है. यह कोशिका पूर्ण रूप से बच्चे को बनने के लिए लाखों में विभाजित होती है. यह विभेदीकरण (differentiation) कहलाता हैं. प्रत्येक सेल मूल सेल की एक कॉपी होता है और उसमें समान आनुवंशिक कोड होता है.
क्लोनिंग में एक बड़ी चुनौती कायिक कोशिकाएं (सोमैटिक सेल) हैं. ये प्रजनन कोशिकाओं को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से से हो सकती हैं, जैसे रक्त कोशिकाएं या मांसपेशी कोशिकाएं. ये कोशिकाएं विभेदित होती हैं, यानी विशेष कार्य के लिए तैयार होती हैं. क्लोनिंग में इन कोशिकाओं के केंद्रक को पुनः प्रोग्राम करना पड़ता है. ताकि वे फिर से एक पूर्ण जीव बना सकें.
क्लोनिंग की सफलता सिर्फ डीएनए की प्रतिकृति पर निर्भर नहीं है. असल में यह विभेदित कायिक कोशिकाओं को फिर से एक पूरा जीव बना सकती है. यह साबित करता है कि कोशिका के केंद्रक में मौजूद आनुवंशिक जानकारी, भले ही कोशिका विशेष काम के लिए तैयार हो चुकी हो, फिर भी पूरे जीव के विकास के सारे निर्देश रखती है. ‘पुनर्प्रोग्रामिंग’ का मतलब है कोशिका की पहचान बदलना.
सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर (SCNT) तकनीक में, एक विभेदित कोशिका का केंद्रक लिया जाता है. इसे एक ऐसे अंडाणु में डाला जाता है जिसका केंद्रक पहले से हटा दिया गया हो. अब इस केंद्रक को अपनी पुरानी पहचान ‘भूलनी’ पड़ती है. अंडाणु के कोशिका द्रव्य के संकेत इसे फिर से भ्रूण के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं. यही पुनर्प्रोग्रामिंग क्लोनिंग को संभव बनाती है.
क्लोनिंग के प्रकार (Types of Cloning in Hindi)
क्लोनिंग को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: आणविक क्लोनिंग (या जीन क्लोनिंग), प्रजनन क्लोनिंग और चिकित्सीय क्लोनिंग. इनके उद्देश्य और प्रक्रियाएँ भिन्न होती हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:
आणविक क्लोनिंग/जीन क्लोनिंग (Molecular Cloning/Gene Cloning)
आणविक क्लोनिंग में किसी जीव से निकाले गए समस्त डीएनए में से किसी महत्वपूर्ण जीन का पता लगाया जाता है. फिर इसकी प्रतिलिपि बनाई जाती है. इसे किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतिलिपियां तैयार करने की विधि भी कहा जाता है. इस प्रक्रिया में, एक वांछित जीन को किसी वाहक (जैसे प्लास्मिड) के साथ जोड़ दिया जाता है.
यह प्रक्रिया मुख्यतः रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग करती है. इस तकनीक में दो या अधिक जीवों से प्राप्त डीएनए अंशों को मिलाकर प्रयोगशाला में नया डीएनए अणु बनाया जाता है. यह संभव है क्योंकि सभी डीएनए का रासायनिक आधार समान होता है.
इस प्रक्रिया के चरणों में जीन का चयन और कटाई (प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग करके), चयनित जीन को वेक्टर में डालना, इस वेक्टर को होस्ट जीव (जैसे ई. कोलाई जीवाणु) में प्रविष्ट कराना, और फिर होस्ट जीव का नए जीन के अनुसार प्रोटीन या अन्य उत्पाद का उत्पादन करना शामिल है.
पीसीआर (पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन) तकनीक का उपयोग भी डीएनए की कृत्रिम प्रतिकृति बनाने के लिए होता है. आणविक क्लोनिंग का उपयोग इंसुलिन और हार्मोन का उत्पादन, रोग-प्रतिरोधक पौधों का निर्माण, उच्च उपज वाली फसलों का विकास, और चिकित्सीय क्षेत्र में जीन थेरेपी के लिए किया जाता है.
प्रजनन क्लोनिंग (Reproductive Cloning)
इस तकनीक में अलैंगिक विधि द्वारा एकल जनक द्वारा नया जीव तैयार किया जाता है. प्रजनन क्लोनिंग का मुख्य उद्देश्य आनुवंशिक रूप से समान व पूर्ण जीव की प्रतिकृति तैयार करना है. इस प्रक्रिया में सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर (SCNT) तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसे न्यूक्लीयर ट्रांसफर भी कहते हैं.
SCNT प्रक्रिया के विस्तृत चरण इस प्रकार हैं:
- सेल संग्रह: वैज्ञानिक वयस्क जीव से एक सोमैटिक सेल (गैर-प्रजनन कोशिका) लेते हैं. इसमें जीव का पूरा डीएनए मौजूद होता है. सोमैटिक सेल शरीर के किसी भी हिस्से से ली जा सकती है, जैसे मांसपेशी या त्वचा.
- अंडाणु कोशिका की तैयारी: एक दूसरी वयस्क जीव से एक अंडाणु कोशिका ली जाती है. उसका नाभिक (nucleus), जिसमें डीएनए होता है, हटा दिया जाता है. इससे अंडाणु कोशिका खाली हो जाती है.
- नाभिकीय हस्तांतरण: सोमैटिक सेल से प्राप्त नाभिक को खाली अंडाणु कोशिका में डाल दिया जाता है.
- उत्तेजना: अंडाणु कोशिका को विद्युत् झटका देकर इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है ताकि वह विभाजित होकर भ्रूण में विकसित होने लगे, जैसे एक सामान्य निषेचित अंडाणु करता है.
- प्रतिरोपण: विकसित हो रहे भ्रूण को एक स्वीकारकर्ता माता (सरोगेट माँ) जीव में प्रतिरोपित किया जाता है, जहाँ वह जन्म तक बढ़ता है.
डॉली भेड़ का ऐतिहासिक क्लोन
डॉली पहली स्तनधारी थीं जिन्हें एक वयस्क सोमैटिक सेल से क्लोन किया गया था. यह 1996 का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि था. डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के रोजलिन इंस्टीट्यूट में हुआ था. इसे शोधकर्ता इयान विल्मोट और कीथ कैंपबेल द्वारा अंजाम दिया गया था. लेकिन, इसके जन्म की घोषणा फरवरी 1997 में की गई. इस क्लोन भेड़ को गायिका डॉली पार्टन के नाम पर डॉली नाम दिया गया था.
डॉली ने अपना सारा जीवन रोजलिन संस्थान में गुजारा और 6 बच्चों को जन्म दिया. फरवरी 2003 में फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारी के कारण सात साल की उम्र में डॉली की मृत्यु हो गई. डॉली की क्लोनिंग ने लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण और जानवरों की संख्या वृद्धि में सहायता की संभावनाओं को उजागर किया, लेकिन साथ ही क्लोनिंग के दुरुपयोग के बारे में दुनिया भर में चर्चा भी शुरू कर दी.

| ‘डॉली’ का जन्म क्यों खास उपलब्धि हैं? |
| स्तनपायी जीवों में भ्रूण (Embryo) का बनना मादा की अंड कोशिका (Ovum) के साथ नर के शुक्राणु (Sperm) के सम्मिलन पर निर्भर है. यही प्राकृतिक नियम है लेकिन डॉ. विल्मुट ने इस प्राकृतिक नियम का अतिरेक कर दिया. उन्होंने एक फिनलैंडी मादा भेड़ के थन से कायिक कोशिका निकालकर, एक स्कॉटिश मादा भेड़ की नाभिक रहित अंडकोशिका का विद्युत आवेश की मदद से योग करा देने में सफलता प्राप्त की और प्रायः 6 दिन बाद (Blastocyst Stage) इस भ्रूण को उसी स्कॉटिश मादा भेड़ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया. यद्यपि यह सब इतना सहज नहीं था. विल्मुट और उनके सहयोगियों को निरंतर 277 प्रयासों के बाद मात्र 29 भ्रूण प्राप्त हुए जो 6 दिनों से अधिक समय तक जीवित रहे. इनमें से भी एक को छोड़कर शेष सभी काल-कवलित हो गए. एकमात्र भ्रूण जो जीवित बचा, उसी से पाँच महीनों के बाद दुनिया की प्रथम स्तनपायी क्लोनित भेड़ ‘डॉली‘ जन्मी. |
चिकित्सीय क्लोनिंग (Therapeutic Cloning)
चिकित्सीय क्लोनिंग का उद्देश्य शोध और चिकित्सा उपचार के लिए कोशिकाएँ तैयार करना होता है. इस प्रक्रिया में एक विशेष जीव के आनुवंशिक रूप से सर्वसम कोशिकाएँ बनाएं जाते है. इसका मुख्य उद्देश्य स्टेम कोशिकाओं (Stem cells) का उत्पादन करना है. स्टेम कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता विद्यमान होती है.
चिकित्सीय क्लोनिंग की प्रक्रिया प्रजनन क्लोनिंग के समान ही भ्रूण निर्माण तक होती है, जिसमें SCNT का उपयोग किया जाता है. भ्रूण के तैयार होने की आरंभिक अवस्था में इससे ‘स्टेम सेल’ को अलग कर लिया जाता है. फिर इन कोशिकाओं को स्टेम कोशिकाओं के रूप में संग्रहित किया जाता है. इनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है.
इन स्टेम कोशिकाओं का उपयोग विभिन्न रोगों का अध्ययन करने, इलाज विकसित करने या चिकित्सा उद्देश्यों के लिए नए ऊतक या अंग उगाने में किया जा सकता है. संभावित अनुप्रयोगों में क्षतिग्रस्त ऊतक या अंगों का निर्माण, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर, हेपेटाइटिस और हृदय रोग जैसी कई खतरनाक बीमारियों के इलाज में सहायता, और चिकित्सीय शोध के लिए आवश्यक शरीर मुहैया कराना शामिल है.
प्राकृतिक क्लोनिंग बनाम कृत्रिम क्लोनिंग
क्लोनिंग प्राकृतिक रूप से भी होती है. प्रकृति में यह सामान्य रूप से अलैंगिक प्रजनन वाले सूक्ष्मजीवों जैसे अमीबा में पाया जाता है. मोनोज़ाइगोटिक (समान) जुड़वाँ बच्चे भी प्राकृतिक क्लोन का एक उदाहरण हैं, क्योंकि वे एक ही निषेचित अंडे से विकसित होते हैं और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं.
बागवानी में, वानस्पतिक प्रजनन (जैसे कलम लगाना) और अपोमिक्सिस (अलैंगिक रूप से बीजों का निर्माण) भी प्राकृतिक क्लोनिंग के उदाहरण हैं. इसके विपरीत, कृत्रिम क्लोनिंग प्रयोगशाला में वैज्ञानिक तकनीकों (जैसे जीन क्लोनिंग और SCNT) का उपयोग करके की जाती है.
क्लोनिंग के अनुप्रयोग
क्लोनिंग तकनीक ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व संभावनाएँ खोली हैं. इसके अनुप्रयोग चिकित्सा, कृषि, पशुधन और संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होते है, जो इस प्रकार हैं:
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा
- क्षतिग्रस्त ऊतक व अंगों का निर्माण और सटीक अंग प्रत्यारोपण संभव.
- आनुवंशिक व असाध्य रोगों का उपचार, दोषपूर्ण जीन को बदलना.
- कैंसर, हृदय रोग, हेपेटाइटिस आदि के इलाज में सहायक.
- दवाओं, टीकों, इंसुलिन व चिकित्सीय प्रोटीन का उत्पादन.
- रोग अध्ययन, ट्रांसजेनिक जानवरों का निर्माण, व्यक्तिगत चिकित्सा (Personalized Medicine) में उपयोग.
- SCNT द्वारा रोगी-विशिष्ट स्टेम सेल व अंग निर्माण, प्रतिरक्षा अस्वीकृति का कम जोखिम.
कृषि और पशुधन
- उच्च गुणवत्ता व रोग-प्रतिरोधक फसलों का विकास (जैसे बीटी कपास, गोल्डन राइस).
- कीट-प्रतिरोधी व अधिक पैदावार वाली फसलें, कठिन जलवायु में उगने योग्य किस्में.
- पशुधन में नस्ल सुधार व उत्पादकता बढ़ाना (जैसे मुर्रा भैंस, गिर नस्ल की ‘गंगा’ बछिया).
- बेहतर दुग्ध उत्पादन और रोग-प्रतिरोधक पशु.
लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण
- विलुप्त या विलुप्तप्राय प्रजातियों का पुनर्जीवन (De-extinction).
- जैव विविधता व जीन पूल का विस्तार, आनुवंशिक विविधता की कमी को दूर करना.
- उदाहरण: 2020 में काले पैरों वाले फेरेट “एलिजाबेथ एन” का क्लोन, मंगोलियाई जंगली घोड़े का क्लोन.
अन्य अनुप्रयोग
- प्लास्टिक सर्जरी व क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत.
- निःसंतानता का उपचार.
- आणविक जीव विज्ञान में जीन के अध्ययन और हेरफेर में उपयोग.
क्लोनिंग से लाभ (Advantages of Cloning)
क्लोनिंग की सहायता से विशेष ऊतकों व अंगों का निर्माण कर वैसी असाध्य व आनुवंशिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है, जो परंपरागत चिकित्सकीय विधियों से ठीक नहीं हो सकतीं.
कैंसर के उपचार में इसका विशेष महत्त्व है क्योंकि कैंसर में कोशिकाएँ विभाजित होने लगती हैं, जिसमें कुछ कोशिकाएँ तो पुनर्रचित हो जाती हैं किंतु अन्य नहीं. क्लोनिंग के द्वारा इन कोशिकाओं की पुनर्रचना की जा सकेगी, विशेषतः हृदय व मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना.
ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन (Xenotransplantation) की न्यून सफलता को देखते हुए अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में क्लोनिंग क्रांति ला सकती है. उल्लेखनीय है कि थेराप्यूटिक क्लोनिंग के द्वारा लीवर, किडनी आदि का निर्माण कर अंग प्रत्यारोपण में मदद मिलेगी.
क्लोनिंग द्वारा विशेष प्रकार की वनस्पतियों व जीवों का क्लोन बनाया जा सकता है, जिससे महत्त्वपूर्ण औषधियों का निर्माण तथा जैव विविधता का भी संरक्षण किया जा सके.
आणविक क्लोनिंग के उपयोग से अनेक मानवोपयोगी प्रोटीनों, जैसे-इंसुलिन आदि का निर्माण किया जा रहा है.
क्लोनिंग के नुकसान (Disadvantages of Cloning)
मानव क्लोन से अपराध बढ़ने की आशंका है. जिस जीव की कोशिका का केंद्रक लिया जाता है, क्लोन उसकी कार्बन कॉपी होता है यानी क्लोनिंग से एक ही तरह के कई लोग पैदा हो सकते हैं.
क्लोन सैनिक तैयार कर पुनः विकसित व धनी देश साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की अवधारणा को जीवित कर सकते हैं तथा वैश्विक आतंकवाद के रूप में, मानव बम के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है.
क्लोनिंग से बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या होगी क्योंकि इसमें सफलता का प्रतिशत बहुत कम है. इस प्रक्रिया में जेनेटिक त्रुटियाँ भी उपस्थित हो रही हैं और कई प्रयोगों में प्रिमैच्योर एजिंग (Premature Ageing) की समस्या देखी जा रही है.
वर्तमान सामाजिक संरचना, जैसे-पारिवारिक संस्था प्रभावित होगी क्योंकि क्लोनिंग के लिये एकल जनक ही उत्तरदायी होगा.
क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न बच्चे और सरोगेट मदर में क्या रिश्ता होगा, इसका निर्धारण करना भी दुष्कर होगा.
मानव अंगों के व्यापार होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. मानव जीवन की महत्ता में कमी आएगी. इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए पूरे विश्व में मानव क्लोनिंग को प्रतिबंधित किया गया है.
क्लोनिंग के अन्य पहलुएं
क्लोनिंग ने कई बहसों को जन्म दिया है. इसलिए कानून द्वारा इसे नियंत्रित करने का प्रयास भी हुआ हैं:
नैतिक चिंताएँ
- मानव गरिमा व पहचान पर प्रश्न – केवल एक जैविक जनक होने से पारिवारिक संरचना पर असर, क्लोन की पहचान का संकट और संभावित मनोवैज्ञानिक समस्याएँ.
- ‘भगवान बनने’ की बहस – प्राकृतिक क्रम में हस्तक्षेप को लेकर धार्मिक और दार्शनिक आपत्तियाँ.
- कम सफलता दर और पशु पीड़ा – प्रयोग में असफलता, जानवरों की पीड़ा और पशु कल्याण संबंधी मुद्दे.
- क्लोन के अधिकार – भविष्य में समान नागरिक अधिकार और भेदभाव से बचाव का प्रश्न.
सामाजिक प्रभाव
- पारिवारिक और जैविक संबंधों में बदलाव – एक ही जैसे व्यक्तियों से सामाजिक सामंजस्य में कठिनाई.
- भेदभाव और असमानता – क्लोन के साथ सामाजिक भेदभाव का खतरा, विविधता में कमी.
- दुरुपयोग की आशंका – “डिजाइनर बच्चे”, मृत्यु की अवधारणा का महत्व घटना, विशिष्ट गुणों वाले व्यक्तियों के क्लोन का गलत इस्तेमाल.
कानूनी और नियामक ढाँचा
- संयुक्त राष्ट्र (2005): मानव गरिमा के विपरीत मानव क्लोनिंग के सभी रूपों पर गैर-बाध्यकारी प्रतिबंध का आह्वान.
- यूरोपीय संघ: प्रजनन मानव क्लोनिंग पर स्पष्ट प्रतिबंध.
- भारत – प्रजनन क्लोनिंग पर प्रतिबंध, केवल चिकित्सीय क्लोनिंग की अनुमति (शोध हेतु).
- अन्य देश – जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, कनाडा में प्रतिबंध; अमेरिका में संघीय स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं.
- चिंता – नियामक विखंडन, ‘स्लिपरी स्लोप’ का खतरा कि चिकित्सीय अनुमति अनियंत्रित प्रजनन क्लोनिंग तक पहुँच सकती है.