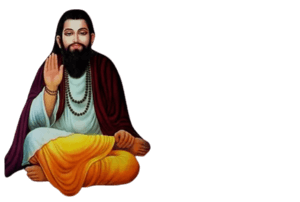“GI टैग” का मतलब भौगोलिक संकेत (Geographical Indication) टैग है. यह एक ऐसा चिह्न है जो उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनके गुण या प्रतिष्ठा उस मूल स्थान के कारण ही होती है.
GI टैग क्या है? (What is GI Tag in Hindi)
GI टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद की उस विशिष्ट क्षेत्र से पहचान स्थापित करता है जहाँ वह उत्पन्न होता है. यह एक प्रमाणन की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं उसके भौगोलिक मूल के कारण हैं.
उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि केवल दार्जिलिंग क्षेत्र में उगाई जाने वाली और विशिष्ट तरीके से संसाधित की जाने वाली चाय ही “दार्जिलिंग चाय” के रूप में बेची जा सकती है.
GI टैग के उद्देश्य और लाभ
GI टैग के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य और लाभ हैं:
- कानूनी सुरक्षा: यह उत्पादों को अनधिकृत उपयोग और नकल से बचाता है. एक बार GI टैग मिलने के बाद, कोई और उस नाम का उपयोग नहीं कर सकता जब तक कि उनका उत्पाद उस विशिष्ट क्षेत्र से न हो और निर्धारित मानकों को पूरा न करता हो.
- उत्पादकों को लाभ: यह स्थानीय उत्पादकों को उनके विशिष्ट उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है. यह उनकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है.
- उपभोक्ताओं के लिए प्रामाणिकता: उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे एक प्रामाणिक और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद खरीद रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति और विशिष्टता प्रमाणित है.
- सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: GI टैग पारंपरिक ज्ञान, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है जो पीढ़ियों से विकसित हुई है.
- निर्यात को बढ़ावा: यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहचान और मांग बढ़ाने में मदद करता है.
‘जीआई मैन ऑफ इंडिया’
रजनी कान्त को ‘जीआई मैन ऑफ इंडिया’ (GI Man of India) के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत में भौगोलिक संकेतक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है. वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) के विशेषज्ञ हैं. वह ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन (Human Welfare Association), वाराणसी के संस्थापक और निदेशक हैं.
रजनी कान्त ने अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्यों के 100 से अधिक उत्पादों को GI टैग दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. उन्हें भारत सरकार, WIPO (World Intellectual Property Organization), और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों द्वारा सम्मानित किया गया है. GI टैग के क्षेत्र में उनके निरंतर प्रयासों के कारण उन्हें “GI मैन ऑफ इंडिया” की उपाधि मिली.
भारत में GI टैग
भारत में, GI टैग माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत प्रशासित किया जाता है, जो 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ. यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा भी मान्यता प्राप्त हैं. भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में GI टैग मिला था.
GI टैग 10 साल के लिए वैध होता है और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है. भारत सरकार “अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने” टैगलाइन के साथ GI उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल कर रही है, जैसे “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)” योजना. भारत में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है, जिनमें शामिल हैं:
- कृषि उत्पाद: जैसे बासमती चावल, नागपुर संतरा, अल्फांसो आम, कश्मीरी केसर.
- हस्तशिल्प: जैसे मैसूर सिल्क, चंदेरी साड़ियाँ, मधुबनी पेंटिंग, कुल्लू शॉल.
- खाद्य पदार्थ: जैसे तिरुपति लड्डू, ओडिशा रसगुल्ला, श्रीविल्लिपुथुर पलकोवा.
- विनिर्मित वस्तुएँ: जैसे डिंडीगुल ताले, मैसूर अगरबत्ती.
बिहार के GI टैग उत्पाद (GI Tag Products of Bihar)
बिहार की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत में कई अनमोल वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें उनकी खासियत और गुणवत्ता के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुआ है. इस टैग से यह साबित होता है कि ये उत्पाद केवल बिहार के खास इलाकों में ही अपनी असली पहचान और बिशेषता के साथ पाए जाते हैं. GI टैग मिलने से न केवल इन उत्पादों की सुरक्षा होती है बल्कि स्थानीय कारीगरों और किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलता है. जिससे बिहार की पारंपरिक कला, कृषि और कारीगरी को बढ़ावा मिलता है. बिहार में अब तक 13 उत्पादों को GI टैग मिल चूका है:
मधुबनी पेंटिंग
मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली है. यह अपनी जीवंतता, जटिल डिजाइनों और गहरी सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता के लिए जानी जाती है.
मधुबनी पेंटिंग को 2007 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ है. यह टैग इस कला की प्रामाणिकता और भौगोलिक उत्पत्ति को प्रमाणित करता है. GI टैग मिलने से इस कला को कानूनी सुरक्षा मिली है, जिससे इसके नाम का अनधिकृत उपयोग रोका जा सकता है और इसकी नकल को भी नियंत्रित किया जा सकता है.
वर्तमान स्थिति
आज, मधुबनी पेंटिंग ने पारंपरिक मिट्टी की दीवारों और फर्शों से आगे बढ़कर कागज, कपड़े, कैनवास, साड़ियों, स्टोल, बैग और अन्य घरेलू सजावट की वस्तुओं पर अपना स्थान बना लिया है. यह कला न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यधिक लोकप्रिय है, और कई कलाकारों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है. सरकार और गैर-सरकारी संगठन इस कला को बढ़ावा देने और इसके कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं.
आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में यहाँ विस्तार से पढ़ सकते हैं.
शाही लीची, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर की शाही लीची भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में अपनी अनूठी मिठास, रसीलेपन और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है. इसे “बिहार का गौरव” भी कहा जाता है. मुजफ्फरपुर की शाही लीची को 2018 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है. हाल ही में, शाही लीची पर डाक टिकट भी जारी किया गया है, जो इसकी बढ़ती राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है.
शाही लीची की विशेषताएँ
मुजफ्फरपुर की जलवायु और मिट्टी शाही लीची के उत्पादन के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, जिससे यहां की लीची का स्वाद और गुणवत्ता अद्वितीय होती है. शाही लीची की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- अद्वितीय स्वाद और सुगंध: यह अपनी असाधारण मिठास, रसीले गूदे और मनमोहक सुगंध के लिए जानी जाती है.
- आकार और रंग: शाही लीची मध्यम से बड़े आकार की होती है, जिसका वजन लगभग 20.5 ग्राम प्रति फल होता है. इसका ऊपरी हिस्सा नरम होता है और रंग हल्का लाल या गुलाबी होता है.
- छोटा बीज: इसमें बीज छोटा होता है, जिससे गूदे का अनुपात अधिक होता है.
- उत्पादन क्षेत्र: मुजफ्फरपुर के अलावा, समस्तीपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण भी शाही लीची के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं. बिहार देश के कुल लीची उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है, जिसमें शाही लीची का बड़ा हिस्सा है.
- पकने का समय: यह मई के दूसरे सप्ताह से जून के पहले सप्ताह के दौरान पकने वाली एक अगेती किस्म है.

जर्दालु आम, भागलपुर
भागलपुर का जर्दालु आम अपनी विशिष्ट सुगंध, मिठास और पोषक गुणों के लिए जाना जाता है. यह बिहार के भागलपुर क्षेत्र की एक प्रमुख पहचान है. भागलपुर के जर्दालु आम को 2018 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया था. यह विशेष किस्म का आम केवल भागलपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में ही अपनी विशिष्ट गुणवत्ता और स्वाद के साथ उगाया जाता है.
जर्दालु आम की विशेषताएँ
जर्दालु आम की कुछ खास विशेषताएँ इसे अन्य आमों से अलग बनाती हैं:
- अद्वितीय स्वाद और सुगंध: यह अपनी खास मीठी सुगंध और स्वादिष्ट, रेशे रहित गूदे के लिए प्रसिद्ध है. इसका स्वाद बहुत ही अनूठा और मनमोहक होता है.
- पतला छिलका और अंडाकार आकार: इस आम का छिलका पतला होता है और इसका आकार अंडाकार होता है, जिससे इसे छीलना आसान हो जाता है.
- पोषक तत्व: जर्दालु आम बायोएक्टिव कंपाउंड और फाइबर से भरपूर होता है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बनाता है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें शुगर का स्तर अन्य आमों की तुलना में कम होता है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है.
- पकने का समय: यह आम आमतौर पर जून से जुलाई के महीनों में पकता है.
- रंग: पकने के बाद इसका रंग हल्का पीला और नारंगी हो जाता है.
मगही पान
मगही पान बिहार के मगध क्षेत्र, विशेष रूप से औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा जिलों में उगाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का पान का पत्ता है. यह अपनी बेहतरीन गुणवत्ता, तीखेपन में कमी और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है.
मगही पान को 2018 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ है. यह टैग इसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और अद्वितीय गुणों को प्रमाणित करता है. GI टैग मगही पान की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करता है, अनधिकृत उपयोग को रोकता है और इसके उत्पादकों को वैश्विक बाजार में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है.
मगही पान की विशेषताएँ
मगही पान की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- कम तीखापन और मीठा स्वाद: अन्य पान की किस्मों की तुलना में, मगही पान में तीखापन (तेज़ स्वाद) कम होता है और इसमें हल्की मिठास होती है. यह इसे चबाने में अधिक सुखद बनाता है.
- कोमलता और बनावट: इसका पत्ता बहुत नरम और कोमल होता है, जो इसे आसानी से चबाने योग्य बनाता है. इसकी बनावट चिकनी होती है.
- अद्वितीय सुगंध: मगही पान में एक विशिष्ट और मनमोहक सुगंध होती है, जो इसे भारत में सबसे लोकप्रिय पान की किस्मों में से एक बनाती है.
- पोषक और औषधीय गुण: यह सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है. इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट और पाचन सहायक गुण होते हैं. इसे पारंपरिक रूप से कई आयुर्वेदिक उपचारों में इस्तेमाल किया जाता है.
- विशेष खेती: मगही पान की खेती विशेष विधियों से की जाती है, जिसे “बरेज” कहा जाता है. यह एक छायादार और नियंत्रित वातावरण होता है जो पान के पौधों के लिए आदर्श होता है.
कतरनी चावल, भागलपुर
भागलपुर का कतरनी चावल बिहार की एक खास पहचान है, जिसे उसकी अनूठी सुगंध, उत्कृष्ट स्वाद और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है. यह बिहार की सबसे प्रीमियम चावल किस्मों में से एक है. कतरनी चावल को 2018 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ है. यह टैग प्रमाणित करता है कि यह विशेष चावल की किस्म मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही अपनी विशिष्ट विशेषताओं के साथ उगाई जाती है.
नोट: कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य का उल्लेख करने से बचें, क्योंकि यह कतरनी चावल से संबंधित नहीं है और पाठक को भ्रमित कर सकता है. कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, जबकि कतरनी चावल बिहार के भागलपुर से संबंधित है.
कतरनी चावल की विशेषताएँ
कतरनी चावल की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- अद्वितीय सुगंध: इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी तीव्र और मनमोहक सुगंध है, जो इसे अन्य चावल की किस्मों से अलग करती है. जब यह पकता है तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है.
- बेहतर स्वाद: यह अपने स्वादिष्ट और मुलायम दानों के लिए प्रसिद्ध है, जो पकने के बाद भी अलग-अलग रहते हैं.
- छोटा और मध्यम दाना: कतरनी चावल के दाने छोटे से मध्यम आकार के होते हैं.
- पाचन में आसान: इसे पचाने में आसान माना जाता है और यह कई पारंपरिक भारतीय व्यंजनों, खासकर पुलाव और बिरयानी, के लिए आदर्श है.
- उच्च पोषक मूल्य: यह फाइबर और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो इसे स्वास्थ्यवर्धक विकल्प बनाता है.
मिथिला मखाना
मिथाला का मखाना (जिसे फॉक्स नट्स या कमल के बीज के रूप में भी जाना जाता है) बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पहचान और वहाँ की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है. यह अपने पोषण संबंधी गुणों, अनूठे स्वाद और औषधीय लाभों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है.
मिथिला मखाना की विशेषताएँ
मिथिला मखाना की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- विशिष्ट खेती और प्रसंस्करण: मिथिला मखाना की खेती तालाबों और जल निकायों में की जाती है. इसकी खेती और प्रसंस्करण एक श्रम-गहन प्रक्रिया है, जिसमें बीज को पानी से निकालना, सुखाना, भूनना और फिर उसके खोल को हटाना शामिल है. यह पारंपरिक विधि इसकी अनूठी गुणवत्ता में योगदान करती है.
- अद्वितीय पोषण मूल्य: यह प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह वसा में कम और ग्लूटेन-मुक्त होता है, जो इसे एक स्वस्थ नाश्ता विकल्प बनाता है.
- औषधीय गुण: आयुर्वेद में मखाने का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता है, जैसे कि पाचन में सुधार, रक्तचाप को नियंत्रित करना और हड्डियों को मजबूत बनाना. इसे आमतौर पर उपवास के दौरान भी खाया जाता है.
- बहुमुखी उपयोग: मखाने को सीधे नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है, या इसे करी, मिठाई (जैसे खीर), और अन्य नमकीन और मीठे व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है.
सिलाव का खाजा
सिलाव का खाजा बिहार की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है, जो अपनी परतदार बनावट और अनूठे स्वाद के लिए जानी जाती है. यह बिहार के नालंदा जिले के सिलाव शहर की एक विशिष्ट पहचान है. सिलाव के खाजा को 2018 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है.
सिलाव के खाजा की विशेषताएँ
सिलाव के खाजा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- अद्वितीय परतदार बनावट: इसकी सबसे खास पहचान इसकी 52 परतें (परत-दर-परत) हैं, जो इसे बेहद कुरकुरा और खस्ता बनाती हैं. यह बनावट इसे अन्य मिठाइयों से अलग करती है.
- सामग्री और निर्माण: इसे मुख्य रूप से मैदा, चीनी और घी से बनाया जाता है. इसे बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल और श्रम-गहन होती है, जिसमें आटे को पतला बेलना, परतों में मोड़ना, तलना और फिर चाशनी में डुबोना शामिल है. यह पारंपरिक तरीका ही इसे विशिष्ट स्वाद और बनावट देता है.
- मीठा और स्वादिष्ट: यह अपनी संतुलित मिठास और घी की खुशबू के लिए पसंद किया जाता है.
- लंबी शैल्फ-लाइफ: इसकी बनावट और सूखेपन के कारण इसे कुछ दिनों तक आसानी से संग्रहीत किया जा सकता है.
भागलपुरी सिल्क
भागलपुरी सिल्क, जिसे अक्सर “तसर सिल्क” के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के भागलपुर शहर की एक ऐतिहासिक और विश्व-प्रसिद्ध पहचान है. भागलपुर को “सिल्क सिटी” (रेशम शहर) के नाम से भी जाना जाता है, और इसका रेशम उद्योग सदियों पुराना है. भागलपुरी सिल्क को वित्त वर्ष 2012-13 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ था.
भागलपुरी सिल्क की विशेषताएँ
भागलपुरी सिल्क की कुछ खास विशेषताएँ इसे अन्य रेशमों से अलग बनाती हैं:
- तसर रेशम: भागलपुरी सिल्क मुख्य रूप से एंथेरिया पफिया नामक रेशमकीट के कोकून से प्राप्त तसर रेशम से बनता है. यह रेशम वन्य होता है, जिससे इसे “अहिंसक रेशम” भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर कोकून से कीट के निकलने के बाद रेशम निकाला जाता है.
- प्राकृतिक चमक और खुरदुरी बनावट: तसर रेशम में एक प्राकृतिक भूरी-सुनहरी चमक होती है और इसकी बनावट थोड़ी खुरदुरी और रेशेदार होती है, जो इसे एक अनूठा, प्राकृतिक रूप देती है.
- हल्का वजन और आरामदायक: भागलपुरी सिल्क के कपड़े हल्के होते हैं और सभी मौसमों में पहनने में आरामदायक होते हैं.
- स्थायित्व: यह काफी टिकाऊ होता है और समय के साथ अपनी चमक बनाए रखता है.
- बहुमुखी उपयोग: भागलपुरी सिल्क का उपयोग साड़ियों (विशेष रूप से भागलपुरी साड़ी), दुपट्टे, शॉल, कुर्ते और अन्य परिधान बनाने में किया जाता है.
- “वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट” में शामिल: केंद्र सरकार की “वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट” (ODOP) योजना के तहत भागलपुरी सिल्क को भागलपुर के प्रमुख उत्पाद के रूप में चुना गया है, जिससे इसके विपणन और ब्रांडिंग को और बढ़ावा मिल रहा है.
सिक्की घास कला
सिक्की घास से बने सामान बिहार, खासकर मिथिलांचल क्षेत्र की एक विशिष्ट हस्तकला है, जिसे सिक्की कला के नाम से जाना जाता है. सिक्की कला, एक प्रकार की “गोल्डन ग्रास क्राफ्ट” है, जिसमें सिक्की नामक एक विशेष प्रकार की सुनहरी घास का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की कलात्मक और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं. यह कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी महिलाओं द्वारा सीखी और सिखाई जाती है. सिक्की घास कला को 24 अगस्त, 2021 को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ है.
सिक्की घास से बने सामान
सिक्की घास के ऊपरी फूलों वाले हिस्से को हटा दिया जाता है, और फिर डंठल को सुखाकर महीन पट्टियों में काटा जाता है. इन पट्टियों का उपयोग करके प्राचीन कॉइलिंग विधि (घुमावदार विधि) से विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं.
सिक्की घास से कई तरह के सामान बनाए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- पारंपरिक वस्तुएं:
- डलिया/टोकरियाँ: विभिन्न आकार और डिज़ाइन की टोकरियाँ, जिनका उपयोग अनाज रखने, उपहार देने (जैसे विवाह में दहेज के रूप में, जिसे पौती कहा जाता है, जिसमें सिंदूर, आभूषण आदि रखे जाते हैं), या पूजा सामग्री ले जाने के लिए किया जाता है.
- मौनी/दालिया: दैनिक घरेलू उपयोग की बड़ी और छोटी टोकरियाँ.
- चटाई: बैठने या सजावट के लिए.
- खिलौने और गुड़िया: बच्चों के लिए रंग-बिरंगे खिलौने, जैसे हाथी, घोड़े, मोर, पक्षी और मानव आकृतियाँ.
- सजावटी और आधुनिक वस्तुएं:
- डिब्बे और बक्से: सूखे मेवे, मसाले, या आभूषण रखने के लिए.
- फूलदान और पेन स्टैंड: घर और दफ्तर की सजावट के लिए.
- पेपरवेट, मोबाइल केस, और कुशन.
- दीवार पर टांगने वाले पैनल और मूर्तियाँ: देवी-देवताओं (जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, गणेश, दुर्गा) और जानवरों की आकृतियाँ.
- ज्वैलरी: जैसे अंगूठियां और कान की बालियाँ.
- अन्य सजावटी वस्तुएं: जो घर और कार्यालय को पारंपरिक कलात्मकता से सजाती हैं.
विशेषताएँ
- प्राकृतिक और टिकाऊ: ये उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक सिक्की घास से बनते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ होते हैं.
- हस्तनिर्मित और अद्वितीय: प्रत्येक उत्पाद कारीगर के हाथों से बनाया जाता है, जिससे हर एक टुकड़ा अद्वितीय और कलात्मक होता है.
- प्राकृतिक और रंगीन: सिक्की घास का अपना सुनहरा रंग बहुत आकर्षक होता है, लेकिन इसे लाल, काले, नीले और हरे जैसे प्राकृतिक रंगों में भी रंगा जाता है ताकि उत्पादों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके.
- कोई खाली जगह नहीं: मधुबनी पेंटिंग की तरह, सिक्की कला में भी अक्सर कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जाती, पूरे स्थान को पैटर्न और डिज़ाइनों से भरा जाता है.
- सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: यह कला बिहार की प्राचीन पारंपरिक शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखती है.
- पर्यावरण-अनुकूल विकल्प: यह प्लास्टिक जैसे हानिकारक सामग्रियों का एक स्थायी और बायोडिग्रेडेबल विकल्प प्रदान करती है.
खटवा एप्लीक (Khatwa Applique)
खटवा एप्लीक बिहार की एक पारंपरिक और विशिष्ट कपड़ा कला है, जिसे अक्सर पैचवर्क के रूप में भी जाना जाता है. यह मिथिलांचल क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण हस्तकला है. खटवा एप्लीक को 26 अगस्त, 2021 को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है.
खटवा एप्लीक क्या है?
खटवा एप्लीक कला में, कपड़ों के छोटे-छोटे रंगीन टुकड़ों को काटकर एक बड़े कपड़े पर सिलाई करके जटिल और आकर्षक डिज़ाइन बनाए जाते हैं. “एप्लिक” शब्द का अर्थ ही होता है “लगाना” या “चिपकाना”, और इस कला में कपड़े के टुकड़ों को आधार कपड़े पर कलात्मक रूप से लगाया जाता है.
यह कला अपनी सटीकता, रंगीनता और रचनात्मकता के लिए प्रसिद्ध है. कारीगर, विशेषकर महिलाएँ, विभिन्न आकारों में कपड़े के टुकड़ों को काटती हैं और फिर उन्हें आधार कपड़े पर टांकती हैं, जिससे एक नया और सुंदर पैटर्न बनता है.
खटवा एप्लीक की विशेषताएँ
खटवा एप्लीक की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- पुनर्चक्रण और रचनात्मकता: इस कला में अक्सर पुराने या बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कला बन जाती है.
- विविध डिज़ाइन: खटवा एप्लीक में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जिनमें ज्यामितीय पैटर्न, फूल, पत्तियां, पशु-पक्षी और यहाँ तक कि पौराणिक आकृतियाँ भी शामिल हैं.
- रंगों का अनूठा प्रयोग: कारीगर रंगों के सामंजस्य और विरोधाभास का उपयोग करके जीवंत और आकर्षक पैटर्न बनाते हैं.
- हाथ से किया गया काम: यह एक श्रम-गहन हस्तकला है जिसमें प्रत्येक टुकड़ा हाथों से सावधानीपूर्वक सिला जाता है, जो इसे विशिष्ट और मूल्यवान बनाता है.
- उपयोग: पारंपरिक रूप से, खटवा एप्लीक का उपयोग डिजाइनर टेंट, शामियाना, और चंदोवा (कैनोपी) बनाने में किया जाता था. आजकल, इसे साड़ी, दुपट्टे, कुशन कवर, वॉल हैंगिंग, बेडस्प्रेड और अन्य घरेलू सजावट की वस्तुओं पर भी देखा जा सकता है.
सुजनी कला
सुजनी कला बिहार की एक अद्वितीय कढ़ाई कला है, जिसमें कपड़ों पर धागों की पतली सिलाई का उपयोग करके विभिन्न कहानियों, दृश्यों और प्रतीकों को उकेरा जाता है. यह एक प्रकार की रजाई सिलाई (quilt stitching) से विकसित हुई है, जहाँ पुराने कपड़ों को एक साथ सिलकर रजाई बनाई जाती थी और उस पर लोक कथाओं, सामाजिक मुद्दों या दैनिक जीवन के दृश्यों को कढ़ाई के माध्यम से जीवंत किया जाता था. यह कला मुख्य रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर, मधुबनी और पूर्णिया जिलों में प्रचलित है. सुजनी कला को 11 दिसंबर, 2006 को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है.
सुजनी कला की विशेषताएँ
सुजनी कला की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- पुनर्चक्रण और सादगी: परंपरागत रूप से, सुजनी में पुराने कपड़ों, जैसे धोती या साड़ियों को परतों में रखकर इस्तेमाल किया जाता था, और फिर उन पर विभिन्न आकृतियाँ और कहानियाँ काढ़ी जाती थीं. यह कला कम से कम संसाधनों में भी सुंदरता रचने की एक मिसाल है.
- विषय-वस्तु: सुजनी कला की कहानियाँ अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर केंद्रित होती हैं. इसमें जन्म, विवाह, फसल चक्र, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, लोककथाएँ, दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, और प्रकृति (जैसे सूरज, चाँद, पेड़, पशु-पक्षी) के दृश्य दर्शाए जाते हैं. यह गरीबी, बाल विवाह, लिंगभेद जैसे सामाजिक मुद्दों को भी उजागर करती है.
- कढ़ाई शैली: इसमें मुख्य रूप से रनिंग स्टिच (सादी सिलाई) का उपयोग किया जाता है, जिससे बारीक रेखाएँ और आकृतियाँ बनाई जाती हैं. रंगों का चुनाव अक्सर प्रतीकात्मक होता है.
- नारी-केंद्रित कला: यह कला पारंपरिक रूप से बिहार की ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनी भावनाओं, अनुभवों और समाज के प्रति अपनी टिप्पणियों को व्यक्त करने का एक माध्यम रही है.
- उपयोग: पहले इसका उपयोग मुख्य रूप से बच्चों के लिए रजाई (सुजनी) और बिस्तर की चादरें बनाने के लिए किया जाता था. अब इसका उपयोग साड़ी, दुपट्टे, कुशन कवर, वॉल हैंगिंग, बैग और अन्य घरेलू सजावट की वस्तुओं में भी किया जाता है, जिससे यह समकालीन बाजार के लिए भी प्रासंगिक बनी हुई है.
मर्चा चावल
मर्चा चावल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की एक अनूठी और सुगंधित चावल की किस्म है, जिसे अपनी खास खुशबू, स्वाद और काली मिर्च जैसे आकार के लिए जाना जाता है. मर्चा चावल (जिसे स्थानीय रूप से ‘मिर्चा‘ या ‘मर्चैया‘ भी कहा जाता है) को 4 अप्रैल, 2023 को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है.
मर्चा चावल की विशेषताएँ
मर्चा चावल की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इसे अन्य चावलों से अलग बनाती हैं:
- अद्वितीय सुगंध: इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी तीव्र और मनमोहक सुगंध है, जो इसे अन्य चावल की किस्मों से अलग करती है. पकने पर इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है.
- काली मिर्च जैसा आकार: इस चावल का दाना छोटा, मोटा और अंडाकार होता है, जो दिखने में काली मिर्च जैसा लगता है, इसी वजह से इसे ‘मर्चा’ (मिर्च का बिगड़ा हुआ रूप) नाम मिला है.
- स्वाद और बनावट: यह एक गैर-बासमती, छोटा दाना और सुगंधित चावल की किस्म है. यह स्वाद में मुलायम, हल्की मिठास लिए हुए और पचने में आसान होता है.
- उत्कृष्ट चूड़ा: मर्चा चावल से बनने वाला चूड़ा (पोहा) अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और सुगंध के लिए देश भर में प्रसिद्ध है.
- विशेष भौगोलिक स्थितियाँ: पश्चिमी चंपारण की विशिष्ट जलवायु और मिट्टी (खासकर बूढ़ी-गंडक/सिकरहना नदी के किनारे वाले ब्लॉक) इस चावल में अनोखी सुगंध और स्वाद पैदा करने में सहायक होती हैं. अक्टूबर-नवंबर में कम तापमान वाला सूक्ष्म वातावरण भी इसकी सुगंध को निखारता है.
- उत्पादन क्षेत्र: यह मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांड़, गौनाहा, नरकटियागंज, रामनगर और चनपटिया जैसे प्रखंडों में उगाया जाता है.
मंजूषा कला, भागलपुर
मंजूषा कला बिहार के भागलपुर क्षेत्र की एक प्राचीन और विशिष्ट लोक कला है, जिसे “अंग कला” या “सर्प चित्रकला” के नाम से भी जाना जाता है. यह कला मुख्य रूप से बिहुला-विषहरी की लोकगाथा पर आधारित है.
मंजूषा कला एक पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली है जो बिहार के अंग प्रदेश (वर्तमान भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र) में पनपी और विकसित हुई. यह कला 7वीं शताब्दी जितनी पुरानी मानी जाती है और इसे बिहार की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक माना जाता है. मंजूषा कला को सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है.
मंजूषा कला की विशेषताएँ
मंजूषा कला की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इसे अन्य चित्रकला शैलियों से अलग बनाती हैं:
- बिहुला-विषहरी की लोकगाथा पर आधारित: यह कला मुख्य रूप से बिहुला-विषहरी की पौराणिक कहानी को चित्रित करती है, जिसमें बिहुला अपने पति बाला लखंदर को सर्पदंश से बचाने के लिए संघर्ष करती है. यह कहानी नारी शक्ति और समर्पण का प्रतीक है.
- रंगों का सीमित प्रयोग: मंजूषा कला में पारंपरिक रूप से केवल तीन मुख्य रंगों का प्रयोग होता है:
- गुलाबी/लाल: उत्सव और खुशी का प्रतीक.
- पीला: विवाह और शुभता का प्रतीक.
- हरा: विषदंश और प्रकृति का प्रतीक.
रंगों का महत्व
इन रंगों का प्रतीकात्मक महत्व होता है और ये कहानी के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं.
- रेखा प्रधान चित्रकला: यह एक रेखा प्रधान कला शैली है, जिसमें मोटी और गतिशील रेखाओं का प्रयोग किया जाता है. आकृतियों का रेखांकन आमतौर पर हरे रंग से किया जाता है.
- मानवाकृतियाँ: मंजूषा कला में मानवाकृतियाँ अक्सर अंग्रेजी के ‘X’ आकार की होती हैं, जिसमें दायाँ पैर तथा बायाँ हाथ और बायाँ पैर तथा दायाँ हाथ अलग-अलग दिशाओं में दिखाए जाते हैं.
- सर्प रूपांकन: चूंकि यह बिहुला-विषहरी की कहानी पर आधारित है, जिसमें सर्पों का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इस कला में सर्प रूपांकन (snake motifs) प्रमुखता से पाए जाते हैं.
- श्रृंखलाबद्ध चित्रकला: मंजूषा कला एक श्रृंखलाबद्ध चित्रकला पद्धति है, जिसमें कहानी को क्रमवार चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से दर्शाया जाता है.
- मंजूषा का शाब्दिक अर्थ: संस्कृत में “मंजूषा” शब्द का अर्थ “बक्सा” होता है. पारंपरिक रूप से, ये बांस, जूट और कागज़ से बने मंदिर के आकार के बक्से होते थे, जिन पर विभिन्न देवताओं और पौराणिक दृश्यों के चित्र बने होते थे.