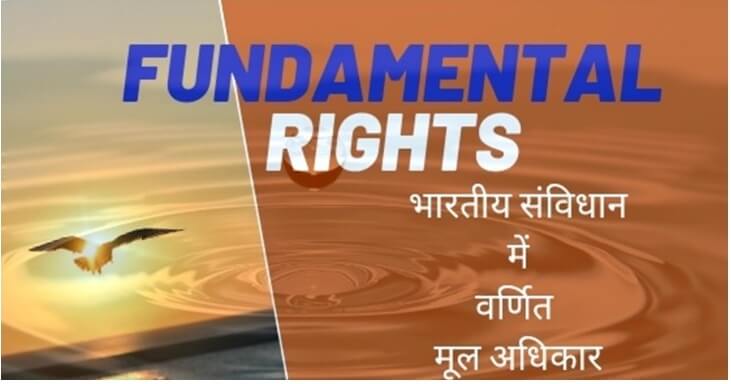भारत के पास अद्वितीय जैव विविधता और विशाल प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है. यह पर्यावरण और वन संरक्षण को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता मानता है. देश की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना एक जटिल चुनौती है. इस दायित्व को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ कानूनी ढाँचे की आवश्यकता है. इस दिशा में, भारत ने विभिन्न अधिनियमों, नियमों और न्यायिक निकायों के माध्यम से एक बहुस्तरीय कानूनी प्रणाली विकसित की है. भारत में इनका नियमन मुख्यतः केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत सम्पन्न होती है.
उपरोक्त कथन के अनुसार, इस लेख में भारत में पर्यावरण और वन सुरक्षा से संबंधित प्रमुख अधिनियमों का का वर्णन किया गया है. साथ ही इनके प्रावधानों, प्रवर्तन तंत्रों और महत्वपूर्ण संशोधनों पर प्रकाश डाला गया है. इसे लेख को पढ़कर आप वन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए क़ानूनी उपायों को समझ सकेंगे.
भारत में पर्यावरण व वन संरक्षण (Laws for Environment and Forest Conservation in India in Hindi)
भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर दो अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं—भाग IV का अनुच्छेद 48A और भाग IVA का अनुच्छेद 51A. अनुच्छेद 48A राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि वे पर्यावरण की रक्षा और उसके सुधार हेतु प्रयास करें तथा देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा सुनिश्चित करें. वहीं, अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य बनाता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण—जैसे वनों, नदियों, झीलों और वन्य जीवों—की सुरक्षा और उन्नयन में योगदान दें और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें.
हालाँकि, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कानून स्वतंत्रता से पूर्व भी अस्तित्व में थे, लेकिन इस दिशा में एक व्यापक और सशक्त कानूनी ढांचे की आवश्यकता 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद गंभीरता से महसूस की गई. इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने भारत सरकार को पर्यावरणीय मुद्दों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया. इसके परिणामस्वरूप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण नीति एवं योजना परिषद की स्थापना की गई. यह संस्था आगे चलकर पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) के रूप में विकसित हुई, जिसे 1985 में एक स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा मिला.
इस मंत्रालय के अधीन देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीतियाँ और नियम बनाए जाते हैं. इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की भी अहम भूमिका होती है. इन संस्थाओं का समन्वय पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
समय के साथ बढ़ते औद्योगीकरण, तीव्र शहरीकरण और लगातार बढ़ती जनसंख्या ने पर्यावरण की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. इन चुनौतियों से निपटने और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार ने समय-समय पर कई नए कानून और नियम लागू किए हैं, जो आज देश की पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं.
भारत में पर्यावरण और वन संरक्षण के कानून
हमारे देश में पर्यावरण और वन संरक्षण के दृष्टि से निम्नलिखित कानून बनाए गए है:
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012
- भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017
- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010
इसके अलावा भारत में कुछ अन्य कानून भी लागु है, जो प्रदुषण नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है. ये इस प्रकार है:
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002
- भारतीय वन अधिनियम, 1927
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम, 1974
- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
- खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और प्रबंधन अधिनियम, 1989, आदि
उपरोक्त में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, कानून और प्राधिकरण का वर्णन आगे किया गया है. अन्यों का वर्णन संबंधित लेख के पाठ में अगले कुछ दिनों में किया जाएगा.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
भारत में वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, एक महत्वपूर्ण और बहुधा चर्चित कानून है. इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य देश के वन्यजीवों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके अवैध शिकार, तस्करी और अंगों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना है. इसमें संकटग्रस्त जानवरों, पक्षियों और पौधों को सूचीबद्ध करके उनके संरक्षण का प्रयास किया गया है.
इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं. इसमें वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान है. इस अधिनियम के तहत ही 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया गया. यह भारत में चिड़ियाघरों की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है. इस प्रकार यह अधिनियम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
छह अनुसूचियाँ
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, वन्यजीवों को उनकी भेद्यता और संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर छह अनुसूचियों में वर्गीकृत करता है. यह वर्गीकरण कानूनी जटिलता और पारिस्थितिक वास्तविकता के बीच संतुलन साधने का प्रयास है. इसका एक उद्देश्य संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देना और संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करना भी है.
- अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2 (भाग-II): इन अनुसूचियों में शामिल वन्यजीवों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है. इन प्रजातियों के शिकार या उन्हें नुकसान पहुँचाने पर उच्चतम दंड निर्धारित है. उदाहरण के लिए, यदि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाए या इतना अशक्त या रोगी हो कि ठीक न हो सके, तो ही मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा लिखित आदेश के माध्यम से उसके आखेट की अनुमति दी जा सकती है.
- अनुसूची-3 और अनुसूची-4: ये अनुसूचियाँ भी वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करती हैं, लेकिन इनके अंतर्गत दंड का प्रावधान अनुसूची 1 और 2 की तुलना में कम कठोर होता है.
- अनुसूची-5: इस अनुसूची में वे जानवर शामिल हैं जिन्हें ‘वर्मिन’ घोषित किया जा सकता है. अर्थात् वे जानवर जिनका शिकार कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकता है.
- अनुसूची-6: यह अनुसूची विशेष रूप से पौधों की प्रजातियों से संबंधित है. इसमें शामिल पौधों की खेती और रोपण पर सख्त रोक है, ताकि उनकी दुर्लभता और पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए उन्हें संरक्षित किया जा सके.
यह वर्गीकरण वन्यजीवों को एक समान इकाई के रूप में नहीं देखता, बल्कि उनकी पारिस्थितिक भेद्यता और संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपनाता है. यह संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने और संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने में मदद करता है.
अपराध से जुड़े प्रावधान और दंड
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधानों को निर्धारित करता है. अधिनियम की धारा 16C के तहत, जंगली पक्षियों या सरीसृपों, उनके अंडों या उनके घोसलों को नुकसान पहुँचाना एक गंभीर अपराध माना जाता है. दोषी पाए जाने पर 3 से 7 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है.
अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास और/या जुर्माने का दंड दिया जाता है. अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 से संबंधित अपराधों, या अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान में शिकार से संबंधित अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान है. जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके तहत अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को अधिक कठोर बना दिया गया है.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूचियाँ (संरक्षण स्तर और दंड)
| अनुसूची संख्या | शामिल प्रजातियों का प्रकार | संरक्षण स्तर | संबंधित अपराधों के लिए दंड का सामान्य प्रावधान |
| अनुसूची-1 | संकटग्रस्त प्रजातियाँ (पशु) | पूर्ण सुरक्षा | उच्चतम दंड (कारावास और/या जुर्माना) |
| अनुसूची-2 (भाग-II) | उच्च संरक्षण प्राप्त प्रजातियाँ | पूर्ण सुरक्षा | उच्चतम दंड (कारावास और/या जुर्माना) |
| अनुसूची-3 | संरक्षित प्रजातियाँ (पशु) | मध्यम सुरक्षा | कम दंड (कारावास और/या जुर्माना) |
| अनुसूची-4 | संरक्षित प्रजातियाँ (पशु) | मध्यम सुरक्षा | कम दंड (कारावास और/या जुर्माना) |
| अनुसूची-5 | वर्मिन (शिकार योग्य जानवर) | कोई सुरक्षा नहीं | शिकार की अनुमति (कुछ शर्तों के अधीन) |
| अनुसूची-6 | विशिष्ट पौधे | पूर्ण सुरक्षा | खेती और रोपण पर रोक, उल्लंघन पर दंड |
अधिकारियों और बोर्डों की भूमिका
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और बोर्डों की नियुक्ति का प्रावधान है. केंद्रीय सरकार एक वन्यजीव संरक्षण निदेशक की नियुक्ति करती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का समन्वय करता है. इसी तरह, राज्य सरकारें राज्य स्तर पर एक मुख्य वन्यजीव संरक्षक और अन्य आवश्यक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं.
अधिनियम में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (धारा 5क) के गठन का भी प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. इस बोर्ड का कर्तव्य वन्यजीव और वनों के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देना, नीतियां बनाना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना और प्रबंधन पर सिफारिशें करना, तथा वन्यजीव या उनके आवासों से संबंधित परियोजनाओं का प्रभाव निर्धारण करना है.
उपरोक्त के समानांतर, राज्य सरकारें राज्य वन्यजीव बोर्ड (धारा 6) का गठन करती हैं, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं. इस बोर्ड का कर्तव्य राज्य सरकार को संरक्षित क्षेत्रों के चयन और प्रबंधन, वन्यजीव और निर्दिष्ट पौधों के संरक्षण के लिए नीति निर्धारण, तथा जनजातियों और अन्य वनवासियों की आवश्यकताओं और वन्यजीव संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उपायों पर सलाह देना है.
संरक्षित क्षेत्र
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान करता है. राज्य सरकारें किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का आशय व्यक्त कर सकती हैं यदि वह वन्यजीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के लिए पारिस्थितिक महत्व का हो. इसी प्रकार, राष्ट्रीय उपवन (राष्ट्रीय उद्यान) भी घोषित किए जा सकते हैं. इन क्षेत्रों में वन्य जीवन को नष्ट करना, उसका विदोहन करना, आग लगाना या हानिकारक पदार्थों का उपयोग करना सख्त वर्जित है.
अधिनियम में संरक्षण आरक्षिति और सामुदायिक आरक्षिति की अवधारणा भी शामिल की गई है. यह प्रावधान स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देती है. वन्यजीव की परिभाषा में जलीय या भूवनस्पतिक प्राणी शामिल हैं. अनुसूची 6 में पौधों के भी संरक्षण का प्रावधान है. इसमें पौधों के प्राकृतिक आवासों को भी शामिल किया गया है. इस प्रकार यह संरक्षण एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षा का दृष्टिकोण दर्शाता है. यह कानून की दूरदर्शिता को है जो केवल ‘आकर्षक’ प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यापक जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देता है.
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (Forest Conservation Act, 1980)
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 वनों की रक्षा के लिए एक सशक्त कानूनी ढाँचा है. यह सुनिश्चित करता है कि विकास कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा भी समान रूप से की जाए. इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों के क्षेत्रफल में कमी को रोकना, वनों की कटाई और गैर-वानिकी कार्यों के लिए भूमि उपयोग को नियंत्रित करना, और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है. इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार है:
- केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक: राज्य सरकारें या कोई अन्य प्राधिकरण किसी भी वनीय भूमि को गैर-वानिकी उपयोग में तभी ला सकते हैं जब उन्हें केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त हो.
- वन क्षेत्रांतरण पर रोक: किसी वन भूमि को किसी निजी संस्था, व्यक्ति या औद्योगिक परियोजना को देने से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है.
- वन कटाई पर नियंत्रण: पेड़ों की कटाई, वनों को साफ़ करने या वन भूमि को खेती, आवास या अन्य कार्यों के लिए परिवर्तित करने पर प्रतिबंध है जब तक कि इसकी अनुमति केंद्र से न ली जाए.
- संशोधन (1988): 1988 में अधिनियम में संशोधन किया गया जिसमें इसे और अधिक कठोर बनाया गया ताकि वनों की अवैध कटाई को रोका जा सके और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो सके.
महत्त्व:
- यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
- यह वनों की अवैध कटाई, वनों के क्षरण और पर्यावरणीय असंतुलन को रोकने में सहायक है.
- यह अधिनियम टिकाऊ विकास और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है.
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए एक व्यापक कानून है. यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) और अनुच्छेद 51A(g) (मूल कर्तव्य) पर आधारित है. अतः यह पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य और नागरिक दोनों को जिम्मेदार बनाता है. यह अधिनियम विशिष्ट प्रदूषण स्रोतों के बजाय ‘पर्यावरण’ को एक समग्र इकाई के रूप में संबोधित करने वाला पहला व्यापक कानून है. इसकी “अम्ब्रेला” प्रकृति यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण संरक्षण के किसी भी पहलू को कानूनी रूप से संबोधित किया जा सके. अतः यह पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए एक लचीला ढाँचा तैयार करता है.
प्रमुख प्रावधान और परिभाषाएँ
अधिनियम में कई महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और प्रावधान शामिल हैं जो इसके दायरे को स्पष्ट करते हैं:
- “पर्यावरण”: इस अधिनियम के तहत, “पर्यावरण” को जल, वायु और भूमि के साथ-साथ इन तीनों तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीवों और संपत्ति के बीच विद्यमान अंतर-संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है.
- “पर्यावरण प्रदूषक”: यह ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है.
- “पर्यावरण प्रदूषण”: इसका अर्थ है पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना.
- “परिसंकटमय पदार्थ”: यह ऐसा पदार्थ या उत्पाद है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या बाह्य हस्तक्षेप के कारण के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण को हानि कर सकती है.
- “हथालना (Handling)”: इसमें किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन (implementation), पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन (Conversion), विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया शामिल है.
केंद्र सरकार की शक्तियाँ और कार्य
यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण के संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है. इन शक्तियों में शामिल हैं:
- राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों की कार्रवाइयों का समन्वय करना.
- पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादित करना.
- पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक बनाना और विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के मानक बनाना.
- उन क्षेत्रों का निषिद्ध (Restriction) करना जहाँ कोई उद्योग, संक्रियाएँ या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन चलाए जाएंगे.
- पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना या उन्हें मान्यता देना और नमूनों के विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त करना.
- पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विषयों की जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना.
- किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बंद करने, उसका प्रतिषेध (Restriction) या विनियमन करने का निदेश देने की शक्ति.
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
अधिनियम प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित करता है. इसमें कम प्रदूषक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना और उद्योगों से उत्सर्जन को कम करने के लिए उपयोग किए गए ईंधन के प्रकार के आधार पर नई सीमाएं निर्धारित करना शामिल है. यह आपदाजनक और नशीले रसायनों के भंडारण और आयात को भी विनियमित करता है.
अपराध और सजाएँ
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है. इसका पालन न करने या उलंघन करने पर पांच वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है. इसके अपराधी पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान किया गया है. यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम दोषसिद्धि के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए ₹5000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि उल्लंघन दोषसिद्धि से एक वर्ष की अवधि से भी अधिक जारी रही तो अपराधी को सात वर्ष कारावास से दंडित किया जा सकता है.
किसी कंपनी के पर्यावरण अपराध करने पर इसके जिम्मेदारी से जुड़े सभी व्यक्ति दोषी माने जाते है. यह तबतक जारी रहता है जबतक वे साबित न कर दे कि इसमें उनकी त्रुटि नहीं है और उन्होंने अपराध रोकने का पूरा प्रयास किया था. इसी तरह, सरकारी विभाग द्वारा नियम भंग होने पर विभाग के मुखिया को दोषी माना जाता है, जब तक वह खुद को निर्दोष साबित न कर दे.
इस तरह के मामलों में न्यायालय तभी सुनवाई कर सकता है जब केंद्र सरकार या उसके अधिकृत व्यक्ति ने शिकायत की हो. हालांकि, आम नागरिकों को भी शिकायत का अधिकार है. लेकिन उसे इसकी लिखित सूचना 60 दिन पहले सरकार को देनी होगी.
संरक्षण के प्रावधान में खामियां
स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण जीने के अधिकार का हिस्सा है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है. इसलिए, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा यह कानून जीवन के अधिकार की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है.
लेकिन इस कानून में कुछ कमियाँ भी हैं. सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है. इसमें राज्य सरकारों की कोई खास भूमिका नहीं है. इससे सत्ता का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण हो जाता है. यह मनमाने और दुरुपयोग की आशंका बढ़ाता है. पर्यावरणीय नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए मजबूत केंद्रीकरण जरूरी है. लेकिन दूसरी तरफ इससे स्थानीय जरूरतें, क्षेत्रीय विविधताएं और जनता की भागीदारी नजरअंदाज हो सकती हैं. एक अच्छे शासन में ऊपर से नियंत्रण और जमीनी स्तर की समझ के बीच संतुलन बनाना जरूरी है.
इसके अलावा, कानून में आम लोगों की भागीदारी के लिए जरूरी प्रावधानों की कमी है. साथ ही, इस कानून में शोर प्रदूषण, अधिक ट्रैफिक और रेडिएशन जैसी आधुनिक पर्यावरणीय समस्याओं को भी ठीक से सम्बोधित नहीं किया गया है.
वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 [Wildlife (Protection) Amendment Act, 2002]

यह भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1972 के मूल अधिनियम में किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन है.
इसका उद्देश्य है –
- वन्य जीवों की अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार पर नियंत्रण को और सख्त बनाना,
- संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करना, और
- दंड और सजा को अधिक कठोर बनाकर रोकथाम सुनिश्चित करना.
इस संसोधन के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है:
- अपराधों के लिए कठोर दंड: अवैध शिकार, तस्करी या वन्य जीवों की हत्या जैसे अपराधों के लिए जुर्माना और सजा को काफी बढ़ाया गया. कुछ अपराधों को गंभीर और गैर-जमानती घोषित किया गया.
- राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) का प्रस्ताव: संगठित अपराधों की रोकथाम और वन्यजीव तस्करी से मुकाबले के लिए विशेष एजेंसी के गठन का आधार तैयार किया गया. इस संशोधन के आधार पर 2007 में WCCB की स्थापना की गई. WCCB को CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) के अंतर्गत नामित नोडल एजेंसी का दर्जा प्राप्त है. यह ब्यूरो वन्यजीव संरक्षण और तस्करी विरोधी अभियान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेता है. साथ ही यह इंटरपोल और अन्य वैश्विक संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम करता है.
- संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा: राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में गतिविधियों को और अधिक नियंत्रित किया गया. इन क्षेत्रों में कोई भी गैर-स्वीकृत कार्य करना अब कानूनन अपराध माना गया.
- वन्यजीव अपराधों की निगरानी: वन अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जाँच कर सकें और त्वरित कार्रवाई कर सकें.
- पुनर्वास और संरक्षण को बढ़ावा: वन्य जीवों और उनके निवास स्थलों के संरक्षण के लिए जागरूकता और संरक्षण योजनाओं को बल मिला.
इस प्रकार, यह संशोधन भारत के वन्य जीवों के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करता है. यह वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण की भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. संगठित वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह अधिनियम एक मजबूत आधार बनाता है.
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम (FRA), 2006 भारत में वन शासन में एक मील का पत्थर है. यह अधिनियम वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए बनाया गया है. ये लोग पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों को विधिवत अभिलिखित नहीं किया जा सका है. इसका एक उद्देश्य औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक वन प्रबंधन प्रथाओं के कारण इनके साथ हुए गंभीर ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना भी है.
FRA वन संरक्षण को स्थानीय समुदायों के अधिकारों और आजीविका के साथ जोड़कर एक अधिक न्यायसंगत और सहभागी मॉडल बनता है. यह आदिवासी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए अभिन्न अंग हैं- को मान्यता देता है. इसका उद्देश्य इन समुदायों को वन-भूमि तक स्थायी पहुँच, वन उपज व संसाधन के उपयोग का अधिकार देना, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना, तथा उन्हें अवैध बेदखली और विस्थापन से बचाना है.
प्रमुख प्रावधान
इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के वन अधिकारों को मान्यता दिया गया है. इसे व्यक्तिगत (स्वामित्व) और सामुदायिक अधिकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- स्वामित्व अधिकार (Individual Forest Rights – IFR): यह अधिनियम जनजाति या अन्य परंपरागत आदिवासियों द्वारा खेती की जा रही वन भूमि पर उनके स्वामित्व को मान्यता देता है. भूमि की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर तक सीमित है. इसमें वन भूमि पर निवास करने और खेती करने का अधिकार भी शामिल है.
- सामुदायिक अधिकार (Community Forest Rights – CFR): ये अधिकार वन पर निर्भर समुदायों की सामूहिक आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं. इनमें शामिल हैं:
- लघु वन उपज (Minor Forest Produce – MFP) पर स्वामित्व: बाँस, झाड़-झंखाड़, स्टंप और बेंत सहित सभी गैर-काष्ठ वन उत्पादों के संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार.
- पारंपरिक उपयोग अधिकार: निस्तार (सामुदायिक वन संसाधन का एक प्रकार) जैसे पारंपरिक उपयोग अधिकार, साथ ही यायावरी या चरागाही समुदायों के लिए मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाहों का उपयोग, और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अधिकार.
- आवास अधिकार: आदिम जनजातीय समूहों (PGTs) और पूर्व-कृषि समुदायों के उनके पारंपरिक आवासों पर अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें घरों और आवासों के लिए सामुदायिक भूमि का स्वामित्व भी शामिल है.
- सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन: यह प्रावधान वन समुदायों को परंपरागत रूप से संरक्षित वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन और स्थायी प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है.
- जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान: जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार.
- अन्य पारंपरिक अधिकार: कोई भी अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है. लेकिन इसमें वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने पर प्रतिबन्ध है.
- राहत और विकास संबंधी अधिकार: अधिनियम अवैध या बलपूर्वक विस्थापित करने के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार प्रदान करता है. इसमें वैकल्पिक भूमि भी शामिल है यदि उन्हें दिसंबर 2005 से पहले अवैध रूप से बेदखल किया गया हो. यह कुछ आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं, जैसे विद्यालय, औषधालय, आंगनवाड़ी, उचित कीमत की दुकानें, विद्युत और दूरसंचार लाइनें, जल आपूर्ति, लघु सिंचाई नहरें, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कौशल उन्नयन केंद्र, सड़कें और सामुदायिक केंद्र के लिए वन भूमि के परिवर्तन का भी प्रावधान करता है. लेकिन परिवर्तित की जाने वाली भूमि एक हेक्टेयर से कम होना चाहिए और ग्राम सभा द्वारा इसकी सिफारिश की गई हो.
- वन संबंधी विषयों का लोकतांत्रिकरण: यह अधिनियम ग्राम सभा को वन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार देता है. इस प्रकार आदिवासी व वनिक समुदायों में लोकतांत्रिक और समुदाय आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है.
- लैंगिक समानता: अधिनियम लैंगिक समानता पर भी बल देता है. व्यक्ति के वन अधिकारों के लिए भू-स्वामित्व पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से या परिवार के एकल मुखिया के नाम से जारी होता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो.
यह अधिनियम केवल भूमि अधिकारों को मान्यता देने से बढ़कर है. भारत के जंगलों में अधिकांशतः आदिवासी समुदाय (जिन्हें सरकार अनुसूचित जनजाति से सम्बोधित करती है) निवास करते है. इनके निवास जंगल के आसपास के लोग भी किसी न किसी तरह इन जंगलों पर निर्भर होते है. यह परम्परा सदियों से जारी है.
प्रशासन का इनतक सिमित पहुँच होने के कारण, ये अब तक मूलधारा के समाज से कटे है. ऐसे में इनके परम्परागत अधिकारों को मान्यता देना इनके जीवन को स्थिरता और सम्मान प्रदान करना है. FRA इसमें काफी हद तक सफल है. मतलब, यह ‘पर्यावरणीय स्थिरता’ को ‘सामाजिक न्याय’ के साथ जोड़ता है.
वन अधिकारों के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया
वन अधिकार अधिनियम के तहत, जंगलों पर पारंपरिक रूप से निर्भर रहने वाले लोगों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए एक तय प्रक्रिया और अलग-अलग स्तरों की समितियाँ बनाई गई हैं. यह पूरी प्रक्रिया समुदाय-आधारित और लोकतांत्रिक तरीके से चलती है.
- ग्राम सभा: यह सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है. ग्राम सभा:
- व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की पहचान करती है,
- दावे स्वीकार करती है,
- उनका सत्यापन और नक्शा तैयार करती है,
- फिर इस पर एक प्रस्ताव पारित करके उपखंड समिति को भेजती है.
अगर किसी व्यक्ति को ग्राम सभा के फैसले से आपत्ति हो, तो वह 60 दिनों के भीतर उपखंड समिति में याचिका दे सकता है.
- उपखंड स्तर की समिति: यह समिति:
- ग्राम सभा के प्रस्तावों की जांच करती है,
- अधिकारों का अभिलेख तैयार करती है,
- इसे उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को भेजती है.
यदि कोई व्यक्ति इस समिति के फैसले से असंतुष्ट है, तो वह 60 दिनों में जिला समिति में अपील कर सकता है.
- जिला स्तर की समिति: यह समिति:
- उपखंड समिति के अभिलेखों की समीक्षा करती है,
- और वन अधिकारों को अंतिम रूप से मंजूरी देती है.
इसका निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होता है.
- राज्य स्तरीय निगरानी समिति (Monitoring Committee): यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि पूरी प्रक्रिया सही ढंग से हो रही है. साथ ही, यह नोडल एजेंसी को रिपोर्ट और आंकड़े प्रस्तुत करती है. यह पूरा ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि वन अधिकारों की मान्यता पारदर्शी, न्यायसंगत और समुदाय की भागीदारी से हो.
इन समितियों की संरचना में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग, और जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं. इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं के तीन सदस्य भी इन समितियों का हिस्सा होते हैं. इनमें से दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों के और कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है.
प्राधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
वन अधिकार अधिनियम के तहत इसके लाभार्थियों के कुछ कर्तव्य भी हैं. इसके तहत उन्हें:
- वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना होगा;
- यह सुनिश्चित करना होगा कि जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं; और
- यह सुनिश्चित करना होगा कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत किसी भी विनाशकारी व्यवहार से संरक्षित है.
- उन्हें ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों का भी पालन करना होगा (विशेष रूप से सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने और वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी क्रियाकलाप को रोकने के लिए).
केंद्रीय सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर निदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी है. केंद्र प्रक्रियात्मक विवरणों, दावों को प्राप्त करने और सत्यापित करने की प्रक्रिया, समितियों की संरचना और कृत्यों, और अन्य आवश्यक मामलों के लिए प्रावधान कर सकता हैं.
अधीनस्थ अपराध और शास्तियाँ
यदि कोई प्राधिकरण या समिति या इसका कोई अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे अपराध का दोषी माना जाएगा. उस पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि कोई सदस्य या विभागाध्यक्ष यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध को रोकने के लिए उचित तत्परता बरती थी, तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा.
कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि ग्राम सभा, राज्य स्तर की मानीटरी समिति को 60 दिन से कम की सूचना नहीं दे देती है और राज्य स्तर की मानीटरी समिति ने ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर ली हो.
वन अधिकार अधिनियम (FRA) का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है. लेकिन इसका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन कई समस्याओं से जूझ रहा है. जैसे—नौकरशाही का विरोध, संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी, और दावों की बड़ी संख्या में अस्वीकृति इत्यादि. यह दिखाता है कि कानून बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके सफल लागू होने के लिए प्रशासन में सुधार, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और राजनीतिक इच्छाशक्ति भी जरूरी है.
इसके अलावा, FRA की कई बातों का दूसरे पुराने कानूनों जैसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 से टकराव होता है. इससे कानूनी भ्रम और टकराव की स्थिति बनती है. समावेशी विकास व बेहतर शासन के लिए पर्यावरण से जुड़े सभी कानूनों में आपसी तालमेल और स्पष्टता लाने की जरूरत है.
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है. ये नियमावली मूल अधिनियम के कार्यान्वयन में मौजूद व्यावहारिक अस्पष्टताओं और परिभाषा संबंधी चुनौतियों को दूर करने का एक विधायी प्रयास थीं. इसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करना था. व्यावहारिक अनुभव के आधार पर हुए ये संसोधन सरकार के आदिवासियों/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है.
प्रमुख संशोधन और उनका प्रभाव
इन नियमावली ने विशेष रूप से सामुदायिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से परिभाषित किया:
- सामुदायिक अधिकारों का स्पष्टीकरण: इस संसोधन के “उपबंध 1, प्रारूप ‘ख’ में” धारा 3-1 (ख) के तहत निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार, धारा 3-1 (ग) के तहत गौण वन उत्पादों पर अधिकार, धारा 3-1 (छ) के तहत मछली, जलाशय और चराई हेतु पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, धारा 3-1 (ङ) के तहत पीटीजी और कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास/बसाहट की सामुदायिक भूमि, और धारा 3-1 (ठ) के तहत अन्य पारंपरिक अधिकार को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है.
- सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन: धारा 3-1 (झ) के अंतर्गत CFR के अधीन सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार हेतु आवेदन/दावे प्राप्त किए जाने और पात्रतानुसार मान्यता संबंधी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है.
सामुदायिक अधिकारों के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
हालांकि नियमों में कई बातें साफ कर दी गई हैं. फिर भी सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) को लागू करने में काफी समस्याएं बनी हुई हैं. अब तक बहुत कम जमीन सामुदायिक अधिकारों के तहत दी गई है. जैसे ओडिशा राज्य में व्यक्तिगत अधिकारों को तो काफी हद तक मान्यता मिली है. लेकिन सामुदायिक अधिकारों की स्थिति कमजोर है.
यह बताता है कि वन अधिकार अधिनियम के लागू होने में एक बड़ा असंतुलन है. व्यक्तिगत अधिकारों को पहचानना प्रशासन के लिए आसान होता है. लेकिन सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए सामाजिक और संस्थागत स्तर पर ज्यादा समन्वय की जरूरत होती है. जब तक सामुदायिक सशक्तिकरण को बराबर महत्व नहीं मिलेगा, तब तक इस कानून का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा. खासतौर से इसलिए क्योंकि सामुदायिक अधिकार वन संसाधनों के टिकाऊ (स्थायी) प्रबंधन में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं.
इसके अलावा, ग्राम सभाओं की भूमिका को नजरअंदाज करना, दावों का बड़ी संख्या में खारिज होना, और संरक्षित क्षेत्रों में लोगों का विस्थापन जैसी समस्याएँ भी अब तक बनी हुई हैं. इससे साफ होता है कि सिर्फ कानूनों में बदलाव कर देना काफी नहीं है. जब तक प्रशासनिक ढांचे में सुधार, अधिकारियों का जागरूकता और जमीनी स्तर प्रयास नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा.
यह पूरे मामले को एक लगातार चल रहे संघर्ष को दिखाता है. एक तरफ अच्छी नीयत से बनाए गए कानून हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हें लागू करने में गंभीर रुकावटें हैं.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान करना है. इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और व्यक्तियों व संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करना भी शामिल है.
यह पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस है. यह भारत में ‘पर्यावरण न्याय’ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थागत विकास को दर्शाता है. पर्यावरणीय विवादों में अक्सर जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू शामिल होते हैं, जिनके लिए सामान्य अदालतों की तुलना में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. NGT का गठन पर्यावरणीय मुकदमेबाजी को सुव्यवस्थित करता है. साथ ही यह न्याय तक पहुंच बढ़ाता है और उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करता है. इस निकाय के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर अधिक केंद्रित और कुशल निर्णय संभव होते हो पाते है.
संरचना
NGT की संरचना में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जो इसे तकनीकी और कानूनी दोनों प्रकार की विशेषज्ञता प्रदान करते हैं:
- अध्यक्ष: NGT का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं.
- न्यायिक सदस्य: ये सदस्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं.
- विशेषज्ञ सदस्य: इन सदस्यों के पास पर्यावरण/वन संरक्षण और संबंधित विषयों में पेशेवर योग्यता और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है.
- प्रत्येक बेंच में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होता है.
- NGT की रजिस्ट्री में महापंजीयक, पंजीयक और उप-पंजीयक शामिल होते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं.
बेंच
NGT की पहुंच और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी कई बेंचें स्थापित की गई हैं:
- प्रधान पीठ: नई दिल्ली में स्थित है, जो अधिकरण का मुख्य स्थान है.
- क्षेत्रीय बेंच: प्रधान पीठ के अतिरिक्त, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में चार अन्य क्षेत्रीय बेंचें स्थापित की गई हैं.
- NGT खुद को अधिक सुलभ बनाने के लिए सर्किट प्रक्रिया का पालन करता है. क्षेत्रीय बेंचों में सदस्यों की कमी होने पर, प्रधान पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य क्षेत्राधिकारों के आवेदनों की दूरस्थ सुनवाई करते है.
- क्षेत्रीय बेंचें भौगोलिक बाधाओं को कम करती हैं.
- पत्र याचिकाएं आम नागरिकों और गैर-सरकारी संगठनों को औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के बिना भी पर्यावरणीय क्षति के मामलों को उठाने का अवसर देती हैं. यह पर्यावरणीय शासन में नागरिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है. साथ ही, हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए न्याय प्राप्त करने के मार्ग को सुगम बनाता है.
प्रक्रिया
NGT की कार्यप्रणाली पारंपरिक अदालतों से भिन्न है. इसकी यह खासियत इसे पर्यावरणीय मामलों में अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करती है:
- NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है. यह NGT को पारंपरिक कानूनी प्रक्रियाओं की कठोरता से परे जाकर अधिक अनुकूली और न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है. यह पर्यावरणीय मामलों की विशिष्ट प्रकृति को पहचानता है, जहाँ साक्ष्य अक्सर गैर-पारंपरिक या तकनीकी होते हैं. यह लचीलापन NGT को साक्ष्य के बजाय तथ्यों और विशेषज्ञ राय पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जिससे पर्यावरणीय क्षति के मामलों में त्वरित और प्रभावी समाधान संभव होता है.
- इसे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिससे यह अपने कार्यों का सुगमता से निर्वहन कर सकता है.
- आवेदन या अपील दाखिल करने की प्रक्रिया सरल है.
- इसका लक्ष्य आवेदन या अपील को दाखिल होने के 6 महीने के भीतर निपटाना है.
- निर्णय/पुरस्कार पारित करते समय, NGT सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत (precautionary principle) और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (polluter pays principle) के सिद्धांतों को लागू करता है. यह NGT की भूमिका को केवल विवादों को निपटाने से आगे बढ़ाता है. यह खासियत इसे ‘पर्यावरण नीति’ के एक सक्रिय आकार देने वाले के रूप में स्थापित करता है.
- “पत्र याचिकाओं” के स्वीकारोक्ति से आम नागरिकों को औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के बिना भी मामले उठाने का अवसर मिलता है.
- NGT के निर्णय की समीक्षा का प्रावधान है. इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है.
भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017
भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017 औपनिवेशिक काल के कानून भारतीय वन अधिनियम, 1927 में एक महत्वपूर्ण संशोधन है. यह बिल भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 का स्थान लेता है. इस संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य गैर-वन क्षेत्रों में बाँस की खेती को बढ़ावा देना है.
प्रमुख खासियत
इस अधिनियम की सबसे प्रमुख खासियत “वृक्ष” की परिभाषा में किया गया परिवर्तन है. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत, “वृक्ष” की परिभाषा में ताड़, बाँस, ठूंठ, झाड़-झंखाड़ और बेंत शामिल थे. इस वर्गीकरण के कारण, बाँस को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी. कई बार इसे गैर-वन क्षेत्रों में उगाया गया होता था. यह बाँस की खेती में एक बड़ी बाधा थी.
नए नियम में, “बाँस” को शब्द को वृक्ष नहीं माना गया है, विशेष रूप से जब इसे गैर-वन क्षेत्रों में उगाया गया हो. वन अधिकार अधिनियम, 2006 में बाँस को गैर-इमारती वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि वन अधिनियम में इसे इमारती लकड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है. भारतीय वन संशोधन अधिनियम, 2017 से यह विसंगति दूर हुई है.
इस प्रकार यह संशोधन ‘नौकरशाही बाधाओं’ को दूर करने और कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक ‘लक्षित विधायी हस्तक्षेप’ का उदाहरण है.
प्रभाव
इस संशोधन के दूरगामी आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव अपेक्षित हैं:
- आर्थिक प्रभाव:
- गैर-वन क्षेत्रों में उगने वाले बाँस को काटने और आर्थिक उपयोग के लिए उसके परिवहन हेतु अब अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी .
- यह किसानों और आदिवासियों की आय बढ़ाने में मदद करेगा.
- यह बाँस-आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाएगा.
- यह 12.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि में बाँस की खेती के लिए एक व्यवहार्य विकल्प तैयार करेगा.
- यह संशोधन राष्ट्रीय बाँस मिशन की सफलता में भी सहायता करेगा.
- पर्यावरणीय प्रभाव:
- गैर-वन क्षेत्रों में बाँस की खेती को बढ़ावा देकर यह देश के हरित आवरण को बढ़ाएगा.
- बाँस मृदा-नमी संरक्षण, भूस्खलन की रोकथाम और पुनर्वास में सहायक है.
- यह वन्यजीव आवासों का संरक्षण करेगा और जैव-भार के स्रोत को बढ़ाएगा.
- बाँस लकड़ी के एक स्थायी विकल्प के रूप में भी कार्य करता है, जिससे वनों पर दबाव कम होता है.
अंत में (Conclusion)
भारत में पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए सशक्त कानूनी ढाँचा मौजूद है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अब भी कई चुनौतियाँ हैं. जमीनी स्तर पर नौकरशाही अड़चनें, संसाधनों की कमी और जन-जागरूकता का अभाव कार्यान्वयन अंतराल को दर्शाते हैं. विभिन्न कानूनों में आपसी विरोध के कारण कानूनी सामंजस्य की आवश्यकता है.
साथ ही, पर्यावरणीय निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को और सुदृढ़ करना ज़रूरी है. जलवायु परिवर्तन और तकनीकी विकास जैसी आधुनिक चुनौतियों के मद्देनज़र कानूनों को समय-समय पर अद्यतन करना भी आवश्यक है. भविष्य के लिए भारत को एकीकृत, सहभागी और लचीला दृष्टिकोण अपनाकर विधायी सुधार, प्रशासनिक दक्षता, समुदायों का सशक्तिकरण और न्यायपालिका की सक्रियता के ज़रिए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना होगा.