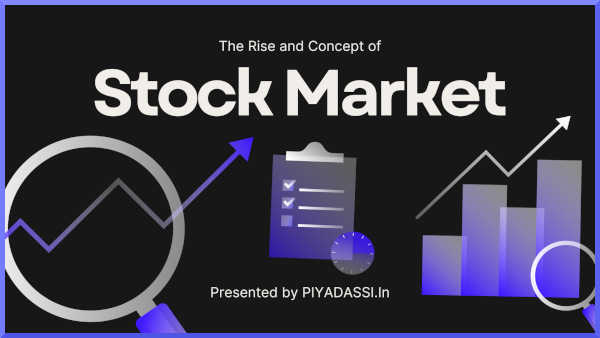भारतीय कृषि में, फसलें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं: खरीफ, रबी, और जायद. फसलें वे वनस्पतियाँ, पेड़-पौधे या पैदावार हैं जिन्हें मनुष्य या पशुओं के उपभोग के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. फिर इन्हें काटा या तोड़ा जाता है. इन फसलों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, और किसान इन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी उगाते हैं. भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं. इस पेशे पर निर्भर लोगों को कृषक या किसान कहा जाता है. भारत में प्रत्यारोपण तकनीक, जापानी प्रत्यारोपण तकनीक और नई श्री तकनीक का उपयोग फसल उत्पादन में होता हैं.
भारतीय कृषि का महत्व (Importance of Indian Culture in Hindi)
भारतीय भूगोल में कृषि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था और आजीविका का एक बड़ा आधार है. भारत की लगभग 49% आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है.
भारत में कुल 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जबकि 195 मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र है, जो कृषि की व्यापकता को दर्शाता है. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है. देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान 14% है. यह न केवल लोगों की आय और धन के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि बड़े उद्योगों के लिए कच्चे माल का एक प्रमुख स्रोत भी है.
कृषि लोगों को भोजन और पशुओं के लिए चारा जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है. यह भारतीय समाज के पोषण और कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है.
फसलों का वर्गीकरण (Classification of Crops in Hindi)
हम फसल उत्पादन को ऋतु, उपयुक्तता, जीवन चक्र, उपयोग व आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं. इस प्रकार फसलों का वर्गीकरण हैं:
ऋतुओं के अधार पर
भारत में फसलों को मुख्यतः तीन ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है: रबी, खरीफ, और जायद.
रबी (शीत ऋतु) की फसलें
रबी की फसलें आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं. इनकी कटाई अप्रैल से मई तक हो जाती है. इन फसलों को बुवाई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है. लेकिन पकने के लिए शुष्क और गर्म वातावरण अनुकूल होता है.
प्रमुख रबी फसलें: गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिजका, हरा चारा, मसूर, आलू, राई, तम्बाकू, लाही, जई, अलसी और सूरजमुखी.
खरीफ फसलें
भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसलें जून-जुलाई में बोई जाती हैं. इनकी कटाई अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होती है. इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है. वहीं पकते समय शुष्क वातावरण की जरूरत होती है.
प्रमुख खरीफ फसलें: कपास, मूँगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उड़द, मूँग, मोठ, लोबिया (चंवला), ज्वार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, ग्वार, जूट और सनई.
जायद फसलें
जायद की फसलें शुष्क हवाओं और तेज गर्मी को सहन करने में सक्षम होती हैं. इसलिए, उत्तर भारत में ये फसलें मार्च-अप्रैल में बोई जाती हैं. इनकी कटाई जून में होती है.
प्रमुख जायद फसलें: तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूँग, उड़द और सूरजमुखी.
भूमि की उपयुक्तता
फसलों को उनकी वृद्धि और उपज के लिए आवश्यक मिट्टी के प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है. मुख्य रूप से इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
- हल्की भूमि की फसलें: कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके लिए हल्की भूमि की आवश्यकता होती है. इस प्रकार की मिट्टी में इन फसलों की वृद्धि अच्छी होती है. प्रमुख फसलें: बाजरा, मूँगफली.
- मध्यम भूमि की फसलें: सब्जियों और कुछ फलों की फसलों के लिए मध्यम भूमि की आवश्यकता होती है. यह मिट्टी इन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है.
- भारी भूमि की फसलें: कपास और धान जैसी फसलों की वृद्धि और उपज भारी भूमि में अच्छी होती है. यह मिट्टी इन फसलों के लिए आदर्श मानी जाती है.
जीवन चक्र के आधार पर
फसलों को उनके जीवन चक्र की अवधि के आधार पर तीन मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है:
- एकवर्षीय फसल: जिन फसलों का जीवन चक्र एक वर्ष या इससे कम समय में पूरा हो जाता है, उन्हें एकवर्षीय फसलें कहा जाता है. उदाहरण: सोयाबीन, गेहूँ, जौ, धान, चना आदि.
- द्विवर्षीय फसल: जिन फसलों का जीवन चक्र 2 साल या इससे कम समय में पूरा होता है, उन्हें द्विवर्षीय फसलें कहा जाता है. इन फसलों में पहले वर्ष वानस्पतिक वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उनमें फूल और बीज आदि का निर्माण होता है. उदाहरण: गन्ना, चुकंदर आदि.
- बहुवर्षीय फसल: जो फसलें दो या दो से अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं, उन्हें बहुवर्षीय फसलें कहा जाता है. इन फसलों के जीवन चक्र में हर साल या एक वर्ष के अंतराल में फूल और फल लगते हैं. उदाहरण: नेपियर घास, लूसर्न आदि.
उपयोग के आधार पर
फसलों को उनके विशिष्ट उपयोग और कार्य के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
कवर क्रॉप्स (Cover Crops)
कवर क्रॉप्स वे फसलें हैं जो जमीन को ढंककर रखती हैं. ये बरसात के मौसम में मिट्टी को कटाव से बचाती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता, उर्वरता, पानी के प्रबंधन, खरपतवार, कीटों, बीमारियों, जैव विविधता और वन्य जीवों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं. ये तेजी से बढ़ती हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में एक जाल की तरह फँसकर कटाव को रोकती हैं. उदाहरण: शकरकंद, लोबिया, उड़द, मूँगफली, पैराग्रास आदि.
समोच्च फसलें (Contour Crops)
इस कृषि प्रणाली में फसलों को ढलान वाले क्षेत्रों में पंक्तियों में रोपा जाता है. समोच्च फसलें भूमि और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.
नकदी फसलें (Cash Crops)
नकदी फसलों का मुख्य उद्देश्य उनकी बिक्री कर तुरंत पैसा कमाना होता है. इन्हें व्यावसायिक फसलें या वाणिज्यिक फसलें (Commercial Crops) भी कहा जाता है. उदाहरण: जूट, कपास, तम्बाकू, गन्ना, चाय, कॉफी और रबर आदि.
बागानी फसलें (Plantation Crops)
भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जिनके बड़े-बड़े बागान लगाए जाते हैं. उदाहरण: कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, नारियल, ताड़, सुपारी और रबर.
ट्रैप फसलें (Trap Crops)
इन फसलों को मृदाजनित हानिकारक जीवों (जैसे परजीवी खरपतवार या कीट-पतंग) को फँसाने के लिए उगाया जाता है. उदाहरण: ओरोबेंकी (Orobanche) को सोलेनेसियस (Solanaceous) पौधों पर फँसाया जाता है.
ऊर्जा फसलें (Energy Crops)
ऊर्जा फसलों को ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उगाया जाता है. प्रमुख ऊर्जा फसलें: इथेनॉल, गन्ना (अल्कोहल प्राप्त करने के लिए), आलू, मक्का, टैपिओका, जेट्रोफा आदि.
आपातकालीन फसलें (Emergency Crops)
ये फसलें तब लगाई जाती हैं जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्य फसलें खराब हो जाती हैं. ये अल्प अवधि की फसलें होती हैं जो तेजी से बढ़ती हैं, ताकि आगामी ऋतु में फिर से सामान्य फसलें उगाई जा सकें. प्रमुख आपातकालीन फसलें: प्याज, मूली, मूँग, उड़द, लोबिया आदि.
बॉर्डर या बैरियर क्रॉप्स (Border/Barrier Crops)
बॉर्डर या बैरियर क्रॉप्स को खेत के चारों ओर मुख्य फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाया जाता है. ये फसलें सामान्यतः खेत की मेढ़ पर लगाई जाती हैं, जिससे हवा की गति कम हो जाती है और उनमें लगे कांटे जानवरों को फसलों तक जाने से रोकते हैं. उदाहरण: चने की फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों ओर कुसुम की फसलें उगाई जाती हैं.
कीट को आकर्षित करने वाली फसलें
इन फसलों को मुख्य फसल को कीट-पतंगों और खरपतवारों से बचाने के लिए सामान्यतः मुख्य फसलों के चारों ओर लगाया जाता है. ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे मुख्य फसल सुरक्षित रहती है. उदाहरण: कपास की फसल को कीट-पतंगों से बचाने के लिए उसके चारों ओर भिंडी की फसल उगाई जाती है.
हरी खाद देने वाली फसलें
इन फसलों का उपयोग भूमि को हरी खाद देने के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है. उदाहरण: सनई, ढैंचा आदि.
भूमि संरक्षण करने वाली फसलें
इन फसलों का रोपण भूमि के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है. इनकी जड़ें मिट्टी को जकड़ लेती हैं और उसे बरसात के पानी में बहने से बचाती हैं. उदाहरण: मूँगफली, मूँग आदि.
अंतर्वर्ती (अल्पकालिक) फसलें
ये फसलें दो मुख्य फसलों के बीच के समय का सदुपयोग करने के लिए लगाई जाती हैं. ये अल्पकालिक होती हैं. उदाहरण: उड़द, मूँग आदि.
सूचक फसलें
सूचक फसलें वे होती हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने पर अपने ऊपर कमी के लक्षण दिखाने लगती हैं. इनका उपयोग मिट्टी के पोषक तत्वों की पहचान करने के लिए किया जाता है. उदाहरण: फूलगोभी, मक्का आदि.
प्रकाश की अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण
फसलों को उनकी वृद्धि, फूल और फलने के लिए आवश्यक प्रकाश की अवधि के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है:
कम प्रकाश अवधि वाले फसल
कुछ पौधे, फूल और फल कम अवधि के लिए सूर्य की रोशनी चाहते हैं. इनकी वृद्धि, फूल और फल बनने के लिए कम समय तक रोशनी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें छोटे दिनों में उगाया जाता है. उदाहरण: सोयाबीन, ज्वार, बाजरा आदि.
अधिक अवधि का प्रकाश
इन फसलों को दिन में अधिक समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है. इसलिए, इन्हें बड़े दिनों में उगाया जाता है ताकि इनमें फूल और फलने की क्रिया ठीक से हो पाए. उदाहरण: बरसीम, जौ, मटर आदि.
प्रकाश निरप्रभावी फसल
इन फसलों पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इन फसलों की छोटे और बड़े दोनों दिनों में अच्छी वृद्धि होती है. उदाहरण: टमाटर.
आर्थिक आधार पर
फसलों को उनके आर्थिक महत्व और उपयोग के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है. यहाँ कुछ प्रमुख श्रेणियाँ दी गई हैं:
चारे की फसलें
ये फसलें मुख्य रूप से पशुओं के चारे के लिए उगाई जाती हैं. उदाहरण: वरसीम, ग्वार, लोबिया आदि.
रेशे वाली फसलें
इन फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग वस्त्र, बोरे और अन्य सामग्री बनाने में होता है. उदाहरण: जूट, सनई, कपास आदि.
तिलहनी फसलें
इन फसलों के बीजों से तेल निकाला जाता है. उदाहरण: मूँगफली, सरसों, सोयाबीन आदि.
औषधि फसलें
ये फसलें औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं और इनका उपयोग दवाओं या हर्बल उत्पादों में किया जाता है. उदाहरण: पुदीना, चायपत्ती आदि.
जड़ वाली फसलें
इन फसलों का खाद्य योग्य भाग उनकी जड़ें होती हैं. उदाहरण: आलू, रतालू, मूली, गाजर आदि.
चीनी देने वाली फसलें
इन फसलों से चीनी या शर्करा प्राप्त की जाती है. उदाहरण: गन्ना, चुकंदर आदि.
मसाले वाली फसलें
इन फसलों का उपयोग भोजन में स्वाद और सुगंध जोड़ने के लिए मसालों के रूप में किया जाता है. उदाहरण: लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी आदि.
अनाज की फसलें
ये फसलें मुख्य रूप से मनुष्य के भोजन के लिए अनाज प्रदान करती हैं. उदाहरण: गेहूँ, जौ, धान आदि.
मोटे अनाज की फसलें
ये भी अनाज की फसलें हैं, लेकिन इन्हें मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है जो अक्सर शुष्क या कम उपजाऊ क्षेत्रों में उगाए जाते हैं. उदाहरण: ज्वार, बाजरा और मक्का आदि.
अन्य मोटे अनाज
इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनाज शामिल हैं जो आमतौर पर मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं. उदाहरण: काकून, रागी, सोवा, चना आदि.
दलहनी फसलें
इन फसलों से दालें प्राप्त होती हैं जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं. उदाहरण: अरहर, चना, मूँग, मटर आदि.
भारत के मुख्य फसलें (Major Crops of India in Hindi)
भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें इस प्रकार हैं:
चावल (Rice)
चावल भारत की एक प्रमुख खरीफ या उष्णकटिबंधीय फसल है. हालाँकि, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जलवायु की अनुकूलता के कारण इसे तीनों फसल ऋतुओं (खरीफ, रबी और जायद) में उगाया जाता है. पश्चिम बंगाल में, इसे ‘ओस’ (शरदकालीन), ‘अमन’ (शीतकालीन) और ‘बोरो’ (ग्रीष्मकालीन) के नाम से तीन फसलों में उत्पादित किया जाता है.
भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्रों में से सबसे अधिक क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है. बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं. भौगोलिक रूप से, पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र, प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, हिमालय की गिरिपद पहाड़ियाँ और तराई प्रदेश चावल उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं.
चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, लगभग 25°C का औसत तापमान, और 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है.
चावल से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य
चावल उत्पादन में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है. वर्तमान में भारत विश्व में शीर्ष चावल निर्यातक राष्ट्र है, जिसके बाद थाईलैंड और वियतनाम का स्थान आता है. भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति ‘जया’ थी. जापान और फिलीपींस में चावल का उत्पादन डपोग विधि द्वारा किया जाता है.
धान के फसलोत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए अज़ोला और नील हरित शैवाल जैसे जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है. ‘खैरा’ धान में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, जो जस्ते की कमी से होता है.
चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा (76%) सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि प्रोटीन (6-7%) और वसा (2.5%) न्यून मात्रा में होते हैं. पॉलिश किए हुए चावल की ऊपरी परत में विटामिन B1 (थायमीन) का अभाव पाया जाता है, और चावल को अधिक धोने से भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है. विटामिन B1 की कमी से ‘बेरी-बेरी’ नामक रोग होता है.
अनुसंधान संस्थान: केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक (ओडिशा) में स्थित है. अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (आई.आर.आर.आई.) का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आईएसएआरसी) वाराणसी में दिसंबर 2018 में स्थापित किया गया था.
भारत में चावल की मुख्य किस्में
भारत में चावल की हजारों किस्में उगाई जाती हैं, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, जलवायु और उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर भिन्न होती हैं. इनमें से कुछ प्रमुख और खास किस्में निम्नलिखित हैं:
1. बासमती चावल
- खासियत: अपनी लंबी दाने, मोहक सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह बिरयानी और पुलाव जैसे व्यंजनों के लिए बहुत पसंद किया जाता है.
- प्रमुख किस्में: पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718. बासमती 370, बासमती 385, सुपर बासमती, बासमती 2000 आदि.
- उत्पादन क्षेत्र: जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश.
2. गैर-बासमती चावल (सामान्य किस्में)
भारत में बासमती के अलावा भी कई अन्य प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, जो अपनी उपज क्षमता, स्थानीय अनुकूलन और पोषण मूल्य के लिए जाने जाते हैं. जया किस्म को”भारत की शान” कहा जाता है और इसने हरित क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह एक अर्ध-बौनी किस्म है जिसकी उपज क्षमता अच्छी होती है.
गैर-बासमती चावल की अन्य किस्में हैं – स्वर्ण, एमटीयू 1010, आईआर 64, सोना मसूरी, सफेद चावल (सामान्य), सेला चावल (Parboiled Rice) इत्यादि.
3. खास सुगंधित और क्षेत्रीय किस्में
भारत में कई क्षेत्रीय चावल की किस्में हैं जो अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती हैं, भले ही वे बासमती न हों.
- गोविंदभोग चावल: पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय, यह छोटा और सुगंधित चावल है जिसका धार्मिक महत्व भी है.
- इंद्रायणी चावल: महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में खेती की जाने वाली यह अंबेमोहर चावल की एक संकर किस्म है, जो सुगंधित और स्वादिष्ट होती है.
- अंबेमोहर चावल: महाराष्ट्र का एक छोटा, सुगंधित चावल जो जल्दी पक जाता है और इसमें आम के फूलों जैसी खुशबू आती है.
- काला चावल (चक हाओ अमुबी): मणिपुर में उगाया जाने वाला यह चावल अपने गहरे रंग, अद्वितीय स्वाद और उच्च पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है.
- मुश्क बुदजी: कश्मीर घाटी में उगाया जाने वाला एक छोटा, तीव्र सुगंध वाला चावल.
- गंधकसाल चावल: केरल के वायनाड में उगाया जाने वाला यह छोटा लेकिन शानदार सुगंध वाला गैर-बासमती चावल है.
- चिन्नौर चावल: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उगाई जाने वाली यह किस्म अपनी खास सुगंध और हल्के मीठे स्वाद के लिए मशहूर है, जिसे “मध्यप्रदेश का बासमती” भी कहा जाता है.
4. औषधीय चावल की किस्में
भारत में कुछ औषधीय गुणों वाली चावल की किस्में भी पाई जाती हैं, जैसे:
- कंठई बांको (छत्तीसगढ़)
- मेहर, सरिफुल, डनवार (ओडिशा)
- अतिकाय और कारी भट्ट (कर्नाटक)
- चेन्नेल्लू, कुंजननेल्लू, एरुमाक्कारी और करुथाचेम्बावू (केरल)
5. गोल्डन राइस (Golden Rice)
चावल में विटामिन-A की कमी को दूर करने के लिये वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक विज्ञान की सहायता से ‘बीटा कैरोटीन’ युक्त पीले रंग के चावल का निर्माण किया, इसे ‘गोल्डन राइस’ का नाम दिया गया. इसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है जो मानव शरीर के अंदर विटामिन-A में परिवर्तित हो जाती है.
गेहूँ (Wheat)
यह रबी की फसल है. गेहूँ की कृषि के लिये उपजाऊ दोमट मिट्टी, ठंडी जलवायु व वार्षिक वर्षा लगभग 50-75 सेमी. की आवश्यकता होती है. इसके लिये सामान्यतः 10°C-15C तापमान (बोते समय 10°C, वृद्धि के समय 15°C और पकते समय 20°C-25°C) की आवश्यकता होती है. यह भारत के कुल कृषि योग्य भूमि के धान के बाद दूसरी मुख्य फसल है.
हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूँ के उत्पादन पर पड़ा है. इसके प्रभाव से न केवल गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का स्तर भी ऊँचा हुआ है. गेहूँ उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात व महाराष्ट्र प्रमुख हैं. कल्याण सोना, सोनालिका, राज-3077, अर्जुन आदि गेहूँ की प्रमुख किस्में हैं. गेहूँ के उत्पादन में चीन प्रथम तथा भारत व रूस क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर हैं.
करनाल बंट एवं रस्ट गेहूँ की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है. रस्ट को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है- यलो रस्ट, ब्राउन रस्ट तथा ब्लैक रस्ट. गेहूँ में बौनेपन का जीन नोरिन-10 है. गेहूँ में 8 से 15 प्रतिशत प्रोटीन, लगभग 1.5 प्रतिशत वसा तथा लगभग 65-70 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट निहित होता है. गेहूँ में ‘ग्लूटेन’ नामक प्रोटीन पाया जाता है.
भारत में उगाई जाने वाली गेहूँ की किस्में
भारत में गेहूँ की अनेक किस्में उगाई जाती हैं, जिन्हें विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों और उपयोग के आधार पर विकसित किया गया है. गेहूँ की किस्में क्षेत्र, मिट्टी के प्रकार, सिंचाई की उपलब्धता और किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती हैं. किसान अक्सर स्थानीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विभागों द्वारा सुझाई गई नवीनतम और सबसे उपयुक्त किस्मों का उपयोग करते हैं.
कल्याण सोना (Kalyan Sona) और सोनालिका (Sonalika) ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था. ये दोनों गेंहू का सामान्य किस्म हैं. गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख और खास किस्में निम्नलिखित हैं:
1. सामान्य रूप से उगाई जाने वाली प्रमुख किस्में: राज-3077 (Raj-3077), अर्जुन (Arjun), एचडी 2967 (HD 2967), एचडी 3086 (HD 3086), पीबीडब्ल्यू 343 (PBW 343), डीडीडब्ल्यू 17 (DDW 17) और डीडीडब्ल्यू 18 (DDW 18) आदि.
2. विशेष प्रकार की किस्में:
- मैकरोनी गेहूँ (Durum Wheat / कठोर गेहूँ): यह शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है. इसलिए इसे कठोर गेंहू भी कहा जाता है. इसका उत्पादन मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किया जाता है. इसका उपयोग सूजी, पास्ता, मैकरोनी और अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में होता है. प्रमुख किस्में: डीडीडब्ल्यू 17, डीडीडब्ल्यू 18, मालव शक्ति (HI 8498).
- ट्रिटिकेल (Triticale): यह एक मानव-निर्मित प्रजाति है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा गेहूँ (Triticum) और राई (Secale) के बीच संकरण (cross-breeding) कराकर उत्पन्न किया गया है. इसमें गेहूँ और राई दोनों के वांछनीय गुण होते हैं, जैसे उच्च उपज, बेहतर पोषण मूल्य और पर्यावरणीय तनावों के प्रति बेहतर सहनशीलता. इसका उपयोग मुख्य रूप से पशु चारा और कुछ खाद्य उत्पादों में होता है.
3. रोग प्रतिरोधी और उन्नत किस्में (हाल की)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय लगातार नई और बेहतर गेहूँ की किस्में विकसित कर रहे हैं जो अधिक उपज देने वाली, रोगों के प्रति प्रतिरोधी और बदलते जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हों. इनमें से कुछ किस्में हैं: पूसा तेजस (Pusa Tejas – HI 8759), एचआई 1621 (HI 1621), डब्ल्यूएच 1183 (WH 1183), डीडीडब्ल्यू 47 (DDW 47) आदि.
मक्का (Maize)
मक्का, जिसे “भारतीय मक्का” या “कॉर्न” के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अत्यधिक आनुवंशिक उपज क्षमता और बहुउपयोगिता के कारण वैश्विक स्तर पर “अनाज की रानी” (Queen of Cereals) के रूप में प्रसिद्ध है. यह विश्वभर में गेहूँ और चावल के बाद सबसे अधिक उगाई जाने वाली अनाज फसल है. भारत में मक्का की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में की जाती है. लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसे रबी और ग्रीष्मकालीन/ जायद फसल के रूप में भी बोया जाता है.
यह C4 पौधों के अंतर्गत आता है. मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है. भारत में इसे पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था. भारत में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार तथा छत्तीसगढ़ मक्का उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं. इसके अतिरिक्त गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में भी इसे उगाया जाता है.
यह देश में चावल और गेहूँ के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन-ए, बी-कॉम्प्लेक्स और खनिज तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है. मक्का, खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है. इसे ग्लूकोज, एल्कोहलिक पेय तथा बायोडीज़ल बनाने में भी प्रयोग किया जाता है.
मक्का अनेक औद्योगिक उत्पादों के लिए प्रमुख कच्चा माल भी है. इससे स्टार्च, तेल, प्रोटीन, मादक पेय, खाद्य स्वीटनर (जैसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप) तथा बायोफ्यूल (इथेनॉल) का निर्माण किया जाता है. इसके अलावा मक्का का प्रयोग फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म निर्माण, वस्त्र, गोंद, पैकेजिंग, कागज उद्योग, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक निर्माण में भी होता है.
मक्का से जुड़े प्रमुख तथ्य
यहाँ भारत में मक्का उत्पादन से जुड़ी शीर्ष 10 रोचक जानकारियाँ दिए गए हैं:
- भारत में गंगा-5, डेक्कन-101 एवं गंगा-11 आदि मक्का की आनुवंशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं.
- भारत विश्व में मक्का उत्पादन के मामले में चौथे से पाँचवें स्थान के बीच रहता है.
- अमेरिका मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर है.
- कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार मिलकर देश के लगभग 55% से अधिक मक्का उत्पादन में योगदान देते हैं.
- भारत में मक्का की खपत का 60% हिस्सा पशु और पोल्ट्री चारे के रूप में उपयोग होता है. शेष भोजन और औद्योगिक उत्पादों में जाता है.
- भारत हर साल 10-12 लाख टन मक्का का निर्यात करता है. भारत से मुख्य खरीदार देश वियतनाम, बांग्लादेश और नेपाल हैं.
- मक्का से इथेनॉल बनाया जाता है, जो भारत की ग्रीन एनर्जी नीति के तहत पेट्रोल में मिलाया जाता है.
- मक्का एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, जो 20°C से 35°C तापमान में अच्छी तरह उगती है.
- 100 ग्राम मक्का में औसतन 365 कैलोरी ऊर्जा, 9.4 ग्राम प्रोटीन, 19 ग्राम फाइबर और कई आवश्यक विटामिन पाए जाते हैं.
- बिहार के कुछ बाढ़ग्रस्त इलाकों में मक्का मुख्य फसल हैं.
मोटे अनाज (Millets)
भारत में मोटे अनाजों का उत्पादन और उपभोग प्राचीन काल से होता आ रहा है. ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं. ये पोषक तत्व और फाइबर से भरपूर होते है. इसलिए इन्हें “सुपरफूड्स” की श्रेणी में रखा जाता है. मोटे अनाजों में ग्लूटेन नहीं होता, जिससे ये पाचन के लिए लाभकारी और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं.
भारत सरकार ने 2018 को ‘मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष‘ घोषित किया था. वहीं, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 2023 को ‘अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष (International Year of Millets)’ के रूप में मनाया. इसका उद्देश्य मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना और इनके पोषण लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना था. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों को “क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स” कहा जाता है क्योंकि ये सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हैं.
भारत विश्व का सबसे बड़ा मोटा अनाज उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन का लगभग 41% हिस्सा भारत में होता है.मोटे अनाजों की खेती कम लागत, कम पानी और पर्यावरण-अनुकूल मानी जाती है.सरकार ‘पोषक-अन्न अभियान‘ के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ियों में बच्चों के भोजन में मोटे अनाजों को शामिल करने पर जोर दे रही है.
1. ज्वार (Sorghum)
क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार भारत की तीसरी सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है. यह फसल मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है और शुष्क एवं अर्ध-शुष्क जलवायु में अच्छी होती है. महाराष्ट्र ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है. इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं.
पोषण तत्वों में वृद्धि के लिए 2018 में ‘परभानी शक्ति‘ नामक देश का पहला बायो-फोर्टिफाइड ज्वार विकसित किया गया. इसमें लौह तत्व और जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है. ज्वार का आटा रोटियाँ, दलिया, डोसा, बेकरी उत्पादों में इस्तेमाल होता है. यह मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी माना जाता है.
2. बाजरा (Pearl Millet)
बाजरा को भारत में “गरीबों का भोजन” कहा जाता था. अब इसे हेल्दी डायट और सुपरफूड के रूप में अपनाया जा रहा है. यह फसल कम पानी में भी उगाई जा सकती है. महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं.
बाजरा मुख्यतः खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिणी भारत में इसे खरीफ एवं रबी दोनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है. इस फसल के लिये 25°C-30°C तापमान तथा 40-50 सेमी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है. इस फसल के लिये हल्की बलुई, छिछली काली व लाल मिट्टी अधिक उपयोगी होती है.
इसमें आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फाइबर और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है. बाजरे से रोटियाँ, खिचड़ी, स्नैक्स, एनर्जी बार और बेकरी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं.
3. रागी (Finger Millet)
रागी मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है. यह दोमट एवं उथली कंटीली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है और इसमें कीट व रोग का प्रकोप भी कम होता है. कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं.
रागी में कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, फाइबर और अमीनो एसिड की उच्च मात्रा पाई जाती है, जिससे यह हड्डियों की मजबूती और एनीमिया की रोकथाम में सहायक है. रागी का प्रयोग रागी रोटी, दलिया, बिस्किट, केक, माल्टेड हेल्थ ड्रिंक आदि बनाने में किया जाता है.
- अन्य मोटे अनाज
- कोदो (Kodo Millet): उच्च फाइबर और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक.
- कुटकी (Little Millet): हृदय रोग और मधुमेह में लाभकारी.
- सांवा (Barnyard Millet): उपवास के समय सेवन किया जाने वाला प्रमुख अनाज.
- कंगनी (Foxtail Millet): प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर.
जौ (Barley)
जौ (Barley) एक शीतोष्ण कटिबंधीय एवं रबी की फसल है. यह फसल भारत के प्राचीन कृषि इतिहास से जुड़ी हुई है. इसका उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 3000 ईसा पूर्व) के समय से ही किया जा रहा है. जौ को इसके उच्च पोषण मूल्य, औषधीय गुणों और बहुउपयोगिता के कारण सदियों से मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है.
जौ की अच्छी उपज के लिए 10°C से 18°C का तापमान उपयुक्त होता है. इसकी खेती के लिए 70 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है. यह फसल दोमट और जल निकासी वाली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगती है. जौ ऐसी फसलों में शामिल है जो कम पानी में भी अच्छी उपज देती हैं, इसलिए यह सूखा-सहिष्णु फसल मानी जाती है.
उत्तर प्रदेश देश में जौ उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं. इसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार और झारखंड में भी उगाया जाता हैं. जौ से सत्तू, दलिया, रोटियाँ, खिचड़ी और विभिन्न पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं. इसे पेय पदार्थ, पशु आहार और औद्योगिक उत्पादन में भी उपयोग किया जाता हैं. जौ का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है. यह वजन नियंत्रित करने में सहायक है और कई आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग होता है.
जौ से जुड़े रोचक तथ्य
- जौ को “हिमालयी क्षेत्रों का प्रमुख अनाज” भी कहा जाता है क्योंकि यह ऊँचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में अच्छी तरह उगता है.
- विश्व स्तर पर रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख जौ उत्पादक देश हैं.
- भारत में जौ की हस्कलेस किस्में (Hull-less barley) विकसित की गई हैं, जो अधिक पोषक और आसानी से पचने योग्य होती हैं.
- यह फसल गेहूँ की तुलना में कम लागत और कम समय में तैयार हो जाती है (आमतौर पर 120-140 दिनों में).
- 100 ग्राम जौ में लगभग 354 किलो कैलोरी ऊर्जा, 73 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 12 ग्राम प्रोटीन, 17 ग्राम फाइबर और प्रचुर मात्र में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं.
- जौ को हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा नियंत्रण में लाभकारी माना जाता है.
दलहन (Pulses)
यह रबी व खरीफ की फसलें हैं. दालों के अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, खेसारी आदि को शामिल किया जाता है. दालों का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता व मृदा संबंधी दशाओं में किया जाता है. इनके उत्पादन हेतु कम नमी की आवश्यकता होती है अर्थात् इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है.
दालें फलीदार परिवार के पौधों के खाद्य बीज हैं. ये फली में उगती हैं और विभिन्न आकार, प्रकार और रंगों में पाई जाती हैं. संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) 11 प्रकार की दालों को मान्यता देता है, जिनमें सूखी फलियाँ, सूखी चौड़ी फलियाँ, सूखी मटर, छोले, लोबिया, अरहर, मसूर, बम्बारा फलियाँ, वेच और ल्यूपिन शामिल हैं.
दालें वैश्विक आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं. इनके नाइट्रोजन-फिक्सिंग गुण स्वस्थ मिट्टी और जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान करते हैं. भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%), और आयातक (14%) है. भारत में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार के मध्य पठारी भागों तथा उत्तर-पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है.
नोट: अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है.
तिलहन (Oilseeds)
भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है. यह मुख्यतः खरीफ व रबी दोनों मौसमों की फसल है. तिलहन के अंतर्गत सरसों (प्रजाति-वरुणा, पीतांबरी, पूसा बोल्ड, जयकिसान), सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली, बिनौला, अलसी, तिल आदि उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं. मालवा पठार, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं.
देश की तिलहन की फसलों में मूंगफली सर्वप्रमुख है. मूंगफली की कृषि के लिये 30-60 सेमी. वार्षिक वर्षा तथा 15°C-25°C तापमान की आवश्यकता होती है. ‘पेगिंग’ मूंगफली की फसल हेतु एक लाभकारी प्रक्रिया है एवं ‘कौशल’ इसकी उन्नत प्रजाति है. गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं.
भारत में कुल तिलहन उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा मूंगफली, सोयाबीन और सरसों से प्राप्त होता है. भारत सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन (National Mission on Oilseeds and Oil Palm) योजना शुरू की हैं. इसका उद्देश्य देश में खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना हैं.
तिलहन के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र
- मालवा पठार (मध्य प्रदेश) – सोयाबीन और सरसों का मुख्य क्षेत्र.
- मराठवाड़ा और विदर्भ (महाराष्ट्र) – मूंगफली और सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी.
- गुजरात और राजस्थान के शुष्क क्षेत्र – मूंगफली, तिल और सरसों की खेती.
- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश – मूंगफली और सूरजमुखी का मुख्य केंद्र.
- केरल और कर्नाटक का तटीय क्षेत्र – नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध.
प्रमुख तिलहन फसलें और उनके तथ्य
1. सरसों (Mustard/Rapeseed): वरुणा, पीतांबरी, पूसा बोल्ड, जयकिसान आदि इसके प्रमुख प्रजातियाँ हैं. इसमें शीतोष्ण जलवायु में अच्छी वृद्धि होती है. इसके लिए 20°C से 25°C तापमान उपयुक्त है. इसके मुख्यतः राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है. इसका उपयोग खाद्य तेल, अचार, पशु चारा और आयुर्वेदिक औषधियों में होता हैं.
2. मूंगफली (Groundnut): यह भारत की सबसे प्रमुख तिलहन फसल है. इसके लिए 30-60 सेमी. वर्ष और 15°C-25°C तापमान की जरूरत होती है. इसका उपयोग खाद्य तेल, मूंगफली बटर, चॉकलेट, पशु चारा और बायोडीजल उत्पादन में होता है.
3. सोयाबीन (Soybean) यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पाद है. यह प्रोटीन से भरपूर होता है. इसके मुख्यतः मध्य प्रदेश (सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक), महाराष्ट्र, राजस्थान में उगाया जाता है. इससे सोया तेल, सोया दूध, सोया चंक्स, पशु आहार और औद्योगिक प्रोटीन उत्पाद बनाए जाते है.
4. सूरजमुखी (Sunflower): सूरजमुखी का तेल कोलेस्ट्रॉल-फ्री होता है, जो हृदय के लिए लाभकारी है. इसेक उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं.
5. नारियल (Coconut): केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में उपजाए जाते है. नारियल तेल, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, बायोफ्यूल और खाद्य उद्योग में इसका उपयोग होता है.
6. अलसी (Linseed/Flaxseed): अलसी का तेल (Flaxseed oil) ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है. इसके मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार हैं.
7. तिल (Sesame): तिल का तेल एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-E से भरपूर है. इक मुख्य क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं.
चाय (Tea)
चाय ‘चीनी’ मूल का पौधा है, भारत में इसका रोपण अंग्रेज़ों ने आरंभ किया. चाय एक प्रकार की रोपड़ या बागानी फसल का उदाहरण है. इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस एवं जीवांश युक्त लैटेराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवाँ क्षेत्रों या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है. इसके लिये 24°C-30°C तापमान व 150-250 सेमी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है. चाय की फसल को उगाने हेतु वर्षभर उष्णार्द्र तथा पालारहित जलवायु की आवश्यकता होती है.
चाय की मुख्यतः दो किस्में भारत में उपजाई जाती हैं- 1. बोहिया या चीनी, 2. असामिका या असमी. चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी व केरल प्रमुख हैं. चाय एक श्रम आधारित फसल है, अतः इसके लिये सस्ता व कुशल श्रम एक अनिवार्य आवश्यकता है.
नोट: भारतीय चाय बोर्ड ‘कोलकाता‘ में स्थित है.
कपास (Cotton)
कपास एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है. इसके बीजों का उपयोग वनस्पति तेल उद्योग और दुधारू पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है. भारत के उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्र कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक व मध्य प्रदेश में इसकी कृषि की जाती है. कपास भारत का देशज पौधा है. ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है. भारत विश्व का ऐसा पहला देश है, जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित की गई है.
काली मिट्टी कपास के उत्पादन हेतु उपयुक्त है. कपास के रेशों बीज से प्राप्त होते हैं. कपास को ‘सफेद सोना’ (White Gold) भी कहा जाता है. इस फसल को उगाने हेतु उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई तथा तेज धूप की आवश्यकता होती है. विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है.
भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कपास की सभी चार प्रजातियों की खेती होती है. ये प्रजातियाँ हैं-
- गोसिपियम आर्बोरियम (एशियाई कपास)
- गोसिपियम हर्बेशियम (एशियाई कपास)
- गोसिपियम बारबेडेंस (मिस्र का कपास)
- गोसिपियम हिर्सुटम (अमेरिकी अपलैंड कपास)
गन्ना (Sugarcane)
यह एक उष्ण एवं उष्णकटिबंधीय फसल है. गन्ने के उत्पादन के लिये 21°C–27°C तापमान तथा 75-150 सेमी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है. गन्ना एक नकदी फसल है. इसके लिये दोमट व काली मिट्टी उपयोगी है. यह सर्वाधिक सिंचित फसल है. इसमें श्रमिकों व उर्वरकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है. गन्ना भारत की स्वदेशी फसल है और बांस परिवार से संबंधित है. गाढ़े गन्ने के रस का उपयोग चीनी, गुड़ और खांडसारी बनाने के लिए किया जाता है.
भारत में उत्पादित गन्ने का दो-तिहाई हिस्सा गुड़ और खान साड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि शेष चीनी कारखानों में संसाधित किया जाता है. चीनी उद्योग के उप-उत्पादों में गुड़, खोई और प्रेसमड शामिल हैं. शीरा (मोलासेस) इथेनॉल के निर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, जो कुछ पेट्रोलियम उत्पादों का कुशल विकल्प भी है.
भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि प्रमुख हैं. यह एक प्रकार की भार हासी फसल है, अतः शर्करा का क्षय कम-से-कम हो इसलिये गन्ना मिलों की स्थापना उत्पादक क्षेत्रों के समीप की जाती है.
गन्ना पूरे वर्ष की फसल है. गन्ने की बुआई, जनवरी से अप्रैल तक तथा कटाई व पेराई अक्टूबर से अप्रैल तक होती है. गन्ने की कृषि के लिये ‘पाला’ हानिकारक होता है. भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयंबुत्तूर (तमिलनाडु) में किया जा रहा है. इसके लिये 1912 में ‘गन्ना प्रजनन संस्थान‘ की स्थापना की गई थी. दक्षिण भारत में गन्ने की कृषि की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण समकारी आर्द्रता युक्त जलवायु, लंबी पेराई का मौसम, सहकारिता की प्रवृत्ति इत्यादि है.
कहवा (Coffee)
कहवा की खेती के लिये उष्ण-आर्द्र जलवायु, 16°C-28°C तापमान, 150-250 सेमी. वार्षिक वर्षा, गहरी व भुरभुरी (Friable) दोमट या लावा निर्मित मिट्टी व ढलानयुक्त भूमि की आवश्यकता होती है. कॉफी का प्रवर्द्धन कहवा के बीजों के द्वारा होता है. भारत में कहवा की दो किस्में ‘अरेबिका’ तथा ‘रोबस्टा’ उगाई जाती हैं. ‘रोबस्टा’ किस्म की कॉफी का उत्पादन भारत में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है. कॉफी बोर्ड भारत के ‘बंगलूरू’ में स्थित है.
भारत में कहवा की खेती की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी. सूफी संत बाबा बूदान यमन से कॉफी के सात बीज लाए और इन्हें कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित बाबा बूदान पहाड़ियों में लगाया. यहीं से भारत में कॉफी उत्पादन का आरंभ हुआ.
भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कॉफी छायादार पेड़ों की छाया में उगाई जाती है, जिससे इसका स्वाद और गुणवत्ता बेहतर होती है. भारत कॉफी उत्पादन में विश्व में 7वें से 8वें स्थान पर है. भारत में मॉन्सून मालाबार कॉफी (Monsoon Malabar Coffee) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी खास पहचान रखती है.
वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों के समीप कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में प्रमुख रूप से किया जा रहा है. भारत वैश्विक स्तर पर लगभग 3.14% कॉफी का उत्पादन करता है, जबकि निर्यात में देश का हिस्सा 70-80% तक है. भारत छठा सबसे बड़ा उत्पादक और पाँचवा सबसे बड़ा निर्यातक है.
जूट (Jute)
जूट (Jute) भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशेदार फसल है. इस श्रेणी में कपास के बाद सबसे अधिक उत्पादन वाली फसल मानी जाती है. यह सस्ता, कोमल, मजबूत और पर्यावरण-अनुकूल प्राकृतिक रेशा है. इसलिए इसे ‘भारत का स्वर्णिम तंतु’ (Golden Fibre of India) कहा जाता है. जूट का उपयोग मुख्य रूप से बोरियों, रस्सियों, कालीनों, गलीचों, तिरपालों, पैकिंग सामग्री और गत्तों के निर्माण में किया जाता है.
हालांकि, सिंथेटिक रेशों (Polypropylene जैसे प्लास्टिक आधारित रेशे) के बढ़ते उपयोग ने जूट उद्योग की मांग को प्रभावित किया. 20वीं शताब्दी के अंत में जूट उद्योग को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. लेकिन आज पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की मांग बढ़ने से जूट उद्योग में पुनरुत्थान देखा जा रहा है.
जूट आमतौर पर फरवरी में बोया जाता है और अक्टूबर (4-6 महीने की अवधि) में काटा जाता है. जूट उत्पादन के लिये उष्ण एवं उच्च आर्द्र जलवायु, नवीन जलोढ़ दोमट मिट्टी (हल्की रेतीली या चिकनी), उच्च तापमान (25°C-30°C), 160-200 सेमी. वार्षिक वर्षा तथा सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है. यह पश्चिम बंगाल (देश का लगभग 70-75%), बिहार, असम तथा इससे लगे हुए पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है.
कपास की तरह, जूट भी मिट्टी की उर्वरता को तेजी से खत्म कर देता है. इसलिए नदियों से आने वाले गाद से भरे बाढ़ के पानी से हर साल मिट्टी को फिर से भरना पड़ता है. यह 100% बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण-अनुकूल है. सरकार द्वारा जूट पैकेजिंग अधिनियम, 1987 (Jute Packaging Material Act) और राष्ट्रीय जूट नीति के माध्यम से जूट उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है.
भारत का फसल मानचित्र (Crop Map of India Hindi)

प्रमुख मसाले (Major Spices)
प्राचीन काल से ही भारत अपने उच्च गुणवत्ता युक्त मसालों के उत्पादन हेतु विख्यात है. यही कारण है कि भारत को मसालों की धरती माना जाता है. ध्यातव्य है कि भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है. भारत द्वारा यूरोप और मध्यपूर्व के अधिकांश देशों को बड़े पैमाने पर मसालों का निर्यात किया जाता है.
इलायची (Cardamom)
इलायची (Cardamom) को ‘मसालों की रानी‘ (Queen of Spices) कहा जाता है. इसका स्वाद और सुगंध इसे विश्व के सबसे लोकप्रिय और महंगे मसालों में शामिल करता है. इलायची उत्पादन में भारत ग्वाटेमाला के पश्चात् द्वितीय स्थान पर है. इसका प्रयोग भोजन, दवाओं के साथ ही इत्र आदि में भी किया जाता है. इलायची उत्पादन हेतु 14°C-32°C तापमान तथा 150 सेमी. से अधिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है. कैप्सूल रॉट और थ्रिप्स की समस्या से इसके फसल प्रभावित होते है.
भारत में इलायची की खेती लगभग 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है. इसका उपज मुख्यतः पश्चिमी घाट के क्षेत्र में होता है. केरल (लगभग 60% योगदान), कर्नाटक और तमिलनाडु इलायची के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं. छोटी इलायची (Green Cardamom) भारत में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली किस्म हैं. काली इलायची (Black Cardamom) मुख्य रूप से सिक्किम, असम और भूटान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है. ICRI (Indian Cardamom Research Institute) इलायची की उन्नत किस्में और खेती तकनीक विकसित करता है.
लाल मिर्च (Red Chilli)
लाल मिर्च को वाणिज्यिक रूप से महत्त्वपूर्ण मसालों में शुमार किया जाता है तथा पूरे विश्व में बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है. इसे ‘अद्भुत मसाला’ (Wonder Spice) के नाम से भी जाना जाता है. इसके कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा भाग भारत में उपजाया जाता है. भारत में लाल मिर्च की खेती लगभग 8-9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है.
10°C-30℃ का तापमान, 60-120 सेमी. वर्षा और लाल दोमट मिट्टी इसके लिये उपयुक्त होती है. तेलंगाना (सबसे बड़ा उत्पादक), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं. थ्रिप्स, लीफ कर्ल वायरस से उत्पादन में गिरावट हो सकती है.
गंटूर संगीवर (Guntur Sannam) अधिक तीखापन और लाल रंग, बैदगी (Byadgi) कम तीखापन लेकिन चमकदार लाल रंग, और रामनाथपुरम (Tamil Nadu) मध्यम तीखापन और सुगंध के लिए मशहूर है. असम और नागालैंड में उपजाई जाने वाली नागा जोलोकिया (Bhut Jolokia) अत्यंत तीखी मिर्च है. यह विश्व की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है.
लौंग (Clove)
यह मूल रूप से इंडोनेशिया में उत्पादित मसाला है. किंतु वर्तमान में ज़ांज़िबार, मेडागास्कर, मलेशिया, श्रीलंका और भारत में भी उपजाया जाता है. इसके उत्पादन हेतु 25°C-35°C तापमान सहित 150 सेमी. से अधिक वर्षा आदर्श होती है. केरल और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं. एंटीबायोटिक गुणों से युक्त होने के कारण इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है.
काली मिर्च (Black Pepper)
काली मिर्च (Black Pepper) को ‘मसालों का राजा‘ (King of Spices) कहा जाता है. यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा व्यापार किया जाने वाला मसाला है. भारत में केरल (90% योगदान) काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक राज्य है. इसके अतिरिक्त, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी छोटे स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है.
ऐतिहासिक रूप से भारत का पश्चिमी घाट की मलाबार तट (Malabar Coast) काली मिर्च का उद्गम स्थल माना जाता है. प्राचीन समय में काली मिर्च का उपयोग मुद्रा (Currency) के रूप में भी किया जाता था. यह मसाला व्यापार का मुख्य केंद्र रही है.
इसे वर्तमान में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड, चीन, ब्राज़ील, कंबोडिया आदि देशों में भी उत्पादित किया जाता है. इसके उत्पादन हेतु 10°C-40°C तापमान तथा 125-200 सेमी. वर्षा सर्वोत्तम होती है. फाइटोफ्थोरा (Phytophthora foot rot) रोग और कीटों का प्रकोप से इसे बचाना होता है.
काली मिर्च के अधपके हरे फलों (ड्रूप्स) को तोड़ा जाता है. फिर इसे धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है. धूप से इसके छिलके का रंग गहरा काला हो जाता है. परिरक्षक गुणों से युक्त होने के कारण इसे अचार, मीट पैकिंग आदि के साथ औषधीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है.इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण और पाचन क्रिया सुधारने में सहायक होता है. यह सर्दी, खांसी, गले की खराश में राहत देता है.
हल्दी (Turmeric)
इसे “स्वर्ण मसाला” (Golden Spice) कहा जाता है. हल्दी मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण-पूर्व एशिया का पौधा है. यह उष्णकटिबंधीय फसल है. इसे लाल मृदा वाले वर्षा सिंचित एवं सिंचाई वाले क्षेत्रों में उपजाया जाता है. इसे जलभराव युक्त क्षेत्र में उत्पादित नहीं किया जा सकता. हल्दी की जड़ों को उबालकर तथा सुखाकर बाज़ार में बेचने हेतु तैयार किया जाता है.
भारत वैश्विक उत्पादन का लगभग 75-80% योगदान देता है और निर्यात में प्रथम स्थान रखता है. देश के लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है. देश के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का योगदान लगभग 40-45% है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एवं कर्नाटक भी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं. इसके पारंपरिक किस्मों को लीफ ब्लॉटच और राइज़ोम रॉट का सामना करना पड़ता है. इसका उत्पाद में नमी के कारण फफूंद की समस्या हो सकती है.
इसे मसाले, अचार, करी पाउडर, बेकरी और पेय पदार्थों में रंग व स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता हैं. इसमें पाया जाने वाला करक्यूमिन (Curcumin) सूजनरोधी, जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते है. यह घाव भरने और त्वचा रोग में भी उपयोगी है.
दालचीनी (Cinnamon)
इसकी व्युत्पत्ति श्रीलंका की मध्य पहाड़ियों से हुई थी. भारत में नीलगिरी और मालाबार पहाड़ी क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है. 20°C-30°C तापमान एवं 120-250 सेमी. वर्षा इसके उत्पादन हेतु आदर्श दशाएँ हैं. वस्तुतः यह ‘सिनामोमम वीरम’ नामक वृक्ष की छाल होती है जिसे सुखाकर भोजन, औषधि निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है. भारत का दालचीनी उत्पादन वैश्विक स्तर पर सीमित है. दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक श्रीलंका (लगभग 80-85% आपूर्ति) है.
विभिन्न फसलें व उन पर लगने वाले रोग (Different crops and their diseases)
सभी प्रमुख फसलों तथा उन पर लगने वाले रोगों की सूची इस प्राकार हैं:
| फसल | प्रमुख रोग | रोग का कारण/रोगाणु |
| गेहूँ | अनावृत कंडुआ (Loose Smut), सेहू (Earcockel), रस्ट (Rust), गेरुई या रतुआ | Ustilago tritici, Tilletia caries, Puccinia spp. |
| धान | खैरा (जस्ते की कमी से), पत्तियों पर भूरा धब्बा (Brown Spot), शीथ झुलसा (Sheath Blight) | जिंक की कमी, Helminthosporium oryzae, Rhizoctonia solani |
| मक्का | तुलसिता रोग (Downy Mildew), पत्तियों पर झुलसा रोग (Leaf Blight) | Peronosclerospora sorghi, Helminthosporium turcicum |
| मूंगफली | टिक्का रोग (Tikka), ड्राईफ्रूट रोट (Dry Fruit Rot) | Cercospora arachidicola, Aspergillus niger |
| सोयाबीन | पीला चित्रण रोग (Yellow Mosaic Virus) | पीला चित्रण विषाणु (Transmitted by whitefly) |
| बाजरा | अरगट (Ergot), हरित बाली (Green Ear), कंडुआ (Smut) | Claviceps fusiformis, फाइटोप्लाज्मा संक्रमण, Sphacelotheca sorghi |
| गन्ना | रेड रॉट (Red Rot) | Colletotrichum falcatum |
| ज्वार | कंडुआ (Smut) | Sphacelotheca cruenta |
| हल्दी | राइज़ोम रॉट (Rhizome Rot), लीफ स्पॉट (Leaf Spot), लीफ ब्लॉटच (Leaf Blotch) | Pythium aphanidermatum, Colletotrichum capsici, Taphrina maculans |
| इलायची | मोज़ेक रोग (Mosaic Virus), फूटी कैप्सूल रोग (Fusarium Capsule Rot) | Cardamom mosaic virus (CdMV), Fusarium oxysporum |
| काली मिर्च | फुट रॉट / क्विक वील्ट (Foot Rot), स्लो डिकलाइन (Slow Decline), एन्थ्रेक्नोज़ (Anthracnose), पिल्लोडी रोग (Phyllody) | Phytophthora capsici, Fusarium spp., Colletotrichum capsici, फाइटोप्लाज्मा |
| दालचीनी | लीफ स्पॉट (Leaf Spot), कांकर (Canker), ग्रे ब्लाइट (Grey Blight) | Colletotrichum gloeosporioides, Phytophthora cinnamomi, Pestalotia palmarum |
भारत की प्रमुख फसलें (2024‑25), उत्पादन व अग्रणी राज्य (Major Crops of India (2024‑25), Production and Leading States)
| फसल / श्रेणी | अनुमानित उत्पादन | अग्रणी उत्पादक राज्यों की सूची |
| कुल खाद्यान्न | ≈ 3,539.6 लाख मीट्रिक टन (MMT) | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब (2017-18 में) |
| चावल (Rice) | 1,364.37 LMT (खरीफ + रबी) | पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार (Desagri, USDA, Indiastat, Press Information Bureau) |
| गेहूँ (Wheat) | 1,154.30 LMT | उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान (Press Information Bureau) |
| गन्ना (Sugarcane) | 4,501.16 LMT | उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक (USDA) |
| मक्का (Maize) | 372.49 LMT (खरीफ + रबी) | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक (USDA) |
| ज्वार + बाजरा (Nutri cereals) | 560.28 LMT | महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश (USDA) |
| कुल तिलहन (Oilseeds) | 416.69 LMT | मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र |
| सोयाबीन (Soybean) | 151.32 LMT | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात (USDA) |
| मूंगफली (Groundnut) | 113.13 LMT | गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र (USDA) |
| रेपसीड एवं सरसों | 128.73 LMT | राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात |
| कपास (Cotton) | ≈ 24,000 लाख बॅल्स (170 किग्रा प्रति बॅल) | गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना (USDA) |
| जूट एवं मेस्ता | जूट: 84.33 लाख बॅल; मेस्ता: 3.15 लाख | पश्चिम बंगाल, बिहार, असम (जूट); मेस्ता – उत्तर पूर्वी राज्य |
| कॉफी (Coffee) | ~360–380 हजार टन (~6.0–6.2 मिलियन बैग) | कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु |
| चाय (Tea) | ~1,285 हजार टन (2024 में ~7.8% गिरावट) | पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला |
| अरहर (Tur / Pigeon Pea) | 35.11 LMT | महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश |
| चना (Gram / Chickpea) | 115.35 LMT | राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा |
| कुल दालें (Pulses) | ~ 40–45 LMT कुल (अरहर, चना, मसूर अन्य मिलाकर) | प्रमुख उत्पादक: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश |
| सूरजमुखी (Sunflower) | तेलहन में सम्मिलित; सटीक आंकड़ा नहीं उपलब्ध | महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश |
| नारियल, रबड़, फल, सब्जी | मंत्रालय की AE में संख्या नहीं; विशिष्ट Horticulture रिपोर्ट में होता है | नारियल: केरल, तमिलनाडु; रबड़: केरला, तामिलनाडु; फल– सब्जी: महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल |
विश्व के प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक एवं निर्यातक राष्ट्र
| फसल | उत्पादक राष्ट्र | निर्यातक राष्ट्र |
| चावल | चीन, भारत, इंडोनेशिया | भारत, थाईलैंड, यू.एस.ए. |
| चाय | चीन, भारत, केन्या | चीन, भारत, श्रीलंका |
| कॉफी | ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया | ब्राज़ील, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड |
| रबर | थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम | थाईलैंड, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट |
| गेहूं | चीन, भारत, रूस | रूस, यू.एस.ए., कनाडा |
विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र
| फसल | देश | उत्पादक क्षेत्र |
| चावल | भारत | असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि. |
| चीन | जेचुआन क्षेत्र, यांग्त्सी व सिक्यांग नदी घाटी क्षेत्र इत्यादि. | |
| इंडोनेशिया | सुलावेसी (सेलेंस), सुमात्रा, जावा इत्यादि. | |
| गेहूं | यू.एस.ए. | डकोटा, मोंटाना, मिन्नीसोटा, कंसास, ओक्लाहोमा, कैलिफोर्निया इत्यादि. |
| रूस | कैस्पियन सागर के तटीय क्षेत्र, साइबेरिया का स्टेपीज क्षेत्र इत्यादि. | |
| चीन | मेकोंग, यांग्त्सी, सीक्यांग नदी घाटी आदि. | |
| मक्का | यू.एस.ए. | ओहियो से नेब्रास्का तथा, से मिन्नसोटा, से मिसौरी (मक्का पेटी) |
| ब्राज़ील | साओ पोलो, रियोग्रांडे आदि. | |
| चीन | जेचुआन बेसिन, सीक्यांग घाटी आदि. | |
| चाय | श्रीलंका | कैंडी बेसिन |
| केन्या | लीमूरो क्षेत्र | |
| चीन | हुआंग्लो घाटी, यांगत्सी घाटी, कीहो घाटी आदि. | |
| कपास | यू.एस.ए. | अलाबामा, टेनेसी, उत्तरी व दक्षिणी कैरोलिना, मिसीसिपी घाटी क्षेत्र आदि. |
इन्हें भी पढ़ें: