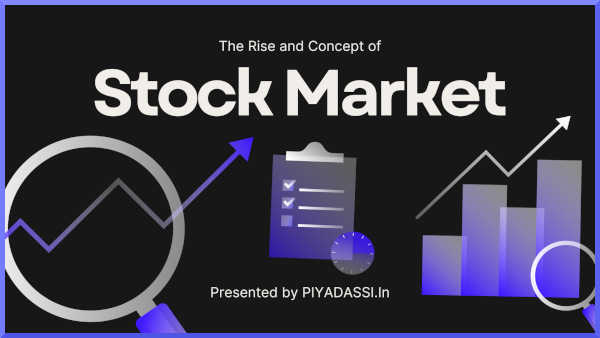श्वेत क्रांति को ‘ऑपरेशन फ्लड’ के नाम से भी जाना जाता है. यह भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और डेयरी उद्योग को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था. यह पहल भारत को डेयरी उत्पादों की कमी वाले देश से वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने पर केंद्रित थी. 1970 में शुरू हुई इस क्रांति ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया.
इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1998 में आया, जब भारत ने दूध उत्पादन के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया. यह एक सामाजिक-आर्थिक कायापलट का प्रतीक थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया. डॉ. वर्गीज कुरियन को “भारत का मिल्कमैन” और “श्वेत क्रांति के जनक” कहा जाता है. उन्हें 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार और 1965, 1966 और 1999 में क्रमशः पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.
श्वेत क्रांति का शुरुआत
श्वेत क्रांति की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 13 जनवरी, 1970 को हुई थी. यह पहल भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा की गई थी. एनडीडीबी की स्थापना 1965 में हुई थी. NDDB का प्राथमिक उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी विकास को व्यवस्थित करना था.
इस क्रांति के पीछे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉ. वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें ‘भारत में श्वेत क्रांति का जनक’ और ‘मिल्क मैन ऑफ इंडिया’ के रूप में जाना जाता है. उनकी जयंती, 26 नवंबर, को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है. डॉ. कुरियन ने भारत की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इस कार्यक्रम की सफलता की एक प्रमुख आधार बनी.
अमूल की जड़ें गुजरात के खेड़ा जिले में 1946 में सरदार पटेल की सलाह पर त्रिभुवन दास पटेल द्वारा स्थापित “खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादक यूनियन” में निहित हैं. यह प्रारंभिक प्रयास बाद में अमूल के रूप में विकसित हुआ. त्रिभुवनदास पटेल का प्रारंभिक कार्य एक मजबूत सहकारी नींव बनाने में महत्वपूर्ण था. इसी पर डॉ. कुरियन ने ‘ऑपरेशन फ्लड’ की विशाल संरचना का निर्माण किया. यह एक सफल बॉटम-अप मॉडल का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार था.
श्वेत क्रांति के उद्देश्य
श्वेत क्रांति के कई बहुआयामी उद्देश्य थे. इसका लक्ष्य केवल दूध उत्पादन बढ़ाना ही नहीं. इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में सुधार लाना भी था. इसके प्रमुख उद्देश्यों में दुग्ध उत्पादकों के सहकारी संघों की स्थापना करके उन्हें सीधे बाजार से जोड़ना शामिल था, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके और किसानों व उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शी व लाभकारी संबंध स्थापित हो सकें. पशु आहार (cattle feed) की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था.
ऑपरेशन फ्लड के प्राथमिक उद्देश्यों में आगामी पाँच वर्षों में दूध की खरीद को 50% तक बढ़ाना और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की पहुंच का विस्तार करना शामिल था. इसका एक दीर्घकालिक लक्ष्य 2029 तक प्रतिदिन की दूध खरीद को 1,000 लाख किलोग्राम तक पहुँचाना भी था. इसके अतिरिक्त, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि (“दूध की बाढ़” लाना), ग्रामीण आय में सुधार करना, और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना था. स्वदेशी पशु नस्लों का संरक्षण और विकास भी राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD 2.0) के तहत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था.
ऑपरेशन फ्लड के चरण
ऑपरेशन फ्लड का कार्यान्वयन एक सुनियोजित, चरणबद्ध रणनीति के तहत किया गया था, जिसे तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया:
चरण I (1970-1980)
इस प्रारंभिक चरण का वित्तपोषण विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत यूरोपियन संघ (EEC) द्वारा उपहार में मिले स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री से किया गया. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने इस कार्यक्रम की विस्तृत योजना बनाई और EEC के साथ सहायता की शर्तों पर बातचीत की.
प्रथम चरण के दौरान, ऑपरेशन फ्लड ने देश के 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों को भारत के चार मुख्य महानगरों – दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के उपभोक्ताओं से जोड़ा. यह महानगरों पर ध्यान केंद्रित करने की एक रणनीतिक बाजार रणनीति थी,. इससे बड़े उपभोक्ता आधार तक पहुंच सुनिश्चित हुई और कार्यक्रम को प्रारंभिक सफलता मिला.
चरण II (1981-1985)
इस चरण में कार्यक्रम का विस्तार हुआ. प्रमुख दुग्ध केंद्रों की संख्या 18 से बढ़कर 136 हो गई.परिणामस्वरूप, दूध 290 से अधिक शहरों और कस्बों के बाजारों में उपलब्ध होने लगा. 1985 के अंत तक, 43,000 आत्मनिर्भर ग्राम दुग्ध सहकारी समितियाँ स्थापित हो चुकी थीं. इससे 42.50 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक जुड़े थे.
इस चरण में घरेलू दूध पाउडर का उत्पादन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा. यह योजना से पहले के 22,000 टन से बढ़कर 1989 तक 1,40,000 टन हो गया. यह वृद्धि मुख्य रूप से ऑपरेशन फ्लड के दौरान स्थापित की गई नई डेयरियों के कारण हुई. इस चरण में EEC से प्राप्त उपहारों और विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों ने भारत को डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में सहायता की.
चरण III (1985-1996)
तीसरा चरण डेयरी सहकारी समितियों को अधिक मात्रा में दूध की खरीद और बिक्री के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित था. सहकारी सदस्यों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों को सघन किया गया. साथ ही प्राथमिक पशु-स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ, पशु आहार और कृत्रिम गर्भाधान सुविधाओं का भी विस्तार किया गया.
इस दौरान 30,000 नई डेयरी सहकारी समितियाँ जोड़ी गईं. महिला दुग्ध सहकारी समितियों और महिला सदस्यों की संख्या में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई. 1988-89 तक दुग्ध शेडों की संख्या 173 तक पहुँच गई. इस चरण में पशु स्वास्थ्य और पशु पोषण में अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया. इस प्रयास से थिलेरियोसिस के टीके, बाईपास प्रोटीन आहार और यूरिया-सीरा खनिज ब्लॉक जैसी नवीन खोजों द्वारा दुधारू पशुओं का उत्पादकता बढ़ा.
सहकारी समिति और ‘आनंद मॉडल’
ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ थीं. ये समितियाँ उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती थीं, उन्हें आवश्यक जानकारी और सेवाएँ प्रदान करती थीं, और उन्हें आधुनिक प्रबंधन व प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करती थीं. सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों में सामाजिक एकता को भी बढ़ावा मिला.
गुजरात के आणंद में स्थित अमूल (आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ) सहकारी आंदोलन की सफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. अमूल मॉडल से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिली. इस तरह उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हुआ.
अमूल का औपचारिक पंजीकरण दिसंबर 1946 में आणंद जिले के दुग्ध उत्पादकों के लिये समुचित बाज़ार उपलब्ध करवाने हेतु हुआ था. सन् 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आणंद का दौरा किया. उन्होंने दुग्ध उत्पादकों और व्यापारियों की समस्याओं का अवलोकन किया. परिणामतः 1965 में यहाँ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना की गई. इसने ही आगे चलकर 1969-70 में ‘ऑपरेशन फ्लड’ अथवा ‘श्वेत क्रांति’ की शुरुआत की.
श्वेत क्रांति की उपलब्धियाँ और प्रभाव
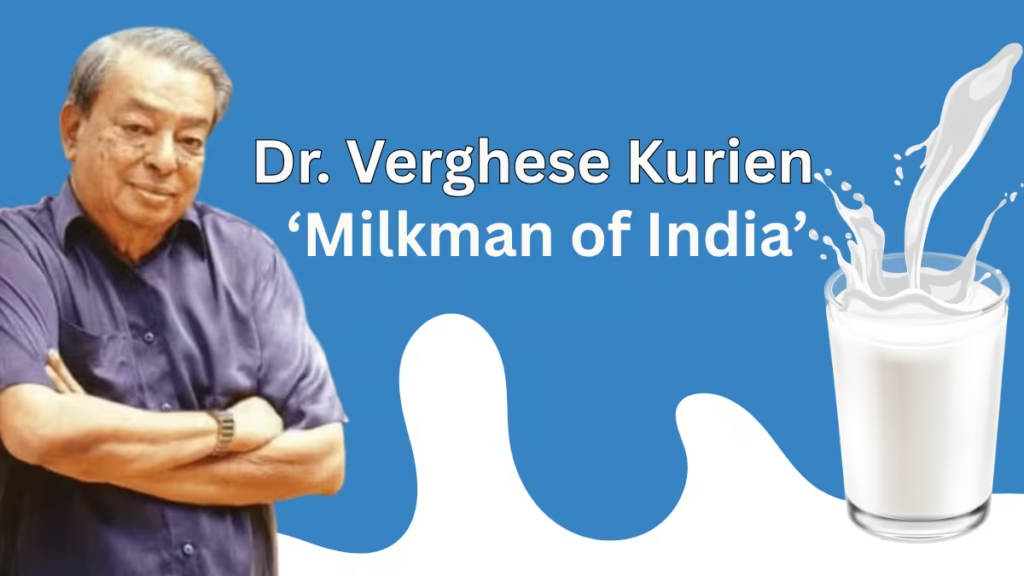
दूध उत्पादन में वृद्धि
श्वेत क्रांति का सबसे प्रत्यक्ष और उल्लेखनीय प्रभाव भारत के दूध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि थी. इस क्रांति से भारत 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया. स्वतंत्रता-पूर्व की तुलना में दूध उत्पादन दस गुना से अधिक बढ़ गया है. हाल के आंकड़ों के अनुसार, भारत का दूध उत्पादन 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.2 मिलियन टन हो गया है. इस प्रकार पिछले 10 वर्षों में 63.56% की जोरदार वृद्धि हुई है. यह वृद्धि दर वैश्विक औसत (2% प्रति वर्ष) से काफी अधिक है. भारत में वार्षिक वृद्धि दर 5.7% है.
भारत 1998 से दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक देश है. अब भारत में दुनिया के कुल दूध का 25 प्रतिशत उत्पादन होता है . 2023-24 में, औसत भारतीय को प्रतिदिन 471 ग्राम से अधिक दूध मिलेगा, जो विश्व औसत 322 ग्राम से कहीं अधिक है.
ग्रामीण आय और रोजगार
ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ने लाखों ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार और नियमित आय के अवसर पैदा किए. वर्तमान में, 8 करोड़ से अधिक परिवार सीधे डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. डेयरी क्षेत्र का कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन से प्राप्त होने वाले कुल उत्पादन मूल्य में 2022-23 में 40% का योगदान था. कृषि क्षेत्र की कुल आय में डेयरी क्षेत्र का योगदान 24% है. इसका अनुमानित मूल्य लगभग 10 लाख करोड़ रुपये है.
पशुपालन को संगठित व्यवसाय के रूप में मान्यता
श्वेत क्रांति ने पशुपालन को एक संगठित और व्यावसायिक कार्य के रूप में मान्यता दिलाई. इस क्रांति ने किसानों में विज्ञान-आधारित पशुपालन की समझ को बढ़ाया. उन्हें आधुनिक तकनीकों और प्रथाओं को अपनाने में मदद मिली. आधुनिक दूध दुहने की तकनीकें और अनुकूलित पशु आहार को बढ़ावा देने से उत्पादकता में वृद्धि हुई. इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ ही किसानों को लाभदायक व्यवसाय भी प्राप्त हुआ.
महिला सशक्तिकरण
भारत के डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का 70% प्रतिनिधित्व है. श्वेत क्रांति 2.0 जैसी पहलों का उद्देश्य महिलाओं को औपचारिक रोजगार में शामिल करके उन्हें और सशक्त बनाना है. ऑपरेशन फ्लड के दौरान भी महिला दुग्ध सहकारी समितियों और महिला सदस्यों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई. यह आर्थिक भागीदारी महिलाओं को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है. साथ ही, घरेलू निर्णय लेने तथा सामुदायिक जीवन में उनकी भूमिका को बढ़ाती है.
सामाजिक प्रभाव
श्वेत क्रांति के दौरान स्थापित सहकारी समितियों ने ग्रामीण समुदायों में सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया. इन सहकारी संरचनाओं ने किसानों को एक साथ आने, संसाधनों को साझा करने और सामूहिक रूप से बाजार तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान किया. इसके अतिरिक्त, इस क्रांति ने ग्रामीण भारत में शीतल भंडारण श्रृंखला (cold storage chain) और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को उत्प्रेरित किया. दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण के लिए आवश्यक सुविधाओं के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हुआ.
पोषण सुरक्षा
दूध की उपलब्धता बढ़ने से गरीब और कुपोषित बच्चों को सबसे अधिक लाभ मिला. उन्हें पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में मदद मिली. दूध को एक पौष्टिक भोजन और प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत माना जाता है. यह व्यापक पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र और सुलभ समाधान प्रदान करता है.
आत्मनिर्भरता
श्वेत क्रांति के कारण भारत दूध की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर देश बन गया है.दूध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर निर्भरता में काफी कमी आई है. यह आत्मनिर्भरता आर्थिक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से रणनीतिक महत्व का है.
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
श्वेत क्रांति की सफलता के बावजूद, इस आंदोलन को कई चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है, जो इसके दीर्घकालिक प्रभावों और भविष्य की रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण हैं.
क्षेत्रीय असमानताएँ
श्वेत क्रांति के लाभ पूरे देश में समान रूप से वितरित नहीं हुए. उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ राज्यों को उल्लेखनीय लाभ हुआ. वहीं असम और ओडिशा जैसे राज्य पीछे ही रह गए. उदाहरण के लिए, गुजरात में सहकारी समितियों का कवरेज 70% से अधिक है, जबकि असम और ओडिशा में 10% से भी कम है. इस तरह श्वेत क्रांति ने पहले से सम्पन्न राज्यों पश्चिमी राज्यों को और भी सम्पन्न बनाया. लेकिन पूर्वी राज्य पिछड़े ही रह गए.
पर्यावरणीय चिंताएँ
डेयरी फार्मिंग के तीव्र विकास से अत्यधिक चराई, जल प्रदूषण, संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ बढ़ीं. डेयरी पशुओं की आबादी में वृद्धि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और पारिस्थितिक दबाव का कारण बनी.
बुनियादी ढांचे
कई ग्रामीण क्षेत्रों में शीतल भंडारण, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी है. कुछ सहकारी समितियों में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप ने कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कम किया.
आर्थिक अस्थिरता
दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रों में बाजार संतृप्त हो गया. अधिशेष दूध के लिए पर्याप्त प्रसंस्करण और विपणन चैनल न होने से मूल्य में उतार-चढ़ाव की समस्या बढ़ी. इससे किसानों के लिए आर्थिक अस्थिरता बढ़ी.
श्वेत क्रांति 2.0
श्वेत क्रांति की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, भारत ने “श्वेत क्रांति 2.0” शुरू की है, जिसका उद्देश्य 2028 तक भारत को वैश्विक डेयरी नेता बनाना है. यह पहल महिला सशक्तीकरण, कुपोषण उन्मूलन, दूध उत्पादन वृद्धि और डेयरी उद्योग के बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है. इसका मुख्य उद्देश्य हैं:
– दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
– डेयरी उद्योग के बुनियादी ढांचे का विकास
– महिला किसानों का सशक्तीकरण
– डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना
– पिछली क्रांति की चुनौतियों का समाधान करना
लक्ष्य
इसका लक्ष्य 5 वर्ष के अंत तक प्रतिदिन 100 मिलियन किलोग्राम दूध की खरीद प्राप्त करना है. इसके लिए मौजूदा 46,000 सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है. साथ ही 56,000 नई सहकारी समितियाँ स्थापित करने का लक्ष्य है. इसके लिए, 200,000 नई MPAC (बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ) का गठन किया जा रहा है. श्वेत क्रांति 2.0 में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है.
महिला सशक्तिकरण और कुपोषण
श्वेत क्रांति 2.0 में डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की औपचारिक भागीदारी बढ़ाने की योजना है. गुजरात इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ 60,000 करोड़ रुपये का कारोबार महिलाओं के हाथ में है. इसके द्वारा बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए दूध की उपलब्धता बढ़ाने पर भी फोकस है. इससे कुपोषण के खिलाफ संघर्ष को मजबूती मिलेगी.
एकीकरण
यह नई पहल मौजूदा सरकारी योजनाओं जैसे डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) और PACS के कम्प्यूटरीकरण जैसे प्रयासों के साथ जुड़कर काम करेगी. इसके अलावा, किसानों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं. पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत एक नया चरण, NPDD 2.0, भी प्रस्तावित है.
श्वेत क्रांति 2.0 द्वारा गुणवत्ता, पोषण सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और टिकाऊ विकास को भी प्राथमिकता दिया गया है. पिछली क्रांति से सीख लेते हुए यह पहल सहकारी ढांचे को अधिक पारदर्शी, समावेशी और दीर्घकालिक रूप से स्थिर बनाने का प्रयास करती है. यह केवल “दूध की बाढ़” का लक्ष्य नहीं रखती, बल्कि “समावेशी और टिकाऊ डेयरी विकास” की दिशा में भी लक्षित है. इस प्रकार भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक परिपक्व और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है.
भारत और वैश्विक डेयरी मॉडल
भारत के डेयरी क्षेत्र का सहकारी मॉडल वैश्विक स्तर पर अद्वितीय है. अन्य देशों के डेयरी विकास मॉडलों का अध्ययन भारत के रणनीतियों की मजबूती और कमजोरियों को समझने में मदद करता है.
भारत का मॉडल
भारत की डेयरी सहकारी समितियाँ लगभग 2 लाख गाँवों में 2 करोड़ किसानों से प्रतिदिन दूध का संग्रह करती है.संग्रहीत दूध सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचता हैं, जिससे बिचौलियों का भूमिका समाप्त हो जाती है. इससे किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए मूल्य का लगभग 70% से अधिक हिस्सा मिलता है. सहकारी समितियों में यह आँकड़ा 80% तक पहुँच जाता है.
उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री का बड़ा हिस्सा किसान स्वयं नियंत्रित करते हैं. यह उन्हें बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित करता है. भारत का डेयरी क्षेत्र अब तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण से बचा हुआ है. ऐसा सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क और व्यापार अवरोधों के कारण हुआ है. ये अवरोध विकसित देशों के सस्ते डेयरी उत्पादों के आयात को सीमित करते हैं.
इस तरह भारत का डेयरी मॉडल ‘आत्मनिर्भरता’ और ‘स्थानीय नियंत्रण’ पर आधारित है. यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों को भी साधता है. यह अन्य विकासशील देशों के लिए भी उदाहरण है.
डेनमार्क और न्यूजीलैंड का मॉडल
डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने डेयरी विकास के लिए तकनीकी दक्षता और उच्च उत्पादकता आधारित मॉडल अपनाए हैं. डेनमार्क में ‘अरला फूड्स’ जैसी बड़ी कंपनियाँ 61 उत्पादन संयंत्रों के माध्यम से 4.7 बिलियन किलोग्राम दूध का प्रसंस्करण करती हैं. डेनमार्क का डेयरी उत्पादों का वार्षिक निर्यात 1.8 बिलियन यूरो है. यहाँ औसतन प्रति फार्म 210 से 250 गायें होती हैं. प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन का अनुपात 1000 लीटर है.
न्यूजीलैंड में ‘फॉन्टेरा’ जैसी कंपनियाँ वैश्विक बाजार पर केंद्रित उत्पादन करती हैं. यहाँ का डेयरी उद्योग अनुकूल मौसम, समय पर वर्षा और हरे-भरे चरागाहों पर आधारित है और निर्यात-उन्मुख है. अतः यह अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग और कीमतों के उतार-चढ़ाव से काफी प्रभावित होता है.
भारत के पड़ोसी देश
भारत के पड़ोसी देशों में डेयरी क्षेत्र ज्यादातर छोटे किसानों और असंगठित विक्रेताओं के हाथ में है. पाकिस्तान विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. लेकिन 90% से अधिक दूध का उत्पादन और वितरण छोटे विक्रेताओं द्वारा किया जाता है. ‘नेस्ले पाकिस्तान’ और ‘एंग्रो फूड्स’ जैसी कंपनियाँ संगठित क्षेत्र पर नियंत्रण रखती हैं.
बांग्लादेश में लगभग 70% किसानों के पास 1-3 गायें हैं. ये देश के 70-80% दूध का उत्पादन करती हैं. श्रीलंका में ‘नेस्ले’ और ‘फॉन्टेरा’ जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मजबूत उपस्थिति है. नेपाल में छोटे किसानों का दबदबा है और यहाँ भैंस का दूध अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.
तुलना
उपरोक्त देशों की तुलना में भारत का डेयरी क्षेत्र सबसे अधिक किसान-आधारित है, जहाँ 15 करोड़ से अधिक डेयरी किसान हैं. हालांकि, प्रति पशु औसत दूध उत्पादन केवल 3 लीटर प्रतिदिन है. वहीं औद्योगिक देशों में यह औसत 30 लीटर प्रतिदिन है. यह एक नीतिगत दुविधा को उजागर करता है कि क्या प्राथमिकता उच्च उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दी जानी चाहिए या समावेशी विकास और ग्रामीण आजीविका को?
डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देशों के मॉडल दक्षता और निर्यात-उन्मुख रणनीतियों पर आधारित हैं. इसके विपरीत भारत का मॉडल ग्रामीण रोजगार, आय वितरण और पोषण सुरक्षा को प्राथमिकता देता है. भले ही प्रति पशु दक्षता कम हो, भारत का सहकारी मॉडल बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करता है. यह ग्रामीण गरीबी को कम करने में भी सहायक है.
निष्कर्ष
वैश्विक स्तर पर कोई एक “सर्वोत्तम” डेयरी डेयरी मॉडल नहीं है. प्रत्येक देश का मॉडल उसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संदर्भ के अनुसार अलग होता है. भारत का मॉडल अपनी अनूठी चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए विकसित हुआ है. यह लाखों ग्रामीण परिवारों को आजीविका और सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही यह औद्योगिक देशों की उत्पादकता के स्तर तक न पहुँचता हो.