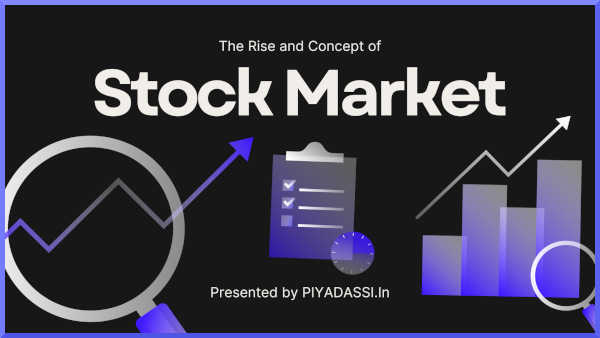इस लेख में करारोपण की परिभाषा, सिद्धांत, वर्गीकरण, और आवश्यकता को सरल और व्यवस्थित भाषा में सभी तथ्यों को शामिल करते हुए समझाया गया है. इसके माध्यम से आप करारोपण के विभिन्न दरों के कारण, कुछ लोगों को कर से छूट और कर सब्सिडी के पीछे के कारणों व सरकार की मंशा को समझ पाएंगे?
करारोपण क्या हैं? (What is Taxation in Hindi)
करारोपण एक प्राचीन अवधारणा है. यह किसी भी सरकार के राजस्व का मुख्य स्त्रोत होता है. सरकार इन राजस्वों का उपयोग जनकल्याण के सार्वजनिक कार्यों, जैसे बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रक्षा आदि में करती हैं. सरकार कर का संग्रह विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित नियमों का पालन करते हुए करती है. इसमें अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति और सरकार के आर्थिक नीतियों का भी सहारा लिया जाता है.
दूसरे शब्दों में, करारोपण का केंद्रीय विचार सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं से लिया जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान है, जिसके बदले में सीधे तौर पर किसी विशिष्ट सेवा की अपेक्षा नहीं की जाती है. हालांकि, अप्रत्यक्ष रूप से यह समाज को सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के रूप में लाभ पहुंचाता है.
करारोपण की परिभाषा (Definitions of Taxation)
करारोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारें सार्वजनिक व्यय को वित्तपोषित करने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं से अनिवार्य शुल्क लेती हैं. इन शुल्कों को कर कहा जाता है. कर और करारोपण एक-दूसरे के पूरक हैं. अर्थशास्त्रियों ने करारोपण के विभिन्न पहलुओं और उद्देश्यों पर जोर देते हुए इसकी अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं. कर की अवधारणा को समझने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करें:
- एडम स्मिथ (Adam Smith): “हर राज्य के निवासियों को, जहाँ तक संभव हो, सरकार के समर्थन में अपने-अपने क्षमताओं के अनुपात में योगदान करना चाहिए, अर्थात, उस आय के अनुपात में जिसका वे संबंधित राज्य के संरक्षण में आनंद लेते हैं.” (संक्षेप में: सरकार के समर्थन के लिए क्षमता के अनुसार अनिवार्य योगदान.)
- डेविड रिकार्डो (David Ricardo): “कर किसी देश के पूंजीगत स्टॉक का एक हिस्सा है जिसे सरकार अपनी आबादी के एक हिस्से को बनाए रखने के लिए उपयुक्त करती है.” (संक्षेप में: सरकार द्वारा आबादी के रखरखाव के लिए पूंजी का एक हिस्सा लेना.)
- जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill): “करारोपण केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों से धन का अनिवार्य उद्ग्रहण है.” (संक्षेप में: सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य धन संग्रह.)
- ए.सी. पिगू (A.C. Pigou): “एक कर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा व्यक्तियों से प्राप्त अनिवार्य अंशदान है, जो उन व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए सीधे तौर पर प्रतिपूर्ति के रूप में नहीं लिया जाता है.” (संक्षेप में: सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सेवाओं के प्रत्यक्ष प्रतिफल के बिना अनिवार्य अंशदान.)
- एडलफ वैगनर (Adolph Wagner): “कर सरकार की आय का एक स्रोत है जो नागरिकों पर बिना किसी प्रत्यक्ष प्रतिलाभ के लगाया जाता है, और जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करना है.” (संक्षेप में: बिना प्रत्यक्ष प्रतिलाभ के सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए सरकारी आय का स्रोत.)
- एफ. बास्टेबुल (F. Bastable): “कर राज्य द्वारा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना प्रत्यक्ष सेवा के जनता से अनिवार्य योगदान है.” (संक्षेप में: राज्य द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं के लिए जनता से बिना प्रत्यक्ष सेवा के अनिवार्य योगदान.)
- ह्यू डल्टन (Hugh Dalton): “कर एक अनिवार्य अंशदान है जो व्यक्तियों द्वारा सरकार को बिना किसी विशेष लाभ की अपेक्षा के किया जाता है.” (संक्षेप में: बिना किसी विशेष लाभ की अपेक्षा के सरकार को अनिवार्य अंशदान.)
- एडविन आर. ए. सेलिगमैन (Edwin R. A. Seligman): “करारोपण वह प्रणाली है जिसके द्वारा सरकारें सार्वजनिक व्यय को वित्तपोषित करने के लिए व्यक्तियों और निगमों से धन एकत्र करती हैं.” (संक्षेप में: सार्वजनिक व्यय के वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा धन संग्रह प्रणाली.)
- आर्थर सी. लेविस (W. Arthur Lewis): “कर वह भुगतान है जो व्यक्ति सरकार को करता है और जिसके बदले में उसे कोई विशिष्ट सेवा प्राप्त नहीं होती.” (संक्षेप में: विशिष्ट सेवा के बिना सरकार को भुगतान.)
- उर्सुला हिक्स (Ursula Hicks): “करारोपण अनिवार्य अंशदान है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, न कि किसी विशेष सेवा के लिए प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में.” (संक्षेप में: सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य अंशदान, न कि प्रत्यक्ष सेवा भुगतान.)
- बेस्टेबिल: “कर व्यक्ति या समूह की संपत्ति का वह हिस्सा है, जो सार्वजनिक सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाता है.”
- शिराज: “कर वह अनिवार्य भुगतान है, जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक भलाई के लिए एकत्र किया जाता है और इसका किसी विशेष लाभ से कोई संबंध नहीं होता.”
इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कर एक अनिवार्य भुगतान है, जिसका उपयोग सरकार सार्वजनिक कार्यों के लिए करती है. करारोपण इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का तरीका है.
करारोपण के सिद्धांत (Theories of Taxation in Hindi)
करारोपण के सिद्धांत सरकारों को कर प्रणाली को निष्पक्ष, कुशल और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं. ये सिद्धांत मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटे गए हैं: मुख्य सिद्धांत, न्याय संबंधी सिद्धांत, और अन्य सिद्धांत.
करारोपण के मुख्य सिद्धांत (Main theories of Taxation in Hindi)
एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक ‘राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज’ (1776) में करारोपण के चार मूल सिद्धांत दिए, जिन्हें बाद में अन्य सिद्धांतों के साथ विस्तारित किया गया. ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
समानता का सिद्धांत (Canon of Equality or Equity)
इस सिद्धांत के अनुसार करों का बोझ करदाताओं के बीच समान या न्यायसंगत रूप से वितरित किया जाना चाहिए. सभी करदाताओं के पास करों का भुगतान करने की समान क्षमता नहीं होती है. इसलिए समानता का यह प्रकार न्याय का हनन है.
अमीर लोग गरीब लोगों की तुलना में अधिक करों का भुगतान करने में सक्षम हैं. इस प्रकार, न्याय की मांग है कि अधिक भुगतान करने की क्षमता वाले व्यक्ति को अधिक करों का भुगतान करना चाहिए. यदि सभी को अपनी क्षमता के अनुसार करों का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो सभी करदाताओं का त्याग समान हो जाता है. यह समानता के सिद्धांत (त्याग) का सार है.
त्याग में समानता स्थापित करने के लिए, करों को भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत के अनुसार लगाया जाना चाहिए.
निश्चितता का सिद्धांत (Canon of Certainty)
किसी व्यक्ति को जो कर देना है वह निश्चित होना चाहिए, लेकिन मनमाना नहीं. एडम स्मिथ के अनुसार, भुगतान का समय, भुगतान का तरीका, भुगतान की जाने वाली राशि, यानी कर देयता, सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए. इस प्रकार निश्चितता के सिद्धांत में बहुत सी चीजें शामिल हैं. यह करदाता के साथ-साथ कर लगाने वाले प्राधिकरण के लिए भी निश्चित होना चाहिए.
केवल करदाताओं को ही नहीं पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और कितना कर चुकाना है. दूसरे शब्दों में, देयता की निश्चितता पहले से ही पता होनी चाहिए. इसी तरह, सरकार द्वारा दी गई समयावधि में वसूले जाने वाले राजस्व की भी निश्चितता होनी चाहिए. इन पहलुओं में किसी भी तरह की अनिश्चितता बहुत सी परेशानियों को आमंत्रित कर सकती है.
मितव्यतित का सिद्धांत (Canon of Economy)
इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि कर एकत्र करने की लागत यथासंभव न्यूनतम होनी चाहिए. कोई भी कर जिसमें उच्च प्रशासनिक लागत और मूल्यांकन में असामान्य देरी और करों का उच्च संग्रह शामिल हो, उसे पूरी तरह से टाला जाना चाहिए.
एडम स्मिथ के अनुसार, प्रत्येक कर को लोगों की जेब से जितना संभव हो उतना कम निकालने और रखने के लिए बनाया जाना चाहिए, साथ ही राज्य के सार्वजनिक खजाने में जो कुछ भी आता है, उससे अधिक होना चाहिए.
सुविधा का सिद्धांत (Canon of Convenience)
करदाता को कर देने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए. कर भुगतान में किसी भी प्रकार की असुविधा करदाता को अधिक कर भार के रूप में झेलना पड़ता है. एडम स्मिथ के अनुसार, ‘‘प्रत्येक कर ऐसे समय और इस ढंग से लगाया जाय कि करदाता को भुगतान की सुविधा हो. प्राय: देखा जा सकता है कि प्रत्येक करदाता कर का सुविधाजनक रूप से भुगतान करना चाहता है.’’
इसी सिद्धांत के तहत, कृषि कर फसल उत्पादन के तुरंत बाद और वेतनभोगियों से वेतन के स्त्रोत से कर का भुगतान लिया जाता है.
उत्पादकता का सिद्धांत (Canon of Productivity)
सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में प्रसिद्ध शास्त्रीय अर्थशास्त्री चार्ल्स एफ. बैस्टेबल के अनुसार, करों को उत्पादक या लागत प्रभावी होना चाहिए. इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कर से प्राप्त राजस्व काफी होना चाहिए. इसके अलावा यह सिद्धांत कहता है कि केवल वही कर लगाए जाने चाहिए जो समुदाय के उत्पादक प्रयास में बाधा न डालें. किसी कर को उत्पादक तभी कहा जाता है जब वह उत्पादन को प्रोत्साहन देता है.
लोच का सिद्धांत (Canon of Elasticity)
आधुनिक अर्थशास्त्री लोच के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं. इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि कर की उपज लचीली या लोचदार होनी चाहिए. इसे इस तरह लगाया जाना चाहिए कि कर की दर को स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सके. जब भी सरकार को धन की आवश्यकता हो, तो उसे कर दरों में वृद्धि करके किसी भी हानिकारक परिणाम को उत्पन्न किए बिना यथासंभव अधिक से अधिक आय प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए. आयकर इस सिद्धांत को पूरा करता है.
सरलता का सिद्धांत (Canon of Simplicity)
प्रत्येक कर लोगों के लिए सरल और समझने योग्य होना चाहिए ताकि करदाता कर सलाहकारों की मदद के बिना इसकी गणना करने में सक्षम हो. जटिल और जटिल कर से अवांछनीय दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, यदि कर प्रणाली जटिल है तो यह करदाताओं को करों से बचने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है.
जटिल कर प्रणाली इस अर्थ में महंगी है कि सबसे ईमानदार शिक्षित करदाताओं को भी सलाहकारों की सलाह लेनी होगी. दूसरी ओर, एक सरल कर प्रणाली त्रुटियों को कम करती है, कर पेशेवरों की आवश्यकता को कम करती है, और करदाताओं और सरकार दोनों के लिए प्रशासनिक लागत को कम करती है.
विविधता का सिद्धांत (Canon of Diversity)
कराधान (करारोपण या Taxation) गतिशील होना चाहिए. इसका मतलब है कि किसी देश की कर संरचना एक या दो करों के बजाय गतिशील या विविध प्रकृति की होनी चाहिए. कर संरचना में विविधता के लिए आबादी के अधिकांश क्षेत्रों की भागीदारी की आवश्यकता होगी. यदि एकल कर प्रणाली शुरू की जाती है, तो केवल एक विशेष क्षेत्र को राष्ट्रीय खजाने में भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में आबादी अछूती रह जाएगी.
जाहिर है, ऐसी कर प्रणाली का प्रभाव कुछ करदाताओं पर सबसे अधिक होगा. एक गतिशील या विविध कर संरचना के परिणामस्वरूप विशाल जनसंख्या के बीच करों का बोझ आवंटित होगा, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर कर का बोझ कम होगा.
उपयुक्तता का सिद्धांत (Canon of Expediency)
यह सिद्धांत व्यावहारिक विचारों को संदर्भित करता है जिन्हें करों को लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए. करों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए, और उन्हें आबादी के बीच अत्यधिक प्रतिरोध या असंतोष पैदा नहीं करना चाहिए.
दूसरे शब्दों में, करों को इस तरह से डिज़ाइन और लागू किया जाना चाहिए जो व्यवहार्य हो और सामाजिक और राजनीतिक वातावरण के साथ संरेखित हो. यह सुनिश्चित करता है कि करों से सामाजिक अशांति या व्यापक प्रतिरोध न हो, जैसा कि बोस्टन टी पार्टी या अन्य कर विद्रोह जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों में देखा गया है. इस सिद्धांत को सुविधा के सिद्धांत का विस्तार भी मान सकते हैं.
करारोपण के न्याय सम्बन्धी सिद्धांत (Justice Theories of Taxation in Hindi)
अर्थशास्त्रियों ने जनता के साथ आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं. इन्हें ही करारोपण का न्याय सम्बन्धी सिद्धांत कहा जाता है. ये सिद्धांत इस प्रकार है:
1. कर देय योग्यता सिद्धांत
कर देय योग्यता सिद्धांत (Ability to pay Taxation theory) का प्रतिपादन 16वीं शताब्दी में जॉन बोर्डिन और 18वीं शताब्दी में बिलियम पेटी और एडम स्मिथ ने किया था. एडम स्मिथ के अनुसार, ‘‘प्रत्येक राज्य की जनता को राज्य की सहायता हेतु अपनी योग्यतानुसार अनुपात में अंशदान करना चाहिए अर्थात् उस आय के अनुपात में देना चाहिए जो कि वे राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं.’’
इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कर देने की योग्यता का निर्धारण करके करारोपण करना चाहिए ताकि वह उस कर का भुगतान आसानी से कर सके. यह सर्वविदित है कि निर्धन वर्ग का कर देने की क्षमता या योग्यता कम होती है. अत: निर्धनों पर कर का आरोपण करके कम मात्रा में अंशदान लिया जाय.
लेकिन, धनाढ्य वर्ग के कर देने की योग्यता अधिक होती है. अत: धनी वर्ग पर करारोपण द्वारा अधिक मात्रा में कर का अंशदान प्राप्त किया जाना चाहिए. इसलिए सरकार द्वारा शासन को कुशलतापूर्ण चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुसार अंशदान कर देना चाहिए या सरकार द्वारा इसी अनुरूप वसूल जाना चाहिए.
कर देय योग्यता के निर्धारण के लिए भावनात्मक तथा आन्तरिक दृष्टिकोणों की सहायता की आवश्यकता होती है. धनाढ्य व गरीब वर्ग के पहचान के लिए उनके आय, संपत्ति और खर्च को आँका जाता है. अक्सर, गरीबों के पास कई लग्जरी संसाधन, जैसे निजी वाहन, जेट, याचट, गोल्फ मैदान इत्यादि नहीं होते है. इस प्रकार वे टोल टैक्स, रोड टैक्स व ट्रांसिट शुल्क से बच जाते है.
2. सेवा लागत सिद्धांत
लोक सत्तायें सार्वजनिक व लोक-कल्याण के कार्यों का निष्पादन करती हैं. इसके लिए एक निश्चित लागत उठानी पड़ती है. इस लागत को अपने देश के नागरिकों से ही बसूला जा सकता है क्योंकि ये कार्य इन्हीं नागरिकों के कल्याण के प्रयास करती हैं. यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि समाज की सेवा पर आने वाली या उठायी जाने वाली लागत के बराबर समाज द्वारा सत्ताओं को कर दिये जाने चाहिए.
लेकिन राज्य द्वारा किए जाने वाले अधिकांश व्यय को प्रत्येक व्यक्ति के लिए तय नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे ठीक से निर्धारित नहीं किया जा सकता. उदाहरण के लिए, हम पुलिस, सशस्त्र बलों, न्यायपालिका आदि की सेवा की लागत को अलग-अलग व्यक्तियों के लिए कैसे माप सकते हैं? डाल्टन ने भी इस सिद्धांत को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि कर में कोई प्रतिफल नहीं है.
सेवा लागत के सिद्धांत के सम्बन्ध में डॉल्टन ने लिखा है कि, ‘‘सेवा लागत का सिद्धांत डाक सेवाओं, विद्युतधारा आदि की पूर्ति पर लागू किया जा सकता है. इन सेवाओं की कीमत इस सिद्धांत के आधार पर निर्धारित की जा सकती है.’’
प्रो० ब्यूहलर ने इस सिद्धांत के विषय में स्पष्ट किया है कि, ‘‘अनेक लेखकों का सुझाव है कि करों को सरकार द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं की लागत के आधार पर ही लगाया जाना चाहिए. वह भी शायद इस आधार पर कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं को चुनने या रद्द करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए.’’
वास्तव में इसे करारोपण का सिद्धांत न मानकर शुल्क आरोपण के रूप में देखा जा सकता है. यह सिद्धांत सेवाओं को प्राप्त न करने वालों पर करारोपण न करने की बात भी स्वीकार करता है.
3. अधिकतम कल्याण का सिद्धांत
करारोपण व्यवस्था में कल्याण आधारित इस सिद्धांत को एजवर्थ तथा पीगू ने अत्यन्त ही महत्वपूर्ण माना है. इस सिद्धांत के अनुसार करारोपण की व्यवस्था इस प्रकार तय की जाय कि व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो सके.
एजवर्थ के अनुसार, ‘‘करारोपण की नीति को समान सीमान्त त्याग पर आधारित करने के उपरान्त ही समाज को अधिकतम कल्याण प्राप्त हो सकता है.’’ इसी सम्बन्ध में पीगू ने एक तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया कि, ‘‘सभी इस बात से सहमत हैं कि सरकार की क्रियाओं का नियमन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसके नागरिकों का कल्याण अधिकतम हो. यही सरकार की सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया की कसौटी है और करारोपण के क्षेत्र में यही न्यूनतम त्याग का सिद्धांत है.’’
इस सिद्धांत को इस अवधारणा पर आधारित किया गया है कि जैसे-जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों व्यक्ति को मिलने वाली आय की सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है. इसीलिए बढ़ी हुई आय पर घटती दर से करारोपण किया जाना चाहिए.
पीगू ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम त्याग के लिए यह आवश्यक है कि करदाताओं द्वारा भुगतान की गयी द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता समान होनी चाहिए. डॉल्टन तथा मसग्रेव ने भी अधिकतम कल्याण के सिद्धानत से सम्बन्धित न्यायपूर्ण वितरण की समस्या को समान सीमान्त त्याग तथा समान सीमान्त कल्याण की तुलना करके हल करने का प्रयास किया.
करारोपण से अधिकतम कलयाण की स्थिति को उस समय प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार द्वारा प्रत्येक मद पर किये गये व्यय से समाज को समान सीमान्त कल्याण प्राप्त हो तथा करारोपण से जनता को होने वाला सीमान्त त्याग समान हो.
4. आय सिद्धांत
करारोपण के आय सिद्धांत का प्रतिपादन इटली के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डि मार्को द्वारा किया गया है. इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित किया गया है. यह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की आय के अनुपात के आधारपर करारोपण करने पर जोर देता है.
डि मार्को के अनुसार, ‘‘जितनी अधिक आय एक व्यक्ति की होती है, उसे उतना ही अधिक कर देना चाहिए, क्योंकि उतनी ही अधिक सेवाओं का उपयोग उसने किया है. अत: धीन व्यक्ति अधिक तथा निर्धन व्यक्ति कम कर देगा. इस प्रकार करों का निर्धारण आय के अनुपात में किया जाना चाहिए.’’
यह सिद्धांत पूर्ण रूप से आय कर से सम्बन्धित किया गया है यदि सम्पूर्ण कर व्यवस्था के लिए आय को आधार बनाया जाय तो अर्थव्यवस्था का संचालन के लिए सरकार की वित्त व्यवस्था अत्यन्त संकुचित रूप में ही रह जायेगी तथा अन्य क्षेत्र करारोपण से बाहर ही रह जायेंगे.
5. वित्तीय सिद्धांत
करारोपण का वित्तीय सिद्धांत कॉलबर्ट के कथन ‘बत्तख को इस प्रकार नोचों कि वह कम से कम शोर मचाये’’ पर आधारित है. प्राचीन काल में सरकारों के सम्मुख मुख्य समस्या अपनी व्यवस्थाओं के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आय अर्जित करने की थी न कि जनता के कल्याण में वृद्धि करने या आर्थिक स्थिरता की.
इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को करारोपण के द्वारा अधिकाधिक पर्याप्त आय प्राप्त हो जानी चाहिए. वर्तमान में सरकारों के सामने आय प्राप्त के साथ समाज के कल्याण एवं त्याग के साथ अर्थव्यवस्था में समान वितरण सम्बन्धी समस्यायें उपस्थित रहती हैं.
करारोपण के अन्य सिद्धांत (Other Theories of Taxation)
करारोपण के अन्य सिद्धांतों में एडोल्फ बैगनर (Adolph Wagner) द्वारा प्रतिपादित 1. सामाजिक-राजनैतिक सिद्धांत, 2. सैलिगमैन के हितप्राप्ति सिद्धांत और 3. जे. एस. मिल का आनुपातिक सिद्धांत को भी शामिल किया गया है.
- सामाजिक राजनैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन इस आधार पर कया गया कि करों का चुनाव सामाजिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए. व्यक्तिगत उद्देश्यों के आधार पर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है. वैगनर के अनुसार सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार का संरक्षण सरकार द्वारा ही सम्भव हो सकता है.
- हित प्राप्ति सिद्धांत के अनुसार सरकार द्वारा समाज को अनेक सामाजिक प्रशासनिक सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं और समाज के जीवन, धन एवं सम्पत्ति की रक्षा भी सरकार के हस्तक्षेप के बिना सम्भव नहीं है. अत: इस सेवाओं की लागत के बदले उन्हें कर का भुगतान सरकाकर को करना ही चाहिए तथा यह वित्तीय भार सेवाओं की प्राप्ति के अनुपात में ही वहन किया जाना चाहिए.
- करारोपण का आनुपातिक सिद्धांत (Proportionate Theory of Taxation):करारोपण में न्याय के विचार को संतुष्ट करने के लिए, जे.एस. मिल और कुछ अन्य शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने करारोपण में आनुपातिक सिद्धांत का सुझाव दिया है. इन अर्थशास्त्रियों का मत है कि यदि व्यक्तियों की आय के अनुपात में कर लगाया जाता है, तो इससे समान त्याग होगा.
- हालाँकि, आधुनिक अर्थशास्त्री इस दृष्टिकोण से अलग हैं. वे कहते हैं कि जब आय बढ़ती है, तो आय की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है. त्याग की समानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उच्च आय वाले व्यक्तियों पर उच्च दरों पर और कम आय वाले लोगों पर कम दरों पर कर लगाया जाए. वे सभी आधुनिक कर प्रणालियों में कराधान की प्रगतिशील प्रणाली के पक्षधर हैं.
- लाभ सिद्धांत (Benefit Theory):इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य को व्यक्तियों पर उनके द्वारा दिए गए लाभ के अनुसार कर लगाना चाहिए. राज्य की गतिविधियों से व्यक्ति को जितना अधिक लाभ मिलता है, उसे सरकार को उतना ही अधिक भुगतान करना चाहिए. यह सिद्धांत गरीब और अमीर में अंतर नहीं करता है. इसलिए, इसे आनुपातिक सिद्धांत के समान ही अत्यधिक आलोचना की गई है.
कराधान का वर्गीकरण (Classification of Taxation)
मुख्य रूप से कराधान के तीन प्रकार होते है. ये निम्नलिखित प्रकार से हैं:
1. आय और संपत्ति का कराधान
ये व्यक्तियों या परिवारों पर प्रत्यक्ष कर हैं. निगम कर, आयकर, प्रतिभूति लेनदेन कर, उपहार कर और संपत्ति कर इसके उदाहरण है. माप के लिए समस्याएँ इन करों की प्रभावशीलता को कम करती हैं. छोटे उद्यमों में स्वरोजगार करने वाले समूहों के लिए आय की गणना करना कठिन होता है, जहाँ वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है. इस तरह राजस्व, परिचालन लाभ और आय के बीच अंतर करना मुश्किल होता है. संपत्ति पर कर लगाना और भी मुश्किल है, क्योंकि संपत्तियाँ अद्वितीय हो सकती हैं और मूल्य को इंगित करने के लिए कोई शेयर मूल्य नहीं होते है.
2. वस्तुओं और सेवाओं पर कराधान
किसी व्यक्ति या परिवारों द्वारा व्यय पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर हैं. इसे फर्मों द्वारा एकत्र किया जाता और यह राजस्व सरकार को चुकाया जाता है. जीएसटी इसका सबसे बेहतर उदाहरण है. इक्साइज़ ड्यूटी, सेल्स टैक्स व वैट भी इसी के उदाहरण है. आय और संपत्ति करों की तुलना में व्यय कर का प्रबंधन करना आसान है. लेकिन आज भी काली अर्थव्यवस्था बनी हुई है और लेखांकन में सभी आर्थिक लेन-देन नहीं दिखाई देते हैं.
अधिक व्यय वाले लोगों पर उच्च कर लगाया जाता है. कई बार कर का यह दर उचित नहीं होता है. इसका कारण है कि कम आय वाले लोगों के लिए भी कर की औसत दर अधिक होती है क्योंकि वे अपनी आय का अधिक हिस्सा मूलभूत वस्तुओं पर व्यय के लिए आवंटित करते हैं. इन वस्तुओं के लिए अमिर और गरीब द्वारा समान दर से कर चुकाना कराधान के मौलिक सिद्धांत का उलँघन करता है.
3. संगठनों पर कर
ये ज्यादातर फर्मों पर कर हैं. फर्मों पर उनकी आय और उनके मुनाफे के स्तर के अनुसार कर लगाया जाता है. उन पर श्रम और ऊर्जा जैसे उत्पादन के कारक के उपयोग के अनुसार भी कर लगाया जाता है. यह कहना संभव है कि सरकारें वास्तव में फर्मों पर कभी कर नहीं लगाती हैं, क्योंकि फर्म को कोई भी कर सीधे उपभोक्ताओं पर टाल देती हैं. विभिन्न प्रकार के कम्पनियों, सोसाइटी, अनुसंधान व शिक्षण संस्थान, स्पोर्ट्स व मित्र क्लब से लिया जाने वाला कर इसी के तहत आता है.
करारोपण की आवश्यकता (Need of Taxation)
करारोपण सरकारों के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि गैर-कर राजस्व (जैसे शुल्क, अनुदान) से सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति संभव नहीं है. करारोपण की आवश्यकता निम्न कारणों से है:
- सार्वजनिक व्यय की पूर्ति: सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, और बुनियादी ढांचे जैसे कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो करों से पूरी होती है.
- आर्थिक नियंत्रण और स्थिरता: करारोपण व्यापार चक्रों, मुद्रास्फीति, और विदेशी प्रभावों को नियंत्रित करने का उपकरण है.
- सामाजिक विसंगतियों का समाधान: कर प्रणाली धन के असमान वितरण और सामाजिक असमानता को कम करने में मदद करती है.