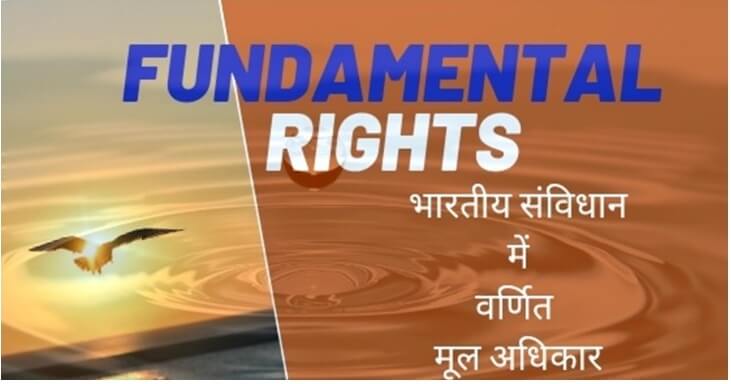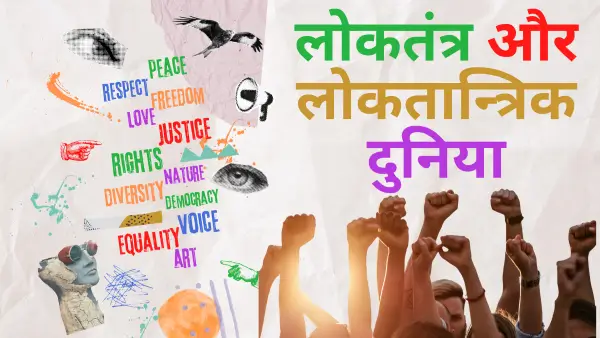आतंकवाद एक ऐसा तत्व है जो जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा हैं. आधुनिक समय मे यह एक राजनीतिक मुद्दे के साथ-साथ एक कानूनी व सैनिक मुद्दा भी बन गया है. यह देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी हैं, किन्तु यह है क्या? इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता और न ही सभी देश इस सम्बन्ध में एकमत है.
यहाँ तक कि विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ भी आज तक आतंकवाद की सर्वानुमति वाली परिभाषा नहीं दे सकी. इसका कारण है कि जिन हिंसात्मक गतिविधियों को अमेरिका या पश्चिमी राष्ट्र आतंवाद कहते हैं, उन्हें इसके समर्थक “जिहाद” “स्वतंत्रता की लड़ाई” “उत्पीड़न व शोषण” के विरुद्ध संघर्ष कहते हैं.
आतंकवाद का अर्थ (Meaning of Terrorism in Hindi)
‘आतंकवाद’ शब्द ‘आतंक’ और ‘वाद’ दो शब्दों से मिलकर बना हैं. ‘आतंक’ से तात्पर्य भय से हैं एवं वाद का तात्पर्य विचार से हैं. आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ उस विचार से होता हैं जिससे भय या दहशत का वातावरण उत्पन्न हो.
मतलब, आतंकवाद, आतंक का दर्शन हैं. यह एक बीमार तथा विश्रृंखलित समाज की देन हैं. यह अपने सभी रूपों में शस्त्ररहित नागरिक समुदाय के विरूद्ध अत्याचार का पर्याय हैं. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति एवं युद्धनीति की शब्दावली में आतंकवाद नवीन नहीं हैं. इसका अस्तित्व थोड़े बहुत रूप में मानव समुदाय के अस्तित्व के साथ-साथ रहा हैं.
आतंकवाद का जन्म दो परिस्थितियों में संभव हैं. प्रथम उस स्थिति में जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय अपनी नाजायज माँगों को मनवाने के लिए आतंक के उपाय के रूप में प्रयोग करता हैं. द्वितीय, स्थिति में आततायी उत्पीड़न का सामना करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय आतंक का रास्ता चुनता हैं. यह स्थिति प्रायः राजनीतिक आंदोलनों के समय उत्पन्न होती हैं.
आतंकवाद की परिभाषा (Definition of Terrorism)
एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करण्ट इंगलिश के अनुसार,” राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद हैं.
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार,” आतंकवाद राजनीतिक लक्ष्यों के लिए भय का प्रयोग करना हैं.”
राष्ट्रसंघ के अनुसार,” आतंकवाद प्रजातन्त्रीय समाजों को अस्थिर करने का मौका हैं और यह ये प्रदर्शित करता हैं कि सरकारें शक्तिहीन हैं.”
ग्रान्टू लारोसी इन्साइक्लोपीडिया के अनुसार,” आतंकवाद को अपने समग्र रूप में उन हिंसात्मक तथा राजनीतिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता हैं, जिनका उद्देश्य हिंसात्मक साधनों द्वारा विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृत करने के लिए दबाव डाला जाता हैं.”
विकिपीडिया के अनुसार,” आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है. अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए, तो उसे आतंकवाद कहते हैं.”
फ्रांस में आतंकवाद से तात्पर्य,” कोई भी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक गतिविधि जिसका उद्देश्य विद्यमान शांति एवं व्यवस्था को नष्ट करना होता हैं, आतंकवाद कहलाता हैं.”
संयुक्त राष्ट्र (UN): संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की कोई एक सार्वभौमिक कानूनी परिभाषा नहीं है. हालांकि, नवंबर 2004 की एक रिपोर्ट में आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसका उद्देश्य “नागरिकों या गैर-लड़ाकों को मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति पहुँचाना हो, जिससे आबादी में भय पैदा हो या किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कोई कार्य करने या न करने के लिए मजबूर किया जा सके”.
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): अमेरिका की परिभाषा राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा पर केंद्रित है. इसमें कहा गया है कि आतंकवाद एक पूर्वनिर्धारित, राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसात्मक अपराध है, जिसे उप-राष्ट्रीय या गुप्त समूहों द्वारा गैर-लड़ाकों के खिलाफ अंजाम दिया जाता है. इस परिभाषा में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों के लिए गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा नागरिकों को निशाना बनाना शामिल है.
यूरोपियन यूनियन (EU): यूरोपीय संघ आतंकवाद को ‘गंभीर अपराध’ मानता है. इसमें लोगों को गंभीर रूप से डराने, सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अनुचित रूप से किसी कार्य को करने या न करने के लिए मजबूर करने, या देश की राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक या सामाजिक संरचना को अस्थिर करने या नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए कृत्य शामिल हैं.
भारत सरकार का आतंकवाद की परिभाषा
भारत सरकार आतंकवाद को एक गंभीर अपराध और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है. भारत में कोई विशिष्ट ‘आतंकवाद’ अधिनियम नहीं है. इससे संबंधित प्रावधानों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) में शामिल किया गया है. इस कानून में वर्ष 2004, 2008 और 2019 में संशोधन किए गए हैं.
UAPA के तहत आतंकवाद की परिभाषा:
यह अधिनियम आतंकवाद को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
- भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को खतरा पहुँचाना.
- लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाना.
- बम, डायनामाइट, विस्फोटक सामग्री या अन्य घातक हथियारों का उपयोग करना.
- अपहरण, हत्या, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, या आवश्यक सेवाओं को बाधित करना.
- नागरिकों, सरकार या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के इरादे से गैरकानूनी कृत्य करना.
भारत की परिभाषा में राज्य-प्रायोजित आतंकवाद पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि भारत को अक्सर सीमा पार से आतंकवाद का सामना करना पड़ता है. इसमें वे कृत्य भी शामिल हैं जो भारतीय नागरिकों या भारत के हितों के खिलाफ विदेश में किए जाते हैं.
उपर्युक्त परिभाषाओं का अवलोकन करने के उपरांत यह कहा जा सकता हैं कि आतंकवाद से तात्पर्य शांति-व्यवस्था के विरूद्ध भय तथा हिंसा का वातावरण निर्मित करने से हैं.
आतंकवादियों के प्रमुख साधन (Key Tools of Terrorists)
ऐसे गुट निम्न साधनों को अपनाते हैं:-
1. विमानों का अपहरण करना.
2. गणमान्य व निरपराध जनसामान्य का अपहरण करना.
3. जन-सामान्य एवं बच्चों को बंधक बनाना एवं फिरौती वसूलना.
4. राजनयिकों का अपहरण व बंधक बनकार ब्लैकमेलिंग करना.
5. निरर्थक व्यक्तिगत एवं सामूहिक हत्यायें करना.
6. तोड़फोड़, बमविस्फोट, रेलपटरियों को तोड़ना.
7. दो समुदायों के मध्य घृणा का वातावरण उत्पन्न करना.
8. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में विध्वंस करना.
9. मानव बम का इस्तेमाल करना.
10. जैव (रासायनिक) आतंकवाद का खतरा उत्पन्न करना.
आतंकवाद की विशेषताएं अथवा लक्षण (Characteristics or Traits of Terrorism)
इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-
1. यह राज्य या समाज के विरूद्ध होता तथा इनके विरूद्ध कार्य करता हैं.
2. इसका राजनीतिक उद्देश्य होता हैं.
4. यह न केवल अपने तात्कालिक शत्रुओं को अपितु सामान्य जनता को भी डराने और उनमें भय एवं आंतक पैदा करने की कोशिश करके उन्हें अवपीड़ित एवं वश में करने का कुप्रयास करता हैं.
5. आतंकवादी अपने कार्यों या हमलों को इतने आकस्मिक और भयंकर रूप से अंजाम देते हैं कि केवल जन-साधारण में ही नहीं अपितु कभी-कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना पैदा हो जाती हैं.
6. इनके कारनामे किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं होते और कभी-कभी तो योजना, दुस्साहस, बर्बरता और संहार के पैमाने के लिहाज से उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता हैं.
7. यह बुद्धिसंगत विचार को समाप्त कर देता हैं. अपने कारनामों के औचित्य को दर्शाने के लिए धार्मिक गंथ्रों या राजनीतिक विचारकों के विचारों को अपने लक्ष्यों के अनुसार तोड़-मोड़कर कुतर्कों की मदद से प्रस्तुत करता हैं. ये समूह इस बात पर बल देते हैं कि जो कुछ वे कर रहे हैं या कह रहे हैं, वही ठीक हैं.
8. यह केवल विरोधी पक्ष पर ही नहीं, बल्कि सजातीय समुदाय पर भी हमला कर सकता हैं.
9. इनमें लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया होती हैं.
10. इसमें की गयी हिंसा मनमानी होती हैं. मतलब ये शत्रु या शिकारों का चयन बिना किसी सोच-समझ या योजना के तथा अन्धाधुन्ध तरीके से करते हैं. इसलिए इसके शिकार किसी भी जाति, धर्म, आयु या वर्ग के यहाँ तक कि मासूम बच्चे, असहाय वृद्ध और निर्दोष महिलाएँ भी हो सकते हैं.
आतंकवाद के उदय/ उत्पत्ति के कारण (Reasons for the Rise/Origin of Terrorism)
आतंकवाद की उत्पत्ति धार्मिक कट्टरतावाद, जातीय उन्माद, रंगभेद, जातीय सर्वोच्चता और बाहारी राष्ट्रों द्वारा पोषण के आधार पर तेजी से विकसित हुई हैं. आतंक एक आतंकवादी गतिविधियों के उत्पन्न होने के विभिन्न देशों में अलग-अलग कारण होते हैं. आज लगभग पूरी दुनिया आतंकवाद से ग्रस्त हैं. आतंकवाद के अनेक कारण हो सकते हैं. किन्तु आतंकवाद के उत्पन्न होने के मूल कारणों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विवाद व अन्य कारण प्रमुख हैं.
आतंकवाद के मुख्य कारणों का निम्नानुसार विवेचन किया जा रहा हैं–
1. आर्थिक कारण
इसकी जड़ मूलतः आर्थिक असमानता हैं. गरीबी, भुखमरी तथा बेरोजगार हैं, जो आर्थिक कारण का आधार होती हैं. बेरोजगार गरीब आसानी से आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं. व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं. सम्पत्ति, सुविधा व संसाधनों के असमान वितरण से व्यक्ति में क्षोभ, विद्वेष व असन्तोष का फायदा आंतकी उठाते हैं एवं अपने लक्ष्य से इसे मुद्दा बनाकर प्रस्तुत करते हैं.
अशिक्षा, शोषण, बेरोजगारी एवं भुखमरी से ग्रस्त अज्ञानी लोग (व्यक्ति) आतंक का सहारा ले लेते हैं. इसका वित्तपोषण अक्सर आमिर वर्ग अपने आर्थिक, राजनैतिक या अन्य हित साधने के लिए करते है. हालांकि सभी लोग आतंकवादी नहीं होते हैं. मगर कुछ लोग तरह-तरह के प्रलोभन में आकार आतंकवाद का रास्ता अपना लेते है. हताशा के माहौल में अक्सर कई लोग आतंकवादियों का राह अपना लेते है.
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार,” सभी देशों की सरकारों ने समय रहते गरीबी की समस्या का हल नहीं किया तो इससे उग्रवाद की समस्या गंभीर रूप से उभर सकती हैं.”
2. मनोवैज्ञानिक कारण
यह एक मानसिक बीमारी या मनोदशा हैं. समाज में कम योग्य तथा अकुशल व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति एवं भूमिका से असन्तुष्ट होकर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होकर समाज में अपनी भूमिका एवं स्थान को प्राप्त करने हेतु समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिये आतंक का सहारा लेते हैं.
समाज में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपनी खीझ और चिन्ता को विध्वंसकारी गतिविधियों के माध्यम से प्रकट करते हैं. कभी-कभी ऐसे शिक्षित मध्यमवर्गीय या उच्च वर्गीय अमीर व्यक्ति भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु सुगम व सरल मार्ग के रूप में आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेते हैं. इसके लिए चित्रपट अधिक जिम्मेदार हैं, जिसमें व्यक्ति के जीवन में रातों-रात परिवर्तन दिखाया जाता हैं.
अल्पसंख्यक एवं उपेक्षित वर्ग में शासन के प्रति अपनी उपेक्षा की भावना भी इसके लिए कुछ सीमा तक अपने दायित्व से बच नहीं सकती. उपेक्षित व अल्पसंख्यक धर्म का सहारा लेते हैं एवं शासनकर्ता को अपना पूर्वाग्रही एवं अन्यायी मानते हैं.
युवा वर्ग की उम्र इसे फैलाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं. बहुसंख्यक आतंकियों की उम्र युवा वर्ग की उम्र होती हैं, युवावस्था में व्यक्ति जोश में ज्यादा होता हैं और होश में कम. आमूलचूल परिवर्तन की मनोदशा वाला यह वर्ग क्रांतिकारी विचारों वाला होता हैं जो अपना आत्मनियंत्रण जल्दी खो देता हैं. आतंकी संगठन इनका फायदा उठाकर अपनी गतिविधियों में संलग्न कर लेते हैं एवं उन्हें मानसिक दृष्टि से अमानवीय, विध्वंसक बनाकर असामाजिक, अनैतिक व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सदा के लिए आतंकवाद में लीन कर देते हैं.
3. सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन
समाज और संस्कृति में आज द्रुतगति से परिवर्तन हो रहा हैं. समाज में परिवर्तन न होने पर बड़े से बड़ा समाज टूट जाता हैं. संस्कृतियों में भी बदलाव हो रहा हैं. इससे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं. सामाजिक जीवन में परिवर्तन का लाभ कुछ व्यक्तियों या एक ही वर्ग के लोगों को यदि प्राप्त होने पर समाज का दूसरा वर्ग जो उपेक्षित हैं; उसमें क्षोभ व कुण्ठा की भावना का जन्म होता हैं. समाज में यह असन्तुलनकारी परिवर्तन समाज के विभिन्न वर्गों में संघर्ष को जन्म देता हैं.
समाज में एकता, अखण्डता व भाईचारा बढ़ाने में भाषा, प्रथाएँ, परम्पराएँ, साहित्य एवं कला के साथ-साथ इन तत्वों में बदलाव होता हैं तो इसके परिणाम भी पूर्व की स्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं. इससे अराजकता व हिंसा का बढ़ावा मिलता हैं. समाज में नवनिर्माण व परिवर्तन की आशा यदि धूमिल होती हैं, तो व्यक्तियों में ईर्ष्या, द्वेष, परिवर्तन या क्रांति का जन्म होता हैं. जब-जब नैतिक मूल्यों का पतन होता हैं, क्रांति या परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता हैं.
सामाजिक परिवर्तन के कारण व्यवस्था, संगठन व संस्थाओं में परिवर्तन होना स्वाभाविक हैं. यदि व्यवस्था व संस्थाएँ परिवर्तन नहीं होती हैं तो बदलती परिस्थितियों में वे अपने दायित्वों के निर्वहन में सफल नहीं हो सकती. समाज में व्याप्त असामाजिक स्थितियाँ (जैसे-भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, रिश्वत, ,बेईमानी) असन्तुष्ट तथा उपेक्षित व्यक्तियों को आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए बढ़ावा देती हैं.
असन्तुष्ट व्यक्ति या समूह बदले के जुनून में हिंसा, प्रतिहिंसा का मार्ग अपनाता हैं. शासन के किसी अंग की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि भी शोषित वर्ग में विद्रोह को जन्म देती हैं. सांस्कृतिक मतभेदों के कारण भी हताशा में आकर लोग आतंकवाद और चरमपंथ के जाल मे फँस जाते हैं.
4. राजनीतिक विवाद
राजनीतिक विवादों से भी इसको प्रोत्साहन मिला हैं. राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित समुदाय या समूह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय देते हैं. भारत में हुर्रियत और पूर्वोत्तर राज्यों में उल्फा, एन.डी.एफ.बी., एन. एस. सी. एन., फिलिस्तीन में अलफतह, चेचेन्या में चेचेन विद्रोही, श्रीलंका में लिट्टे जैसे संगठनों ने राजनीतिक विवाद के नाम पर आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया हैं. राजनीतिक विवादों के कारण दुःखी, गरीब, अशिक्षित तथा मजबूर लोग इन जैसे संगठनों के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं.
5. शासक व शासितों में संपर्क का अभाव
शासक व शासित अर्थात् सरकार व जनता में संवादहीनता भी आतंकवाद का मार्ग प्रशस्त करती हैं. कई बार लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में भी शांतिपूर्ण तरीकों से माँगी गई जायज माँगों की अनदेखी होती हैं. वहीं, नाजायज माँगों को आतंकी भाषा में माँगने पर मंजूर कर लिया जाता है. इससे वैधानिक मार्ग मतलब शांति का मार्ग के स्थान पर अवैधानिक मार्ग अपनाने के लिए जन-समूह का झुकाव बढ़ता जाता हैं.
6. कानून व न्याय व्यवस्था के दोष
कानूनों की जटिलता के कारण जनता में विक्षोभ उत्पन्न होता हैं. न्याय की विलम्बकारी भूमिका से भी लोगों में अन्य मागों से बदले की भावना बढ़ने लगती हैं. सुविधा सम्पन्न एवं अमीर लोगों को कानून व न्याय दोनों आसान लगते हैं जबकि गरीबों व असुविधा वाले वर्ग के लिए यह दोनों बाधक लगती हैं. कानून की जटिलता, अधिकता एवं न्याय में देरी के कारण उग्र स्वाभाव के नवयुवकों के द्वारा आतंक या हिंसा का मार्ग अपना लिया जाता हैं.
7. नवयुवकों में असन्तोष
आतंकवादी सामान्यतः मध्यमवर्गीय परिवार के शिक्षित नवयुवक होते हैं, जो शिक्षित होने के साथ-साथ बेरोजगार भी होते हैं. रोजगार की अनुपलब्धता के कारण ये नवयुवक आतंकवाद की ओर सजह आकर्षित हो जाते हैं. योग्य होने के बाद भी नौकरी प्राप्त करने के लिए जब ये युवा भटकते हैं एवं तस्करों, अवैध धंधों में लिप्त लोगों को विलासितापूर्ण जीवन जीते देखते हैं तो सहज ही आतंकवादियों के संपर्क में आकर उनकी गतिविधियों को अपना लेते हैं.
8. शस्त्रों की प्राप्ति में सुगमता
इन्हें अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र की प्राप्ति विघ्नसंतोषियों द्वारा सुगमता से उपलब्ध करा दी जाती हैं. आधुनिक व अवैध हथियारों ने आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया हैं.
आतंकवाद के उदय के कारणों का विवेचन करने पर स्पष्ट होता हैं कि आतंकवाद ऐसी मानसिकता की उपज हैं जो सभ्य समाज में भय का वातावरण निर्मित कर अपने निहित उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं. भुखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक व सामाजिक असमानता इसका मुख्य कारण हैं.
आतंकवाद के उद्देश्य (Objectives of Terrorism)
आतंकवाद कुछ व्यक्तियों के द्वारा निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य हैं. इसका मुख्य उद्देश्य हिंसक गतिविधियों द्वारा राज्य या समाज से अपनी जायज-नाजायज माँगों को मनवाना हैं. आतंकवाद एक व्यक्ति द्वारा अथवा व्यक्तियों के समूह के कार्यों का परिणाम हो सकता हैं.
यह किसी भी प्रकार का हो सभी आतंकवादियों का प्रायः एक ही उद्देश्य होता हैं वह यह हैं कि उनके लक्ष्य या मनसूबे की प्राप्ति में बाधा पहुँचाने वाले लोगों, समूहों, वर्गों, राजनेताओं से बदला लेना. इसके लिए वे शांति व्यवस्था एवं जन-सामान्य को अपना निशाना बनाते हैं. इनके लक्ष्य सामान्यतया अवैधानिक, विध्वंसकारी व अनैतिक होते हैं.
राजनीतिक-सामाजिक क्रांति की बात करते हुए इनका उद्देश्य ऐसी सत्ता एवं नीतियों को उखाड़ फेंकना होता हैं, जो उन्हें विरोधकारी महसूस होती हैं. इस हेतु आतंकवादी ऐसे नागरिक समुदाय पर अत्याचार और हिंसा का सहारा लेते है. लेकिन, ये निर्दोष नागरिक आतंकियों के लिए अवांछनीय नीति या निर्णय विशेष के लिए दोषो नहीं होते हैं.
ये अपनी गतिविधियों द्वारा राज्य व समाज में भय तथा आतंक का वातावरण लम्बे समय तक जारी रखना चाहते हैं, जिससे जनता का विश्वास सरकार से उठ जाए. इसका स्वाभाविक परिणाम आर्थिक विनाश के साथ राजनीतिक व प्रशासनिक अस्थिरता का होना हैं. ये इन तरीकों का उपयोग सरकार को कमजोर कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में करते है.
संक्षेप, में आतंकवाद के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैं:-
1. अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करना.
2. अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेषकर युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना और अपने आदेशों के पक्ष में उनके दिल व दिमाग में विष घोलना और उन्हें संगठन के लिए मर मिटने को तैयार करना.
3. धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक सम्पत्ति को अन्धाधुन्ध नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी माँगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना.
4. विरोधियों और मुखबिरों को किसी भी कीमत पर सहन या क्षमा न करना और उन्हें खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाना. उसी प्रकार उनकी आंदोलन या गतिविधियों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करना, अपने समर्थकों या अनुयायियों की हर तरह से मदद करना और उनके पकड़े जाने पर उन्हें छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना.
5. शासन व सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास करना ताकि वे अपने कारनामों को अंजाम दे सकें.
6. देश की सुरक्षा, शांति व अखण्डता के लिए हर संभव खतरा उत्पन्न करना ताकि देश में भय, आतंक व असुरक्षा का वातावरण बना रहे.
7. देश के अन्य अलगाववादी शक्तियों को भड़काना ताकि सरकार व जनता का सिर दर्द बना रहें.
आतंकवाद के परिणाम (Consequences of Terrorism)
आज सर्वत्र आतंकवाद की आँधी धीरे-धीरे सभी कुछ तहस-नहस कर रही हैं जिसके कारण कुछ भयंकर परिणाम सामने आते हैं, जो निम्नलिखित हैं:-
1. दंगे-फसाद को बढ़ावा
आतंकी गतिविधियों से से दंगे-फसादों को अत्यंत बढ़ावा मिलता हैं. जगह-जगह मारकाट व खून की होलियाँ खेली जाती हैं, जो एक राष्ट्र के लिए भयंकर स्थिति होती हैं. उदाहरण के लिए पंजाब व कश्मीर में आतंकवाद का बोलबाला हैं. आतंकवादी कभी भी आकर आतंक फैलाने के लिए परिवार के परिवार नष्ट कर जाते हैं. लोगों के समूह के समूह की हत्या कर दी जाती है. आज के व्यक्त ये हत्याओं के साथ-साथ अपहरण भी करने लगे हैं, जिससे अब इनका निर्द्वन्द्व साम्राज्य फैलता जा रहा हैं. परिणामस्वरूप जगह-जगह भय और आतंक का माहौल बन रहा है.
2. सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय
बढ़ते हुए आतंकवाद के फलस्वरूप जनता के मन में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होता है. वह यह सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि यह सरकार हमारी जान व माल की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं.
3. असुरक्षा की भावना का उदय
इन कुकृत्यों से भयंकर परिणामों के कारण जनता में असुरक्षा की भावना का उदय होता है. उनके मन में भय व्याप्त हो जाता हैं कि वह कहीं भी जाने में सुरक्षित नहीं हैं. बच्चों में बचपन से ही एक भय समा जाता हैं. परिणामस्वरूप उनका विकास स्वाभाविक गति से नहीं हो पाता हैं.
4. राष्ट्रीय एकता में बाधक
आतंकवाद राष्ट्रीय एकता में भी बाधक हैं क्योंकि यह एक विशिष्ट सम्प्रदाय के लोगों द्वारा फैलाया जाता हैं और जिस राष्ट्र में विभिन्न सम्प्रदाय एक-दूसरे से बैर रखेंगे वहाँ एकता हो ही नहीं सकती. अतः यह विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा करता हैं. इससे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचती हैं.
5. राष्ट्र की आर्थिक स्थिति असन्तोषजनक
इसके फलस्वरूप हजारों-लाखों करोड़ रूपये की आर्थिक हानि सरकार को उठानी पड़ती है. इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पर भी होता हैं. आतंकवादी निर्दोष व्यक्तियों की हत्यायें करते हैं, लूटपाट करते हैं व आगजनी करते हैं. इससे जान-माल का काफी नुकसान होता हैं. जनता के हुए इस नुकसान को सरकारी कोष से पूरा करना पड़ता हैं. अतः राष्ट्र को आर्थिक हानि भी होती हैं.
आतंकवाद को दूर करने के उपाय/ सुझाव
आतंकवाद से लड़ने का अचूक व कारगर तरीका कोई भी देश अभी तक ईजाद नहीं कर पाया हैं. दशकों से कश्मीर, पंजाब, असम, उत्तरी-पूर्वी राज्यों, गोरखालैण्ड और झारखंड आदि क्षेत्र आतंकवाद की चपेट में हैं. यह आज भी किसी न किसी रूप में जारी हैं. हिंसा समाप्त करने का हर संभव तरीका सरकार अपना चुकी हैं. लेकिन आंतरिक और बाह्य परिसतिथियों के कारण यह आज भी कायम है.
फिर भी हम आतंकवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ उपायों को निम्न रूप में समझा सकते हैं:-
1. उचित नैतिक शिक्षा
इसे दूर करने के लिए युवाओं व बालकों को उचित नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता हैं, जिससे वह पथ-भ्रष्ट न हों और किसी विदेशी शक्ति के हाथ का खिलौना नहीं बनें. साथ ही वहाँ की चमक-दमक व उनकी तरफ से दिये गये प्रलोभनों को भी नहीं स्वीकारें.
2. बाहरी शक्तियों का कठोरता से दमन
भारत में आतंक फैलाने वाली जो बाहरी शक्तियाँ हैं उनका कठोरता से दमन किया जाना चाहिए. इसके लिए सरकार को कठोरतम कानून का सहारा लेना चाहिए. आतंकी गतिविधि में लिप्त आरोपियों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में होना चाहिए. दोषियों को जल्द व कठोर सजा मिलने से आतंकवाद के प्रति आकर्षण भयवश ही सही, कम होगा.
3. जनता में जागरूकता की भावना पैदा करना
इसे दूर करने के लिए जनता में जागरूकता की भावना का होना अति आवश्यक हैं. वह भीरू न बनकर रहे. जरूरत के व्यक्त इसके खिलाफ उठ खड़ी हो. वह उन आतंकवादियों का दमन करने को तत्पर हो जाये जो देश में आतंक व अलगाववाद फैला रहे हैं.
4. सीमाओं पर कठोर नियन्त्रण
सीमाओं पर नियंत्रण को कठोर कर दिया जाना चाहिए, जिससे कोई आतंकवादी भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश न कर सके. जो अवैध रूप से प्रवेश करना भी चाहे, उसे उसको कठोरतापूर्वक दमित करने का उपाय होना चाहिए. इस स्थिति से निपटने के लिए सीमाओं पर तैनात बल को हमेशा सतर्क रहना आवश्यक हैं.
5. राजनैतिक एकता
आतंकवाद आज की ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्या हैं. अतः इस समय आवश्यकता इस बात की हैं कि रभी राजनैतिक दल व नेता, पक्ष और विपक्ष के द्वन्द्व से उभकर एक ऐसी सफल राष्ट्रीय योजना बनायें जिससे इसका अन्त हो सके.
6. बेरोजगारी पर लगाम
आतंकवादी गतिविधियों में अक्सर बेरोजगार युवा संलिप्त हो जाते है. उनमें उच्च आय की लालसा होती है. यह लालसा कई बार अवैध गतिविधियों से पूर्ण होती है. ऐसे में सरकार सभी को मुफ़्त उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण दे सकती है. इससे वे उच्च आय प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे और अवैध गतिविधियों से दूर रहना चाहेंगे.
आतंकवाद रोकने के वैश्विक प्रयास
आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है जिसके लिए किसी एक देश द्वारा अकेले निपटना संभव नहीं है. इसलिए, दुनिया भर के देश और संगठन इस समस्या से निपटने के लिए एक समन्वित और बहु-आयामी वैश्विक रणनीति पर काम कर रहे हैं. इस रणनीति के मुख्य स्तंभों में शामिल हैं:
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझाकरण
आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, देशों के बीच मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है.
- खुफिया जानकारी साझा करना: विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसियां आतंकवादी समूहों की गतिविधियों, उनके वित्तपोषण के तरीकों और संभावित हमलों के बारे में जानकारी साझा करती हैं. यह जानकारी अक्सर द्विपक्षीय समझौतों या बहुराष्ट्रीय मंचों, जैसे कि इंटरपोल और यूरोपीय संघ की खुफिया इकाइयों के माध्यम से साझा की जाती है.
- अंतर्राष्ट्रीय संधियां और कानून: संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन इससे संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियां और सम्मेलन स्थापित करते हैं. इनमें से एक प्रमुख प्रयास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) है, जिसे भारत ने प्रस्तावित किया था. इसका उद्देश्य आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा स्थापित करना और सभी सदस्य देशों को आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए बाध्य करना है.
- अपराधियों का प्रत्यर्पण: देश आतंकवाद के आरोपी व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रत्यर्पण संधियों का उपयोग करते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी आतंकवादी एक देश से दूसरे देश में भागकर कानूनी कार्रवाई से बच न सके.
आतंकवाद का वित्तपोषण रोकना
आतंकवादी समूहों को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है. इसलिए, उनके वित्तपोषण के स्रोतों को बाधित करना एक प्रमुख वैश्विक रणनीति है.
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF): FATF एक महत्वपूर्ण अंतर-सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए वैश्विक मानक तय करता है. यह देशों को इन अपराधों से लड़ने के लिए कानूनी और नियामक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करता है.
- संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाती है. इन प्रतिबंधों का उद्देश्य उनकी वित्तीय संपत्तियों को फ्रीज करना और उन्हें धन हस्तांतरित करने से रोकना है.
कट्टरपंथ और ऑनलाइन भर्ती का मुकाबला करना
आतंकवादी संगठन अक्सर युवाओं को अपनी विचारधारा से प्रभावित करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं.
- ऑनलाइन सामग्री को हटाना: विभिन्न देश सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर आतंकवाद से संबंधित प्रचार सामग्री को हटाने के लिए काम कर रहे हैं. ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म (GIFCT) इस तरह के प्रयासों का एक उदाहरण है.
- सामुदायिक जुड़ाव: सरकारों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा उन समुदायों के साथ काम किया जा रहा है, जो कट्टरपंथ की चपेट में आ सकते हैं. इसका उद्देश्य सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा देना है ताकि आतंकवादी विचारधाराओं को फैलने से रोका जा सके.
- शिक्षा और जागरूकता: शिक्षा के माध्यम से युवाओं को आलोचनात्मक सोच विकसित करने और कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रति प्रतिरोधी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
कानून प्रवर्तन और सैन्य कार्रवाई
जब अन्य उपाय विफल हो जाते हैं, तो आतंकवादी समूहों के खिलाफ कानून प्रवर्तन और सैन्य कार्रवाई की जाती है.
- विशेष बल: विभिन्न देशों के पास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) जैसी विशेष इकाइयां हैं जो आतंकवादी हमलों और बंधक संकटों से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं.
- हवाई हमले और सैन्य अभियान: कुछ स्थितियों में, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सैन्य अभियान और हवाई हमले किए जाते हैं. नाटो के नेतृत्व वाले आतंकवाद विरोधी अभियान इसका एक उदाहरण हैं.
भारत में आतंकवाद की प्रकृति
भारत अपनी भौगोलिक, जातीय, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक विविधता के कारण आतंकवाद की एक जटिल और बहु-आयामी प्रकृति का सामना करता है. यहाँ आतंकवाद एक तरह का नहीं, बल्कि कई रूपों में मौजूद है. इनके अलग-अलग कारण और उद्देश्य हैं. भारत में आतंकवाद की प्रकृति को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में समझा जा सकता है:
1. सीमा पार से प्रेरित आतंकवाद (Cross-Border Terrorism)
यह भारत में आतंकवाद का सबसे प्रमुख और घातक रूप है. इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाना और भारत से इस क्षेत्र को अलग करना है. पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकवादी समूह, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन इसके मूल स्त्रोत है.
ये समूह भारत में घुसपैठ, आत्मघाती हमले, विस्फोट और अन्य हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं. इसे अक्सर “राज्य-प्रायोजित आतंकवाद” कहा जाता है, क्योंकि इन समूहों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से वित्तीय, सैन्य और तार्किक सहायता मिलती है.
2. वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism – LWE)
इसे अक्सर “नक्सलवाद” या “माओवाद” के रूप में जाना जाता है. यह राजनीतिक व्यवस्था को हिंसक तरीकों से उखाड़ फेंकने और एक नई सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम करती है. यह विचारधारा गरीब, आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में असंतोष का लाभ उठाती है.
मुख्य रूप से सीपीआई (माओवादी) जैसे समूह इसके पीछे हैं. यह आतंकवाद मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में फैला हुआ है. यह क्षेत्र “रेड कॉरिडोर” कहलाता है. इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं.
3. जातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद (Ethno-Nationalist Terrorism)
यह आतंकवाद किसी विशेष जातीय समूह के लिए अलग राज्य या स्वायत्तता की मांग से प्रेरित होता है. इनका लक्ष्यजातीय पहचान के आधार पर स्व-शासन या अलगाववाद की मांग करना है. यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, और त्रिपुरा में सक्रिय है. यहाँ के कुछ प्रमुख समूह उल्फा (असम), एनएससीएन (नागालैंड) आदि हैं. इनमें से कई समूहों ने अब शांति प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर दिया है.
4. धार्मिक आतंकवाद (Religious Terrorism)
इस प्रकार का आतंकवाद धार्मिक कट्टरपंथ और वैचारिक असहिष्णुता पर आधारित होता है. धार्मिक वर्चस्व स्थापित करना, दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाना और धार्मिक पहचान के आधार पर समाज को विभाजित करना इनका ध्येय होता है. भारत में सिमी (SIMI) जैसे कुछ स्वदेशी समूह और विदेशी समूहों से प्रेरित स्थानीय गुट इस प्रकार के आतंकवाद में शामिल रहे हैं. 2008 के अहमदाबाद बम विस्फोट और अन्य हमलों में इस प्रकार के आतंकवाद की झलक मिली है.
5. अन्य उभरते खतरे
उपरोक्त प्रमुख श्रेणियों के अलावा, भारत को कुछ नए और उभरते हुए आतंकवादी खतरों का भी सामना करना पड़ रहा है:
- साइबर आतंकवाद: आतंकवादी समूह भर्ती, प्रचार और हमलों की योजना बनाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं. वे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे पावर ग्रिड और वित्तीय प्रणालियों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं.
- नार्को-आतंकवाद: यह आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के बीच का संबंध है. आतंकवादी समूह अपने अभियानों को वित्तपोषित करने के लिए ड्रग्स की तस्करी से होने वाली कमाई का उपयोग करते हैं. यह खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में पनपता है.
आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की रणनीति
भारत ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें कानूनी, संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विभिन्न मोर्चे शामिल हैं.
कानूनी और संस्थागत ढांचा
भारत की आतंकवाद-विरोधी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ इसका कानूनी और संस्थागत ढांचा है.
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967: भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है. इस अधिनियम को समय-समय पर संशोधित किया गया है, जैसे 2004, 2008 और 2019 में. इन संसोधनों का उद्देश्य इसे वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप बनाना था. UAPA गैरकानूनी गतिविधियों, आतंकवादी कृत्यों और उनके वित्तपोषण को रोकने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है. इसमें व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान भी शामिल है.
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA): 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद 2008 में NIA की स्थापना की गई थी. यह एक केंद्रीय आतंकवाद-विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है जिसे भारत में आतंकवादी हमलों, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य सुरक्षा-संबंधी अपराधों की जांच करने का अधिकार है. इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना और मामलों की त्वरित जांच करना है.
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG): NSG एक विशिष्ट कमांडो बल है जिसे ‘ब्लैक कैट्स’ के नाम से भी जाना जाता है. इसका गठन 1984 में किया गया था. इसे आतंकवादी हमलों, बंधक संकट और अपहरण जैसी स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. NSG देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी इकाइयां रखता है ताकि त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके.
खुफिया तंत्र और डेटा साझाकरण
आतंकवादी हमलों को रोकने में खुफिया जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
- खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क: भारत के पास खुफिया एजेंसियों का एक मजबूत नेटवर्क है. इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) मुख्य है. यह विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है. वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) आंतरिक सुरक्षा और घरेलू खुफिया जानकारी पर काम करता है. ये एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें विफल करने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं.
- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID): NATGRID एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे 2012 में शुरू किया गया था. यह एक एकीकृत डेटाबेस है जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे आयकर, बैंक खाते, रेलवे और हवाई यात्रा डेटा को जोड़ता है. इसका उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों को एक ही स्थान पर व्यापक खुफिया जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे वे संभावित खतरों की पहचान कर सकें.
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
भारत मानता है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है.
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT): भारत 1990 के दशक के उत्तरार्ध से संयुक्त राष्ट्र में CCIT नामक एक वैश्विक संधि का प्रस्ताव कर रहा है. इसका उद्देश्य आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा देना, सभी देशों को आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने और उनके वित्तपोषण पर रोक लगाने के लिए बाध्य करना है.
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF): भारत FATF का एक सक्रिय सदस्य है. यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जो आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing) और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) को रोकने के लिए वैश्विक मानक तय करता है. FATF आतंकवादियों के लिए धन के प्रवाह को बाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग: भारत विभिन्न देशों और क्षेत्रीय समूहों जैसे ब्रिक्स, जी20, और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के साथ आतंकवाद-रोधी सहयोग को बढ़ावा देता है. यह खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने और अपराधियों के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करता है.
विश्व व भारत के 10 बहुचर्चित और घातक आतंकी हमले
आतंकवाद ने विश्व और भारत दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. यहाँ विश्व और भारत में हुए कुछ बहुचर्चित और घातक आतंकी हमलों की सूची दी गई है, जिन्होंने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है.
वैश्विक आतंकी हमलें
- 11 सितंबर, 2001 का हमला (अमेरिका): यह अब तक का सबसे घातक आतंकी हमला माना जाता है. अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने चार यात्री विमानों का अपहरण किया. दो विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकराया गया, जिससे वे ढह गए. तीसरे विमान को पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मुख्यालय) से टकराया गया, जबकि चौथा विमान यात्रियों के प्रतिरोध के कारण पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए.
- माद्रिद ट्रेन बम हमला, 2004 (स्पेन): 11 मार्च, 2004 को स्पेन की राजधानी माद्रिद में एक ट्रेन पर सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए. इन हमलों में 192 लोग मारे गए और 2,000 से अधिक घायल हुए. यह हमला अल-कायदा से प्रेरित एक आतंकवादी समूह ने किया था.
- लंदन बम हमला, 2005 (यूनाइटेड किंगडम): 7 जुलाई, 2005 को लंदन में तीन भूमिगत ट्रेनों और एक बस पर आत्मघाती बम विस्फोट हुए. इन हमलों में 52 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए. इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा से जुड़े एक समूह ने ली थी.
- पेरिस हमला, 2015 (फ्रांस): 13 नवंबर, 2015 को पेरिस में इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) के आतंकवादियों ने कई स्थानों पर सिलसिलेवार हमले किए, जिनमें बैटाक्लान थिएटर, रेस्तरां और स्टेड डी फ्रांस शामिल थे. इन हमलों में 130 लोग मारे गए और 350 से अधिक घायल हुए.
- इराक का कैंप स्पाइकर नरसंहार, 2014: जून 2014 में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के आतंकवादियों ने इराक के टिकरित में कैंप स्पाइकर पर हमला किया. इस हमले में लगभग 1,700 निहत्थे इराकी वायु सेना के कैडेटों को मार दिया गया, जिन्हें बाद में सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया.
भारत में प्रमुख आतंकी हमले
- 26/11 मुंबई हमला, 2008: 26 नवंबर, 2008 को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कई प्रतिष्ठित स्थानों पर हमला किया. इनमें ताज महल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन और नरीमन हाउस शामिल थे. इस हमले में 166 लोग मारे गए, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे.
- पुलवामा हमला, 2019: 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक भरी गाड़ी से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले की एक बस को टक्कर मार दी. इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए. हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी.
- भारतीय संसद पर हमला, 2001: 13 दिसंबर, 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के पांच आतंकवादियों ने नई दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला किया. हालांकि, सुरक्षाबलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और सभी हमलावरों को मार गिराया. इस हमले में 6 दिल्ली पुलिस के जवान, 2 संसद सुरक्षा सेवा के कर्मी और एक माली शहीद हुए.
- पठानकोट हमला, 2016: 2 जनवरी, 2016 को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने पंजाब के पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर हमला किया. यह हमला कई दिनों तक चला, जिसमें 7 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हुए.
- अहमदाबाद बम विस्फोट, 2008: 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट की अवधि में 21 बम विस्फोट हुए. इन हमलों में 56 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए. इंडियन मुजाहिदीन नामक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.