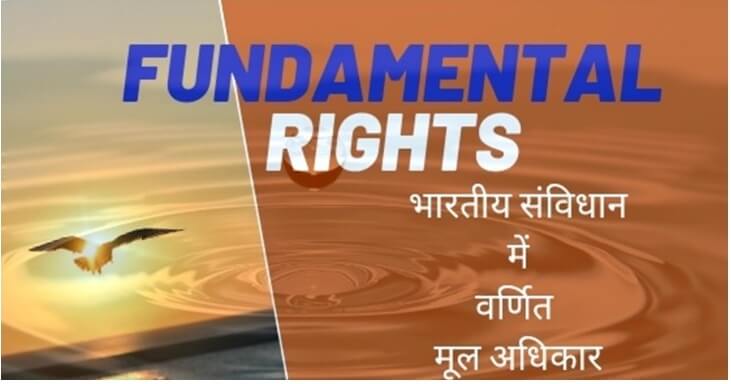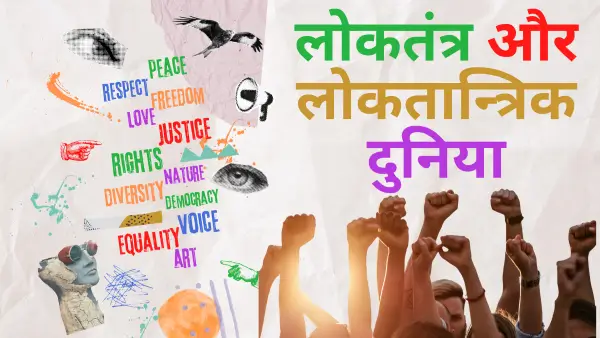केंद्र सरकार ने कई प्रयासों द्वारा त्रिभाषा सूत्र (Three Language Model in Hindi) को देश में लागू करने का प्रयास किया है. लेकिन दक्षिणी राज्यों विशेषतः तमिलनाडु ने इसे थोपने का प्रयास कहकर खारिज किया है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हिन्दी को तीसरे भाषा के रूप में अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया था. लेकिन व्यापाक विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया. इससे एक बार फिर से त्रिभाषा सूत्र चर्चा में आ गया और विवाद की स्थिति बन गई. तो आइए हम त्रिभाषा सूत्र का विकास व अन्य पहलुओं को जानते है.
त्रिभाषा सूत्र क्या हैं?
त्रिभाषा सूत्र एक शैक्षिक नीति है जो भारत में स्कूलों में तीन भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव रखती है. यह नीति 1968 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में अपनाई गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है.
त्रिभाषा सूत्र के प्रमुख सिद्धांत
त्रिभाषा सूत्र के तहत, स्कूलों में छात्रों को निम्नलिखित तीन भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं:
- पहली भाषा (मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा): यह वह भाषा है जो छात्र की मातृभाषा या उसके क्षेत्र में सबसे अधिक बोली जाती है. यह भाषा शिक्षा का माध्यम भी होती है, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर.
- दूसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में, यह एक आधुनिक भारतीय भाषा (जैसे तमिल, बंगाली) या अंग्रेजी होती है. गैर-हिंदी भाषी राज्यों में, यह हिंदी या अंग्रेजी होती है.
- तीसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में, यह अंग्रेजी या कोई और आधुनिक भारतीय भाषा होती है जो दूसरी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई गई हो. गैर-हिंदी भाषी राज्यों में, यह कोई और आधुनिक भारतीय भाषा होती है जो पहली और दूसरी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई गई हो, जैसे कि हिंदी या अंग्रेजी.
त्रिभाषा सूत्र और भारत
भारत, अपनी अद्वितीय भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है. हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएँ सूचीबद्ध हैं. साथ ही, सैकड़ों बोलियाँ देश के सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध करती हैं. यह भाषाई बहुलता राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है. इस पृष्ठभूमि में, त्रिभाषा सूत्र एक दूरदर्शी नीतिगत उपकरण के रूप में उभरा. इसका उद्देश्य इस भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए राष्ट्रव्यापी संचार और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है. इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करना, विभिन्न भाषाई समूहों के बीच के अंतर को समाप्त करना और राष्ट्रीय सद्भाव को मजबूत करना है.
त्रिभाषा सूत्र एक व्यापक रूप से चर्चित नीति है. इसके बावजूद इसका भारतीय संविधान में उल्लिखित कोई कानूनी या संवैधानिक प्रावधान नहीं है. यह एक नीति संकल्प है जिसे भारत सरकार ने राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके बनाया. इसका यही नीतिगत स्वरूप राज्यों को इसे लागू करने या अस्वीकार करने की स्वायत्तता प्रदान करता है, जो शिक्षा के समवर्ती विषय (Concurrent List) में होने के साथ मिलकर केंद्र-राज्य संबंधों में एक स्थायी तनाव का मूल कारण बनता है. यह अंतर्निहित विरोधाभास दर्शाता है कि इस नीति पर होने वाला विवाद केवल भाषा को लेकर नहीं है, बल्कि यह भारत के संघीय ढाँचे में शक्ति संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है.
त्रिभाषा सूत्र का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
त्रिभाषा सूत्र की अवधारणा अचानक उत्पन्न नहीं हुई. यह आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आकार देने वाले विभिन्न आयोगों और समितियों की सिफारिशों का परिणाम थी. ये आयोग और उनकी सिफारिशें इस प्रकार हैं:
प्रारंभिक शिक्षा आयोग
भारत के पहले शिक्षा आयोग का गठन डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में हुआ था. इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है. इस आयोग ने त्रिभाषा नीति की सिफारिश की थी. इस नीति के तहत, छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी (भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में), और अंग्रेजी (अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए एक सहायक भाषा के रूप में) का अध्ययन करना था.
इस सूत्र का उद्देश्य मातृभाषा में दक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय और वैश्विक संचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी की समझ को गहरा करना था. इसके बाद, 1955 में डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया गया. इसने द्विभाषा सूत्र का प्रस्ताव दिया. इसमें क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी के अध्ययन पर जोर दिया गया, जबकि अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित किया गया.
इसी क्रम में, 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् ने त्रिभाषा सूत्र को इसके मूल रूप में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रखा. इसमें इसका अनुमोदन भी हुआ.
1961 में मुख्यमंत्रियों की कान्फ्रेन्स
सन् 1961 में मुख्यमंत्रियों की एक कान्फ्रेन्स में इस सूत्र का एक सरल रूप स्वीकार किया गया, जिसका कारण सामाजिक एवं राजनीतिक था, न कि शैक्षिक. इस सूत्र द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्र अपनी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त एक राष्ट्र भाषा तथा अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन कर सकेंगे ताकि वे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी सुविधानुसार कार्य कर सकें. त्रिभाषा सूत्र में निम्नलिखित दोष भी पाये जाते हैं-
- माध्यमिक स्तर पर बालक का पाठ्यक्रम अत्यन्त बोझिल हो जाता है, क्योंकि उसे अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों के साथ-साथ तीन भाषाएँ भी पढ़नी पड़ेंगी.
- विद्यालयों में यदि छात्र विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकार करें, तो विद्यालय के लिए विभिन्न भाषाओं के अध्ययन कराने की व्यवस्था करना सम्भव न होगा.
- यदि सभी भाषाओं के पठन-पाठन की योजना तैयार की जाए, तो बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध करना एक कठिन कार्य है.
- त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में विशाल धनराशि की आवश्यकता होगी.
1964 तक
सन् 1961 में डॉ० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में भावात्मक एकता समिति का गठन किया गया. इस समिति ने त्रिभाषा सूत्र को निर्मित और कार्यान्वित करने के लिए सुझाव दिए. सन् 1962 में स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद गठित की गई. इसने भी त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया.
कोठारी आयोग (1964-66)
त्रिभाषा सूत्र को आधिकारिक और विस्तृत रूप भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा दिया गया. यह कोठारी आयोग के नाम से लोकप्रिय है. इस आयोग को भारतीय शिक्षा क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए नियुक्त किया गया था. कोठारी आयोग ने एक संशोधित त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया और इसमें कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया. इस संशोधन के अनुसार हिन्दी को ‘राजभाषा’ के रूप में मान्यता दी गई.
किन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अनिच्छुक राज्यों/प्रदेशों पर इसे लादा न जाए. संशोधित त्रिभाषा सूत्र का मूल उद्देश्य यह है कि मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक सभी छात्र निश्चित रूप से करें. संघीय भाषा का अध्ययन सम्पूर्ण देश में किया जाए यानी हिन्दी और अंग्रेजी. तीसरा भाषा (एक आधुनिक भारतीय या विदेशी) भाषा का अध्ययन शैक्षिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कराया जाए.
इसकी सिफारिशों के आधार पर, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस सूत्र को स्वीकार किया गया. इसे एक राष्ट्रीय नीतिगत प्रस्ताव के रूप में प्रतिपादित किया गया. कोठारी आयोग ने इस सूत्र को राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक निकटता को बढ़ावा देने के एक उपकरण के रूप में देखा. यह इस धारणा को भी दूर करता कि हिंदी अन्य भाषाओं पर प्रभुत्व स्थापित कर रही है.
मूल त्रिभाषा सूत्र का ढाँचा (1968)
1968 की नीति के अनुसार, त्रिभाषा सूत्र का ढाँचा हिंदी भाषी और गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लिए अलग-अलग था. इसका उद्देश्य भाषाई अंतर को कम करना था:
(1) पहली भाषा: यह अनिवार्य रूप से मातृभाषा या उस क्षेत्र की भाषा होगी.
(2) दूसरी भाषा:
- हिंदी भाषी राज्यों में: कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा (जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा को प्राथमिकता दी गई) या अंग्रेजी.
- गैर-हिंदी भाषी राज्यों में: हिंदी या अंग्रेजी.
(3) तीसरी भाषा:
- हिंदी भाषी राज्यों में: अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा, जो दूसरी भाषा के रूप में न ली गई हो.
- गैर-हिंदी भाषी राज्यों में: अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा, जो दूसरी भाषा के रूप में न ली गई हो.
नोट: नीति में यह भी संस्तुति थी कि हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिण की कोई भाषा पढ़ाई जानी चाहिए.
1986 और 1992 की नीति
कोठारी आयोग की सिफारिशों के बाद, त्रिभाषा सूत्र को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके 1992 के संशोधन में भी दोहराया गया. हालांकि, 1992 की नीति में यह स्वीकार किया गया कि इस सूत्र का कार्यान्वयन “असमान” रहा और इसे ठीक से लागू नहीं किया जा सका है. यह स्वीकारोक्ति इस बात का संकेत थी कि दशकों तक एक ही नीतिगत खामियों को दोहराया गया. यह परिणाम अपेक्षित नहीं था.
नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 में त्रिभाषा सूत्र
पुरानी नीतियों की कमियों और कार्यान्वयन में आई बाधाओं से सबक लेते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा सूत्र को एक नए और अधिक लचीले स्वरूप में पुनर्जीवित किया गया. यह नीति, जो 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करती है. यह बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र पर फिर से बल देती है.
NEP 2020 के प्रमुख प्रावधान
नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 का दृष्टिकोण पिछली नीतियों की तुलना में अधिक परिष्कृत और व्यावहारिक है. इसमें निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल हैं:
- स्वतंत्रता: नई नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा “ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाएगी”. यह नीति राज्यों, क्षेत्रों और यहाँ तक कि छात्रों को भी तीन भाषाओं को चुनने की स्वतंत्रता देती है. इसे भाषा थोपने को लेकर संवेदनशील राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है.
- प्राथमिकता: NEP 2020 में तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय मूल की होनी चाहिए. यह नियम सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों पर लागू है.
- मातृभाष: इस नीति में शिक्षा का माध्यम घर या मातृभाषा या स्थानीय भाषा रखने पर जोर है. कम से कम ग्रेड 5 और आदर्श रूप से ग्रेड 8 और उसके आगे भी ऐसे करने को कहा गया है. यह कदम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाया गया है.
- विकल्प: छात्रों को छठी या सातवीं कक्षा में अपनी चुनी हुई भाषाओं में से किसी एक को बदलने की अनुमति दी गई है. लेकिन, माध्यमिक शिक्षा पूरी होने तक छात्र तीन भाषाओं में अच्छे से निपुण हो जाएँ. उनमें से एक भाषा को साहित्यिक स्तर पर सीखें.
- विदेशी भाषा: NEP 2020 के तहत, छठी कक्षा से छात्र कोरियन, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य विदेशी भाषाएँ भी सीख सकते हैं. यह कदम छात्रों को वैश्विक संस्कृति और करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए उठाया गया है.
NEP 2020 के तहत त्रिभाषा सूत्र का 1968 से तुलना
| विशेषता | मूल त्रिभाषा सूत्र (1968) | NEP 2020 के तहत संशोधित सूत्र |
| पहली भाषा | मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा | मातृभाषा/स्थानीय भाषा, शिक्षा का माध्यम (ग्रेड 5/8 तक) |
| भाषा चयन | हिंदी भाषी/गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लिए निर्धारित | राज्य, क्षेत्र, और छात्र की पसंद पर आधारित |
| भारतीय भाषाएँ | हिंदी भाषी राज्यों में एक भारतीय भाषा आवश्यक | तीन में से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ अनिवार्य |
| अनिवार्यता | राज्यों पर लागू होने की उम्मीद, पर कार्यान्वयन में कठोरता | स्पष्टीकरण कि कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी |
| अन्य प्रावधान | – | छठी कक्षा से विदेशी भाषा सीखने का विकल्प, कक्षा 6/7 में भाषा बदलने की सुविधा |
त्रिभाषा सूत्र का महत्व
भारत जैसे बहुभाषी और विविध देश के लिए कई मायनों में गहरा है. इसका उद्देश्य भाषाई सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है. यहाँ इसके प्रमुख महत्व दिए गए हैं:
राष्ट्रीय एकता और भाषाई सामंजस्य
त्रिभाषा सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है. यह नीति हिंदी भाषी राज्यों में एक आधुनिक भारतीय भाषा (अधिमानतः दक्षिण भारत की कोई भाषा) और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के शिक्षण को प्रोत्साहित करती है. यह भाषाई खाई को पाटने में मदद करता है, जिससे लोग एक-दूसरे की संस्कृति और भाषाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं. यह केवल एक शैक्षिक नीति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक सेतु का काम करती है.
बहुभाषावाद को बढ़ावा
यह सूत्र छात्रों को कम से कम तीन भाषाएं सीखने का अवसर देता है: मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, हिंदी (अगर वह मातृभाषा नहीं है) और अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा. यह बहुभाषावाद (multilingualism) को बढ़ावा देता है, जो संज्ञानात्मक लचीलेपन, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ाता है. अध्ययनों से पता चला है कि बहुभाषी व्यक्तियों में बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताएँ होती हैं.
शैक्षिक और व्यावसायिक लाभ
- ज्ञान का विस्तार: तीन भाषाओं का ज्ञान छात्रों को साहित्य, विज्ञान और कला के विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक द्वार खोलता है.
- रोजगार के अवसर: त्रिभाषा सूत्र के तहत सीखी गई हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों में बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करता है. उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत का एक छात्र यदि हिंदी और अंग्रेजी जानता है, तो वह उत्तर भारत में व्यावसायिक रूप से अधिक सफल हो सकता है, और इसके विपरीत,
- पारस्परिक संचार: यह लोगों को अपने देश के भीतर विभिन्न समुदायों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है.
सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ
यह सूत्र भाषाई और सांस्कृतिक दीवारों को तोड़ने में मदद करता है. जब एक उत्तर भारतीय छात्र तमिल या कन्नड़ जैसी भाषा सीखता है, तो उसे उस क्षेत्र के साहित्य, इतिहास और कला को समझने का मौका मिलता है. इसी तरह, एक दक्षिण भारतीय छात्र के लिए हिंदी सीखना उत्तर भारत की संस्कृति, सिनेमा और संगीत को जानने का माध्यम बनता है. यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है, जिससे एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है.
संक्षेप में, त्रिभाषा सूत्र केवल भाषाओं को सिखाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह भारत की पहचान को बनाए रखने, उसकी विविधता का जश्न मनाने और एक एकीकृत भविष्य के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी प्रयास है.
चुनौतियाँ और राजनीतिक विरोध
यद्यपि त्रिभाषा सूत्र एक आदर्शवादी नीति है, लेकिन इसका कार्यान्वयन दशकों से कई चुनौतियों से घिरा रहा है.
विफलता के कारण
त्रिभाषा सूत्र का समुचित कार्यान्वयन नहीं हो पाया है. इसका एक प्रमुख कारण शिक्षण संसाधनों और योग्य शिक्षकों की कमी है. कई राज्यों में अतिरिक्त भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिससे यह नीति केवल कागजों तक सीमित रह गई. इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों ने राजनीतिक कारणों से भी इस नीति को अपनाने में अनिच्छा दिखाई.
तमिलनाडु का हिंदी विरोधी आंदोलन
तमिलनाडु में हिंदी का विरोध एक ऐतिहासिक और गहरी जड़ें जमाया हुआ मुद्दा है. विरोध का यह इतिहास 1937 से शुरू होता है. इस साल मद्रास प्रेसीडेंसी में सी. राजगोपालाचारी की सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ. फलतः राजाजी को इस्तीफा देना पड़ा था.
1960 के दशक में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की समय-सीमा नजदीक आई. इसके बाद राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए. इन आंदोलन का तत्कालीन मुख्यमंत्री अन्नादुरई के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की सरकार ने संज्ञान लिया. फिर, त्रिभाषा सूत्र को समाप्त करने और एक स्थायी द्विभाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया. तब से, तमिलनाडु इस नीति का दृढ़ता से पालन कर रहा है. राज्य में केवल केंद्रीय विद्यालयों या सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों में ही हिंदी पढ़ाई जाती है.
संसाधन की कमी और उदासीनता
- हिंदी भाषी राज्यों की उदासीनता: त्रिभाषा सूत्र का लक्ष्य हिंदी भाषी राज्यों में भी एक दक्षिण भारतीय भाषा को पढ़ाना था. लेकिन यह लगभग नगण्य रहा. उत्तर भारतीय राज्यों ने मुख्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में चुना, जिससे सूत्र का आपसी आदान-प्रदान (reciprocity) का सिद्धांत कमजोर हो गया. यह उदासीनता दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी भावनाओं को और बल देती है. इस कारण वहाँ के लोगों को लगता है कि यह एक एकतरफा थोपा गया नियम है.
- शिक्षण संसाधनों की कमी: त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों और अन्य संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती रही है. कई स्कूलों में दक्षिण भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं थे, जिससे इस नीति का कार्यान्वयन कठिन हो गया.
तमिलनाडु का सफल द्विभाषा मॉडल
तमिलनाडु का दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) को अपनाना एक सफल मॉडल साबित हुआ. इस मॉडल ने तमिल लोगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सेवा क्षेत्र में तमिलनाडु के विकास में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अंग्रेजी भाषा के ज्ञान ने तमिलनाडु के युवाओं को देश-विदेश में बेहतर रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान किए. यह हिंदी के मुकाबले एक मजबूत व्यावहारिक तर्क था, जिसे तमिल लोगों ने स्वीकार किया.
इस मॉडल ने अपनी क्षेत्रीय भाषा तमिल के गौरव को बनाए रखते हुए अंग्रेजी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाया. इससे उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोने का डर नहीं रहा, जो त्रिभाषा सूत्र के साथ जुड़ा हुआ था.
वर्तमान स्थिति
सीबीएसई स्कूलों का प्रसार: तमिलनाडु में सीबीएसई स्कूलों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि हिंदी का विरोध पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है. लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हिंदी सीखने की रुचि मौजूद है. व्यापार और पर्यटन के कारण भी तमिलनाडु में हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, खासकर चेन्नई जैसे बड़े शहरों में. यह दिखाता है कि लोग व्यावहारिक कारणों से हिंदी सीख रहे हैं, भले ही इसे सरकारी स्तर पर अनिवार्य न किया गया हो.
NEP 2020 पर वर्तमान विवाद
तमिलनाडु शुरू से ही दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) का पालन करता रहा है. हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है. उनका मानना है कि यह उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा है. तमिलनाडु सरकार ने NEP 2020 के तहत त्रिभाषा फार्मूले को अपनाने पर जोर देने का भी कड़ा विरोध किया है. स्थानीय सरकार द्वारा इस नीति को “हिंदी थोपने” का प्रयास बताया गया है. उनका तर्क है कि यह गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर अनुचित रूप से भाषाई दबाव है.
तमिलनाडु सरकार ने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने NEP 2020 को लागू न करने के कारण समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाली धनराशि रोक दी है, जिसे तमिलनाडु सरकार ‘ब्लैकमेल’ मानती है. वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि NEP 2020 किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपती है और यह सिर्फ बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त करना है.
यह विरोध दर्शाता है कि यह मुद्दा केवल नीतिगत प्रावधानों तक सीमित नहीं है. NEP 2020 का सूत्र पिछली नीतियों की तुलना में अधिक लचीला है. यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी. लेकिन फिर भी तमिलनाडु का विरोध जारी है. यह भाषाई पहचान के संरक्षण का नीति प्रतीत होता है. साथ ही, दशकों पुराने भाषाई संघर्ष और राज्य की स्वायत्तता से जुड़ा एक गहरा भावनात्मक और राजनीतिक संघर्ष दिखता है.
संवैधानिक और कानूनी ढाँचा
भारत का संवैधानिक ढाँचा त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन और विवादों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है.
शिक्षा: एक समवर्ती विषय
भारतीय संविधान के तहत शिक्षा एक समवर्ती विषय (Concurrent List) है. इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही शिक्षा से संबंधित नीतियाँ और कानून बना सकती हैं. यह प्रावधान ही राज्यों को केंद्र की सिफारिशों को अपनाने या अस्वीकार करने का कानूनी आधार देता है. ऐसा तमिलनाडु के मामले में देखा गया है.
भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान
संविधान के कई अनुच्छेद भाषाई नीति को प्रभावित करते हैं:
- अनुच्छेद 343: यह भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी (देवनागरी लिपि में) का प्रावधान करता है. साथ ही, अंकों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग करने का प्रावधान है. इसमें 15 साल तक अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में उपयोग करने की अनुमति है.
- अनुच्छेद 346: यह राज्यों और संघ के बीच संचार की आधिकारिक भाषा से संबंधित है. यह प्रावधान करता है कि दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से हिंदी को संचार की आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग कर सकते हैं.
- अनुच्छेद 350A: यह भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रावधान करता है.
- अनुच्छेद 351: यह संघ का कर्तव्य बताता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा दे.
- अनुच्छेद 29: यह नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है.
ये संवैधानिक प्रावधान एक अंतर्निहित तनाव को दर्शाते हैं. एक तरफ तो अनुच्छेद 351 केंद्र को हिंदी के प्रसार का अधिकार देता है, वहीं शिक्षा का समवर्ती विषय होना राज्यों को अपनी शैक्षिक नीतियों पर नियंत्रण देता है. त्रिभाषा सूत्र का विरोध इसी संवैधानिक तनाव का एक प्रमुख उदाहरण है. इससे साबित होता है कि भारत में नीति-निर्माण अक्सर संघीय संबंधों की जटिलताओं से प्रभावित होता है.
आगे की राह (Conclusion)
त्रिभाषा सूत्र भारत की भाषाई स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास रहा है. यह एक आदर्शवादी नीति है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है. लेकिन इसका कार्यान्वयन दशकों से राजनीतिक और संसाधन-संबंधी चुनौतियों से ग्रस्त रहा है. NEP 2020 ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है. साथ ही, ऐतिहासिक विरोध और संघीय स्वायत्तता की बहस अभी भी जारी है.
आगे की राह के लिए एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:
- संसाधन आवंटन: त्रिभाषा सूत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय और संरचनात्मक संसाधनों का आवंटन आवश्यक है. इसमें योग्य भाषा शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती और उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री का विकास शामिल है.
- राजनीतिक संवाद: केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास-निर्माण और सार्थक संवाद की आवश्यकता है. नीति को जबरदस्ती थोपने के बजाय, भाषाई पहचान का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक ढाँचा विकसित करना महत्वपूर्ण है.
- जन जागरूकता: NEP 2020 के लचीले प्रावधानों और त्रिभाषा सूत्र के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में व्यापक जन जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस पर होने वाला विरोध केवल ऐतिहासिक धारणाओं और गलतफहमियों पर आधारित न हो.
त्रिभाषा सूत्र, अपने सार में, भारत की बहुलतावादी पहचान का एक प्रतिबिंब है. इसका सफल कार्यान्वयन ही इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भाषा एक विभाजनकारी शक्ति के बजाय राष्ट्रीय सद्भाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक माध्यम बने.