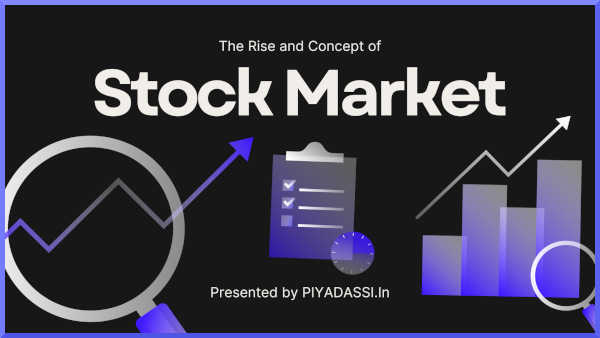इस लेख में भारत में सीमा शुल्क और टैरिफ से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किया गया है. इसमें, सीमा शुल्क के ऐतिहासिक विकास, इसके पीछे के कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न प्रकार के टैरिफ जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को संग्रहीत किया गया है. इसके अलावा आधुनिक वैश्विक व्यापार तंत्र में इसके प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं को भी समाहित किया गया है.
हमने विश्लेषन किया हैं कि कैसे सीमा शुल्क प्राचीन काल से विकसित होते हुए आधुनिक आर्थिक नीति, औद्योगिक संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रमुख साधन बन गया है. लेख में यह भी दर्शाया गया है कि भारत ने अपनी औपनिवेशिक विरासत से निकलकर एक स्वतंत्र, आधुनिक और डिजिटल-संचालित सीमा शुल्क प्रशासन की ओर कैसे कदम बढ़ाया है. भारतीय सीमा शुल्क तंत्र राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
वैश्विक सीमा शुल्क और टैरिफ का इतिहास
सीमा शुल्क का इतिहास मानव सभ्यता के व्यापारिक संबंधों जितना ही पुराना है. शुरुआत में इसे टोल या प्रवेश शुल्क के रूप में वसूला जाता था. प्राचीन मेसोपोटामिया और एथेंस कुछ तय स्थानों में प्रवेश करने वाले माल पर सीमा शुल्क लगाता था. मध्ययुगीन यूरोपीय शहरों में नगर द्वार से प्रवेश करने वाले व्यापारियों से कर वसूला जाता था. वहीं, रोमन साम्राज्य में, पोर्टोरियम (portorium) नामक सीमा शुल्क का उपयोग बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता था. ये शुरुआती शुल्क शासकों के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्त्रोत थे. इसका उपयोग आर्थिक नीति या रणनीति के लिए नहीं होता था.
16वीं से 18वीं शताब्दी तक, व्यापारवाद (mercantilism) के दर्शन ने टैरिफ को एक नया राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य प्रदान किया. इस विचारधारा के तहत किसी भी राष्ट्र की संपत्ति को सोने और चांदी के संचय से मापा जाता था. आयात को धन के बहिर्वाह के रूप में देखा जाने लगा. इस सिद्धांत के परिणामस्वरूप, आयात पर भारी शुल्क एक सामान्य प्रथा बन गई. इसका एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण 17वीं शताब्दी का ब्रिटेन का नेविगेशन अधिनियम था. इसके कानून के द्वारा उपनिवेशों में माल के आयात को ब्रिटिश जहाजों तक सीमित कर दिया. साथ ही, टैरिफ के माध्यम से विदेशी प्रतिद्वंद्वियों से खरीद को हतोत्साहित किया.
19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का काफी विस्तार हुआ. इस कारण ब्रिटेन में मुक्त व्यापार का समर्थन बढ़ने लगा. यह टैरीफ में कमी का कारण बना. लेकिन सदी के अंत तक कुछ “शिशु उद्योगों” (infant industries) को विकसित करने और विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए फिर से संरक्षणवाद उभर गया.
(नोट:संरक्षणवाद की अवधारणा को जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने औपचारिक रूप दिया था.)
20वीं सदी की शुरुआत में टैरिफ ने वैश्विक वाणिज्य को फिर से परिभाषित किया. अमेरिका ने 1930 में स्मूट-हॉले टैरिफ अधिनियम लाया. इसके द्वारा अमेरिका ने 20,000 से अधिक सामानों पर शुल्क बढ़ा दिया. जवाब में अन्य देशों ने प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाए. इस अधिनियम को वैश्विक व्यापार के पतन और वैश्विक मंदी को गहरा करने का एक प्रमुख कारण माना गया. इस अनुभव, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करने की ओर उन्मुख हुई.
इस तरह 1947 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) पर हस्ताक्षर किए गए. इसका उद्देश्य धीरे-धीरे टैरिफ को कम करना था. कई दशकों की वार्ताओं के बाद, विकसित राष्ट्रों के बीच टैरिफ में नाटकीय रूप से गिरावट आई. अंततः, 1995 में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization – WTO) की स्थापना हुई. इस संस्था ने टैरिफ को कम करने और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
टैरिफ और व्यापार नीति
शुरुआत में टैरिफ केवल राजस्व जुटाने का एक साधन था. व्यापारवाद बढ़ने के साथ इसका उपयोग राष्ट्रीय धन के संचय और प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करने के लिए किया गया. 19वीं शताब्दी में “शिशु उद्योगों” को संरक्षण देने के लिए इसका उपयोग एक आर्थिक रणनीति के रूप में हुआ. 20वीं शताब्दी में स्मूट-हॉले टैरिफ ने दिखाया कि टैरिफ का दुरुपयोग वैश्विक आर्थिक पतन का कारण बन सकता है.
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, GATT और WTO के तहत, टैरिफ को कम करने और व्यापार को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया. यह इतिहास दिखाता है कि टैरिफ एक साधारण राजस्व उपकरण से विकसित होकर एक जटिल भू-राजनीतिक और आर्थिक हथियार बन गया है.
यह अब केवल राजस्व का स्रोत नहीं है (जो विकसित देशों के लिए उनके GDP का केवल 0.2% से 0.4% है), बल्कि एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भू-राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने (जैसे चीन–अमेरिका व व्यापार युद्ध व अमेरिका द्वारा कई देशों पर उच्च टैरिफ थोपना), घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए किया जाता है. इसका उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए भी किया जाता है (जैसे भारत द्वारा पाकिस्तान पर 100 फीसदी सीमा शुल्क).
भारत में सीमा शुल्क
भारत में सीमा शुल्क की अवधारणा काफी प्राचीन है. प्राचीन काल में व्यापारी के किसी राज्य में प्रवेश करते समय राजा को एक ‘उपहार’ देना पड़ता था. यह समय के साथ ‘सीमा शुल्क’ बन गई. भारत में आधुनिक सीमा शुल्क का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जुड़ा है.
| 1612 में, ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) ने मुगल सम्राट जहांगीर से सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया. यह भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी व्यापारिक और राजनीतिक पैठ की शुरुआत थी. 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व एकत्र करने का अधिकार (दीवानी) प्राप्त कर लिया. इस प्रकार EIC इन क्षेत्रों की वास्तविक शासक बन गई. 1857 के विद्रोह के बाद, भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया. इसलिए इससे पहले के राज को कंपनी राज व इसके बाद के राज को ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाता है. इस नए शासन का एक मुख्य उद्देश्य भारत से राजस्व निकालना था. |
ब्रिटिशों ने टैरिफ का उपयोग भारत को कच्चे माल के स्रोत और ब्रिटिश कारखानों के लिए एक बाजार में बदलने के लिए किया. इन नीतियों ने पारंपरिक भारतीय उद्योगों को दंडात्मक शुल्क और प्रतिबंधात्मक विनियमों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया. भारत के पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, कपड़ा, इस्पात और जहाज निर्माण उद्योग पर इसका काफी नकारात्मक असर हुआ.
एक उल्लेखनीय उदाहरण 1894 में कपास के सामानों पर 5% आयात शुल्क की शुरूआत थी. इसका विरोध होने लगा. फिर, भारतीय कपास के सामानों पर भी उत्पाद शुल्क (excise duty) लगाकर प्रतिसंतुलित (counterbalance) किया गया. इस कदम ने भारतीय उद्योग को ब्रिटिश आयात पर कोई प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने से रोका. यह नीति 1925 तक लागू रही.
स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा शुल्क के कानून खंडित रूप में थे. सीमा शुल्क का नियमन 1878 का समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1924 का भूमि सीमा शुल्क अधिनियम और 1911 के भारतीय विमान अधिनियम के तहत होता था. इस प्रकार समुद्र, भूमि व वायुमार्ग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलग-अलग कानून थे. यह कानूनी ढाँचा एक संप्रभु राष्ट्र की जरूरतों के अनुरूप नहीं था. इसे देखते हुए 1962 का सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act, 1962) लागू किया गया. यह भारत में सीमा शुल्क का एकीकृत कानून था.
1962 के अधिनियम द्वारा राजस्व संग्रह सुव्यवस्थित किया गया. साथ ही, आयात-निर्यात को विनियमित करने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने, तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत ढाँचा का प्रावधान किया गया. यह भारत की नई राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति को दर्शाता है.
भारतीय सीमा शुल्क का कानूनी और संवैधानिक ढाँचा
भारतीय संविधान में सीमा शुल्क लगाने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार है. अनुच्छेद 265 यह प्रावधान करता है कि “कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर न लगाया जाएगा और न ही एकत्र किया जाएगा”. यह सीमा शुल्क सहित सभी करों के लिए एक कानून की आवश्यकता को अनिवार्य करता है. संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (List I) की प्रविष्टि 83 (Entry No. 83) केंद्र सरकार को आयात और निर्यात पर शुल्क लगाने और एकत्र करने का अधिकार देती है. इससे केंद्र सरकार को सीमा शुल्क कानून बनाने के लिए आवश्यक विधायी शक्ति भी मिलती है.
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
भारत में सीमा शुल्क कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 एक मूलभूत क़ानून है. यह 1 फरवरी 1963 को लागू हुआ था. यह अधिनियम भारत के आर्थिक हितों की भी रक्षा करता है. साथ ही, वैध व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है.
इसके प्रमुख उद्देश्यों में आयात और निर्यात का विनियमन, घरेलू उद्योग का संरक्षण, राजस्व का संग्रह, तस्करी की रोकथाम, और विदेशी मुद्रा का संरक्षण शामिल है. इस अधिनियम में आयात-निर्यात प्रक्रिया, माल की निकासी, मूल्यांकन, और अपील के लिए एक नियम-आधारित ढाँचा वर्णित है. 2021 के सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम द्वारा व्यापार सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलाव किए. इसके द्वारा जाँच पूरी करने के लिए एक निश्चित अवधि (दो वर्ष, एक वर्ष तक विस्तार योग्य) निर्धारित करना और सशर्त छूट की वैधता को दो साल तक सीमित करना शामिल है.
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के साथ ही सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, भारत में सीमा शुल्क कानून के दो प्रमुख अंगों में से एक है. यह अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले शुल्कों की दरों को निर्दिष्ट करता है. इसमें दो अनुसूचियां हैं. अनुसूची 1 आयात के लिए दरों और वर्गीकरण को सूचीबद्ध करती है. अनुसूची 2 में निर्यात के लिए दरों को सूचीबद्ध किया गया है. अधिनियम में अन्य शुल्कों, जैसे अतिरिक्त शुल्क (CVD), एंटी-डंपिंग शुल्क, और तरजीही शुल्क (Preferential Tariff) के प्रावधान भी शामिल हैं.
अन्य प्रावधान
इन दो प्रमुख अधिनियमों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के एक विस्तृत नेटवर्क द्वारा पूरक किया जाता है. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 157, CBIC को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार देती है. इन नियमों में बैगेज नियम, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, और ड्रॉबैक नियम शामिल हैं.
भारत में सीमा शुल्क के प्रकार
मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty – BCD)
मूल सीमा शुल्क (BCD) भारत में आयातित माल पर लगने वाला प्राथमिक कर है. यह एक निश्चित मूल्य (ad valorem) या प्रति इकाई (specific) शुल्क दर के रूप में लगाया जाता है. इसकी दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में निर्दिष्ट हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड के आधार पर निर्धारित होती हैं.
प्रतिरक्षी और सुरक्षा शुल्क
घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए दो विशेष प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं:
- प्रतिरक्षी शुल्क (Protective Duties): ये शुल्क टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर लगाए जाते हैं. इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है. यह एक दीर्घकालिक नीति निर्णय होती है.
- सुरक्षा शुल्क (Safeguard Duties): ये अस्थायी उपाय हैं जो तब लागू किए जाते हैं जब आयात में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि होती है. इस आयात से घरेलू उद्योगों को गंभीर नुकसान होने का खतरा होता है. ये WTO के समझौते के तहत आपातकालीन कार्रवाई के रूप में योग्य होते हैं. इनका उद्देश्य घरेलू उद्योग को बाहरी बाजार के दबाव के खिलाफ खुद को समायोजित करने के लिए समय देना होता है.
प्रतिकारी और एंटी-डंपिंग शुल्क
ये दोनों ही जांच-आधारित होते हैं. ये शुल्क व्यापार को बाधित करने के बजाय “समान अवसर” (level playing field) सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं. यह इस बात को स्वीकारता है कि बाजार बल हमेशा स्वतंत्र नहीं होते हैं. उन्हें विदेशी सरकारों की नीतियों या शिकारी व्यापार प्रथाओं (predatory trade practices) द्वारा विकृत किया जा सकता है. भारत, WTO के सिद्धांतों का पालन करते हुए भी, अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से इन उपायों का उपयोग करता है.
- प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty – CVD): यह आयातित माल पर लगाया जाने वाला शुल्क है. इसका उद्देश्य विदेशी सरकारों द्वारा अपने घरेलू उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी का मुकाबला करना है. इसके द्वारा घरेलू उत्पादकों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाता है. आयातक राष्ट्र द्वारा सब्सिडी वाले निर्यात की गहन जांच करने पर ही WTO इसकी अनुमति देता है.
- एंटी-डंपिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty – ADD): यह उन विदेशी माल पर लगाया जाता है जो भारत में “सामान्य मूल्य” (normal value) से कम कीमत पर निर्यात किए जाते हैं. इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना और एक समान अवसर प्रदान करना है.
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बाद
भारत में GST व्यवस्था लागू होने के बाद, सीमा शुल्क में दो प्रमुख कर जोड़े गए:
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Integrated Goods and Services Tax – IGST): यह आयात पर लगाया जाने वाला एक प्रमुख कर है. यह देश में घरेलू सामानों पर लगने वाले GST के बराबर होता है. यह कर तटस्थता सुनिश्चित करता है. व्यापारी आमतौर पर IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) प्राप्त कर सकते हैं.
- सामाजिक कल्याण अधिभार (Social Welfare Surcharge – SWS): यह आयातित माल पर देय कुल सीमा शुल्क पर लगाया जाने वाला एक अधिभार है. यह सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से लगाया जाता है.
सीमा शुल्क का मूल्यांकन और गणना
सीमा शुल्क का मूल्यांकन आयातित माल के “मूल्य” को निर्धारित करने की प्रक्रिया है. इसी निर्धारित मूल्य पर शुल्क लगाया जाता है . यह मूल्यांकन मनमाना या काल्पनिक नहीं होना चाहिए. यह लेनदेन मूल्य (transaction value) पर आधारित होना चाहिए. यदि लेनदेन मूल्य स्वीकार्य नहीं हो तो कई वैकल्पिक विधियों का उपयोग किया जाता है. मूल्यांकन नियम 2007 में इनका विस्तार से वर्णन किया गया हैं.
इसके लिए समान या समतुल्य वस्तुओं के लेनदेन मूल्य पर आधारित तुलनात्मक मूल्य विधि, आयातित देश में बाद के बिक्री मूल्य पर आधारित कटौती मूल्य विधि, या उत्पादन लागत पर आधारित परिकलित मूल्य विधि का उपयोग होता है.
स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच (SVB) की भूमिका
कई बार आपूर्तिकर्ता और आयातक के बीच कोई विशेष संबंध होता है. बहु-राष्ट्रीय कंपनियां इसका एक उदाहरण है. ऐसे में स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच (SVB) यह सुनिश्चित करना है कि आयातित माल का मूल्यांकन सही “बाजार मूल्य” पर हो. SVB आपूर्तिकर्ता और आयातक के बीच के संबंधों की गहराई से जांच करता है. इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इस विशेष संबंध के कारण माल का अवमूल्यन (undervaluation) किया गया है?
चूँकि सीमा शुल्क वस्तु के मूल्य पर आरोपित होता हैं. इसलिए इसका सही होना कर संग्रह व राजस्व सुरक्षा के लिए जरूरी है. इस तरह SVB सरकार के राजस्व की रक्षा करता है और आयात पर लगने वाले शुल्क की चोरी को रोकता है.
हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड का महत्व
हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organisation – WCO) द्वारा विकसित एक वैश्विक वर्गीकरण प्रणाली है. भारत में उपयोग किया जाने वाला HS कोड 8-अंकीय होता है. यह प्रत्येक उत्पाद को एक विशिष्ट श्रेणी में रखता है, जिससे लागू शुल्क दरें निर्धारित होती हैं.
HS कोड द्वारा प्रत्येक उत्पाद को एक मानकीकृत और वैश्विक पहचान मिलती है. यह शुल्क दरों को निर्धारित करने में व्यक्तिपरक निर्णय को समाप्त करता है. साथ ही, एकरूप करारोपण, व्यापार की पारदर्शिता और भविष्यवाणी क्षमता (predictability) को बढ़ाता है. यह व्यवसायों को लागतों की सही-सही गणना करने और दंड से बचने में भी मदद करता है. इस प्रकार, यह व्यापार सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है. इससे आयातकों को जटिल और मनमाने वर्गीकरणों से छुटकारा मिलती है.
सीमा शुल्क की गणना
सीमा शुल्क की गणना में माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य (Assessable Value) को निर्धारित करना और फिर उस पर विभिन्न प्रकार के शुल्कों को लागू करना शामिल है. कुल शुल्क की गणना के लिए निम्नलिखित चरण लागू होते हैं:
- मूल्यांकन योग्य मूल्य (AV) का निर्धारण: यह माल का कुल मूल्य है जिस पर शुल्क लगाया जाता है. इसमें आमतौर पर घोषित मूल्य, शिपिंग लागत और बीमा शामिल होता है.
AV = Declared Price + Shipping + Insurance - BCD की गणना: मूल्यांकन योग्य मूल्य (AV) पर BCD दर लागू करें.
BCD = AV × BCD Rate - SWS की गणना: BCD राशि पर SWS दर (आमतौर पर 10%) लागू होती है.
SWS = BCD Amount × SWS Rate - IGST के लिए मूल्य का निर्धारण: IGST की गणना के लिए आधार मूल्य AV, BCD, और SWS का योग होता है.
Value for IGST = AV + BCD + SWS - IGST की गणना: चरण 4 से प्राप्त मूल्य पर IGST दर लागू करें.
IGST = Value for IGST × IGST Rate - कुल देय शुल्क: यह BCD, SWS, IGST और अन्य लागू शुल्कों (जैसे ADD) का योग होता है.
Total Duty = BCD + SWS + IGST (+ Other applicable duties)
एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है:
| शुल्क का प्रकार | सूत्र | गणना | देय राशि |
| मूल्यांकन योग्य मूल्य (AV) | – | मान लें: ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| मूल सीमा शुल्क (BCD) | AV×BCD Rate | ₹1,00,000×10% | ₹10,000 |
| सामाजिक कल्याण अधिभार (SWS) | BCD Amount×SWS Rate | ₹10,000×10% | ₹1,000 |
| IGST के लिए मूल्य | AV+BCD+SWS | ₹1,00,000+10,000+1,000 | ₹1,11,000 |
| एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) | Value for IGST×IGST Rate | ₹1,11,000×18% | ₹19,980 |
| कुल देय राशि | BCD+SWS+IGST | ₹10,000+1,000+19,980 | ₹30,980 |
भारतीय सीमा शुल्क प्रशासन
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है. यह सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क (excise duties) और GST सहित अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए शीर्ष प्राधिकरण है. CBIC के प्रमुख कार्य हैं: नीति का निर्माण, राजस्व संग्रह, व्यापार सुविधा, तस्करी की रोकथाम, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग. CBIC का आदर्श वाक्य “देश सेवार्थ कर संचय” है, जिसका अर्थ है राष्ट्र की सेवा के लिए कर संग्रह .
डिजिटलिकरण और व्यापार सुविधा
हाल के वर्षों में, CBIC ने “फेसलेस, संपर्क-रहित और पेपरलेस कस्टम्स” के दृष्टिकोण के साथ कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं. पारंपरिक सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में भौतिक दस्तावेज, अधिकारियों के साथ बार-बार संपर्क, और लंबी प्रतीक्षा अवधि शामिल थी. इससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती थी और व्यापार में देरी होती थी. CBIC द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहलें इस पुरानी व्यवस्था को संबोधित करती हैं.
- फेसलेस असेसमेंट (Faceless Assessment): यह पहल दूरस्थ (remote) मूल्यांकन को सक्षम बनाती है. इससे क्षेत्रीय विवेक कम होता है. फलतः अधिकारियों के पास मूल्यांकन के लिए एकमात्र सहारा कानूनी प्रावधान रहता है. इससे पारदर्शिता बढ़ती है. इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को मानकीकृत और तेज करना है.
- ICEGATE (Indian Customs Electronic Gateway): यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आयातकों और निर्यातकों को दस्तावेज अपलोड करने, बिलों को ट्रैक करने और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा देता है. यह GSTN और DGFT जैसे अन्य सरकारी पोर्टलों से भी जुड़ा हुआ है.
- SWIFT (Single Window Interface for Facilitating Trade): यह एक एकीकृत डिजिटल फॉर्म के माध्यम से कई विभागों (जैसे FSSAI, PQIS) के साथ इंटरफ़ेस को कम करता है. यह व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाता है.
उपरोक्त दक्षता के कारण भारत के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) रैंकिंग में सुधार हुआ हैं. इससे अनुपालन लागत भी कम हुआ है. साथ ही पारदर्शिता और अर्थव्यवस्था में तरलता भी बेहतर हुए है. यह संकेत देता हैं कि भारत का व्यापार नीति केवल सुरक्षावाद (protectionism) तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने एकीकरण को सुविधाजनक बनाने पर भी केंद्रित है.
कुल मिलाकर, भारत का सीमा शुल्क ढाँचा व्यापार को विनियमित करने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सफल रहा है. यह वैश्विक व्यापार के बदलते मानदंडों के अनुकूल भी रहा है. भविष्य में, डिजिटलकरण का विस्तार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण, और AI-आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग व्यापार को और अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बना सकता है. इससे भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति और मजबूत होगी.