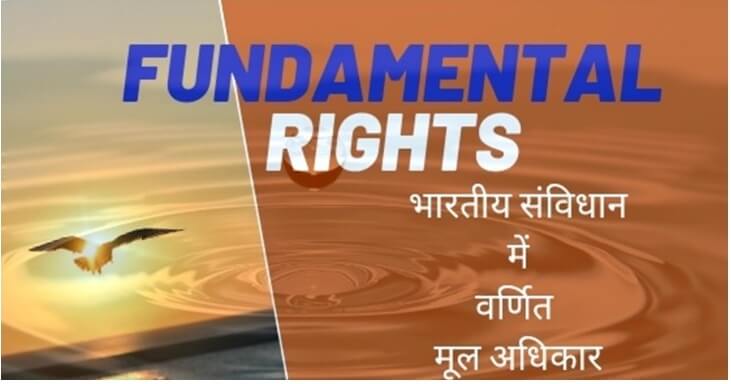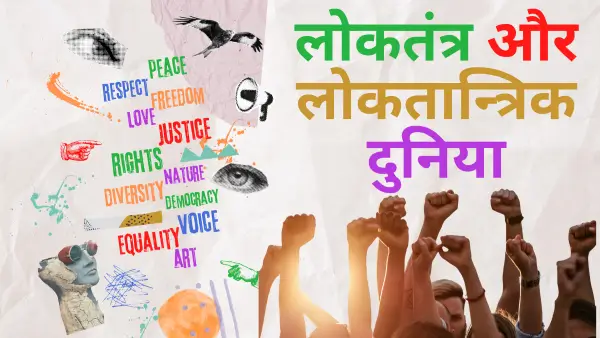भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐतिहासिक अनुभवों और वैश्विक घटनाओं से सीख ली. इसलिए, उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन प्रावधान जोड़े. इसके कारण प्रशासनिक तंत्र के विफल होने पर, भारतीय संघीय ढाँचे का एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित होने की क्षमता है.
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे अद्वितीय बताया है. संविधान के भाग-XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के दौरान सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं. आपातकालीन प्रावधान सरकार को असाधारण परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है. आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित हैं. संकट की स्थिति में आपातकाल लागू किया जाता है, जैसे:
- बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह.
- राज्यों की वित्तीय स्थिरता के खतरे पर.
- संपूर्ण राष्ट्र या किसी हिस्से में प्रशासनिक तंत्र के विफल होने पर.
आपातकालीन प्रावधान से सम्बद्ध अनुच्छेद
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 352 | राष्ट्रिय आपात का उद्घोषणा |
| 353 | आपात के उद्घोषणा का प्रभाव |
| 354 | आपात के दौरान राजस्व के वितरण सम्बन्धी उपबंध |
| 355 | बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा संघ का कर्तव्य |
| 356 | राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का उपबंध |
| 357 | राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में विधायी शक्तियों का प्रयोग |
| 358 | आपातकाल के दौर में अभिव्यक्ति की स्वंत्रता (अनुच्छेद 19) के उपबंधों का निलंबन |
| 359 | आपातकाल के दौरान भाग तीन में वर्णित अधिकारों का निलंबन का प्रावधान |
| 359ए | संविधान (तिरसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 19S9 द्वारा निरस्त, (6-1-1990 से प्रभावी) |
| 360 | वित्तीय आपात से सम्बंधित उपबंध |
आपातकाल के प्रकार (Types of Emergency)
भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आपात तीन प्रकार के होते हैं.
- राष्ट्रिय आपात (अनुच्छेद 352)
- संवैधानिक आपात या राज्यों में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
राष्ट्रीय आपात (National Emergency in Hindi)
अनुच्छेद 352(1) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को समाधान या विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से भारत या इसके किसी भूभाग के सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया हैं या खतरा उत्पन्न होने की आशंका है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352(3) के तहत राष्ट्रिय आपातकाल की घोषणा कर सकता है.
राष्ट्रिय आपातकाल की विशेषताएँ
- 42वें संविधान संसोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल क परामर्श मानने को बाध्यकारी बनाया गया है. 44वां संविधान संसोधन भी इस व्यवस्था को कमोबेश बनाए रखता है.
- अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रिय आपात का उद्घोषणा नहीं कर सकता है जब तक संघ का मंत्रिमंडल इस आशय का लिखित प्रस्ताव उसे न भेजे. 44वां संविधान संसोधन द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया.
- ऐसे उद्घोषणा के किसी संकल्प को संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत तथा उपस्थित ससस्यों के दो-तिहाई मत द्वारा पारित करना आवश्यक है.
- राष्ट्रपति आपात के घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है. एक महीने के अंदर इसे अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहता है. किन्तु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए प्रवर्तन में बना रह सकता है.
- 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 में संशोधन किया, जिससे आपातकाल की घोषणा को और लचीला बनाया गया. इसने यह प्रावधान किया कि आपातकाल की घोषणा पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में लागू की जा सकती है, और इसे “आंतरिक अशांति” (जो पहले “आंतरिक गड़बड़ी” थी) के आधार पर भी घोषित किया जा सकता है. अनुच्छेद 353 के तहत केंद्र की कार्यकारी शक्तियां इस प्रावधान से और व्यापक हो जाती हैं.
राष्ट्रिय आपातकाल के प्रभाव
इसके लागु होने के व्यापक और गंभीर प्रभाव होते है. इनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं:
A. कार्यपालिका सम्बन्धी प्रभाव:
- पुरे देश का प्रशासनिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है.
- संघीय कार्यपालिका राज्यों के कार्यपालिका को यह निर्देश दे सकती हैं कि राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें.
- राज्य सरकार को स्थगित नहीं किया जाता.
B. विधायी प्रभाव
- संसद अनु. 250 के द्वारा सारे देश या उसके किसी भाग के लिए कानूनों का निर्माण कर सकता है.
- संसद राज्य सूचि में दिए गए विषयों पर भी कानून क निर्माण कर सकता है.
- आपातकाल उद्घोषणा राज्य विधानमंडल को स्थगित नहीं करती, परन्तु संघ और राज्यों में शक्तियों के विधायी विभाजन में अवश्य परिवर्तन हो जाता हैं.
C. वित्तीय प्रभाव: अनु. 354 के अनुसार राष्ट्रपति संघ और राज्यों के राजस्व विभाजन में परिवर्तन कर सकता हैं जिसे संसद क अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए.
D. मूल अधिकारों पर प्रभाव
- 44वां संविधान संसोधन अधिनियम द्वारा यह स्थापित किया गया हैं कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के स्थिति में जारी आपातकाल के स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है.
- सशस्त्र विद्रोह के कारण लगे आपात में अनु. 19 प्रभावी रहेगा.
- अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता.
| भारत में अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) लागू किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किए गए. ये आपातकाल निम्नलिखित हैं: 1. भारत-चीन युद्ध (बाहरी आक्रमण के कारण) घोषणा तिथि: 26 अक्टूबर, 1962 समाप्ति तिथि: 10 जनवरी, 1968 कारण: भारत-चीन युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा को खतरे के कारण. विवरण: यह आपातकाल भारत पर चीन के आक्रमण के कारण लागू किया गया था. इस दौरान देश की सुरक्षा और रक्षा को मजबूत करने के लिए कई विशेष शक्तियों का उपयोग किया गया. 2. भारत-पाकिस्तान युद्ध (बाहरी आक्रमण के कारण) घोषणा तिथि: 3 दिसंबर, 1971 समाप्ति तिथि: 21 मार्च, 1977 कारण: भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बाहरी आक्रमण का खतरा. विवरण: यह आपातकाल 1971 के युद्ध के संदर्भ में लागू किया गया, जो बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण था. यह आपातकाल 1975 के आपातकाल के साथ ओवरलैप हुआ. 3. आंतरिक अशांति (Internal Emergency) घोषणा तिथि: 25 जून, 1975 समाप्ति तिथि: 21 मार्च, 1977 कारण: तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने “आंतरिक अशांति” का हवाला देते हुए आपातकाल घोषित किया. विवरण: यह सबसे विवादास्पद आपातकाल था, जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले और विपक्षी आंदोलनों के दबाव में लागू किया. इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी पर रोक और कई विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई. नोट: ये तीनों आपातकाल भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं. 1978 में 44वें संशोधन के बाद, “आंतरिक अशांति” के आधार पर आपातकाल घोषित करने की शक्ति को हटा दिया गया और इसे “सशस्त्र विद्रोह” से बदल दिया गया. इसके अलावा, क्षेत्रीय स्तर पर राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) का भी प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर केवल उपरोक्त तीन आपातकाल ही लागू हुए हैं. |
राज्यों में राष्ट्रपति शासन(अनुच्छेद 356)
अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देता है. इसे “सांविधानिक आपातकाल” भी कहा जाता है. इसका उपयोग तब किया जाता है जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो. इस प्रावधान का आधार 1935 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 93 है, और इसका पहला उपयोग 20 जून 1951 को पंजाब में किया गया था.
प्रक्रिया
राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
- राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है. राष्ट्रपति अन्य स्रोतों से भी संतुष्ट हो सकता है.
- राष्ट्रपति, राज्यपाल का प्रतिवेदन मानने के लिए बाध्य नहीं हैं. वह स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता हैं.
- राष्ट्रपति एक घोषणा जारी करता है, जिसके तहत राज्य सरकार के कार्यों को निलंबित किया जाता है. इसके बाद राज्यपाल ही राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाता है.
- इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित करना होता है. इस अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन छह माह के लिए किर्यान्वयित रहता है. यदि अनुमोदन नहीं होता, तो घोषणा समाप्त हो जाती है.
- इसकी प्रारंभिक अवधि छह महीने की होती है. लेकिन संसद की मंजूरी से इसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. लेकिन, राष्ट्रपति शासन के अवधि का विस्तार के लिए हर छह महीने में पुनरावलोकन करना जरुरी हैं. तीन वर्ष से अधिक के लिए संविधान संसोधन करना होगा.
- इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में हो. यह संघीय ढांचे को कमजोर न करे.
अनुच्छेद 365 के अनुसार, यदि राज्य, संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देशों का अनुपालन करने या उन्हें प्रभावी करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकता हैं कि राज्य का शासन विधि के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है. इस प्रकार भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है.
न्यायिक समीक्षा और कानूनी ढांचा
न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 356 के उपयोग पर एक महत्वपूर्ण अंकुश रही है. 38वें संविधान संसोधन 1975 में इसे न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं माना गया. राजस्थान राज्य बनाम संघ (1975) में माना गया कि यदि राष्ट्रपति का फैसला अतार्तिक या दुर्भावना से प्रेरित हो, तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती हैं. 44वें संविधान संसोधन (1975) में भी इसे न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन माना गया.
1994 के S.R. Bommai v. Union of India मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है. शीर्षस्थ अदालत ने कहा कि इसका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. राज्य विधानसभा को बिना उचित कारण के भंग नहीं किया जा सकता.
इसके अतिरिक्त, गुजरात मजदूर सभा मामले (2020) में, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आंतरिक अशांति के कारण ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो.
घोषणा के प्रभाव
राष्ट्रपति शासन की घोषणा के कई प्रभाव होते हैं:
- राज्य सरकार/कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया जाता है. इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार के समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाते है.
- राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाता है. अक्सर मुख्य सचिव और अन्य सलाहकारों की मदद से राज्यपाल शासन चलाते हैं.
- राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है, जिससे संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति ग्रहण कर लेती है.
- राष्ट्रपति संसद के सत्र के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है. साथ ही, राज्य के वित्तीय प्रबंधन के लिए संसद को अधिकार दे सकता है.
यह व्यवस्था शासन की निरंतरता सुनिश्चित करती है. लेकिन संघीय ढांचे पर सवाल उठाती है, क्योंकि यह राज्य की स्वायत्तता को सीमित करती है.
डॉ. अम्बेकर के विचार
डॉ. बी.आर. अम्बेकर, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, ने अनुच्छेद 356 पर गहन विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि यह प्रावधान केवल असाधारण परिस्थितियों में और अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए. उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि यह “मृत अक्षर” (dead letter) बन जाएगा, अर्थात् इसका उपयोग न हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कानूनी तौर पर उचित होना चाहिए, और यह राज्यों की स्वायत्तता को कम नहीं करने के लिए है.
उनके अनुसार, अनुच्छेद 355 (जो अनुच्छेद 356 से जुड़ा है) केंद्र को राज्यों की रक्षा करने और संविधान बनाए रखने का कर्तव्य देता है. लेकिन इसका उपयोग मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए.
अनुच्छेद 356 के प्रयोग
डॉ. आंबेडकर का इस अनुच्छेद के प्रयोग पर डर सही साबित हुआ है. अनुच्छेद 356 का उपयोग 1950 से अब तक 135 बार किया गया है, और इसका विस्तृत रिकॉर्ड भारत सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी में “Presidents_Rule_in_St_UT_Eng_9th_ed_2016.pdf” दस्तावेज़ में उपलब्ध है.
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ही ऐसे राज्य हैं जहां अब तक कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया. मणिपुर ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है. फ़िलहाल वहां फ़रवरी 2025 से ग्यारहवीं बार राष्ट्रपति शासन लागू है.
उपयोग के कारण और विवाद
राष्ट्रपति शासन के उपयोग के कारणों में राजनीतिक अस्थिरता, विधानसभा में बहुमत खोना, गंभीर लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं, और चुनावों में देरी शामिल हैं. हालांकि, इसका उपयोग अक्सर राजनीतिक दुरुपयोग के लिए आलोचित किया गया है.
केंद्र-राज्य सम्बन्ध पर सरकारिया आयोग (1988) और पंचायती आयोग ने सिफारिश की है कि इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में और अंतिम उपाय के रूप में किया जाए, जो संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है.
निष्कर्षतः, अनुच्छेद 356 एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद प्रावधान है, जिसका उपयोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता को संबोधित करने के लिए किया जाता है. डॉ. अम्बेकर की आशा के विपरीत, इसका दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से हुआ है. न्यायिक समीक्षा ने इसके उपयोग को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
वित्तीय आपातकालीन प्रावधान (अनु. 360)
वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जा सकता है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो. नीचे इसके प्रावधान, प्रक्रिया और प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
प्रावधान
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 360 के तहत, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह इस बात से संतुष्ट हों कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को गंभीर खतरा है, तो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं.
- घोषणा का आधार: यह तब लागू हो सकता है जब देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में हो, जैसे कि भारी राजकोषीय घाटा, मुद्रा संकट, या बाहरी ऋण चूक की स्थिति.
- संसदीय अनुमोदन: वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से दो महीने के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है. यदि लोकसभा भंग हो, तो इसे 30 दिनों के भीतर नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा अनुमोदित करना होगा.
- अवधि: यह तब तक लागू रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे रद्द न करें.
प्रक्रिया
- राष्ट्रपति द्वारा घोषणा: राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की सलाह पर, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं.
- संसदीय अनुमोदन: घोषणा को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अनुमोदित करना होता है.
- केंद्र का नियंत्रण: घोषणा के बाद, केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय मामलों पर अधिक नियंत्रण रख सकती है.
- न्यायिक समीक्षा: वित्तीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है, यदि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है.
प्रभाव
- केंद्र का बढ़ा हुआ नियंत्रण: केंद्र सरकार राज्यों को उनके वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है. राज्य सरकारों को अपने विधायी प्रस्तावों को केंद्र के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना पड़ सकता है.
- वेतन और भत्तों में कटौती: केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों, जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं, के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है. राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों में करों के विभाजन के अनुपात को बदल सकते है. राष्ट्रपति किसी भी राज्य को आर्थिक निर्देश दे सकता है.
- वित्तीय नीतियों का केंद्रीकरण: केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को नियंत्रित कर सकती है. अनुच्छेद 207 से सम्बंधित अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना अनिवार्य हैं.
- आर्थिक सुधारों का कार्यान्वयन: सरकार कठोर आर्थिक उपाय लागू कर सकती है, जैसे कि सब्सिडी में कटौती, कर वृद्धि, या सार्वजनिक व्यय में कमी.
- नागरिकों पर प्रभाव: वेतन कटौती, कर वृद्धि, और आर्थिक कठिनाइयों के कारण नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है. सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं में कमी आ सकती है.
विशेष नोट
भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है. यह आपातकाल अन्य आपातकालों (राष्ट्रीय और राज्य आपातकाल) से अलग है और इसका फोकस विशेष रूप से वित्तीय संकट पर होता है.
यदि आप आपातकालीन प्रावधानों पर और विस्तृत या अन्य जानकारी चाहते हैं या किसी विशिष्ट पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में बताएं!