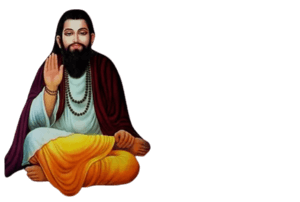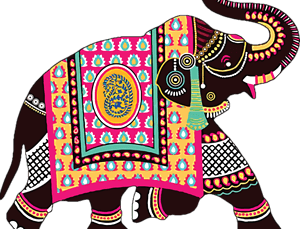अंतर्राष्ट्रीय आणविक उर्जा विभाग (IAEA) एक अंतरसरकारी संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है. साथ ही, परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिये इसके उपयोग को रोकना चाहता है. इसकी स्थापना वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विश्व की “शांति के लिये परमाणु” संगठन के रूप में की गई थी. 1956 में आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (न्यूयार्क) में 70 देशों की सरकारों द्वारा आईएईए के विधान पर हस्ताक्षर किये गये. 27 जुलाई, 1957, से यह अभिकरण प्रभावी हो गया. यह अपनी स्वयं की संस्थापक संधि – IAEA के कानून द्वारा शासित है.
यह UNGAव UNSC दोनों को रिपोर्ट करता है. वर्ष 2005 में, इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिये किये गए काम के लिये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. 2024 के अंत तक अभिकरण के सदस्यों की संख्या 180 थी. भारत इसका संस्थापक सदस्य हैं. इसका मुख्यालय विएना में है. आईएईए संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र से तदर्थ एक स्वायत अंतरराष्ट्रीय संगठन है. 1974 में कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) आईएईए में शामिल हुआ था. इसने ने 1994 में आईएईए की अपनी सदस्यता वापस ले ली.
IAEA का प्रशासनिक ढांचा
आईएईए के मुख्य घटकों में सामान्य सम्मेलन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तथा सचिवालय शामिल हैं. सामान्य सम्मेलन में सभी सदस्य शामिल हैं, जो वार्षिक बैठक के माध्यम से अभिकरण के कार्यक्रमों व बजट को अंतिम स्वीकृति देते हैं तथा महानिदेशक की नियुक्ति एवं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कुछ सदस्यों का चुनाव करते हैं.
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 35 रादस्य होते हैं, जिनमें से 22 का चुनाव सामान्य सम्मेलन द्वारा न्यायपूर्ण भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है. शेष 18 सदस्यों को उनकी अग्रणी नाभिकीय तकनीक एवं नाभिकीय पदार्थ उत्पादन क्षमता के आधार पर नामांकित किया जाता है. बोर्ड ऑफ गवनर्स की बैठक वर्ष में चार बार होती है.
सचिवालय का प्रधान एक महानिदेशक होता है, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है. महानिदेशक संगठन के कार्यचालन हेतु जिम्मेदार होता है तथा अपने कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करता है. वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति के मामलों पर महानिदेशक तथा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को परामर्श देने के लिए 1958 में एक वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया. 1975 में परमाणु विस्फोटों पर एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्श समूह बनाया गया, जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों को प्रोत्साहित करता है.
आईएईए और इसके भूतपूर्व महानिदेशक, मोहम्मद अलबरदेई को संयुक्त रूप से नोबल शांति पुरस्कार वर्ष 2005 में प्रदान किया गया था.
IAEA के उद्देश्य
इस अभिकरण का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए आणविक ऊर्जा के योगदान को विस्तारित एवं प्रोत्साहित करना है. संगठन यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार की सहायता का उपयोग किसी प्रकार के सैन्य उद्देश्य की पूर्ति में न हो. आईएईए की गतिविधियों के चार प्रमुख क्षेत्र हैं-
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों की स्थापना;
- एक सुरक्षोपाय कार्यक्रम का प्रशासन ताकि आणविक खनिजों का सैनिक उपयोग न हो सके;
- तकनीकी सहायता, तथा;
- नाभिकीय अनुसंधान एवं विकास में सहायता.
संहिता
इस एजेंसी ने विकिरण सुरक्षा हेतु मूलभूत सुरक्षा मानदंडों का संहिताकरण किया है तथा विशिष्ट प्रकार के क्रिया-कलापों (जिनमें रेडियोधर्मी पदार्थों का सुरक्षित परिवहन तथा रेडियोधर्मिता सक्रिय कचरा प्रबंधन शामिल हैं) से जुड़े विनियम तथा व्यवहार मानदंड जारी किये हैं. एजेंसी के कार्यात्मक सुरक्षा पुनर्विचार दलों द्वारा नाभिकीय संयंत्रों का दौरा किया जाता है (यदि सम्बद्ध देश इस प्रकार का निवेदन करता है). संगठन से जुड़े पक्ष नाभिकीय दुर्घटनाओं के बारे में पूर्व अधिसूचना एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं.
सभी प्रकार एवं आकार के नाभिकीय संयंत्रों हेतु सुरक्षोपाय मानदंड स्वीकार किये गये हैं. सुरक्षोपाय आईएईए द्वाराअनुप्रयुक्त तकनीकी साधन है, जो यह सुनिश्चित करते है की नाभिकीय उपकरणों व् पदार्थों का उपयोग विशष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया है. सुरक्षोपाय प्रणाली मूलतः नाभिकीय पदार्थ गणना विधि पर आधारित है, जिसमें परिरोधन नीति एवं निगरानी को महत्वपूर्ण उपाय माना गया है. नाभिकीय अप्रसार संधि (1968) की शर्तो के अधीन गैर-परमाणु हथियार वाले देशों को आईएईए के साथ सुरक्षोपाय समझौते सम्पन्न करने पड़ते हैं.
परमाणु शस्त्र रखने वाले देशों ने भी एजेंसी के मानदंडों को लागू करने के लिए आईएईए के साथ समझौते किये हैं. एजेंसी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाड़ी युद्ध-विराम (1991) की शर्तो के अंतर्गत इराक में नाभिकीय अनुसंधान सुविधाओं के निरीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है. एजेंसी ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनी परमाणु शस्त्र क्षमता का परित्याग करने की घोषणा (1993) को सत्यापित किया है.
IAEA की संधियाँ
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) कई महत्वपूर्ण संधियों का प्रशासन करती है जो परमाणु सुरक्षा, सुरक्षा और गैर-प्रसार से संबंधित हैं. इन संधियों के अलावा, आईएईए विभिन्न सम्मेलनों और समझौतों का भी प्रबंधन करता हैं:
1. परमाणु अप्रसार संधि (NPT) – 1968
यह सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त परमाणु नियंत्रण संधि है. इसे 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और 1970 में यह लागू हुई. इसके मुख्य प्रावधान हैं:
- यह संधि पाँच देशों को “परमाणु हथियार संपन्न राज्य” (Nuclear-Weapon States – NWS) के रूप में परिभाषित करती है. ये वे देश हैं जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार का निर्माण और परीक्षण किया था. इन देशों में अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन शामिल हैं.
- यह गैर-परमाणु हथियार वाले राज्यों को परमाणु हथियार विकसित करने या प्राप्त करने से रोकती है.
- यह परमाणु हथियार संपन्न राज्यों को परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करने के लिए बाध्य करती है.
- यह सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के अधिकार की गारंटी देती है.
भारत का रुख: भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि यह विश्व को दो श्रेणियों में विभाजित करती है: परमाणु हथियार वाले और बिना परमाणु हथियार वाले.
2. बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) – 1967
यह संधि 10 अक्टूबर, 1967 को लागू हुई थी. इसका उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है. यह संधि पृथ्वी की परिक्रमा में या चंद्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंडों पर सामूहिक विनाश के हथियारों (nuclear weapons) की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है.
3. त्लाटेलोल्को की संधि (Treaty of Tlatelolco) – 1967
इस संधि का पूरा नाम “लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में परमाणु हथियारों के निषेध के लिए संधि” है. यह 14 फरवरी, 1967 को हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी. इसका उद्देश्य लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को परमाणु हथियार-मुक्त क्षेत्र घोषित करना था. यह इस तरह की पहली संधि थी.
4. परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर वियना कन्वेंशन (1977)
यह कन्वेंशन नाभिकीय क्षति के मामलों में नागरिक दायित्व के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा स्थापित करता है. इसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालक किसी भी दुर्घटना के लिए जवाबदेह हैं.
5. परमाणु सुरक्षा पर कन्वेंशन (1994)
यह कन्वेंशन दुनिया भर में उच्च स्तर की परमाणु सुरक्षा प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है. यह सदस्य राज्यों के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सहकर्मी-समीक्षा तंत्र (peer-review mechanism) स्थापित करता है.
6. परमाणु सामग्री के भौतिक संरक्षण पर कन्वेंशन (1987)
यह कन्वेंशन परमाणु सामग्री के अवैध अधिग्रहण, उपयोग और परिवहन को रोकने के लिए सदस्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है. यह कन्वेंशन परमाणु सामग्री की चोरी या डायवर्जन को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय उपायों को मजबूत करने पर केंद्रित है. इसका एक 2005 का संशोधन भी है जो इसके दायरे को बढ़ाता है.
7. प्रयुक्त ईंधन प्रबंधन की सुरक्षा और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन की सुरक्षा पर संयुक्त सम्मेलन (2001)
यह सम्मेलन प्रयुक्त परमाणु ईंधन और रेडियोधर्मी अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन के लिए वैश्विक सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है. यह सदस्य राज्यों को उनके राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों की सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं की समीक्षा करने का अवसर देता है.
8. परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW)
यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) नामक एक और महत्वपूर्ण संधि है. यह एक हालिया समझौता है जिसे 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था और यह 22 जनवरी 2021 से लागू हुआ. यह संधि परमाणु हथियारों को बनाने, रखने, उपयोग करने या धमकी देने को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है. हालांकि, भारत, अमेरिका, रूस, चीन और अन्य परमाणु हथियार वाले देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.
इसके अलावा, आईएईए द्वारा तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के तहत नाभिकीय शक्ति विकास, नाभिकीय सुरक्षा, रेडियोधर्मी कचरा प्रबंधन., आणविक उर्जा उपयोग के वैधानिक पहलू, उद्योग, कृषि, जल-विज्ञान व चिकित्सा विज्ञान में विकिरण तथा समस्थानिकों के प्रयोग इत्यादि क्षेत्रों में विकासशील देशों की सहायता प्रदान की जाती है.
IAEA के अन्य कार्य
नाभिकीय शोध एवं विकास कार्यक्रमों के तहत आईएईए सामुद्रिक रेडियोधर्मिता की अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला (मोनाको), अंतरराष्ट्रीय सैद्धान्तिक भौतिकी केन्द्र (ट्रीस्टे) तथा अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय सुधार प्रणाली (सीबर्सडॉर्फ, ऑस्ट्रिया) के कार्य संचालन हेतु जिम्मेदार है. यह संगठन नियोजित ताप परमाणविक संलयन प्रतिक्रिया के सम्बंध में यूरोपीय संघ, जापान एवं अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा किये गये कायों को भी समन्वित करता है.
परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICONS)
वैश्विक परमाणु सुरक्षा समुदाय के लिए IAEA का परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICONS) एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है. यह दुनिया भर के परमाणु विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नेताओं को परमाणु सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा करने और उनसे निपटने के लिए एक मंच प्रदान करता है.
ICONS 2024
ICONS 2024 का आयोजन ऑस्ट्रिया के विएना में IAEA मुख्यालय में किया गया था. इस सम्मेलन में परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्री से संबंधित कई प्रमुख चिंताओं पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से परमाणु अपशिष्ट के प्रबंधन और सुरक्षा पर.
वर्तमान में, 145 राज्य IAEA को परमाणु या रेडियोधर्मी सामग्री के खो जाने, चोरी हो जाने, गलत तरीके से निपटाए जाने या उपेक्षित होने की घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं. यह दर्शाता है कि परमाणु सामग्री की सुरक्षा एक वैश्विक चुनौती है.
रेडियोधर्मी पदार्थ केवल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों तक ही सीमित नहीं हैं. इनका व्यापक रूप से चिकित्सा सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है. इनके व्यापक उपयोग के कारण इनकी सुरक्षा और प्रबंधन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है.
“डर्टी बम” का खतरा: सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चरमपंथियों द्वारा “डर्टी बम” में रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग करना है. “डर्टी बम” कोई परमाणु हथियार नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक विस्फोटकों के साथ रेडियोधर्मी सामग्री का मिश्रण होता है. यह परमाणु बम जितना विनाशकारी नहीं होता है. लेकिन विस्फोट से निकलने वाली रेडियोधर्मी सामग्री हवा में फैलकर बड़े पैमाने पर भय, दहशत और रेडियोलॉजिकल संदूषण पैदा कर सकती है. इससे जानमाल को भारी नुकसान हो सकता है.