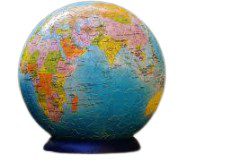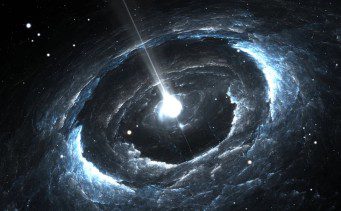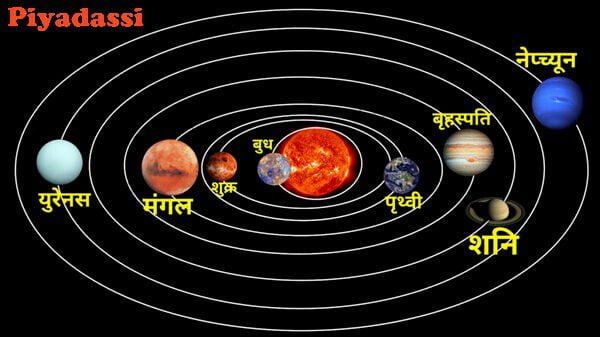उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है. इसलिए, इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं. यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है.
यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है. इसकी समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है. यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3,200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है. इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत सहायक है.
उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण (Formation of Plains in North India)
तृतीयक काल में, इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने से हिमालय का निर्माण हुआ. इन दो विवर्तनिकी प्लेटों के निरंतर अभिसरण के कारण हिमालय में उत्थान हुआ और एक बड़े सिंक्लाइन अर्थात् अभिनति के रूप में प्रायद्वीप एवं हिमालय के मध्य एक गहरें अवसाद का जमाव प्रारम्भ हुआ है.
हिमालय से बहने वाली नदियों के द्वारा अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में लाए गए अवसाद के निक्षेपण के परिणामस्वरूप उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ. इन नदियों में गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र मुख्य हैं. ये बारहमासी नदी बरसात में आज भी हिमालय से बड़े पैमाने पर अवसाद बहाकर मैदानी इलाकों में जमा कर देती हैं, जहाँ इनका बहाव अपेक्षाकृत धीमा होता है. इस प्रकार धरती के निर्माण काल से आरंभ हुई प्रक्रिया आज भी अनवरत जारी हैं.
उत्तर भारत के मैदानों का प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण
उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जाता है-
- पंजाब का मैदान
- गंगा का मैदान
- राजस्थान का मैदान
- ब्रह्मपुत्र का मैदान
पंजाब का मैदान
सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों-झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को ‘पंजाब का मैदान’ कहते हैं. उसका भौगोलिक विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में है.
भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत ‘बारी’ और ‘बिस्त’ दोआब क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है. पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि (बांगर) को ‘बैड लैंड’ (Bad land) या ‘अनुर्वर भूमि’ कहते हैं. पंजाब के पर्वतपदीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को ‘चॉस’ (Choss) या ‘चोस’ (Chos) कहते हैं. इस प्रकार के चोस (Chos) होशियारपुर ज़िले में सर्वाधिक पाये जाते हैं.
दोआब और पंजाब
‘दोआब’ दो शब्दों से मिलकर बना है – दो तथा आब अर्थात् पानी. इसी प्रकार ‘पंजाब’ भी दो शब्दों से मिलकर बना है – पंज का अर्थ है पाँच तथा आब का अर्थ है पानी. दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र के दोआब हैं-
| दोआब | नदी |
| बिस्त दोआब | व्यास – सतलुज |
| बारी दोआब | व्यास – रावी |
| रचना दोआब | रावी – चेनाब |
| चज दोआब | चेनाब – झेलम |
| सिंधु-सागर दोआब | झेलम, चेनाब एवं सिंधु |
गंगा का मैदान
इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक है. गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः तीन मैदानी प्रदेशों में सीमांकित किया गया है-
- ऊपरी गंगा का मैदान;
- मध्य गंगा का मैदान;
- निम्न गंगा का मैदान.
निर्माण
गंगा के मैदान की रचना एक ‘अग्रगर्त’ (Foredeep) में हुई है. जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त निर्मित हो गया, जो धीरे-धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया, जिससे अंततः गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ.
भौगोलिक खासियत
गंगा के मैदान में यत्र-तत्र गर्त पाये जाते हैं, जिसे पटना के निकट ‘जल्ला’ तथा मोकामा के निकट ‘टाल’ कहते हैं. पश्चिम बंगाल में जल से भरे ऐसे गर्तों को ‘बील’ (Beel) कहा जाता है. जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग ज़िले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र ‘दुआर’ (Duar) कहलाता हैं.
गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण कमी आती जाती है. मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है. मध्य गंगा के मैदान में ‘गोखुर झील’ (Oxbow Lake) अधिक पाई जाती हैं क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्प के रूप में बहती हैं.
ऊपरी गंगा का मैदान
यह गंगा के मैदान का सबसे पश्चिमी और ऊपरी भाग है. इसके उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में प्रायद्वीपीय सीमा और पश्चिम में यमुना नदी स्थित है. पश्चिम से पूर्व की तरफ इसे गंगा-यमुना दोआब, रोहिलखंड का मैदान और अवध के मैदान में विभाजित किया जा सकता हैं. इसका ढलान औसतन लगभग 25 सेमी प्रति किमी हैं.
बहुत कम ढलान के कारण नदियाँ मैदान में धीमी गति से प्रवाहित होती हैं. इससे नदी की प्रमुख विशेषताओं जैसे नदी द्वारा कटाव, नदी के मोड़, ऑक्सबो झीलें, बांध, छोड़ी गई नदी की धाराएँ, रेतीले क्षेत्र (भूर) आदि का निर्माण होता है.
मध्य गंगा का मैदान
यह ऊपरी गंगा के मैदान के पूर्व में स्थित है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है. इसके उत्तर में हिमालय की तलहटी और दक्षिणी सीमा में प्रायद्वीपीय भाग स्थित है. इस क्षेत्र में बहुत कम ढलान के कारण नदियाँ इस समतल भूमि क्षेत्र में धीमी गति से प्रवाहित होती हैं. परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में तटबंध, चट्टानें, ऑक्सबो झीलें, दलदल, ताल, खड्ड आदि नदी संबंधी विशेषताओं द्वारा चिह्नित किया गया है.
इस क्षेत्र की लगभग सभी नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं, जिससे क्षेत्र की बाढ़ की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है. कोसी नदी इसके लिए विशेष रूप से जानी जाती है, और इसे ‘बिहार का शोक’ कहा जाता है.
प्रमुख पश्चिम से पूर्व इससे सम्बद्ध क्षेत्र हैं- गंगा-घाघरा दोआब, घाघरा-गंडक दोआब और गंडक-कोसी दोआब (मिथिला मैदान).
निचला गंगा का मैदान
यह मध्य गंगा मैदान के पूर्व में स्थित है, जो बिहार के पूर्वी भाग, सम्पूर्ण बंगाल और बांग्लादेश के अधिकाँश हिस्सों में फैला हुआ है. इसके उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छोटानागपुर उच्चभूमि, और पूर्व में बांग्लादेश सीमा हैं. इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता डेल्टा निर्माण है, जो इस मैदान के लगभग 2/3 भाग का क्षेत्रफल है.
गंगा, ब्रह्मपुत्र के साथ इस मैदान के तटीय भाग पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है. यह डेल्टा, जिसे गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है, मैंग्रोव और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है.
चूँकि गंगा के मैदान सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक हैं और यहाँ विश्व की सबसे घनी आबादी पाई जाती है, इसलिए उत्तर भारत के इस मैदान का अगले भाग में विस्तार से वर्णन किया जा रहा हैं.

राजस्थान का मैदान
इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत-पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब-हरियाणा के मैदान तक तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है. राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है.
25 सेमी. समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान में ‘राजस्थान बांगर’ और ‘थार मरुस्थल’ की विभाजक रेखा है. राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को ‘रोही’ (Rohi) कहते हैं.
राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है. यहाँ कृषि हेतु जल संसाधन के लिये ‘इंदिरा गांधी नहर’ का विकास किया गया है. राजस्थान के मैदान में ‘सांभर झील’ भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय ‘खारे पानी की झील’ है तथा ‘लूनी’ इस मैदान की एक प्रमुख नदी है.
इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को ‘बॉलसन’ कहते हैं. चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को ‘प्लाया’ (Playa) कहते हैं. सांभर झील ‘बॉलसन’ (Bolson) का अच्छा उदाहरण है. डीडवाना, कुचामन, सरगोल तथा अन्य झीलें ‘प्लाया’ के उदाहरण हैं. समस्त मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीले तथा बरखान पाये जाते हैं. राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूपों से ढंका है.
राजस्थान के मैदान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:
मरुस्थली
राजस्थान के मैदान का पूर्वी भाग, जो रेगिस्तान है, को मरुस्थली के नाम से जाना जाता है. यह मारवाड़ मैदान के एक बड़े भाग को कवर करता है. हालांकि सतह पर यह एक जलोढ़ मैदान जैसा दिखता है, लेकिन भूगर्भिक रूप से यह प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है.
यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि इसमें रेत का एक विशाल विस्तार है जिसमे नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट की कुछ चट्टानें हैं. इसका पूर्वी भाग चट्टानी है, जबकि पश्चिमी भाग स्थानान्तरित रेत के टीलों से ढका हुआ है, जिन्हें स्थानीय भाषा में धरियान कहा जाता है.
राजस्थान बागर
थार मरुस्थल का पूर्वी भाग अरावली पर्वतमाला तक का अर्ध-शुष्क मैदान है जिसे राजस्थान बाग़र के नाम से जाना जाता है. अरावली से निकलने वाली कई छोटी मौसमी धाराएँ इस क्षेत्र में बहती हैं और छोटे- छोटे उपजाऊ क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, जिन्हें रोही कहा जाता है.
लूनी नदी ऐसी ही एक धारा का उदाहरण है जो अरावली के दक्षिण-पश्चिम में बहती है और कच्छ के रण में गिरती है. लूनी के उत्तरी भाग को थाली या रेतीला मैदान कहा जाता है. थार मरुस्थल में कई खारी झीलें भी हैं जैसे सांभर, डिडवाना, खाटू आदि.
भारतीय मरुस्थल (Indian Desert)
25 सेमी. वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है. भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों से ढँका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है, जिसे ‘थार का मरुस्थल’ कहा जाता है.
थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है. विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व ‘थार के मरुस्थल’ में ही पाया जाता है.
ढाल के आधार पर थार के मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है- (i) उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है (ii) दक्षिणी भाग, जिसका ढाल कच्छ के रन की ओर है.
कच्छ के रन को ‘सफेद मरुस्थल’ भी कहा जाता है. यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है जो हजारों वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है. इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है. अधिकांश नदियाँ अंतः स्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है. लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है.
इस क्षेत्र की भू-गर्भिक चट्टानी संरचना, प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है. किंतु यहाँ की धरातलीय स्थलाकृतियाँ भौतिक अपक्षय एवं पवनों द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे- रेत के टीले, बरखान, छत्रक आदि.
ब्रह्मपुत्र का मैदान
यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है. मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण-पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है. ढाल प्रवणता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन गये हैं, जैसे- माजुली द्वीप.
असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा परंतु दक्षिणी किनारे का ढाल मेघालय की तरफ मंद पाया जाता है. यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है तथा यहाँ मुख्य रूप से चावल तथा पटसन की खेती की जाती है.
ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित शंकुओं के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गोखुर झील, बील, दलदल एवं तराई क्षेत्र बन गए हैं.
उत्तर भारत के मैदानों का भौतिक विभाजन
उत्तर का विशाल मैदान (Uttar Ka Vishal Maidan) की उच्चावचीय विशेषताएँ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक अत्यंत एकरूप हैं. चट्टानें, तटबंध, खड्ड और कोहल इन विशाल मैदानों की एकरूप एकरसता को तोड़ते हैं. उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर पाँच महत्त्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है- भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा.

भाबर
उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को ‘भाबर’ कहा जाता है. यह भू-भाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है.
इसकी चौड़ाई सामान्यत: 8 से 10 किमी. है. इस भू-भाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं. यह क्षेत्र कृषि के लिये उपयुक्त नहीं होता है.
तराई
यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है. इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किमी. है. भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं.
वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है. इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है एवं कृषि के लिये विशेषकर-गन्ना, चावल एवं गेहूँ हेतु अधिक उपयुक्त है.
बांगर
यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है. उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ (बांगर) का बना है. इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है. इसमें कंकड़ भी पाये जाते हैं. शुष्क क्षेत्रों में इसमें लवणीय एवं क्षारीय उत्फुल्लन देखे जाते हैं, जिन्हें ‘रेह’ अथवा ‘कल्लर’ कहा जाता है.
बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है. इसलिये यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता. यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जलस्तर की गहराई अधिक होती है. बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है. ऐसी भूमि को ‘भूड़’ कहते हैं.
खादर
यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है. इसमें काँप मिट्टी भी पाई जाती है. इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है. खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है.
यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है. इसमें भूमिगत जलस्तर ऊँचा होता है. खादर भूमि की मृदा में ‘चीका’ की अधिकता होती है, जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है. यह क्षेत्र/मिट्टी चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है.
डेल्टा
यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है. इसका विस्तार निचली गंगा घाटी (पश्चिम बंगाल) में पाया जाता है. इसमें पुराना व नया पंक तथा दलदल सम्मिलित हैं. यहाँ उच्च भूमि को ‘चार’ (Chars) कहते हैं.
उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं. नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है. ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत-सी धाराओं में बँट जाती हैं. इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है. यह डेल्टा से अलग होती हैं.
डेल्टा और वितरिका में अंतर
डेल्टा और वितरिकाएँ, नदियों द्वारा निर्मित भू-आकृतियाँ हैं. डेल्टा एक त्रिकोणीय आकार का मैदान होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदी एक बड़े जल निकाय (जैसे समुद्र या झील) में मिलती है. वितरिकाएँ वे छोटी-छोटी धाराएँ या चैनल हैं जिनमें नदी विभाजित हो जाती है, खासकर जब वह डेल्टा क्षेत्र में प्रवेश करती है.
| डेल्टा | वितरिकाएँ |
| डेल्टा एक जलोढ़ मैदान होता है, जो नदी द्वारा लाए गए तलछट (मिट्टी, रेत, गाद) के जमाव से बनता है. | वितरिकाएँ नदी के मुहाने पर बनने वाली छोटी-छोटी धाराएँ हैं, जो मुख्य नदी से अलग होकर बहती हैं. |
| नदी जब एक बड़े जल निकाय में प्रवेश करती है, तो उसकी गति कम हो जाती है, और वह अपने साथ लाए गए तलछट को जमा करना शुरू कर देती है. | यह नदी के पानी को डेल्टा क्षेत्र में वितरित करने में मदद करती हैं. |
| यह तलछट जमाव नदी को कई धाराओं या वितरिकाओं में विभाजित होने के लिए मजबूर करता है. | वितरिकाएँ डेल्टा क्षेत्र में तलछट के जमाव और नदी के बहाव को प्रभावित करती हैं. |
| डेल्टा का आकार और आकार नदी की गति, तलछट की मात्रा और जल निकाय की विशेषताओं पर निर्भर करता है. | वितरिकाएँ समय के साथ बदल सकती हैं, क्योंकि नदी अपने मार्ग को बदलती रहती है और नए तलछट जमा करती है. |
| उदाहरण: नील नदी का डेल्टा, गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मिसिसिपी नदी का डेल्टा. |