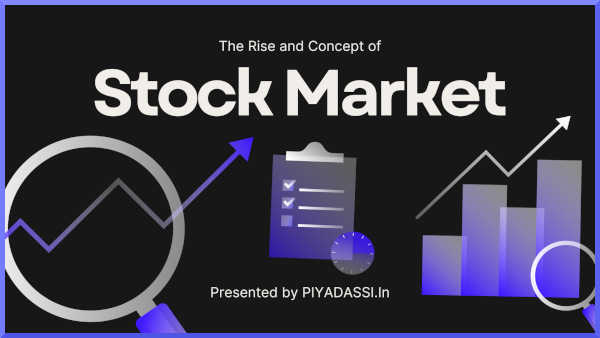हरित क्रांति का अर्थ कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से हुए उस बदलाव से है, जिसमें अल्प समय में कृषि उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई और जिसे आने वाले समय तक बनाए रखा जा सका. ‘हरित’ शब्द कृषि फसलों का संकेतक है और ‘क्रांति’ का तात्पर्य तेजी से हुए स्थायी परिवर्तन से है. इस प्रकार कृषि उत्पादन में क्रन्तिकारी वृद्धि को ‘हरित क्रांति‘ कहा जाता है.
भारतीय संदर्भ में, हरित क्रांति 1960 के दशक के मध्य में आई, जब उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, आधुनिक तकनीक और कृषि मशीनरी के प्रयोग से कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई. इसके तहत कृषि में तकनीकी ज्ञान, कृषि क्षेत्र में ऋण और शिक्षा के विस्तार ने भी अहम भूमिका निभाई. कृषि वैज्ञानिकों ने इस अभूतपूर्व कृषि उत्पादन वृद्धि को ‘हरित क्रांति’ का नाम दिया.
1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किए गए कृषि अनुसंधान का परिणाम हरित क्रान्ति के रूप में सामने आया था. डॉ. बोरलॉग को “हरित क्रांति के जनक” के रूप में भी जाना जाता है. इन्हें 1970 में उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYVs) के विकास के लिए शान्ति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया.
बोरलॉग के पदचिन्हों पर चलते हुए भारत में इसका नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन ने किया, जिससे गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई. इस क्रांति ने 1967-68 और 1977-78 के बीच भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश से अग्रणी कृषि देशों में बदल दिया.
हरित क्रांति में मुख्य रुप से दो बाते आती हैं:- पहला, उत्पादन तकनीक में सुधार और दुसरा कृषि उत्पादन में वृद्धि.
हरित क्रांति को नवीन कृषि रणनीति के नाम से भी जाना जाता है. नई कृषि युक्ति (New Agricultural Strategy) को 1966 ई0 में एक पैकेज के रुप में शुरु किया गया और इसे अधिक उपज देने वाले किस्मों का कार्यक्रम (High Yielding Variety Programme) की संज्ञा दी गई.
इस रणनीतिक योजना का वित्तपोषण भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन (Ford and Rockefeller Foundation) ने किया था.
हरित क्रांति (Green Revolution) क्या हैं?
हरित क्रांति का नाम 1968 में विलियम गॉडन ने दिया था. यह 1960 के दशक में भारत में शुरू हुई एक महत्वपूर्ण कृषि क्रांति थी. हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण दौर था जब 1960 के दशक में खेती के पारंपरिक तरीकों को बदलकर आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया. इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल, के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई. इस क्रांति का उद्देश्य भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और भुखमरी की समस्या का समाधान करना था.
हरित क्रांति के प्रमुख घटक
- उच्च उपज वाली किस्में (High Yielding Variety – HYV): नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित गेहूं और चावल की उन्नत किस्मों का उपयोग किया गया. ये बीज पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक उत्पादन देते थे और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी थे.
- रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक: मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसलों को कीटों से बचाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग किया गया.
- उन्नत सिंचाई प्रणाली: नहरों, नलकूपों और पम्प सेटों के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिससे अधिक भूमि पर खेती संभव हुई.
- कृषि मशीनीकरण: ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों और अन्य आधुनिक मशीनों के उपयोग से खेती के काम को आसान और तेज बनाया गया.
हरित क्रांति के कारण
- खाद्यान्न की कमी और अकाल: स्वतंत्रता के बाद, भारत को लगातार अकाल और खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा. अमेरिका जैसे देशों से खाद्य सहायता (जैसे PL-480) पर निर्भरता बढ़ रही थी, जिसने सरकार को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया.
- बढ़ती जनसंख्या: तेजी से बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक थी.
- वैज्ञानिक शोध और तकनीकी विकास: नॉर्मन बोरलॉग के शोध और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से उच्च उपज वाली किस्मों का विकास हुआ, जिसने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया.
हरित क्रांति के जनक
- विश्व में: नॉर्मन बोरलॉग (Norman Borlaug), एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक, को “विश्व में हरित क्रांति का जनक” माना जाता है. उन्होंने गेहूं की बौनी किस्मों को विकसित किया, जिनसे उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई. उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- भारत में: डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक, को “भारत में हरित क्रांति का जनक” कहा जाता है. उन्होंने बोरलॉग द्वारा विकसित बीजों को भारतीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल बनाया और उन्हें भारतीय किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
हरित क्रांति के उद्देश्य
- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि: हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाना था. इसका परिणाम यह हुआ कि भारत खाद्य आयात पर अपनी निर्भरता कम करने में सफल रहा.
- आत्मनिर्भरता प्राप्त करना: इस क्रांति ने भारत को खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान की, जिससे देश को भुखमरी की समस्या से लड़ने में मदद मिली.
- कृषि का व्यावसायीकरण: मशीनीकरण, उर्वरकों और उन्नत बीजों के उपयोग ने खेती को एक व्यावसायिक उद्यम में बदल दिया.
हरित क्रांति के लाभ (Benefits of Green Revolution):
- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि – हरित क्रांति से गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का और दालों का उत्पादन बढ़ा, जिससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कई गुना बढ़ा, साल 1978-79 में भारत में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ. यह उस वक्त विश्व में सर्वाधिक था.
- परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन – किसानों में आधुनिक तकनीक अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी और खेती अब केवल जीविकोपार्जन से आगे बढ़कर एक आय का साधन बन गई.
- कृषि बचतों में वृद्धि – उत्पादन वृद्धि से किसानों के पास अधिक बचतें हुईं. किसानों ने इस धन का उपयोग कृषि यंत्रों और नए तकनीक खरीदने में किया. इससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला. इसलिए हरित क्रांति को कृषि में पूंजीवाद का प्रवेश कहा जा सकता है.
- आत्मविश्वास में वृद्धि – किसानों, सरकार और जनता में यह विश्वास बढ़ा कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि खाद्यान्न निर्यात भी कर सकता है.
- खाद्यान्न आयात में कमी – हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न आयात लगभग समाप्त हो गया, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई.
- कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती – कृषि के आधुनिकीकरण से उद्योगों के साथ कृषि का संबंध और मजबूत हुआ, जैसे कि कृषि यंत्रों और उर्वरकों की मांग बढ़ी.
- रोजगार के नए अवसर – उत्पादन वृद्धि के कारण फसल कटाई और कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार बढ़ा, जिससे सेवा और परिवहन क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़े.
- ग्रामीण विकास – हरित क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निर्माण कार्यों में वृद्धि हुई, और बैंकों की गतिविधियां भी बढ़ीं.
हरित क्रांति से कृषि में आधुनिकता आई, उत्पादन बढ़ा, और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई.
हरित क्रांति की हानि (Loss from Green Revolution)
हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए. इन नुकसानों का सारांश निम्नलिखित है:
- कृषि विकास में असंतुलन: हरित क्रांति का लाभ सीमित क्षेत्रों और कुछ फसलों तक ही हुआ. इससे केवल कुछ राज्यों (जैसे पंजाब, हरियाणा) में ही कृषि में प्रगति हुई, जबकि अन्य राज्यों में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ. यह क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाने वाला कारक बना.
- सीमित फसल उत्पादन: हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल की पैदावार पर केंद्रित रही. अन्य फसलों जैसे दालों, तिलहन और कपास के लिए उच्च उपज वाले बीज सफल नहीं रहे, जिससे फसलों की विविधता में कमी आई.
- आय में असमानता: हरित क्रांति से बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ, जबकि छोटे किसानों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ. इसके परिणामस्वरूप आय में असमानता बढ़ी और कई छोटे किसानों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी.
- पूंजीवादी खेती को बढ़ावा: हरित क्रांति के लिए मशीनों, उर्वरकों, और सिंचाई में बड़े निवेश की जरूरत थी, जो केवल बड़े किसान ही कर सकते थे. इससे छोटे किसानों को नए तकनीकी लाभ से वंचित रहना पड़ा.
- रोजगार के अवसरों में कमी: मशीनों के उपयोग से श्रमिकों की आवश्यकता कम हो गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी.
- भूमि और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हुई और लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. भूजल के अत्यधिक उपयोग से जल स्तर घट गया और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा.
- भूमि सुधार कार्यक्रमों की अनदेखी: हरित क्रांति से बड़े किसानों को लाभ हुआ, लेकिन भूमि सुधार की कमी के कारण छोटे किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल सका.
- जरूरी सुविधाओं की कमी: छोटे किसानों के पास सिंचाई, आर्थिक सहायता, और सस्ती कृषि सामग्रियों की कमी थी, जिससे वे हरित क्रांति का पूरा लाभ नहीं उठा सके.
- उत्पादन लागत में वृद्धि: आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से उत्पादन लागत बढ़ी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया.
इन कारणों से हरित क्रांति ने जहां कुछ क्षेत्रों में लाभ पहुंचाया, वहीं कई समस्याएं भी उत्पन्न कीं, जो आज भी भारतीय कृषि के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं.
व्यापक हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें
- भूमि सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा: हरित क्रांति की व्यापकता के लिए प्रभावी भूमि सुधार आवश्यक है. सीमा निर्धारण से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटा जाना चाहिए और चकबंदी को प्रभावी बनाकर खेतों के बंटवारे पर रोक लगानी होगी, जिससे नई तकनीकों का सही ढंग से प्रयोग किया जा सके.
- कृषि वित्त का विस्तार: छोटे किसान भी हरित क्रांति का लाभ उठा सकें, इसके लिए वित्तीय संस्थाओं को उन्हें आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराना चाहिए. कृषि की नई तकनीकें अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए.
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार: विशेषकर सूखे और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है. लघु सिंचाई परियोजनाओं, वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करके पानी, बिजली और श्रम की बचत की जा सकती है.
- हरित क्रांति का अन्य फसलों पर विस्तार: गेहूं और चावल के साथ-साथ दालें, कपास, तिलहन, गन्ना आदि फसलों के उन्नत बीजों का विकास होना चाहिए. इससे कृषि उत्पादन में संतुलन आएगा और कृषि में समग्र सुधार संभव होगा.
- सीमांत और छोटे किसानों को लाभ देना: हरित क्रांति का लाभ बड़े किसानों तक सीमित रहा है, इसलिए छोटे किसानों को सहकारी खेती अपनाने, भूमि सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने और बैंक द्वारा सरलता से कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है.
- मूल्य नीति को प्रोत्साहनकारी बनाना: सरकार की मूल्य नीति का विस्तार अन्य फसलों तक भी होना चाहिए ताकि सभी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और असंतुलन दूर हो सके.
- उन्नत किस्म के बीजों का विकास: गेहूं और चावल के अलावा अन्य फसलों जैसे दाल, तिलहन, कपास और पटसन के उन्नत बीज विकसित किए जाने चाहिए, जिससे विविधता में वृद्धि हो और छोटे किसानों को अधिक विकल्प मिलें.
- शुष्क खेती को प्रोत्साहन: सिंचाई सुविधाओं से वंचित सूखे क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाने की जरूरत है जो कम समय में पक सकें और सूखे से प्रभावित न हों.
- फसल बीमा योजना: छोटे और सीमांत किसानों को जोखिम से सुरक्षा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाया जाना चाहिए. इससे प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
सदाबहार हरित क्रांति (Evergreen Green Revolution)
1990 के दशक के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति (Second Green Revolution) की अवधारणा का विकास हुआ. इसे ‘सदाबहार क्रांति’ (Evergreen Revolution) भी कहा गया. प्रथम हरित क्रांति से भिन्न द्वितीय हरित क्रांति में सभी फसलों एवं कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा. द्वितीय हरित क्रांति फसल विविधता, उपयुक्त फसल प्रतिरूप, फसल प्रबंधन, पौधों एवं मृदा संरक्षण आदि विषयों को भी समाहित करती है.
द्वितीय हरित क्रांति में धारणीय कृषि पद्धति के साथ जैविकीय उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों के प्रयोग पर बल दिया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत कृषि के सतत् विकास हेतु आधारभूत संरचना तथा संस्थागत ढाँचे को मजबूत करना, जैसे- शीत भंडारों की व्यवस्था, सड़क योजनाएँ, कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा, दूरसंचार का विकास, मूल्य परिवर्तन हेतु कृषि प्रसंस्करण पर बल देना आदि को शामिल किया जा रहा है. इसके अंतर्गत नवीन सरकारी समितियों का गठन कर छोटे व सीमांत कृषकों को भी उन्नत बीज, उर्वरक, अत्याधुनिक मशीनें आदि के क्रय हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
सदाबहार हरित क्रांति का विचार डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं. हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में मदद की, लेकिन इसके साथ ही कई पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियाँ भी आईं. गहन कृषि और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण भूमि की उर्वरता घटने लगी, जलस्तर कम हुआ, और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. इन प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान के रूप में सदाबहार हरित क्रांति का प्रस्ताव रखा गया.
सदाबहार हरित क्रांति का उद्देश्य
सदाबहार हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी कृषि प्रणाली विकसित करना है, जो न केवल उत्पादकता बढ़ाए बल्कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, और समाज के लिए भी टिकाऊ हो. इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
- पर्यावरण के अनुकूल कृषि: सदाबहार हरित क्रांति का मुख्य सिद्धांत यह है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि इस तरह से होनी चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुँचाए. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खेती, प्राकृतिक उर्वरक, और कीट प्रबंधन तकनीकों का उपयोग बढ़ावा दिया जाता है. इस प्रकार की तकनीकों से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, जल प्रदूषण कम होता है और पारिस्थितिकी संतुलित रहती है.
- स्थायी प्रौद्योगिकी: सदाबहार हरित क्रांति में कृषि की ऐसी प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार किया जाता है, जो टिकाऊ हों और कम संसाधनों में अधिक उत्पादन दे सकें. उदाहरण के लिए, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जीरो टिलेज (बिना जुताई की खेती), और जल-संवर्धन तकनीकें इसके कुछ पहलू हैं, जिनसे जल संसाधनों की बचत की जा सकती है और भूमि का क्षरण कम होता है.
- जैव विविधता का संरक्षण: परंपरागत हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसी कुछ चुनिंदा फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था. इसके विपरीत, सदाबहार हरित क्रांति विभिन्न प्रकार की फसलों को अपनाने का पक्षधर है. यह न केवल खाद्यान्न में विविधता लाता है बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षित करता है. विविध फसलों की खेती से कीटों और बीमारियों का खतरा कम होता है और यह पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है.
- कृषि में नवाचार का प्रसार: सदाबहार हरित क्रांति में पारंपरिक कृषि ज्ञान और नवीन कृषि तकनीकों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है. इससे किसान नई तकनीकों को आसानी से अपना सकते हैं और उनके लिए कृषि अधिक लाभकारी हो जाती है.
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी: सदाबहार हरित क्रांति का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है. इस क्रांति में ऐसी तकनीकों का विकास किया जाता है जो छोटे किसानों के लिए सस्ती और सुलभ हों, ताकि वे भी कृषि में स्थिरता ला सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो.
- सामाजिक और आर्थिक टिकाऊपन: इस क्रांति में उत्पादकता वृद्धि का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि यह समाज में सभी वर्गों के लिए लाभकारी और संतुलित होना चाहिए. सदाबहार हरित क्रांति में आय के समान वितरण पर जोर दिया जाता है ताकि सभी किसान, विशेष रूप से छोटे और गरीब किसान, इसका लाभ उठा सकें. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय की असमानता कम होती है और सामाजिक संतुलन बना रहता है.
सदाबहार हरित क्रांति के लाभ
- पर्यावरण संरक्षण: इस क्रांति के अंतर्गत जैविक और प्राकृतिक तकनीकों का उपयोग बढ़ता है, जिससे पर्यावरणीय क्षरण कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बना रहता है.
- पोषण सुरक्षा: जैव विविधता को बढ़ावा देने के कारण विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जिससे लोगों को पोषण में भी सुधार होता है.
- आर्थिक स्थिरता: छोटे और सीमांत किसान भी नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है और आर्थिक असमानता कम होती है.
- पारिस्थितिकी संतुलन: सदाबहार हरित क्रांति के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर कृषि पद्धतियाँ विकसित की जाती हैं, जिससे भूमि, जल और जैव विविधता का संरक्षण होता है.
कृषि व कृषि से सम्बद्ध अन्य तथ्य
NPK अनुपात (Nitrogen-Phosphorus-Potassium Ratio)
रासायनिक खेती में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम के एक निश्चित मिश्रण का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है जोकि एनपीके (NPK) के नाम से प्रचलित है. NPK का अनुपात अलग-अलग फसलों के लिये अलग-अलग होता है. हरित क्रांति के समय NPK का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया. भारत में दलहनी फसलों में यह अनुपात 1:2:1 या 1:2:2 है.
नाइट्रोजन
नाइट्रोजन फसलों की वृद्धि हेतु आवश्यक तत्त्व है. यह फसलों में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है. यूरिया नाइट्रोजन का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता है, जो पौधों के विकास के लिये आवश्यक है.
जब साधारण यूरिया का प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा भी पौधों द्वारा ग्रहण नहीं की जाती और वह निक्षालन द्वारा मृदा में मिल जाती है. जिससे नाइट्रोजन की क्षति तो होती ही है, साथ ही मृदा की उर्वरता भी प्रभावित होती है तथा भूमिगत जल भी अशुद्ध हो जाता है. इसके लिये ‘स्लो रिलीज नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर’ तैयार किये गए हैं. इनमें सल्फर कोटेड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया प्रमुख हैं.
नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग से नाइट्रीकरण मंद गति से होने लगता है तथा नाइट्रोजन का निक्षालन व वाष्पीकरण द्वारा हास कम हो जाता है. नाइट्रोजन अधिक समय तक मृदा में रहती है, जिससे पौधे नाइट्रोजन को लंबे समय तक ग्रहण कर सकते हैं. इससे यूरिया की कम मात्रा में अधिक फसल उत्पादन होगा तथा लागत भी कम आयेगी.
फॉस्फोरस
फॉस्फोरस पौधों में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं हेतु आवश्यक है. कम अवधि वाली फसलों में घुलनशील फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है.
पोटेशियम
पोटेशियम फसलों में पोषक तत्त्वों व पानी के स्थानांतरण में सहायक होता है तथा फसलों में रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
यह योजना 13 जनवरी, 2016 को शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम के बोझ को कम करना और खराब मौसम से फसलों की सुरक्षा के साथ-साथ किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.
प्रमुख बिंदु:
- कम प्रीमियम दरें:
- खरीफ फसलों के लिए 2.0%
- रबी फसलों के लिए 1.5%
- वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5%
- सरकारी सब्सिडी: सरकारी सब्सिडी पर ऊपरी सीमा की बाध्यता हटा ली गई है. यदि शेष प्रीमियम 90% हो, तो भी यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है (उत्तर-पूर्वी राज्यों में केंद्र का हिस्सा 90% और राज्य का 10% है).
- नोडल एजेंसी: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है.
- पुरानी योजनाओं का प्रतिस्थापन: यह योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसे सेवा कर से छूट दी गई है.
- व्यापक कवरेज: यह योजना ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, भूस्खलन, बाढ़, और पोस्ट हार्वेस्टिंग फसलों के नुकसान सहित कई प्रकार की आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है.
- तकनीक का उपयोग: फसल कटाई और नुकसान का आकलन शीघ्र और सही तरीके से करने के लिए रिमोट सेंसिंग, स्मार्टफोन और जीपीएस जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है. फसल कटाई प्रयोग के आँकड़े तत्काल स्मार्टफोन के माध्यम से अपलोड कराए जाते हैं.
- संचालन: इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआई सी) सहित विभिन्न सूचीबद्ध बीमा कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता है.
समसामयिक एवं अन्य तथ्य:
- दावों का भुगतान: 2016 में योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 78.41 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया है और ₹1.83 लाख करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है.
- नामांकन में वृद्धि: पंजीकृत किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो 2022-23 में 3.17 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 4.19 करोड़ हो गई है, यह 32% की वृद्धि है.
- गैर-ऋणी किसानों की भागीदारी: गैर-ऋणधारक किसानों के आवेदनों की संख्या 2014-15 में 20 लाख से बढ़कर 2024-25 में 522 लाख हो गई है, जो इस योजना की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है.
- डिजिटल नवाचार: दावों के त्वरित और पारदर्शी निपटान के लिए डिजीक्लेम (DigiClaim) मॉड्यूल शुरू किया गया है. यह मॉड्यूल राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को पीएफएमएस (PFMS) और बीमा कंपनियों की प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है.
- दावा निपटान में विलंब पर जुर्माना: दावों के भुगतान में देरी को रोकने के लिए, 2024 के खरीफ सीजन से बीमा कंपनियों पर 12% का स्वतः जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
- योजना का विस्तार: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है.
- स्वैच्छिक भागीदारी: अब यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है, और कुल लाभार्थियों में से 55% गैर-ऋणी किसान हैं.
- दावों के निपटान में चुनौतियाँ: कुछ राज्यों द्वारा अपने हिस्से के प्रीमियम का समय पर भुगतान न करने के कारण दावों के निपटान में देरी की चिंताएं बनी हुई हैं. हालांकि, सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
मेरा गाँव, मेरा गौरव (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि को वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ना है. इसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कृषि वैज्ञानिक गाँवों को गोद लेते हैं और किसानों को कृषि से संबंधित वैज्ञानिक सलाह और सहायता प्रदान करते हैं. यह पहल किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
महत्वपूर्ण तथ्य:
- मुख्य लक्ष्य: इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य खेती को वैज्ञानिक ज्ञान-विज्ञान से लैस करना है. इसमें कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जाता है, जिससे किसान अपनी समस्याओं का समाधान सीधे वैज्ञानिकों से प्राप्त कर सकें.
- वैज्ञानिकों की भूमिका: ICAR के वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ प्रत्येक वर्ष एक गांव का चयन करते हैं और वहां की विशिष्ट कृषि समस्याओं का अध्ययन करते हैं. वे किसानों को नई किस्मों, बेहतर उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई तकनीकों और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हैं.
- मौसम संबंधी पूर्वानुमान: इस योजना के तहत मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्रणालियों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है. इससे किसान अपनी फसलों को मौसम की अनिश्चितताओं से बचा सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक बारिश, सूखा या ओलावृष्टि.
- क्षमता निर्माण: योजना में वैज्ञानिकों और किसानों दोनों के क्षमता निर्माण पर बल दिया गया है. वैज्ञानिकों को किसानों की जमीनी समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है, जबकि किसानों को नई तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाता है.
- किसानों की आय दोगुनी करना: यह पहल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के अनुरूप थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था. यद्यपि 2022 का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन इस तरह की पहलें कृषि उत्पादकता और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण रही हैं.
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: इस कार्यक्रम के तहत मोबाइल ऐप्स, कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs), और किसान कॉल सेंटरों जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि वैज्ञानिक सलाह आसानी से किसानों तक पहुंचाई जा सके.
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY): यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करना है.
- अन्य संबंधित पहलें: इस पहल के साथ ही, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाएं भी किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक रही हैं.
भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम
- हरित क्रांति- खाद्यान्न उत्पादन
- श्वेत क्रांति- दुग्ध उत्पादन
- नीली क्रांति-मत्स्य उत्पादन
- भूरी क्रांति- कोको उत्पादन
- रजत क्रांति- अंडा/कुक्कुट उत्पादन
- पीली क्रांति- तिलहन उत्पादन
- लाल क्रांति- टमाटर/मांस उत्पादन
- गुलाबी क्रांति- झींगा मछली उत्पादन/प्याज उत्पादन/औषध उत्पादन
- बादामी क्रांति- मसाला उत्पादन
- सुनहरी क्रांति- फल उत्पादन/शहद उत्पादन
- गोल क्रांति- आलू उत्पादन
- सदाबहार क्रांति- जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को
- फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित
- रजत रेशा क्रांति- कपास उत्पादन
- सुनहरा रेशा क्रांति- जूट उत्पादन
- सेफ्रॉन क्रांति- केसर उत्पादन
- ग्रे/स्लेटी- उर्वरक उत्पादन
- हरित सोना क्रांति-बाँस उत्पादन
- मूक क्रांति- मोटे अनाज के उत्पादन
- परामनी क्रांति- भिंडी उत्पादन
- इंद्रधनुषीय क्रांति- सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से
कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थाएँ
नीचे भारत में कृषि सम्बद्ध विभिन्न संस्थान और उनके मुख्यालय का स्थान वर्णित है.
- भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान – कानपुर
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) – मुंबई
- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड – हैदराबाद (तेलंगाना)
- राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान – कटक
- राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान – करनाल (हरियाणा)
- भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान – लखनऊ
- विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय – फरीदाबाद
- चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान – जयपुर
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान – नई दिल्ली
- राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड – दिल्ली
- केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान – राजमुंद्री (आंध्र प्रदेश)
- केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान – शिमला
- केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान – लखनऊ
- केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान – कासरगोड (केरल)
- केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान – कोलकाता
- भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान – वाराणसी
- केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान – मैसूर
- केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान – बीकानेर
निष्कर्ष
सदाबहार व हरित क्रांति एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो कृषि को न केवल उत्पादकता की दृष्टि से बल्कि पर्यावरण और समाज के प्रति भी जिम्मेदार बनाता है. सदाबाहार क्रांति तो हरित क्रांति के प्रतिकूल प्रभावों को सुधारने का भी प्रयास करता है, जिसमें पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता को प्राथमिकता दी जाती है. सदाबहार हरित क्रांति से हम एक ऐसी कृषि व्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी टिकाऊ और लाभकारी हो.