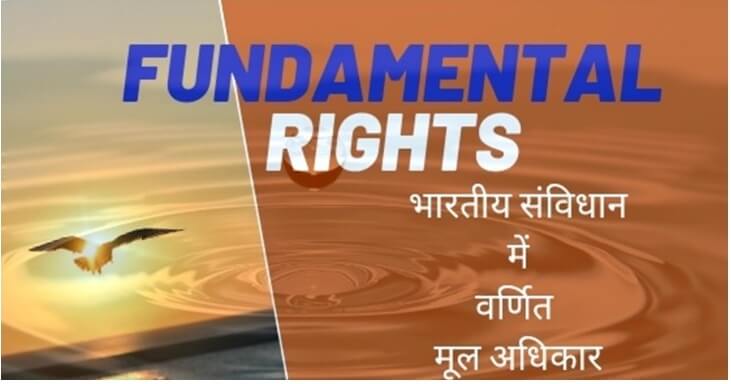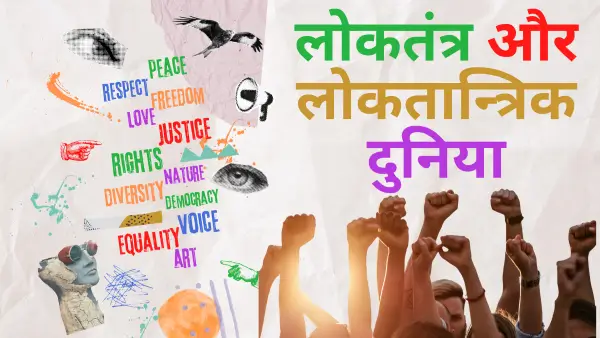वित्त आयोग भारत के संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है. इसका स्वरुप अर्धन्यायिक व सलाहकारी है. इसका प्राथमिक उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण, राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांतों और अन्य वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना है. इस प्रकार यह संस्था भारत के राजकोषीय संघवाद की आधारशिला है.
भारतीय संविधान के भाग-12 में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है. इसके बारे में अनुच्छेद 280 व 281 में वर्णन है. अनुच्छेद 280(1)में राष्ट्रपति को संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, या आवश्यकतानुसार उससे पहले, एक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया है.
| अनुच्छेद 280, भारतीय संविधान 1950 |
| (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, आदेश द्वारा एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा. ( 2) संसद विधि द्वारा उन अर्हताओं का अवधारण कर सकेगी जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी तथा वह रीति जिससे उनका चयन किया जाएगा. ( 3) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करे- (क) संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जो इस अध्याय के अधीन उनके बीच विभाजित की जानी है या की जा सकेगी, तथा ऐसी आय के अपने-अपने हिस्से का राज्यों के बीच आबंटन; (ख) वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के लिए सहायता अनुदान को नियंत्रित करेंगे; (ग) भारत सरकार द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग ख में अनुच्छेद 278 के खंड (1) या अनुच्छेद 306 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के साथ किए गए किसी करार की शर्तों का जारी रहना या उनमें परिवर्तन; और (घ) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला. (4) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा और अपने कार्यों के निष्पादन में ऐसी शक्तियां रखेगा जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे. |
| अनुच्छेद 281, भारत का संविधान 1950 |
| राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा. |
वित्त आयोग की संरचना (Structure of Finance Commission)
वित्त आयोग के 4 सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है. राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऐसे वित्तीय या अन्य हित न हों जो आयोग के सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकें.
योग्यताएँ
वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 के अनुसार, अध्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामलों में अनुभव आवश्यक है. अन्य चार सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं:
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं/रहे हैं, या नियुक्त होने के योग्य हैं.
- भारत सरकार के वित्त और लेखा मामलों का विशेष ज्ञान रखते हों.
- प्रशासन और वित्तीय मामलों में व्यापक अनुभव रखते हों.
- अर्थशास्त्र के विशेष ज्ञाता हों.
पद अवसान (अयोग्यता और हटाने की प्रक्रिया)
वित्त आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया संविधान में सीधे तौर पर वित्त आयोग के लिए विस्तृत नहीं है, लेकिन अयोग्यता के मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं. इसके सदस्यों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अयोग्य ठहराया जा सकता है या वे पद से मुक्त हो सकते हैं. एक सदस्य को निम्नलिखित कारणों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है:
- यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो.
- यदि वह दिवालिया हो.
- यदि उसे किसी अनैतिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो.
- यदि उसके ऐसे वित्तीय या अन्य हित हों जो आयोग के सुचारू कामकाज में बाधा डाल सकते हैं.
- सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं.
कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति
प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद पर रहता है. सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं. आयोग की सिफारिशें आमतौर पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए लागू होती हैं.
वित्त आयोग के कार्य व शक्तियां
वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित सिफारिशें करना है. यह भारत के राजकोषीय संघवाद को मजबूत करता है.
केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण
आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें देना है. यह ‘विभाज्य पूल’ (divisible pool) से राज्यों को मिलने वाले हिस्से (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) और विभिन्न राज्यों के बीच इस हिस्से के आवंटन (क्षैतिज हस्तांतरण) दोनों पर निर्णय लेता है.
क्षैतिज हस्तांतरण आमतौर पर आयोग द्वारा निर्धारित एक सूत्र के आधार पर तय किया जाता है, जिसमें राज्य की जनसंख्या, प्रजनन स्तर, आय स्तर, भूगोल, वन क्षेत्र, और कर प्रयास जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है. यह सूत्र राज्यों के बीच आय असमानताओं को कम करने और सार्वजनिक सेवाओं के समानीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है.
सहायता अनुदान के सिद्धांत (Grants-in-Aid)
आयोग भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 275) से राज्यों के राजस्व को सहायता अनुदान के लिए सिद्धांतों की सिफारिश करता है. ये अनुदान उन राज्यों को दिए जाते हैं जिन्हें अपने वित्तीय अंतर को पाटने और न्यूनतम सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है. आयोग विशिष्ट क्षेत्रों या सुधारों के लिए लक्षित अनुदान भी प्रदान कर सकता है.
राज्य की संचित निधि में वृद्धि के उपाय
संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद इसे राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करने का भी कार्य सौंपा गया है. ऐसा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए किया जाता है.
अन्य मामले
वित्त आयोग को राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के हित में भेजे गए किसी भी अन्य मामले पर भी सिफारिशें देनी होती हैं. इसमें रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अलग फंडिंग तंत्र की जांच जैसे विषय शामिल हो सकते हैं.
आयोग की शक्तियां और प्रक्रिया
वित्त आयोग को अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है. अपने कार्यों के निष्पादन में, आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं. इसमें गवाहों को बुलाना, किसी भी दस्तावेज को प्राप्त करना और किसी भी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना शामिल है. आयोग कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकता है जो विचाराधीन मामले के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो.
सलाहकारी भूमिका
वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं. यह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं. लेकिन यह एक उच्च-स्तरीय संवैधानिक निकाय है. इसलिए, इसके सिफारिशों का अत्यधिक महत्व होता है. केंद्र तथा राज्यों के बीच एक स्वस्थ और सहकारी वित्तीय संबंध बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उन्हें आम तौर पर स्वीकार किया जाता है. राष्ट्रपति आयोग की प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं.
15वां वित्त आयोग
15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद किया गया था. इसके अध्यक्ष एन. के. सिंह थे. आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 फरवरी, 2020 को संसद में प्रस्तुत की, जबकि अंतिम रिपोर्ट 2021-26 की अवधि के लिए 30 अक्टूबर, 2020 को प्रस्तुत की गई.
कर हस्तांतरण की कसौटियाँ और हिस्सेदारी
15वें वित्त आयोग ने केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 2015-20 की अवधि के 42% से घटाकर 2020-21 के लिए 41% करने की सिफारिश की. यह 1% की कमी जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय संसाधनों से प्रावधान करने के लिए की गई थी.
कर हस्तांतरण के लिए आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंड और उनके भार नीचे वर्णित है. इन मानदंडों का उद्देश्य राज्यों के बीच क्षैतिज असमानताओं को कम करने और वित्तीय संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना था:
- आय असमानता(भार 45%): यह मानदंड राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में अंतर को मापता है. कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक हिस्सा मिलता है.
- जनसंख्या (2011): 15% भार.
- क्षेत्र: 15% भार.
- वन और पारिस्थितिकी (भार 10%): यह मानदंड राज्यों में घने वन क्षेत्र के हिस्से पर आधारित है.
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (भार 12.5%): यह मानदंड जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के लिए राज्यों को पुरस्कृत करता है.
- कर प्रयास (भार 2.5%): यह मानदंड उच्च कर संग्रह दक्षता वाले राज्यों को पुरस्कृत करता है.
अनुदान और सिफारिशें
15वें वित्त आयोग ने विभिन्न प्रकार के अनुदानों की सिफारिश की:
- राजस्व घाटा अनुदान: 2020-21 में, 14 राज्यों के लिए ₹74,340 करोड़ के कुल राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया था, जिसके लिए आयोग ने अनुदान की सिफारिश की.
- स्थानीय निकायों को अनुदान: 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को कुल ₹90,000 करोड़ के अनुदान निर्धारित किए गए. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹60,750 करोड़ (67.5%) और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹29,250 करोड़ (32.5%) निर्धारित किया गया. इन अनुदानों का वितरण जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर 90:10 के अनुपात में किया गया.
- क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान: 2020-21 में पोषण के लिए ₹7,375 करोड़ का अनुदान अनुशंसित किया गया. अंतिम रिपोर्ट में स्वास्थ्य, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, न्यायपालिका, ग्रामीण कनेक्टिविटी, रेलवे, पुलिस प्रशिक्षण और आवास जैसे क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रस्तावित किए गए.
- आपदा जोखिम प्रबंधन: आयोग ने स्थानीय स्तर पर शमन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन कोष (NDMF और SDMF) स्थापित करने की सिफारिश की.
राजकोषीय सुदृढीकरण पर सुझाव
आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को अपने संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियमों के अनुसार राजकोषीय घाटे और ऋण स्तरों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी. आयोग ने कर आधार को व्यापक बनाने, कर दरों को सुव्यवस्थित करने और सरकार के सभी स्तरों पर कर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता बढ़ाने की भी सिफारिश की. इसने जीएसटी कार्यान्वयन में चुनौतियो को भी उजागर किया. इन चुनौती में संग्रह में बड़ी कमी और उच्च अस्थिरता शामिल है. आयोग ने राज्यों द्वारा केंद्रीय मुआवजे पर निरंतर निर्भरता पर चिंता व्यक्त की .
आलोचनाएँ और चुनौतियाँ
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर कुछ आलोचनाएँ भी सामने आईं. दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या मानदंड के लिए 2011 की जनगणना के उपयोग पर चिंता व्यक्त की. इससे जनसंख्या नियंत्रण में उनके बेहतर प्रदर्शन के कारण उन्हें कम हिस्सेदारी मिली. इसके अलावा, उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) के बढ़ते उपयोग के कारण विभाज्य पूल के सिकुड़ने की समस्या भी उठाई गई (ये राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं).यह राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को सीमित करता है और उनका केंद्र पर निर्भरता बढ़ाता है.
16वां वित्त आयोग
16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में किया गया है, जिसके अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं. इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए होगी. 16वें वित्त आयोग की संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:
- केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करना.
- भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को स्थापित करना, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत.
- राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को पूरक करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों की पहचान करना.
- आपदा प्रबंधन वित्तपोषण का मूल्यांकन करना.
- रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अलग फंडिंग तंत्र की आवश्यकता और संचालन की जांच करना.
चुनौतियाँ
16वें वित्त आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. जीएसटी के दौर में, कई कर मिलकर एक कर (जीएसटी) बन गया है. इससे राज्यों के अपने टैक्स कम हो गए हैं. ऐसे में राज्यों को केंद्र से मिलने वाला मदद बहुत जरूरी हो गया है. “फ्रीबी” संस्कृति और पुरानी पेंशन प्रणाली पर राज्यों के लौटने जैसे मामलों पर भी आयोग को ध्यान देना होगा. पिछले आयोगों द्वारा लगाए गए शर्तों के साथ अनुदानों की प्रभावशीलता की समीक्षा करना भी इसकी एक चुनौती होगी. कई राज्य वर्षों बाद भी क्षेत्रीय असमानता और विभिन्न आयामों पर पिछड़े हुए है. यह राष्ट्रिय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है. इसे पाटने के लिए प्रयास करना भी नए वित्त आयोग की एक चुनौती है.
वित्त आयोग का आवश्यकता व महत्व
वित्त आयोग भारत की संघीय राजकोषीय प्रणाली का एक अनिवार्य स्तंभ है, जिसकी आवश्यकता और महत्व कई आयामों से स्पष्ट होता है.
राजकोषीय संघवाद का आधार
भारत एक संघीय देश है जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन है. हालांकि, कराधान शक्तियाँ मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास केंद्रित हैं. लेकिन व्यय की बड़ी जिम्मेदारियाँ राज्यों पर हैं. यह एक राजकोषीय अंतर पैदा करता है. वित्त आयोग इस अंतर को पाटने के लिए एक संवैधानिक तंत्र प्रदान करता है. इस प्रकार संसाधनों का न्यायसंगत और विवेकपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित होता है. यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है. इससे राजकोषीय असंतुलन को कम करने और पूरे देश में संतुलित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलती है.
राज्यों के बीच असमानताओं को कम करना
वित्त आयोग सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से वंचित राज्यों को भी पर्याप्त सहायता मिले ताकि वे न्यूनतम सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर सकें और अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकें. यह निम्न-आय वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति राजस्व में वृद्धि करके राजस्व असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है1.
वित्तीय अनुशासन और स्थिरता
वित्त आयोग राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियमों का पालन करने के सिद्धांतों पर सलाह देता है. आयोग की सिफारिशें सरकारों को स्थायी सार्वजनिक वित्त बनाए रखने और अत्यधिक ऋण संचय को रोकने के लिए प्रोत्साहित करती हैं.
केंद्र-राज्य संबंधों को सुदृढ़ करना
वित्त आयोग के कार्यप्रणाली में सभी स्तरों की सरकारों के साथ व्यापक परामर्श शामिल होता है. यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करता है. यह वित्तीय विवादों को सुलझाने और राष्ट्रीय तथा राज्य नीति उद्देश्यों को संरेखित करने में मदद करता है, जिससे समावेशी शासन को बढ़ावा मिलता है.
स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण
संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद, वित्त आयोग की भूमिका में स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना भी शामिल हो गया है. यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लिए वित्तीय संसाधन जमीनी स्तर पर उपलब्ध हों. इस प्रकार यह विकेन्द्रीकृत शासन को सुगम बनाता है.
अब तक गठित वित्त आयोग
भारत में संविधान लागू होने के बाद से अब तक 16 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है. पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा श्री के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल, 1952 को गठित किया गया था. नीचे अब तक गठित वित्त आयोगों की सूची, उनके अध्यक्ष और परिचालन अवधि के साथ दी गई है:
| वित्त आयोग | स्थापना वर्ष | अध्यक्ष | परिचालन अवधि |
| (1) प्रथम | 1951 | के. सी. नियोगी | 1952–57 |
| (2) द्वितीय | 1956 | के. संथानम | 1957–62 |
| (3) तृतीय | 1960 | अशोक कुमार चंदा | 1962–66 |
| (4) चतुर्थ | 1964 | पी. वी. राजमन्नार | 1966–69 |
| (5) पंचम | 1968 | महावीर त्यागी | 1969–74 |
| (6) षष्ठम | 1972 | के. ब्रह्मानंद रेड्डी | 1974–79 |
| (7) सप्तम | 1977 | जे. एम. शेलट | 1979–84 |
| (8) अष्टम | 1983 | वाई. बी. चव्हाण | 1984–89 |
| (9) नवम | 1987 | एन. के. पी. साल्वे | 1989–95 |
| (10) दशम | 1992 | के. सी. पंत | 1995–2000 |
| (11) एकादश | 1998 | ए. एम. खुसरो | 2000–2005 |
| (12) द्वादश | 2002 | सी. रंगराजन | 2005–2010 |
| (13) त्रयोदश | 2007 | डॉ. विजय एल. केलकर | 2010–2015 |
| (14) चतुर्दश | 2013 | डॉ. वाई. वी. रेड्डी | 2015–2020 |
| (15) पंचदश | 2017 | एन. के. सिंह | 2020-21; 2021-26 |
| (16) षोडश | 2023 | अरविंद पनगढ़िया | 2026-31 |